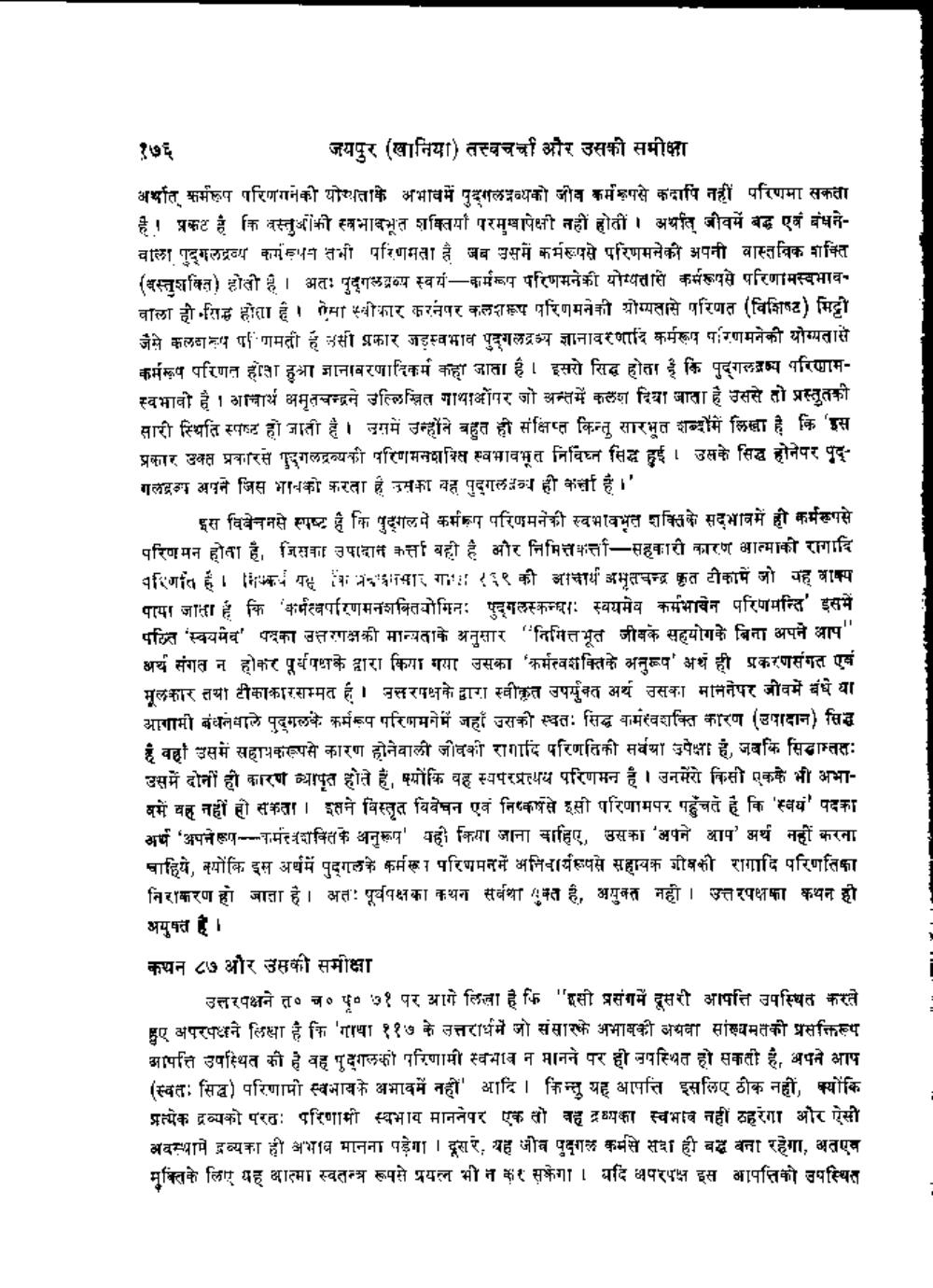________________
१७६
जयपुर (खानिया) तस्वचर्चा और उसकी समीक्षा
अर्थात् कर्मरूप परिणगने की योग्यता के अभाव में पुद्गलद्रव्यको जीव कर्मरूपसे कदापि नहीं परिणमा सकता है! प्रकट है कि वस्तुओं की स्वभावभूत शक्तियाँ परमुखापेक्षी नहीं होतीं । अर्थात् जीवमें बद्ध एवं बंधनेवाला पुद्गलद्रव्य कर्मरूप तभी परिणमता है जब उसमें कर्मरूपसे परिणमने को अपनी वास्तविक शक्ति (स्तुति) होती है। अतः पुद्गलद्रव्य स्वयं-कर्मरूप परिणमनेकी योग्यतासे कर्मरूपसे परिणामस्वभाववाला ही सिद्ध होता है। ऐसा स्वीकार करनेपर कलशरूप परिणमनेकी योग्यतासे परिणत (विशिष्ट) मिट्टी जैसे कल गमती है उसी प्रकार जस्वभाव पुद्गलद्रभ्य ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमनेकी योग्यता से कर्मरूप परिणत होता हुआ जानावरणादिकर्म कहा जाता है। इसरो सिद्ध होता है कि पुद्गलय परिणामस्वभावी है । आचार्य अमृतचन्द्रने उल्लिखित गाथाओं पर जो अन्तमें कला दिया जाता है उससे तो प्रस्तुतकी सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है । उसमें उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त किन्तु सारभूत शब्दों में लिखा है कि 'इस प्रकार उक्त प्रकारसे गुद्गलद्रव्यको परिणमनशक्ति स्वभावभूत निर्विघ्त सिद्ध हुई। उसके सिद्ध होनेपर पुद् गला अपने जिस भावको करता है उसका वह पुद्गल ही कर्त्ता है । '
11
इस विवेचनसे स्पष्ट है कि पुद्गल में कर्मरूप परिणमनेकी स्वभावभूत शक्ति के सद्भाव में हो कर्मरूपसे परिणमन होता है, जिसका उपादान कर्ता वही है और निमित्तकर्ता सहकारी कारण आत्माकी रागादि है। १६९ को आचार्य अमृतचन्द्र कृत टीकामें जो वह भाषप पाया जाता है कि 'कर्मत्वपरिणमनशक्ति योगिनः पुद्गलस्कन्धरः स्वयमेव कर्मभावेन परिणमन्ति' इसमें पठित 'स्वयमेव' पत्रका उत्तरपक्षकी मान्यता के अनुसार "दिमित्तभूत जीवके सहयोग के बिना अपने आप अर्थ संगत न होकर पूर्वपथके द्वारा किया गया उसका 'कर्मवशक्ति के अनुरूप अर्थ ही प्रकरणसंगत एवं मूलकार तथा टीकाकारसम्मत है । उत्तरपक्ष के द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त अर्थ उसका माननेपर जीवमें बंधे या आगामी बंधनेवाले पुद्गल के कर्मरूप परिणाम में जहाँ उसकी स्वतः सिद्ध कर्मस्वशक्ति कारण ( उपादान) सिद्ध है वह उसमें सहायकरूपसे कारण होनेवाली जीवकी रागादि परिणतिकी सर्वथा उपेक्षा है, जबकि सिद्धान्ततः उसमें दोनों ही कारण व्याप्त होते हैं, क्योंकि वह स्वपरप्रत्यय परिणमन है । उनमें किसी एकके भी अभा
में वह नहीं हो सकता। इसने विस्तृत विवेचन एवं निष्कर्षसे इसी परिणामपर पहुँचते है कि 'स्वयं' पदका अर्थ 'अपने रूप-स्त्रक्ति के अनुरूप यही किया जाना चाहिए, उसका 'अपने आप' अर्थ नहीं करना चाहिये, क्योंकि इस अर्थ में पुद्गल के कर्मरूप परिणमनमें अनिवार्यरूपसे सहायक जीवको रागादि परिणतिका निराकरण हो जाता है। अतः पूर्वपक्षका कथन सर्वथा मुक्त है, अयुक्त नहीं। उत्तरपक्षका कथन ही अयुक्त है।
कथन ८७ और उसकी समीक्षा
उत्तरपक्षनेत० ० पृ० ७१ पर आगे लिखा है कि "इसी प्रसंग में दूसरी आपत्ति उपस्थित करते हुए अपने लिखा है कि 'गाथा ११७ के उत्तरार्धमें जो संसारके अभावको अथवा सांख्यमतको प्रसक्तिरूप आपत्ति उपस्थित की है वह मुद्गलको परिणामी स्वभाव न मानने पर ही उपस्थित हो सकती है, अपने आप ( स्वत: सिद्ध) परिणामी स्वभाव के अभाव में नहीं' आदि। किन्तु यह आपत्ति इसलिए ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यको परतः परिणामी स्वभाव माननेपर एक तो वह द्रव्यका स्वभाव नहीं ठहरेगा और ऐसी अवस्थामे द्रव्यका ही अभाव मानना पड़ेगा । दूसरे, यह जीव पुद्गल कर्मसे सदा ही बद्ध बना रहेगा, अतएव मुक्ति के लिए यह आत्मा स्वतन्त्र रूपसे प्रयत्न भी न कर सकेगा। यदि अपरपक्ष इस आपत्तिको उपस्थित