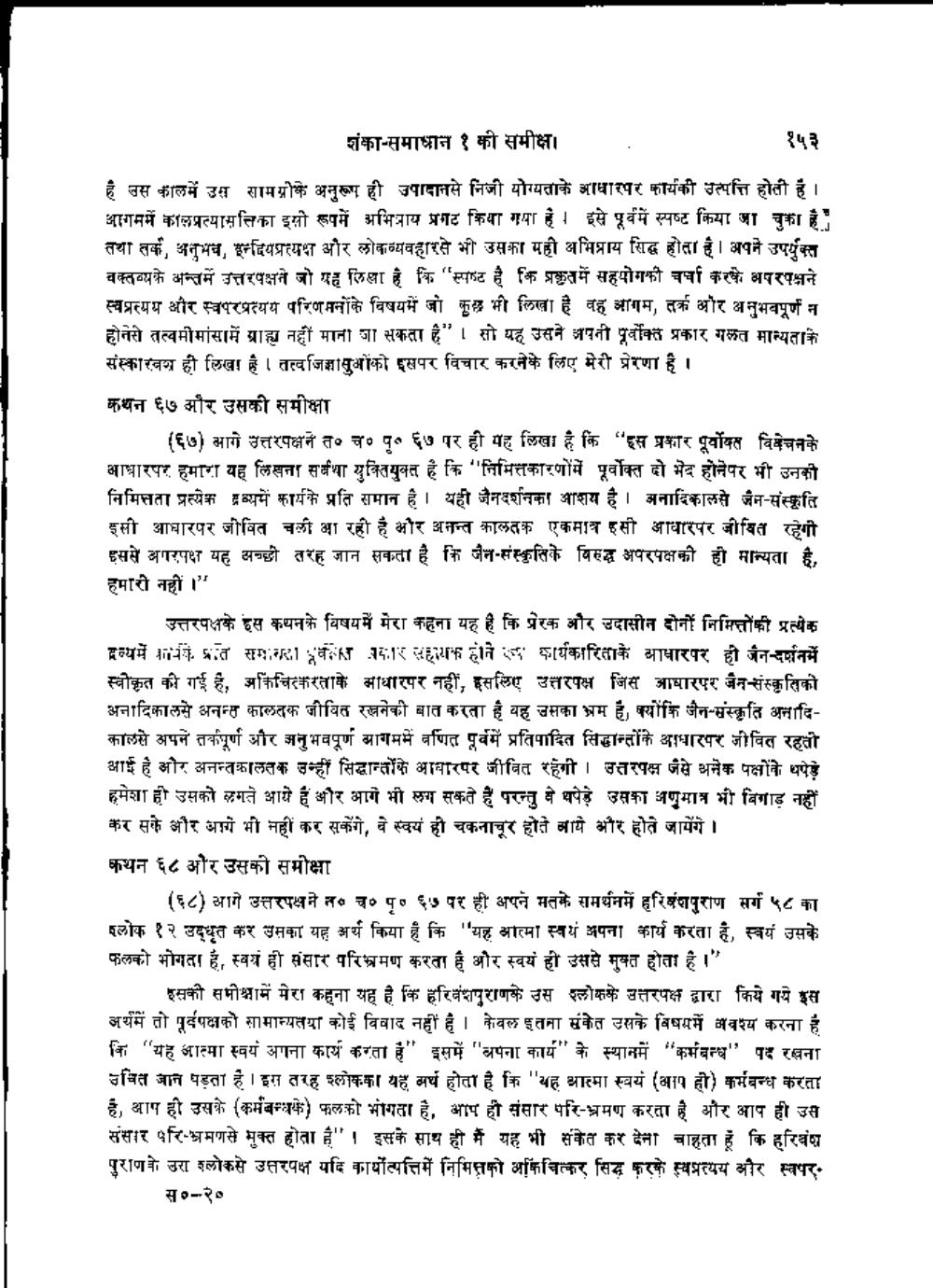________________
शंका-समाधान १ की समीक्षा
१५३
हैं उस काल में उस सामग्री के अनुरूप ही उपादानसे निजी योग्यता के आधारपर कार्यकी उत्पत्ति होती है । आगम में कालप्रत्यासत्तिका इसी रूप में अभिप्राय प्रगट किया गया है। इसे पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है तथा तर्क, अनुभव, इदयप्रत्यक्ष और लोकव्यवहारसे भी उसका यही अभिप्राय सिद्ध होता है । अपने उपर्युक्त वक्तव्य के अन्त में उत्तरपक्षने जो यह लिखा है कि "स्पष्ट कि प्रकृत में सहयोगी चर्चा करके अपरपक्षने स्वप्रत्यय और स्वपप्रत्यय परिणमनों के विषयमें जो कुछ भी लिखा है वह आगम, तर्क और अनुभवपूर्ण न होनेसे तत्वमीमांसा में ग्राह्य नहीं माना जा सकता है"। सो यह उसने अपनी पूर्वोक्त प्रकार गलत मान्यता के संस्कार ही लिखा है । तत्वजिज्ञासुओं को इसपर विचार करने के लिए मेरी प्रेरणा है ।
कथन ६७ और उसकी समीक्षा
(६७) आगे उत्तरपक्षनेत० च० पू० ६७ पर ही यह लिखा है कि "इस प्रकार पूर्वोक्त विवेचनके आधारपर हमारा यह लिखना सर्वथा युक्तियुक्त हैं कि "निमित्तकारणों में पूर्वोक्त दो भेद होनेपर भी उनकी निमितता प्रत्येक द्रव्यमें कार्य के प्रति समान है। यही जैनदर्शनका आशय है। अनादिकालसे जैन-संस्कृति इसी आधारपर जीवित चली आ रही है और अनन्त कालतक एकमात्र इसी आधारपर जीवित रहेगी इससे अपरपक्ष यह अच्छी तरह जान सकता है कि जैन संस्कृति के विरुद्ध अपरपक्षकी हो मान्यता है, हमारी नहीं ।"
उत्तरपक्षके इस कथन के विषय में मेरा कहना यह है कि प्रेरक और उदासीन दोनों निमित्तोंकी प्रत्येक द्रव्यमें आके प्रति समानाकार सहायक होते कार्यकारिता के आधारपर ही जैन दर्शनमें स्वीकृत की गई है, अकिचित्करताके माधारपर नहीं, इसलिए उत्तरपक्ष जिस आधारपर जैन संस्कृतिको अनादिकालसे अनन्त कालतक जीवित रखनेकी बात करता है वह उसका भ्रम है, क्योंकि जैन- संस्कृति अनादिकालसे अपने तर्कपूर्ण और अनुभवपूर्ण आगम में वर्णित पूर्वमें प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधारपर जीवित रहती आई है और अनन्तकालतक उन्हीं सिद्धान्तोंके आधारपर जीवित रहेंगी। उत्तरपक्ष जैसे अनेक पक्षोंके थपेड़े हमेशा हो उसको लगते आये हैं और आगे भी लग सकते हैं परन्तु मे थपेड़े कर सके और आगे भी नहीं कर सकेंगे, वे स्वयं ही चकनाचूर होते आये और होते जायेंगे । कथन ६८ और उसको समीक्षा
उसका अणुमात्र भी बिगाड़ नहीं
(६८) आगे उत्तरपक्ष ने त० च० पृ० ६७ पर ही अपने मलके समर्थन में हरिवंशपुराण सर्ग ९८ का श्लोक १२ उद्धृत कर उसका यह अर्थ किया है कि "यह आत्मा स्वयं अपना कार्य करता है, स्वयं उसके फलको भोगता है, स्वयं ही संसार परिभ्रमण करता है और स्वयं ही उससे मुक्त होता है ।"
इसकी समीक्षा में मेरा कहना यह है कि हरिवंशपुराणके उस श्लोकके उत्तरपक्ष द्वारा किये गये इस अर्थ में तो पूर्वपक्षको सामान्यतया कोई विवाद नहीं है । केवल इतना संकेत उसके विषय में अवश्य करना है. कि "यह आत्मा स्वयं अपना कार्य करता है" इसमें "अपना कार्य" के स्थान में "कर्मबन्ध" पद रखना उचित जान पड़ता है। इस तरह श्लोक का यह अर्थ होता है कि "यह आत्मा स्वयं (आप हो) कर्मबन्ध करता है, आप ही उसके (कर्मबन्धके) फलको भोगता है, आप ही संसार परिभ्रमण करता है और आप ही उस संसार परिभ्रमण से मुक्त होता है"। इसके साथ ही में यह भी संकेत कर देना चाहता हूँ कि हरिवंश पुराणके उरा श्लोकसे उत्तरपक्ष यदि कार्योत्पत्ति में निमितको चित्कर सिद्ध करके स्वप्रत्यय और स्वपर
स०-२०