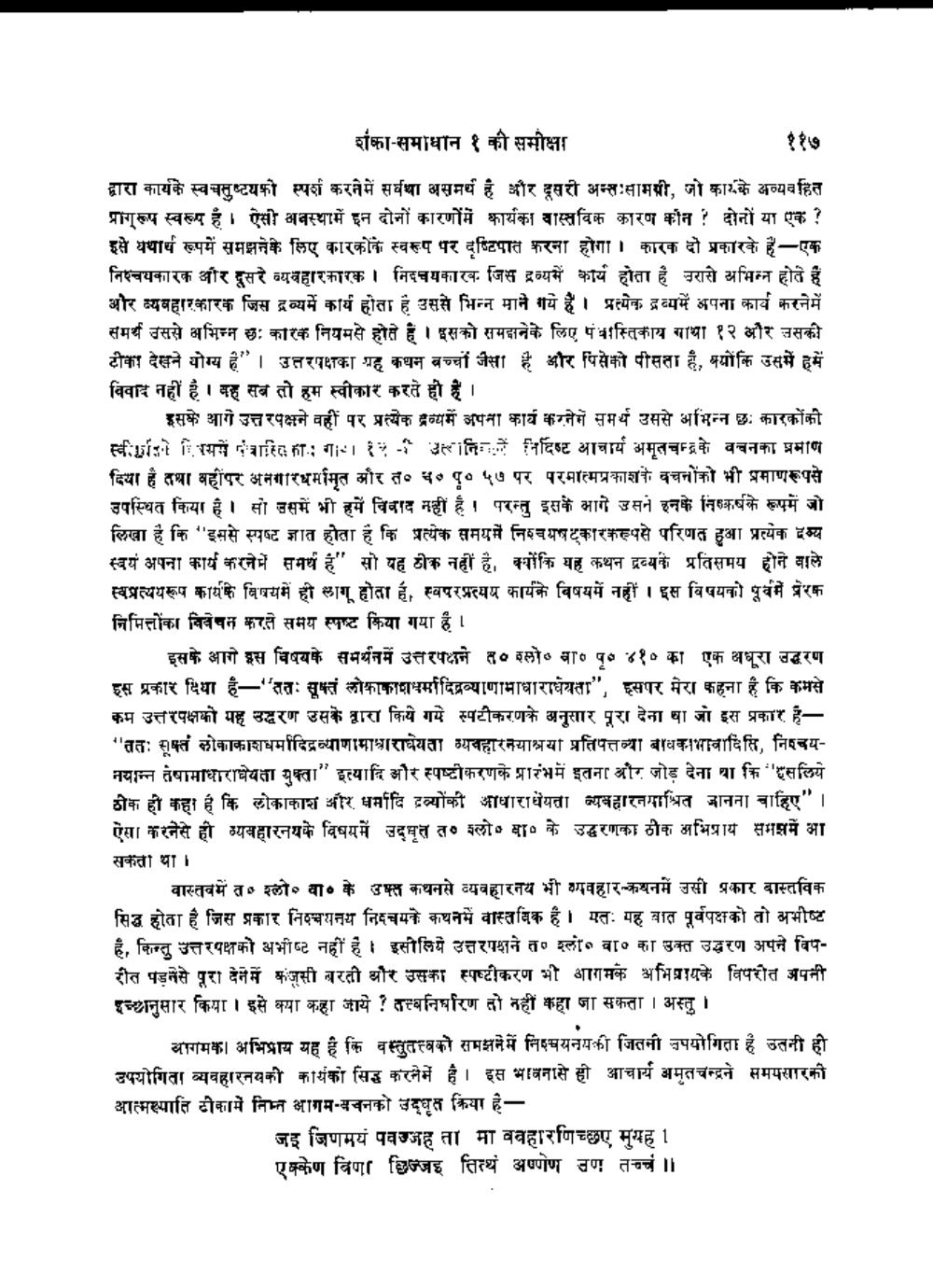________________
शंका-समाधान १ की समीक्षा
૭
द्वारा कार्य के स्वचतुष्टयको स्पर्श करने में सर्वथा असमर्थ है और दूसरी अन्तःसामग्री, जो कार्य अव्यवहित प्रागुरूप स्वरूप है। ऐसी अवस्था में इन दोनों कारणों में कार्यका वास्तविक कारण कोन ? दोनों या एक ? इसे यथार्थ रूपमें समझने के लिए कारकोंके स्वरूप पर दृष्टिपात करना होगा । कारक दो प्रकारके है - एक निश्चयकारक और दूसरे व्यवहारकारक। निदचयकारक जिस द्रव्यमें कार्य होता है उसे अभिन्न होते हैं और व्यवहारकारक जिस द्रव्यमें कार्य होता है उससे भिन्न माने गये हैं । प्रत्येक द्रव्य में अपना कार्य करने में समर्थ उससे अभिन्न छः कारक नियमसे होते हैं । इसको समझने के लिए पंचास्तिकाय गाथा १२ और उसकी टीका देखने योग्य है" । उत्तरपक्षका ग्रह कथन बच्चों जैसा है और पिसेको पीसता है, क्योंकि उसमें हमें विवाद नहीं है । वह सब तो हम स्वीकार करते ही हैं ।
इसके आगे उत्तरपक्षने वहीं पर प्रत्येक द्रव्य में अपना कार्य करने में समर्थ उससे अभिन्न छः कारकों की स्वागत निर्दिष्ट आचार्य अमृतचन्द्र के वचनका प्रमाण दिया है तथा वहीं पर अनगारधर्मामृत और त० ० ० ५७ पर परमात्मप्रकाशके वचनोंको भी प्रमाणरूपसे उपस्थित किया है। सो उसमें भी हमें विवाद नहीं है । परन्तु इसके आगे उसने इनके निष्कर्ष के रूपमें जो लिखा है कि "इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रत्येक समय में निश्चय कारकरूपसे परिणत हुआ प्रत्येक दम्य स्वयं अपना कार्य करने में समर्थ है " सो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह कथन द्रव्य के प्रतिसमय होने वाले स्वप्रत्ययरूप कार्यके विषय में ही लागू होता है, स्वपर प्रत्यय कार्यके विषय में नहीं । इस विषयको पूर्व में प्रेरक निमितोका विवेचन करते समय स्पष्ट किया गया है ।
इसके आगे इस विषय के समर्थन में उत्तरपक्षने त० श्लो० वा० पृ० ४१० का एक अधूरा उद्धरण इस प्रकार दिया है- " ततः सूक्तं लोकाकाशधर्मादिद्रव्याणामाधाराधेयता", इसपर मेरा कहना है कि कमसे कम उत्तरपक्षको मह उद्धरण उसके द्वारा किये गये स्पष्टीकरणके अनुसार पूरा देना था जो इस प्रकार है"ततः सूक्तं लोकाकाशधर्मादिद्रव्याणामाश्राराधेयता व्यवहारनयाश्रया प्रतिपत्तव्या बाधकाभावादिति निश्चयनयान्न तेषामाधाराधेयता युक्ता" इत्यादि और स्पष्टीकरणके प्रारंभ में इतना और जोड़ देना था कि "इसलिये ठीक ही कहा है कि लोकाकाश और धर्मादि द्रव्योंकी आधाराधेयता व्यवहारनगाश्रित जानना चाहिए" I ऐसा करनेसे ही व्यवहारनयके विषय में उद्धृत त० श्लो० वा० के उद्धरणका ठीक अभिप्राय समझ में आ
सकता था ।
वास्तव में त० श्लो० वा० के उक्त कथनसे व्यवहारनय भी व्यवहार कथनमें उसी प्रकार वास्तविक सिद्ध होता है जिस प्रकार निश्चय निश्चयके कथनमें वास्तविक हैं । यतः यह बात पूर्वपक्षको तो अभीष्ट हैं, किन्तु उत्तरपक्षको अभीष्ट नहीं है । इसीलिये उत्तरपक्षनेत श्ली० वा० का उक्त उद्धरण अपने विपरीत पड़ने से पूरा देने में कंजूसी बरती और उसका स्पष्टीकरण भी आगमक अभिप्रायके विपरीत अपनी इच्छानुसार किया । इसे क्या कहा जाये ? तनिर्धारण तो नहीं कहा जा सकता । अस्तु ।
मक । अभिप्राय यह है कि वस्तुतत्त्वको समझने में निश्चयनयकी जितनी उपयोगिता है उतनी ही उपयोगिता व्यवहारनयकी कार्यको सिद्ध करनेमें है। इस भावना से ही आचार्य अमृतचन्द्रने समयसारकी आत्मस्याति टीका में निम्न आगम वचनको उद्घृत क्रिया है
जई जिणमयं पवजह ता मा बवहारणिच्छए, मुग्रह 1 एक्केण विणा छिज्जह तित्थं अण्णेण उण तच्चं ॥