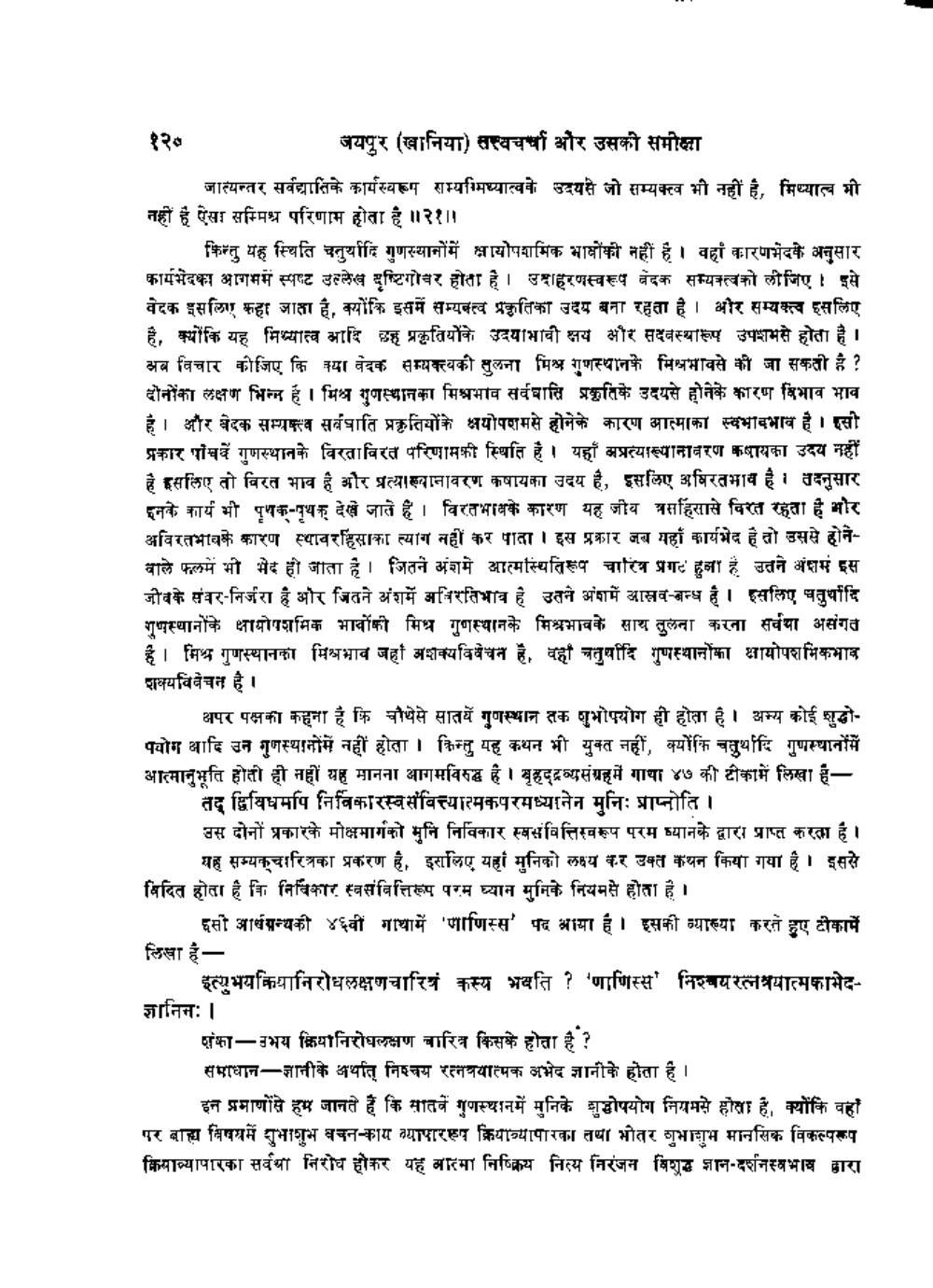________________
जयपुर (खानिया) सस्वचर्चा और उसकी समीक्षा जात्यन्तर सर्वद्यातिके कार्यस्वरूप सम्यग्मिध्यात्वके उदयसे जो सम्यक्त्व भी नहीं है, मिथ्यात्व भी नहीं है ऐसा सम्मिश्र परिणाम होता है ॥२१॥
किन्तु यह स्थिति चतुर्यादि गुणस्यानोंमें क्षायोपशमिक भाषोंकी नहीं है। वहां कारण दके अनुसार कार्यभेदका आगममें स्पष्ट उल्लेख दृष्टिगोचर होता है। उदाहरणस्वरूप बंदक सम्यक्त्वको लीजिए। इसे वेदक इसलिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय बना रहता है । और सम्यक्त्व इसलिए है, क्योंकि यह मिथ्यात्व आदि छह प्रकृतियोंके उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशमसे होता है । अब विचार कीजिए कि क्या वेदक सम्यक्त्वकी सलना मिश्र गुणस्थानके मिश्रमावसे की जा सकती है? दोनोंका लक्षण भिन्न है । मिथ गुणस्थानका मिश्रभाव सर्वघाति प्रकृतिके उदयसे होनेके कारण विभाव भाव है। और वेदक सम्यक्त्व सर्वपाति प्रकृतियोंके क्षयोपशमसे होनेके कारण आत्माका स्वभावभाव है। इसी प्रकार पांचवें गुणस्थानके विरताविरत परिणामकी स्थिति है। यहाँ अप्रत्याख्यानावरण करायका उदय नहीं है इसलिए तो विरत भाव है और प्रत्यारवानावरण कषायका उदय है, इसलिए अधिरतभाव है। तदनुसार इनके कार्य भी पृथक-पृथक् देखे जाते है। विरतभावके कारण यह जीव अहिंसासे विरत रहता है और अविरतभावके कारण स्थावरहिंसाका त्याग नहीं कर पाता । इस प्रकार जब यहाँ कार्यभेद है तो उससे होनेवाले फलमें भी भेद हो जाता है। जितने अंशमे आत्मस्थितिरूप चारित्र प्रगट' हुना है उतने जीवके संवर-निर्जरा है और जितने अंशमें अविरतिभाव है उतने अंशमें आसव-बन्ध है। इसलिए चतुर्थादि गुणस्थानोंके क्षायोपशमिक भावोंकी मिश्र गुणस्थानके मिश्रभावके साथ तुलना करना सर्वथा असंगत है। मिश्र गुणस्थानका मिश्रभाव जहाँ अशक्यविवेचन है, वहीं चतुर्थादि गुणस्थानोंका क्षायोपशमिकभाव शक्यविवेचन है।
अपर पक्षका कहना है कि चौथेसे सातये गुणस्थान तक शुभोपयोग ही होता है। अभ्य कोई शुद्धोपयोग आदि उन गुणस्थानोंमें नहीं होता। किन्तु यह कथन भी युक्त नहीं, क्योंकि चतुर्थादि गुणस्थानों में आत्मानुभूति होती ही नहीं यह मानना आगमविरुद्ध है । बृहद्रव्यसंग्रहमें गाया ४७ की टीकामें लिखा है
तद् द्विविधपि निर्विकारस्व संवित्त्यारमकपरमध्यानेन मुनिः प्राप्नोति । उस दोनों प्रकारके मोक्षमार्गको मुनि निर्विकार स्वसंवित्तिस्वरूप परम ध्यानके द्वारा प्राप्त करता है।
यह सम्यक्चारित्रका प्रकरण है, इसलिए यहाँ मुनिको लक्ष्य कर उक्त कथन किया गया है। इससे विदित होता है कि निर्विकार स्वसंवित्तिरूप परम घ्यान मुनिके नियमसे होता है।
इसी आर्थग्रन्थकी ४६वी गाथामें 'गाणिस्स' पद पाया है। इसकी व्याख्या करते हुए टीका लिखा है
इत्युभयक्रियानिरोधलक्षणचारित्रं कस्य भवति ? 'णाणिस्स' निश्चयरलत्रयात्मकाभेदज्ञानिनः ।
शंका-उभय क्रियानिरोघलक्षण बारिब किसके होता है ? समाधान-ज्ञानीके अर्थात् निश्चय रत्नत्रयात्मक अभेद ज्ञानीके होता है ।
इन प्रमाणोंसे हम जानते है कि सात गुणस्थानमें मुनिके शुद्धोपयोग नियमसे होता है, क्योंकि वहाँ पर बाह्य विषयमें शुभाशुभ वचन-काय व्यापारमा क्रियान्यापारका तथा भौतर शुभाशुभ मानसिक विकल्परूप क्रियान्यापारका सर्वश्रा निरोध होकर यह आत्मा निष्क्रिय नित्य निरंजन विशद्ध ज्ञान-दर्शनस्वभाव द्वारा