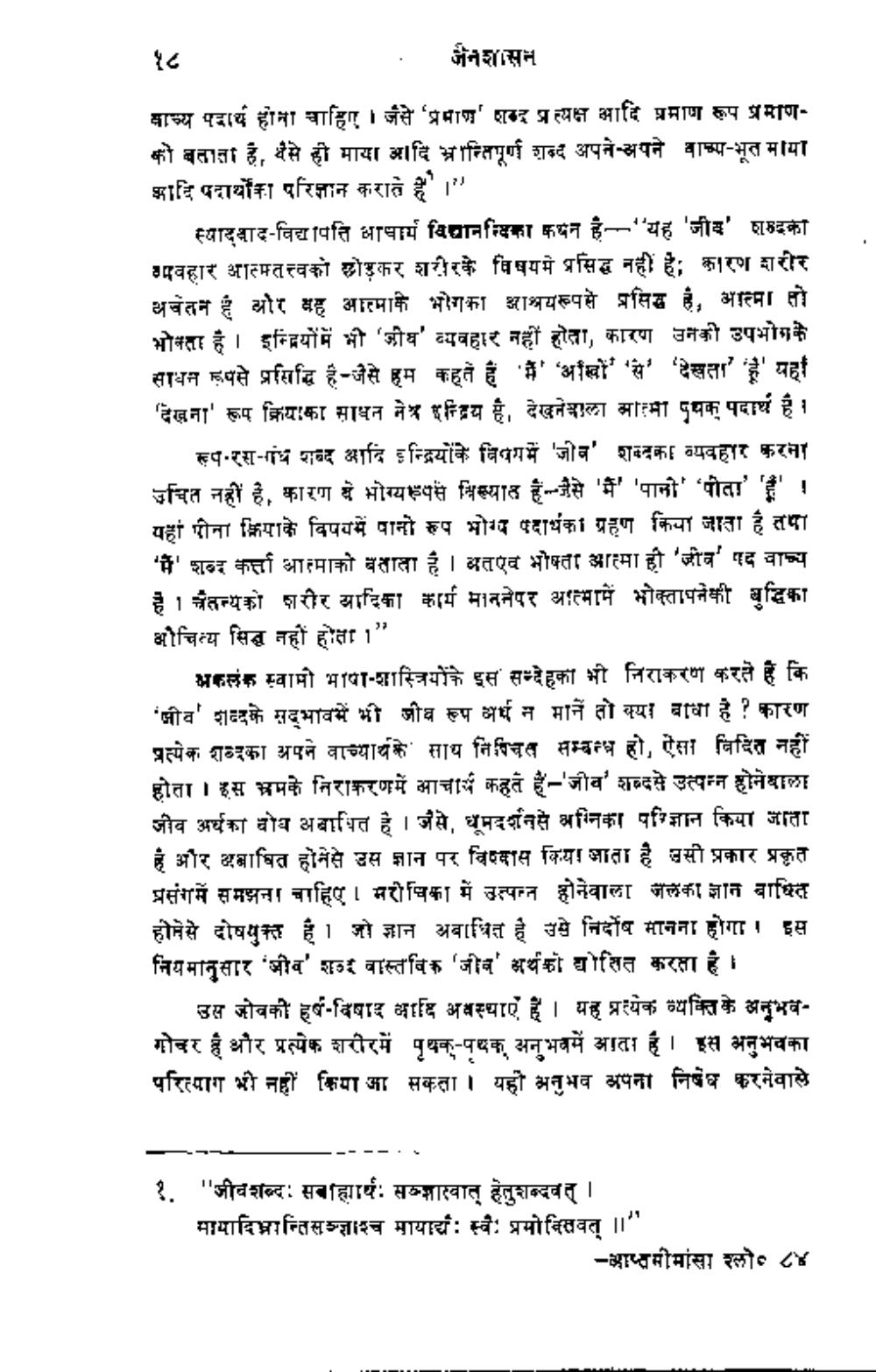________________
૧૮
जैनशासन
वाच्य पदार्थ होना चाहिए। जैसे 'प्रमाण' शब्द प्रत्यक्ष आदि प्रमाण रूप प्रमाणको बताता है, वैसे ही माया आदि भ्रान्तिपूर्ण शब्द अपने-अपने बाप-भूत माया कादि पदार्थोंका परिज्ञान कराते हैं
ין
स्याद्वाद - विद्यापति आचार्य विधानविका कथन है- 'यह 'जीव' शब्दका उपहार आत्मतत्त्वको छोड़कर शरीर के विषय मे प्रसिद्ध नहीं है; कारण शरीर अवेतन है और वह आत्माके भोगका आश्रयरूपसे प्रसिद्ध है, आत्मा तो भोक्ता है । इन्द्रियों में भी 'जीव' व्यवहार नहीं होता, कारण उनकी उपभोग के सावन रूपसे प्रसिद्धि है-जैसे हम कहते हैं मैं' 'आँखों' 'से' 'देखता' 'है' यहाँ 'देखना ' रूप क्रियाका साधन ने इन्द्रिय है। देखनेवाला मात्मा पृथक पदार्थ हैं।
रूप-रस-गंध शब्द आदि इन्द्रियोंके विषय में 'जीव' शब्दका व्यवहार करना उचित नहीं है, कारण हे भोग्यरूपसे विख्यात है-जैसे 'में' 'पानी' 'पीता' 'हूँ' । यहां पीना क्रियाके पियमें पानों रूप भोग्य पदार्थका ग्रहण किया जाता है तथा 'मैं' शब्द कर्ता आत्माको बताता है। बतएव भोक्ता आत्मा ही 'जीव' पद चाच्य है । चैतन्यको शरीर आदिका कार्य माननेपर आत्मामें भोक्ता पनेकी बुद्धिका ओचित्य सिद्ध नहीं होता 1 "
अकलंक स्वामी भाषा शास्त्रियोंके इस सन्देहका भी निराकरण करते हैं कि 'शीव' शब्द के सद्भावमें भी जीव रूप अर्थ न मानें तो क्या बाबा है ? कारण प्रत्येक शब्दका अपने वाच्यार्थ के साथ निश्चित सम्बन्ध हो, ऐसा विदित नहीं होता । इस भ्रम के निराकरण में आचार्य कहते हैं- 'जीव' शब्द से उत्पन्न होनेवाला जीव अर्थका वो अबाधित है । जैसे, धूमदर्शन से अग्निका परिज्ञान किया जाता हूँ और अबाधित होनेसे उस ज्ञान पर विश्वास किया जाता है उसी प्रकार प्रकृत प्रसंग में समझना चाहिए। मरीचिका में उत्पन्न होनेवाला जलका ज्ञान बाधित होने से दोषयुक्त हूँ। जो ज्ञान अबाधित है उसे निर्दोष मानना होगा। इस नियमानुसार 'जीव' शब्द वास्तविक 'जीव' अर्थको घोषित करता है ।
उस जो की हर्ष-विषाद आदि अवस्थाएं हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति के अनुभवगोवर है और प्रत्येक शरीर में पृथक-पृथक अनुभव में आता है। इस अनुभव का परित्याग भी नहीं किया जा सकता । यहाँ अनुभव अपना निषेध करनेवाले
१. "जीवशब्दः सबाह्यर्थः सशास्वात् हेतुशब्दवत् । मायादिभ्रान्तिसज्ञाश्च मायाद्यैः स्वैः प्रयोवितवत् ||"
-आप्तमीमांसा श्लो० ८४