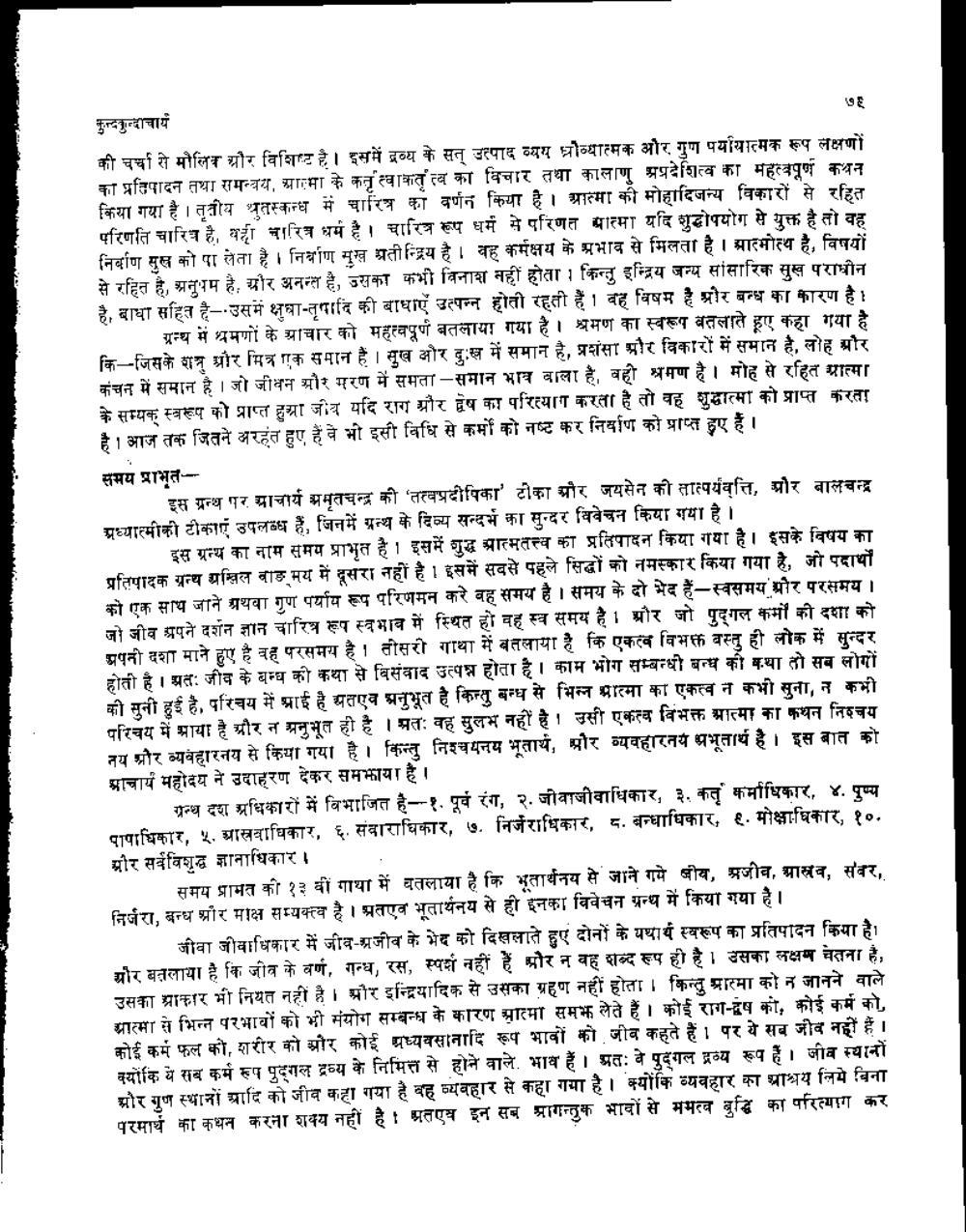________________
७६
कुन्दकुन्दाचार्य
की चर्चा से मौलिक और विशिष्ट है। इसमें द्रव्य के सत् उत्पाद व्यय श्रीव्यात्मक और गुण पर्यायात्मक रूप लक्षणों का प्रतिपादन तथा समन्वय आत्मा के कर्तृत्वाकर्तृत्व का विचार तथा कालाणु श्रप्रदेशित्व का महत्वपूर्ण कथन किया गया है। तृतीय शुतस्कन्ध में चारित्र का वर्णन किया है। आत्मा की मोहादिजन्य विकारों से रहित परिणति चारित्र है, वही चारित्र धर्म है। चारित्र रूप धर्म से परिणत बात्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त है तो वह निर्वाण 'सुख को पा लेता है। निर्माण सुख अतीन्द्रिय है। वह कर्मक्षय के प्रभाव से मिलता है। आत्मोत्थ है, विषयों से रहित है, अनुपम है, और अनन्त है, उसका कभी विनाश नहीं होता । किन्तु इन्द्रिय जन्य सांसारिक सुख पराधीन है, बाधा सहित है-- उसमें क्षुधा तृपादि की बाधाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। वह विषम है और बन्ध का कारण है । ग्रन्थ में श्रमणों के आचार को महत्वपूर्ण बतलाया गया है। श्रमण का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है। कि - जिसके शत्रु और मित्र एक समान हैं। सुख और दुःख में समान है, प्रशंसा और विकारों में समान है, लोह और कंचन में समान है । जो जीवन और मरण में समता-समान भाव वाला है, वही श्रमण है। मोह से रहित ग्रात्मा के सम्यक् स्वरूप को प्राप्त हुग्रा जीव यदि राग और द्वेष का परित्याग करता है तो वह शुद्धात्मा को प्राप्त करता है । आज तक जितने अरहंत हुए हैं वे भी इसी विधि से कर्मों को नष्ट कर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं ।
समय प्राभूत
इस ग्रन्थ पर आचार्य अमृतचन्द्र को 'तत्वप्रदीपिका' टीका और जयसेन की तात्पर्यवृत्ति, और बालचन्द्र अध्यात्मीकी टीकाएं उपलब्ध हैं, जिनमें ग्रन्थ के दिव्य सन्दर्भ का सुन्दर विवेचन किया गया है ।
इस ग्रन्थ का नाम समय प्राभृत है। इसमें शुद्ध आत्मतत्व का प्रतिपादन किया गया है। इसके विषय का प्रतिपादक ग्रन्थ अनिल वाङमय में दूसरा नहीं है । इसमें सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार किया गया है, जो पदार्थों को एक साथ जाने अथवा गुण पर्याय रूप परिणमन करे वह समय है। समय के दो भेद हैं- स्वसमय और परसमय । जो जीव अपने दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वभाव में स्थित हो वह स्व समय है । और जो पुद्गल कर्मों की दशा को बतलाया है कि एकत्व विभक्त वस्तु ही लोक में सुन्दर अपनी दशा माने हुए है वह परसमय है। तीसरी गाथा होती है | अतः जीव के बन्ध की कथा से विसंवाद उत्पन्न होता है । काम भोग सम्बन्धी बन्ध की कथा तो सब लोगों की सुनी हुई है, परिचय में श्राई है अतएव अनुभूत है किन्तु बन्ध से भिन्न श्रात्मा का एकत्व न कभी सुना, न कभी परिचय में भाया है और न अनुभूत ही है । अतः वह सुलभ नहीं है । उसी एकत्व विभक्त आत्मा का कथन निश्चय नय और व्यवहारनय से किया गया है। किन्तु निश्चयनय भूतार्थ, और व्यवहारतय अभूतार्थ है। इस बात को श्राचार्य महोदय ने उदाहरण देकर समझाया है ।
ग्रन्थ दश अधिकारों में विभाजित है -१. पूर्व रंग, २. जीवाजीवाधिकार, ३. कर्तृ कर्माधिकार, ४. पुष्य पापाधिकार, ५. आस्त्रवाधिकार, ६. संकाराधिकार ७. निर्जराधिकार, ८. बन्धाधिकार, ९. मोक्षाधिकार, १०. और सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार ।
कि भूतार्थनय से जाने गये जीव, अजीव, आस्रव, संवर, समय प्रामत की १३ वी गाथा में बतलाया निर्जरा, बन्ध और माक्ष सम्यक्त्व है । श्रतएव भूतार्थनय से ही इनका विवेचन ग्रन्थ में किया गया है ।
जीवा जीवाधिकार में जीव अजीव के भेद को दिखलाते हुए दोनों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन किया है। योर बतलाया है कि जीव के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श नहीं हैं और न वह शब्द रूप ही है । उसका लक्षण चेतना है, उसका आकार भी नियत नहीं है। और इन्द्रियादिक से उसका ग्रहण नहीं होता। किन्तु श्रात्मा को न जानने वाले आत्मा से भिन्न परभावों को भी संयोग सम्बन्ध के कारण आत्मा समझ लेते हैं। कोई राग-द्वेष की, कोई कर्म को, कोई कर्म फल को, शरीर को और कोई श्रध्यवसानादि रूप भावों को जीव कहते हैं। पर ये सब जीव नहीं है । क्योंकि ये सब कर्म रूप पुद्गल द्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव हैं। अतः वे पुद्गल द्रव्य रूप हैं । जीव स्थानों और गुण स्थानों आदि को जीव कहा गया है वह व्यवहार से कहा गया है। क्योंकि व्यवहार का आश्रय लिये बिना परमार्थ का कथन करना शक्य नहीं है। अतएव इन सब श्रागन्तुक भावों से ममत्व बुद्धि का परित्याग कर