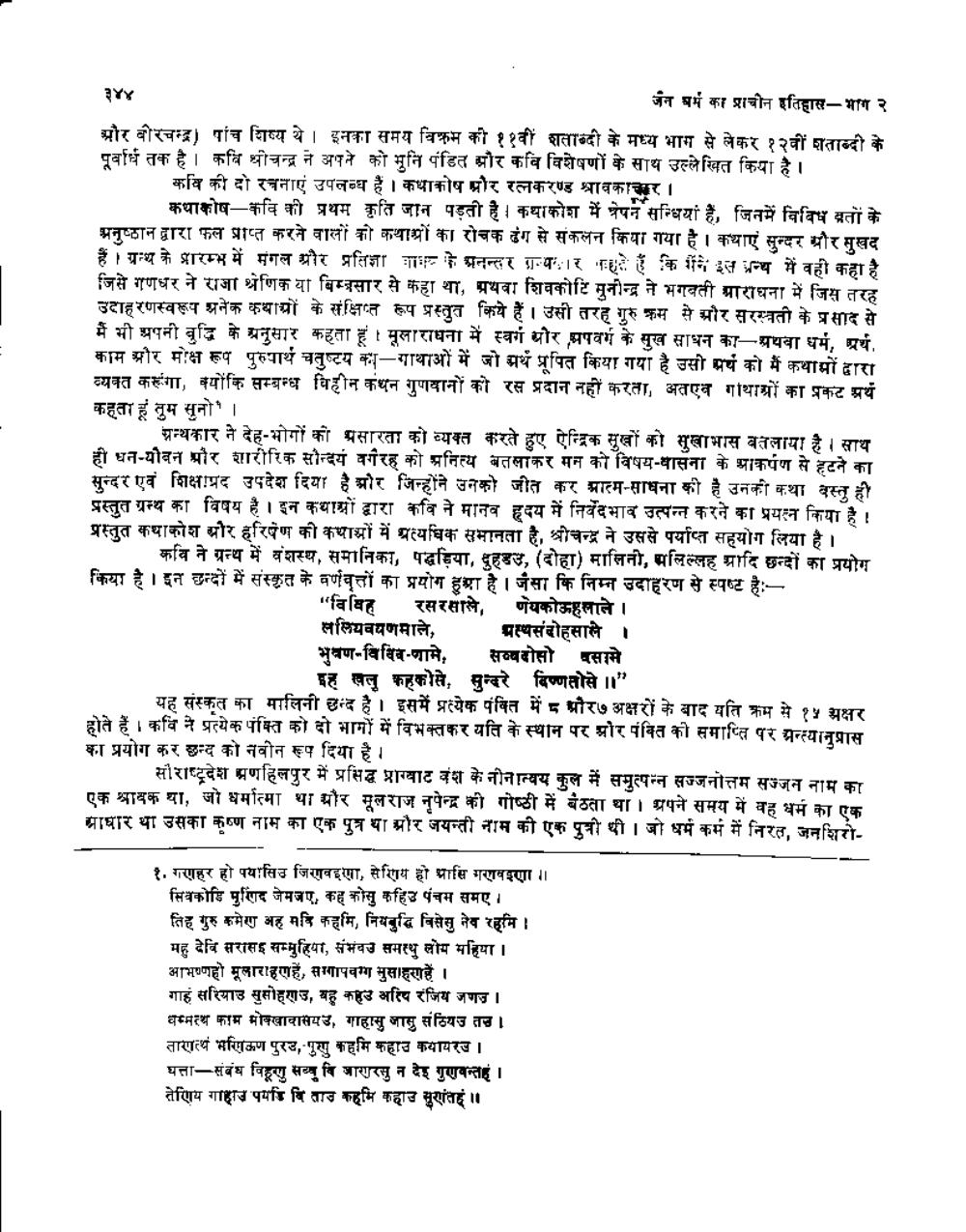________________
३४४
जैन धर्म का प्राचीन इतिहास-भाग २
और वीरचन्द्र) पांच शिष्य थे। इनका समय विक्रम की ११वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर १२वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक है। कवि श्रीचन्द्र ने अपने को मुनि पंडित और कवि विशेषणों के साथ उल्लेखित किया है।
कवि की दो रचनाएं उपलब्ध हैं। कथाकोष प्रौर रलकरण्ड श्रावकाचार ।
कथाकोष-कवि की प्रथम कृति जान पड़ती है । कथाकोश में प्रेपन सन्धियां हैं, जिनमें विविध व्रतों के अनुष्ठान द्वारा फल प्राप्त करने वालों को कथाओं का रोचक ढंग से संकलन किया गया है। कथाएं सुन्दर और सुखद हैं। ग्रन्थ के प्रारम्भ में मंगल और प्रतिज्ञा नाम के अनन्तर प्रयाः । र महते हैं कि मैंने इस अन्ध में वही कहा है जिसे गणधर ने राजा श्रेणिक या बिम्बसार से कहा था, अथवा शिवकोटि मुनीन्द्र ने भगवती पाराधना में जिस तरह उदाहरणस्वरूप अनेक कथानों के संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किये हैं। उसी तरह गुरु क्रम से और सरस्वती के प्रसाद से मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं। मुलाराधना में स्वर्ग और प्रपवर्ग के सुख साधन का अथवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय का-गाथाओं में जो अर्थ पूपित किया गया है उसी प्रथं को मैं कथामों द्वारा व्यक्त करूंगा, क्योंकि सम्बन्ध विहीन कथन गुणवानों को रस प्रदान नहीं करता, अतएव गाथाओं का प्रकट अर्थ कहता हूँ तुम सुनो।
ग्रन्थकार ने देह-भोगों को प्रसारता को व्यक्त करते हुए ऐन्द्रिक सुखों को सुखाभास बतलाया है। साथ ही धन-यौवन और शारीरिक सौन्दयं वगैरह को अनित्य बतलाकर मन को विषय-वासना के आकर्षण से हटने का सुन्दर एवं शिक्षाप्रद उपदेश दिया है और जिन्होंने उनको जीत कर प्रात्म-साधना की है उनकी कथा बस्तु ही प्रस्तुत ग्रन्थ का विषय है। इन कथानों द्वारा कवि ने मानव हृदय में निर्वेदभाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। प्रस्तुत कथाकोश और हरिषेण की कथाओं में अत्यधिक समानता है, श्रीचन्द्र ने उससे पर्याप्त सहयोग लिया है।
कवि ने ग्रन्थ में वंशस्थ, समानिका, पद्धड़िया, हडड, (दोहा) मालिनी, मलिल्लह प्रादि छन्दों का प्रयोग किया है। इन छन्दों में संस्कृत के वर्णवृत्तों का प्रयोग हुया है। जैसा कि निम्न उदाहरण से स्पष्ट है:
"विविह रसरसाले, णयकोऊहलाले । ललियवयणमाले, प्रस्थसंदोहसाले । भुवण-विविव-णामे, सव्वदोसो बसामे
बह खलु कहकोसे, सुन्दरे विणतोसे ॥" यह संस्कत का मालिनी छन्द है। इसमें प्रत्येक पंक्ति में 5 और७ अक्षरों के बाद यति क्रम से १५ अक्षर होते हैं। कवि ने प्रत्येक पंक्ति को दो भागों में विभक्तकर यति के स्थान पर और पंक्ति को समाप्ति पर अन्त्यानुप्रास का प्रयोग कर छन्द को नवीन रूप दिया है।
सौराष्ट्रदेश प्रणहिलपुर में प्रसिद्ध प्राग्वाट वंश के नीनान्वय कुल में समुत्पन्न सज्जनोत्तम सज्जन नाम का एक श्रावक था, जो धर्मात्मा था और मूलराज नृपेन्द्र की गोष्ठी में बैठता था। अपने समय में वह धर्म का एक प्राधार था उसका कृष्ण नाम का एक पुत्र था और जयन्ती नाम की एक पुत्री थी । जो धर्म कर्म में निरत, जनशिरो
१. गणहर हो पयासिउ जिरणवइणा, सेरिणय हो भासि गणवइया ।। सिवकोडि मुरिणद जेमजए, कह कोसु कहिउ पंचम समए। तिह गुरु कमेण अह मदि कहमि, नियबुद्धि विसेसु नेव रहमि । महु देवि सरासइ सम्मुहिया, संभवउ समस्थ लोय महिया । आभण्णहो मूलाराहणहे, सग्गापवग्ग मुसाहरणहें । गाहं सरियाउ सुसोहणउ, बहु कहउ अस्थि रंजिय जणउ । धम्मरथ काम मोक्खावासपउ, गाहासु जासु संठियउ त । ताणत्यं मणिऊण पुरउ, पुणु कहमि कहाउ कथायरज । पत्ता-संबंध विहूणु सव्यु वि जागरसु न देइ गुणवन्तहं । तेणिय गाहाज पडि वि ताउ कहामि कहाउ सुरणंतहं ।।