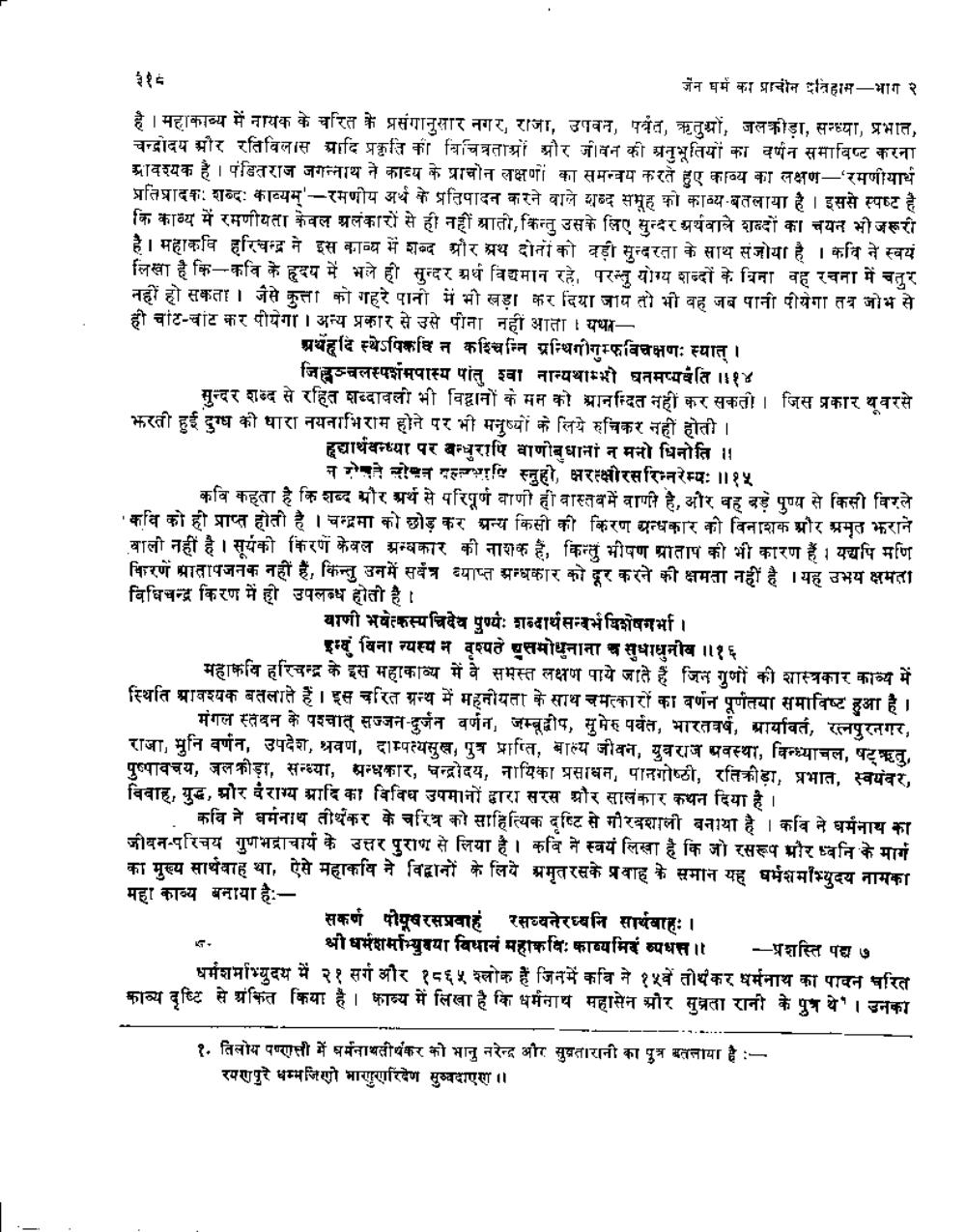________________
जैन धर्म का प्राचीन इतिहाम-भाग २
है । महाकाव्य में नायक के चरित के प्रसंगानुसार नगर, राजा, उपवन, पर्वत, ऋतुओं, जलक्रीड़ा, सन्ध्या, प्रभात, चन्द्रोदय और रतिविलास प्रादि प्रकृति का विचित्रताओं और जीवन की अनुभूतियों का वर्णन समाविष्ट करना आवश्यक है। पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य के प्राचीन लक्षणों का समन्वय करते हुए काव्य का लक्षण–'रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्'-रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाले शब्द समुह को काव्य-बतलाया है । इससे स्पष्ट है कि काव्य में रमणीयता केवल अलंकारों से ही नहीं पाती,किन्तु उसके लिए सुन्दर अर्थवाले शब्दों का चयन भी जरूरी है। महाकवि हरिचन्द्र ने इस काव्य में शब्द और अथ दोनों को बड़ी सुन्दरता के साथ संजोया है । कवि ने स्वयं लिखा है कि-कवि के हृदय में भले ही सुन्दर अर्थ विद्यमान रहे, परन्तु योग्य शब्दों के बिना वह रचना में चतुर नहीं हो सकता। जैसे कुत्ता को गहरे पानी में भी खड़ा कर दिया जाय तो भी बह जब पानी पीयेगा तब जोभ से ही चांट-चांट कर पीयेगा। अन्य प्रकार से उसे पीना नहीं आता । यथा
अहदि स्थेऽपिकदिन कश्चिन्नि प्रन्थिगीगम्फविचक्षणः स्यात् ।
जिहञ्चलस्पर्शमपास्य पातु श्वा नान्यथाम्भो घनमप्यर्वति ।।१४ सुन्दर शब्द से रहित शब्दावली भी विद्वानों के मन को आनन्दित नहीं कर सकती। जिस प्रकार थूवरसे झरती हुई दुग्ध की धारा नयनाभिराम होने पर भी मनुष्यों के लिये रुचिकर नहीं होती।
हृद्यार्थवन्ध्या पर बन्धुरापि वाणोबुधानां न मनो धिनोति ।।
नरोने लोगन पलागि स्नुहो, शरत्क्षीरसरिन्नरम्यः ॥१५ कवि कहता है कि शब्द और अर्थ से परिपूर्ण वाणी ही वास्तव में वाणी है, और वह बड़े पुण्य से किसी विरले 'कवि को ही प्राप्त होती है । चन्द्रमा को छोड़ कर अन्य किसी की किरण अन्धकार को विनाशक और अमृत झराने वाली नहीं है । सूर्यको किरण केवल अन्धकार की नाशक हैं, किन्तु भीषण प्राताप की भी कारण हैं । यद्यपि मणि किरणे प्रातापजनक नहीं हैं, किन्तु उनमें सर्वत्र व्याप्त अन्धकार को दूर करने की क्षमता नहीं है । यह उभय क्षमता विधिचन्द्र किरण में ही उपलब्ध होती है।
याणी भवेत्कस्यचिदेव पुण्यः शब्दार्थसन्दर्भपिशेषगर्भा।
इन् विना ग्यस्य न वृश्यते यत्समोधुनाना च सुधाधुनीव ॥१६ महाकवि हरिचन्द्र के इस महाकाव्य में वे समस्त लक्षण पाये जाते हैं जिन गुणों की शास्त्रकार काव्य में स्थिति आवश्यक बतलाते हैं। इस चरित ग्रन्थ में महनीयता के साथ चमत्कारों का वर्णन पूर्णतया समाविष्ट हुआ है।
मंगल स्तवन के पश्चात् सज्जन-दुर्जन वर्णन, जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत, भारतवर्ष, पार्यावर्त, रत्नपुरनगर, राजा, मुनि वर्णन, उपदेश, श्रवण, दाम्पत्यसुख, पुत्र प्राप्ति, बाल्य जीवन, युवराज अवस्था, विन्ध्याचल, षट् ऋतु, पुष्पावचय, जल कीड़ा, सन्ध्या, अन्धकार, चन्द्रोदय, नायिका प्रसाधन, पानगोष्ठी, रतिक्रीड़ा, प्रभात, स्वयंवर, विवाह, युद्ध, और वैराग्य आदि का विविध उपमानों द्वारा सरस और सालंकार कथन दिया है।
कवि ने धर्मनाथ तीर्थकर के चरित्र को साहित्यिक दृष्टि से मौरवशाली बनाया है । कवि ने धर्मनाथ का जीवन-परिचय गुणभद्राचार्य के उत्तर पुराण से लिया है। कवि ने स्वयं लिखा है कि जो रसरूप और ध्वनि के मार्ग का मुख्य सार्थवाह था, ऐसे महाकवि ने विद्वानों के लिये अमृतरसके प्रवाह के समान यह धर्मशाभ्युदय नामका महा काव्य बनाया है:
सकर्ण पोपुषरसप्रवाहं रसध्यनेरध्वनि सार्थवाहः ।
श्रीधर्मशर्माभ्युक्या विधानं महाकविः काव्यमिदं व्यवस। -प्रशस्ति पद्य ७ धर्मशर्माभ्युदय में २१ सर्ग और १८६५ श्लोक हैं जिनमें कवि ने १५वें तीर्थकर धर्मनाथ का पावन चरित काव्य दृष्टि से अंकित किया है। काव्य में लिखा है कि धर्मनाथ महासेन और सुव्रता रानी के पुत्र थे। उनका
१. तिलोय पण्णसी में धर्मनाथतीर्थकर को भानु नरेन्द्र और सुनतारानी का पुत्र बतलाया है :
रपणपुरे धम्मजियो भाराणरिदेण सुवदाए ।