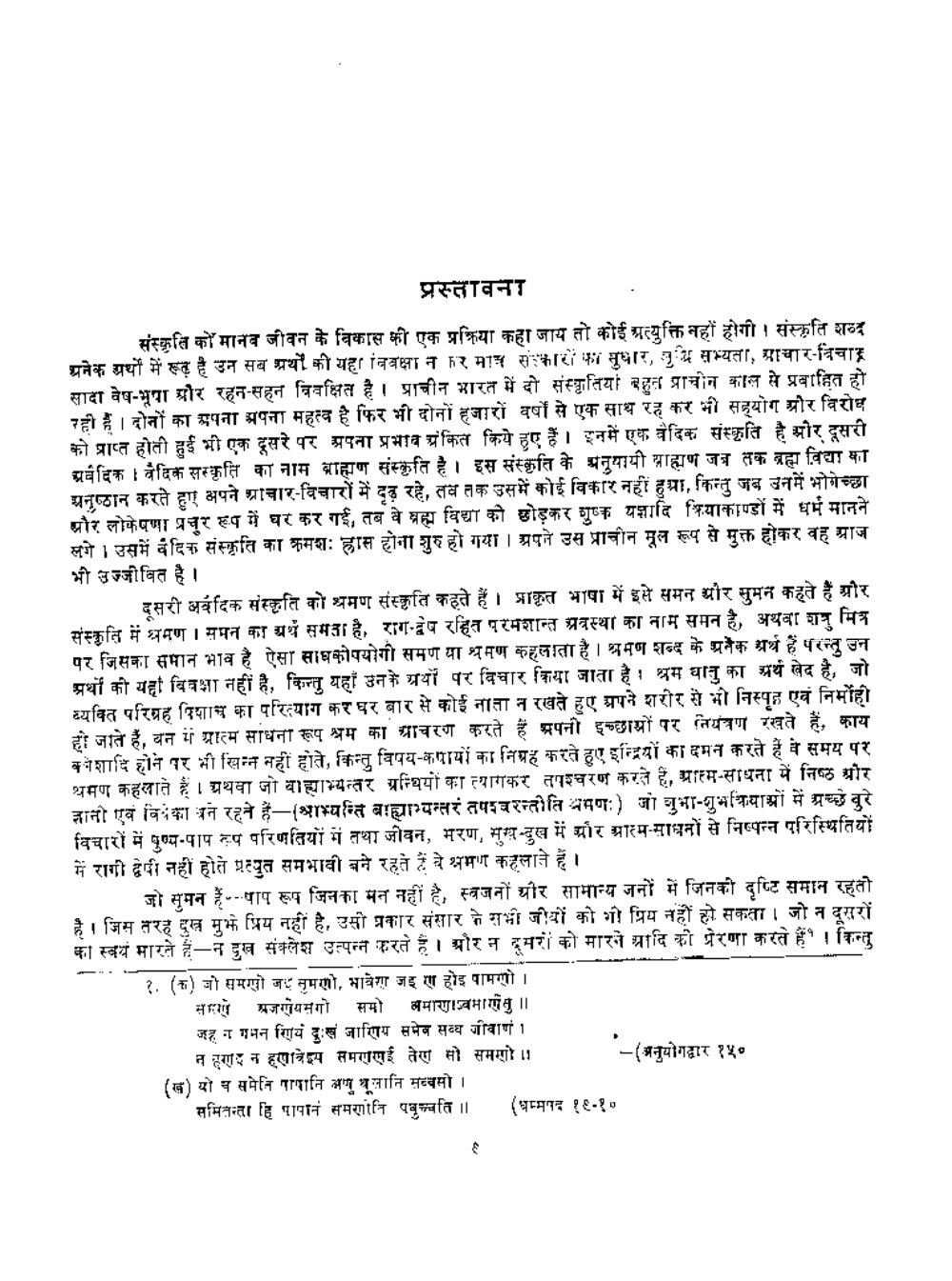________________
प्रस्तावना
संस्कृति को मानव जीवन के विकास की एक प्रक्रिया कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। संस्कृति शब्द अनेक अर्थों में रूत है उन सब अर्थों की यहा विवक्षा न र मात्र संस्कारों का सुधार, सुदि सभ्यता, प्राचार-विचार सादा वेष-भपा और रहन-सहन विवक्षित है। प्राचीन भारत में दो संस्वातिया रहन प्राचीन काल से प्रवाहित हो रही है। दोनों का अपना अपना महत्व है फिर भी दोनों हजारों वर्षों से एक साथ रह कर भी सहयोग और विरोध को प्राप्त होती हुई भी एक दूसरे पर अपना प्रभाव ग्रंकित किये हुए हैं। इनमें एक वैदिक संस्कृति है और दूसरी अवैदिक । वैदिक संस्कृति का नाम ब्राह्मण संस्कृति है। इस संस्कृति के अनुयायी माह्मण जब तक ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान करते हए अपने प्राचार-विचारों में दृढ रहे, तब तक उसमें कोई विकार नहीं हया, किन्तु जब उनमें भोगेच्छा और लोकेपणा प्रचुर रूप में घर कर गई, तब वे ब्रह्म विद्या को छोड़कर शुष्क यज्ञादि क्रियाकापड़ों में धर्म मानने लगे। उसमें वैदिक संस्कृति का क्रमशः ह्रास होना शुरु हो गया । अपने उस प्राचीन मूल रूप से मुक्त होकर वह प्राज भी उज्जीवित है।
दसरी अदिक संस्कृति को श्रमण संस्कृति कहते हैं। प्राकृत भाषा में इसे समन और सुमन कहते हैं और संस्कृति में श्रमण । समन का अर्थ समता है, राग-द्वेष रहित परमशान्त अवस्था का नाम समन है, अथवा शत्रु मित्र पर जिसका समान भाव है ऐसा साधकोपयोगी समण या श्रमण कहलाता है । श्रमण शब्द के अनेक अर्थ है परन्तु उन अर्थों की यहां विवक्षा नहीं है, किन्तु यहाँ उनके अयों पर विचार किया जाता है। श्रम धातु का अर्थ खेद है, जो व्यक्ति परिग्रह पिशाच का परित्याग कर घर बार से कोई नाता न रखते हए अपने शरीर से भी निस्पह एवं निमोही हो जाते हैं, बन में यात्म साधना रूप श्रम का याचरण करते हैं अपनी इच्छानों पर नियंत्रण रखते हैं, काय को शादि होने पर भी खिन्न नहीं होते, किन्तु विषय-कपायों का निग्रह करते हुए इन्द्रियों का दमन करते हैं वे समय पर श्रमण कहलाते हैं । अथवा जो बाह्याभ्यन्तर ग्रन्धियों का त्यागकर तपश्चरण करते हैं, प्रात्म-साधना में निष्ठ और ज्ञानी एवं विका बने रहते हैं-(श्राभ्यन्ति बाह्याभ्यन्तरं तपश्चरन्तीति अमणः) जो जुभा-शुभत्रियाओं में अच्छे बुरे विचारों में पुण्य-पाप रूप परिणतियों में तथा जीवन, मरण, मुख-दुख में और प्रात्म-साधनों से निष्पन्न परिस्थितियों में रागी द्वेषी नहीं होते प्रत्युत समभावी बने रहते हैं वे श्रमण कहलाते हैं।
जो सुमन हैं..पाप रूप जिनका मन नहीं है, स्वजनों और सामान्य जनों में जिनको दृष्टि समान रहती है । जिस तरह दुख मुझे प्रिय नहीं है, उसी प्रकार संसार के सभी जीयों को भी प्रिय नहीं हो सकता। जो न दुसरों का स्वयं मारते है-न दुख संक्लेश उत्पन्न करते हैं। और न दमरों को मारने प्रादि की प्रेरणा करते हैं । किन्तु १. (क) जो समतो जा नुमणो, भावेश जइ रण होइ पामणो ।
माग अजयमगो समो अमारणाऽवमाणे तु ।। जह न गमन भियं दुःख जारिणय समेव सब्ध जीवाण ।
न हाद न हपविश्य समणगई तेरण सो समगो।। -(अनुयोगद्वार १५० (ख) यो च समेनि पापानि अणु थलानि सच्चसो ।
समितन्ता हि पापानं समयोति पबुञ्चति ।। (धम्मपद १६-१७