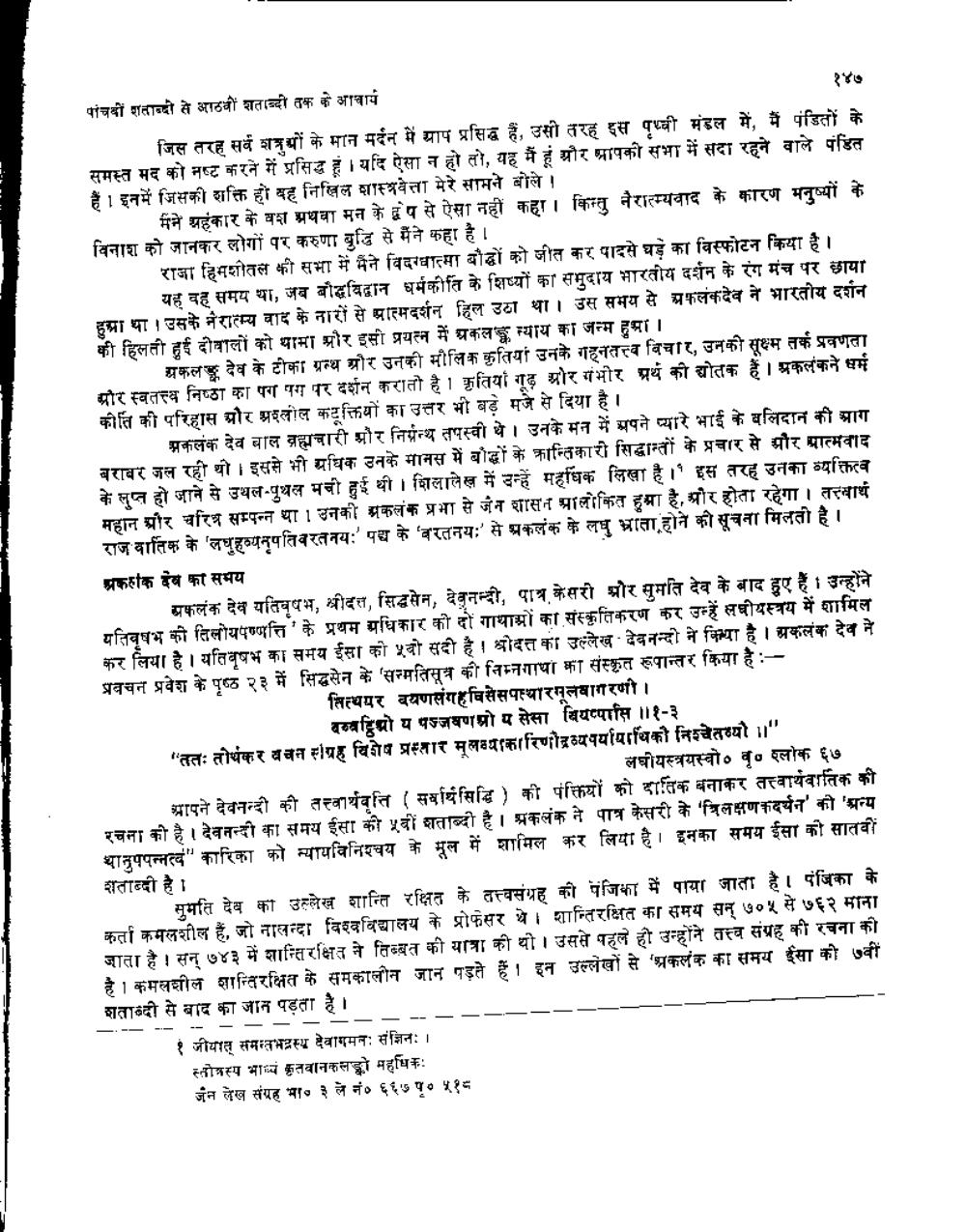________________
पांचवीं शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक के आचार्य
जिस तरह सर्व शत्रयों के मान मर्दन में ग्राप प्रसिद्ध हैं, उसी तरह इस पृथ्वी मंडल में, मैं पंडितों के समस्त मद को नष्ट करने में प्रसिद्ध हूं। यदि ऐसा न हो तो, यह मैं हूं और प्रापकी सभा में सदा रहने वाले पंडित हैं । इनमें जिसकी शक्ति हो वह निखिल शास्त्रवेत्ता मेरे सामने बोले।
मने अहंकार के वश अथवा मन के द्वेष से ऐसा नहीं कहा । किन्तु नैरात्म्यवाद के कारण मनुष्यों के विनाश को जानकर लोगों पर करुणा बुद्धि से मैंने कहा है।
राजा हिमशोतल की सभा में मैंने विदग्धात्मा बौद्धों को जीत कर पादसे घड़े का विस्फोटन किया है।
यह वह समय था, जब बौद्धविद्वान धर्मकीति के शिष्यों का समुदाय भारतीय दर्शन के रंग मंच पर छाया हुया था। उसके नैरात्म्य वाद के नारों से प्रात्मदर्शन हिल उठा था। उस समय से अफलंकदेव ने भारतीय दर्शन की हिलती हुई दीवालों को थामा और इसी प्रयत्न में अकलाइयाय का जन्म हुमा।
अकलकूदेव के टीका ग्रन्थ और उनकी मौलिक कृतियां उनके गहनतत्त्व विचार, उनकी सूक्ष्म तर्क प्रवणता और स्वतत्त्व निष्ठा का पग पग पर दर्शन कराती है। कृतियां गढ़ और गंभीर प्रथं की घोतक हैं। प्रकलंकने धर्म कीति की परिहास और अश्लील कक्तियों का उत्तर भी बड़े मजे से दिया है।
अकलंक देव बाल ब्रह्मचारी और निम्रन्थ तपस्वी थे। उनके मन में अपने प्यारे भाई के बलिदान की आग बराबर जल रही थी। इससे भी अधिक उनके मानस में बौद्धों के क्रान्तिकारी सिद्धान्तों के प्रचार से और प्रात्मवाद के लुप्त हो जाने से उथल-पुथल मची हुई थी। शिलालेख में उन्हें महधिक लिखा है। इस तरह उनका व्यक्तित्व महान और चरित्र सम्पन्न था। उनकी अकलंक प्रभा से जैन शासन पालोकित हना है, और होता रहेगा। तत्वार्थ राज वार्तिक के 'लघुहव्यनृपतिवरतनयः पद्य के 'बरतनयः' से अकलंक के लधु भ्राता होने की सूचना मिलती है। अकांक देव का समय
अफलंक देव यतिवृषभ, श्रीदत्त, सिद्धसेन, देवुनन्दी, पात्र केसरी और सुमति देव के बाद हुए हैं। उन्होंने यतिवृषभ की तिलोयपण्णत्ति के प्रथम अधिकार को दो गाथानों का संस्कृतिकरण कर उन्हें लघीयस्त्रय में शामिल कर लिया है। यतिवृषभ का समय ईसा को ५वी सदी है। श्रीदत का उल्लेख देवनन्दी ने किया है । अकलंक देव ने प्रवचन प्रवेश के पष्ठ २३ में सिद्धसेन के 'सन्मतिसूत्र की निम्नगाथा का संस्कृत रूपान्तर किया है:
तित्थयर बयणसंगहविसेसपस्थारमूलवागरणी।।
बग्वाट्रिनो य पज्जवणम्रो य सेसा बियप्पासि ॥१-३ "ततः तीर्थकर वचन संग्रह विशेष प्रस्तार मूलध्याकारिणौद्रव्यपर्यायाथिको निश्चेतव्यो ।"
लघीयस्त्रयस्वो० वृ० श्लोक ६७ आपने देवनन्दी की तत्त्वार्थवति । सर्वार्थ सिद्धि) की पंक्तियों को दातिक बनाकर तत्वार्थवातिक की रचना की है। देवनन्दी का समय ईसा की ५वीं शताब्दी है। अकलंक ने पात्र केसरी के 'विलक्षणकदर्थन' को 'अन्य थानुपपन्नत्व" कारिका को न्यायविनिश्चय के मूल में शामिल कर लिया है। इनका समय ईसा की सातवीं शताब्दी है।
सुमति देव का उल्लेख शान्ति रक्षित के तत्त्वसंग्रह की पंजिका में पाया जाता है। पंजिका के कर्ता कमलशील हैं, जो नालन्दा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। शान्तिरक्षित का समय सन् ७०५ से ७६२ माना जाता है। सन् ७४३ में शान्ति रक्षित ने तिब्बत की यात्रा की थी। उससे पहले ही उन्होंने तत्त्व संग्रह की रचना की है। कमलशील शान्तिरक्षित के समकालीन जान पड़ते हैं। इन उल्लेखों से 'अकलंक का समय ईसा की ७वीं शताब्दी से बाद का जान पड़ता है।
- - - -- - - - - १ जीयात् समन्तभद्रस्य देवागमनः संजिनः । स्तोत्रस्य भाज्यं कृतवानकलको महधिकः जन लेख संग्रह भा० ३ ले नं० ६६७ १०५१५