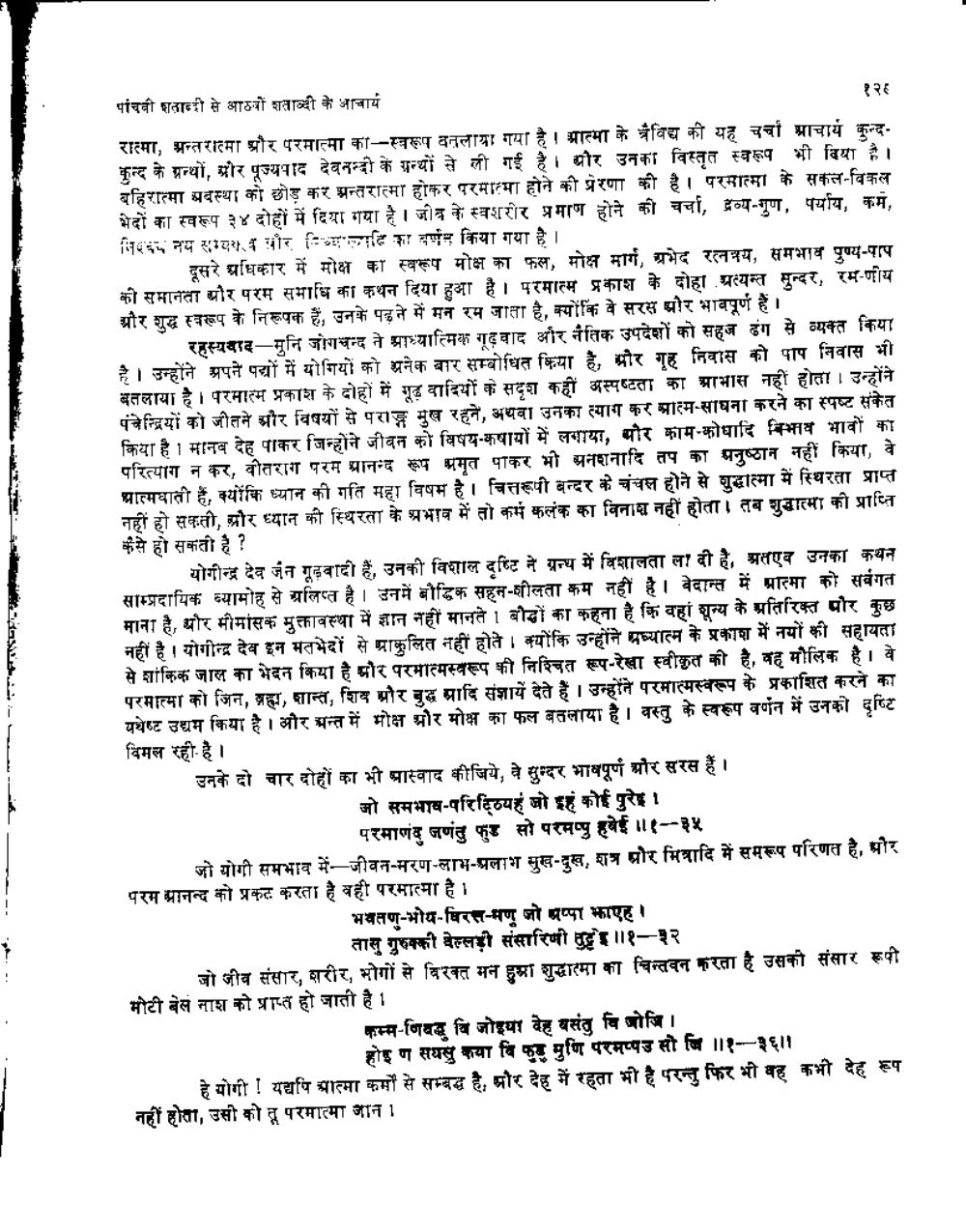________________
पांचवी शताब्दी से आठवीं शताब्दी के आचार्य
१२६
रात्मा अन्तरात्मा और परमात्मा का स्वरूप वतलाया गया है। आत्मा के त्रैविद्य की यह चर्चा आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थों, और पूज्यपाद देवनन्दी के ग्रन्थों से ली गई है। और उनका विस्तृत स्वरूप भी दिया है। बहिरात्मा अवस्था को छोड़ कर अन्तरात्मा होकर परमात्मा होने की प्रेरणा की है। परमात्मा के सकल विकल भेदों का स्वरूप ३४ दोहों में दिया गया है। जीव के स्वशरीर प्रमाण होने की चर्चा, द्रव्य-गुण, पर्याय, कर्म, विनय सम्ययवराव किया गया है।
दूसरे अधिकार में मोक्ष का स्वरूप मोक्ष का फल, मोक्ष मार्ग, ग्रभेद रत्नत्रय, समभाव पुण्य-पाप की समानता और परम समाधि का कथन दिया हुआ है। परमात्म प्रकाश के दोहा प्रत्यन्त सुन्दर, रमणीय और शुद्ध स्वरूप के निरूपक हैं, उनके पढ़ने में मन रम जाता है, क्योंकि वे सरस और भावपूर्ण हैं ।
रहस्यवाद – मुनि जोगचन्द ने प्राध्यात्मिक गूढ़वाद और नैतिक उपदेशों को सहज ढंग से व्यक्त किया है । उन्होंने अपने पद्मों में योगियों को अनेक बार सम्बोधित किया है, और गृह निवास को पाप निवास भी बतलाया है। परमात्म प्रकाश के दोहों में गूढ़ वादियों के सदृश कहीं अस्पष्टता का आभास नहीं होता। उन्होंने पंचेन्द्रियों को जीतने और विषयों से पराङ्ग मुख रहने, अथवा उनका त्याग कर श्रात्म-साधना करने का स्पष्ट संकेत किया है। मानव देह पाकर जिन्होंने जीवन को विषय कषायों में लगाया, और काम कोधादि विभाव भावों का परित्याग न कर, वीतराग परम प्रानन्द रूप अमृत पाकर भी अनशनादि तप का अनुष्ठान नहीं किया, वे श्रात्मघाती हैं, क्योंकि ध्यान की गति महा विषम है । चित्तरूपी बन्दर के चंचल होने से शुद्धात्मा में स्थिरता प्राप्त नहीं हो सकती, और ध्यान की स्थिरता के प्रभाव में तो कर्म कलंक का विनाश नहीं होता। तब शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है ?
योगोन्द्र देव जैन गूढ़वादी हैं, उनकी विशाल दृष्टि ने ग्रन्थ में विशालता ला दी हैं, अतएव उनका कथन साम्प्रदायिक व्यामोह से ग्रलिप्त है। उनमें बौद्धिक सहन-शीलता कम नहीं है। वेदान्त में श्रात्मा को सर्वगत माना है, और मीमांसक मुक्तावस्था में ज्ञान नहीं मानते । बौद्धों का कहना है कि वहां शून्य के अतिरिक्त मौर कुछ नहीं है । योगीन्द्र देव इन मतभेदों से प्राकुलित नहीं होते। क्योंकि उन्होंने अध्यात्म के प्रकाश में नयों की सहायता से शांकिक जाल का भेदन किया है और परमात्मस्वरूप की निश्चित रूप-रेखा स्वीकृत की है, वह मौलिक है। वे परमात्मा को जिन, ब्रह्म, शान्त, शिव और बुद्ध प्रादि संज्ञायें देते हैं । उन्होंने परमात्मस्वरूप के प्रकाशित करने का यथेष्ट उद्यम किया है। और अन्त में मोक्ष और मोक्ष का फल बतलाया है। वस्तु के स्वरूप वर्णन में उनकी दृष्टि मिल रही है।
उनके दो चार दोहों का भी प्रास्वाद कीजिये, वे सुन्दर भावपूर्ण और सरस हैं। जो समभाव-परिट्ठियहं जो इहं कोई पुरेद्र
परमानंद जणंतु फुड सो परमप्पु हवेई ॥१-३५
जो योगी समभाव में - जीवन-मरण - लाभ - प्रलाभ सुख-दुख, शत्र और मित्रादि में समरूप परिणत है, और परम आनन्द को प्रकट करता है वही परमात्मा है ।
भवतणु-भय- विरस - मणु जो अप्पा झाएह । तासु गुरुक्की बेल्लड़ी संसारिणी तुट्टई ॥१-३२
जो जीव संसार, शरीर, भोगों से विरक्त मन हुआ शुद्धात्मा का चिन्तवन करता है उसकी संसार रूपी मोटी बेल नाश को प्राप्त हो जाती है ।
कम्म- वि वि जोइया देह वसंतु वि जोजि ।
होइ ण सय कया वि कुष्ठु मुणि परमप्पड सौ जि ॥१-३६॥
हे योगी ! यद्यपि आत्मा कर्मों से सम्बद्ध है, और देह में रहता भी है परन्तु फिर भी वह कभी देह रूप नहीं होता, उसी को तू परमात्मा जान