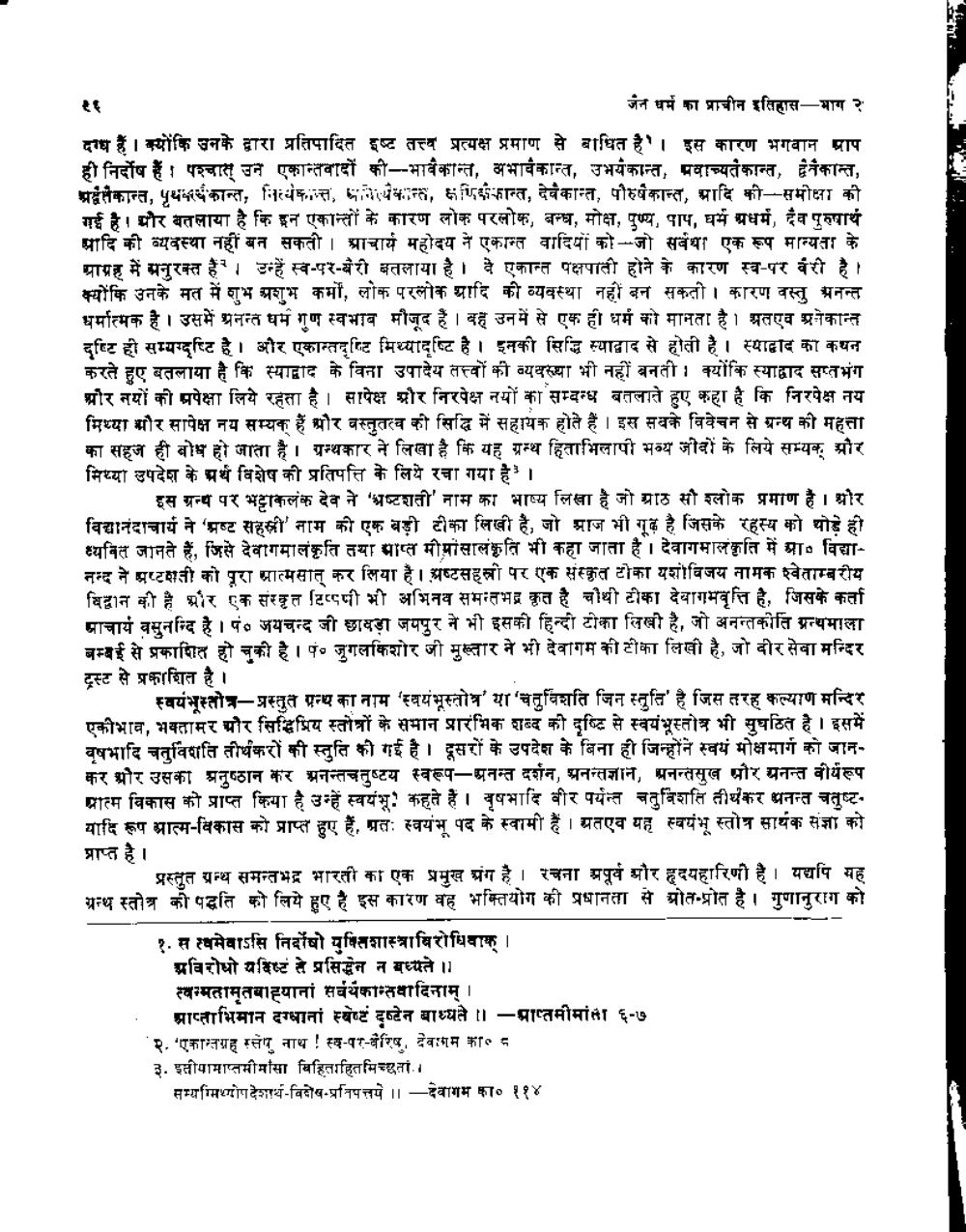________________
१
जैन धर्म का प्राचीन इतिहास-भाग २ दग्ध हैं। क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित इष्ट तत्त्व प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। इस कारण भगवान प्राप ही निर्दोष हैं। पश्चात् उन एकान्तवादों की--भावकान्त, अभावंकान्त, उभयकान्त, प्रवाच्यतकान्त, द्वेतकान्त, प्रवतकान्त, पृथकान्त, नित्यकान्त, भविस्यकान्त, क्षणिकान्त, देवैकान्त, पौरुषकान्त, मादि की-समीक्षा की गई है। मौर बतलाया है कि इन एकान्तों के कारण लोक परलोक, बन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप, धर्म अधर्म, देव पुरुषार्थ पादि की व्यवस्था नहीं बन सकती। प्राचार्य महोदय ने एकान्त वादियों को-जो सर्वथा एक रूप मान्यता के प्राग्रह में अनुरक्त हैं। उन्हें स्व-पर-बैरी बतलाया है। वे एकान्त पक्षपाती होने के कारण स्व-पर वरी है। क्योंकि उनके मत में शुभ अशुभ कर्मों, लोक परलोक आदि की व्यवस्था नहीं बन सकती। कारण वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। उसमें अनन्त धर्म गुण स्वभाब मौजूद हैं । वह उन में से एक ही धर्म को मानता है। अतएव अनेकान्त दृष्टि ही सम्यग्दृष्टि है। और एकान्तदृष्टि मिथ्यादृष्टि है। इनकी सिद्धि स्याद्वाद से होती है। स्थाद्वाद का कथन करते हुए बतलाया है कि स्याद्वाद के विना उपादेय तत्त्वों की व्यवस्था भी नहीं बनती। क्योंकि स्याद्वाद सप्तभंग और नयों की अपेक्षा लिये रहता है। सापेक्ष और निरपेक्ष नयों का सम्बन्ध बतलाते हुए कहा है कि निरपेक्ष नय मिथ्या और सापेक्ष नय सम्यक हैं और वस्तुतत्व की सिद्धि में सहायक होते हैं । इस सबके विवेचन से ग्रन्थ की महत्ता का सहज ही बोध हो जाता है। ग्रन्थकार ने लिखा है कि यह ग्रन्थ हिताभिलापी भव्य जीवों के लिये सम्यक् और मिथ्या उपदेश के अर्थ विशेष की प्रतिपत्ति के लिये रचा गया है।
इस ग्रन्थ पर भट्टाकलंक देव ने 'अष्टशती' नाम का भाष्य लिखा है जो पाठ सौ श्लोक प्रमाण है । और विद्यानंदाचार्य ने 'प्रष्ट सहस्री' नाम की एक बड़ी टीका लिखी है, जो आज भी गढ़ है जिसके रहस्य को थोड़े ही ध्यक्ति जानते हैं, जिसे देवागमालकृति तथा प्राप्त मीमांसालंकृति भी कहा जाता है। देवागमाल कृति में प्रा. विद्यानन्द ने प्रष्टक्षती को पूरा प्रात्मसात् कर लिया है। अष्टसहस्री पर एक संस्कृत टीका यशोविजय नामक श्वेताम्बरीय विद्वान की है और एक संस्कृत टिप्पणी भी अभिनव समन्तभद्र कृत है चौथी टीका देवागमवृत्ति है, जिसके कर्ता प्राचार्य वसुनन्दि है। पं० जयचन्द जी छाबड़ा जयपुर ने भी इसकी हिन्दी टीका लिखी है, जो अनन्तकोति ग्रन्थमाला बम्बई से प्रकाशित हो चुकी है। पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार ने भी देवागम की टीका लिखी है, जो दीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट से प्रकाशित है।
स्वयंभूस्तोत्र-प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम 'स्वयंभूस्तोत्र' या 'चतुर्विशति जिन स्तुति' है जिस तरह कल्याण मन्दिर एकीभाव, भक्तामर और सिद्धिप्रिय स्तोत्रों के समान प्रारंभिक शब्द की दृष्टि से स्वयंभूस्तोत्र भी सुघठित है। इसमें वृषभादि चविशति तीर्थकरों की स्तुति की गई है। दूसरों के उपदेश के बिना ही जिन्होंने स्वयं मोक्षमार्ग को जानकर और उसका अनुष्ठान कर अनन्तचतुष्टय स्वरूप-अनन्त दर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्त वीर्यरूप मात्म विकास को प्राप्त किया है उन्हें स्वयंभू: कहते हैं। वृषभादि वीर पर्यन्त चतुविशति तीर्थकर अनन्त चतुष्ट. यादि रूप आत्म-विकास को प्राप्त हुए हैं, प्रतः स्वयंभू पद के स्वामी हैं। प्रतएव यह स्वयंभू स्तोत्र सार्थक संज्ञा को प्राप्त है।
प्रस्तुत ग्रन्थ समन्तभद्र भारती का एक प्रमुख अंग है। रचना अपूर्व और हृदयहारिणी है। यद्यपि यह ग्रन्थ स्तोत्र की पद्धति को लिये हुए है इस कारण वह भक्तियोग की प्रधानता से ओत-प्रोत है। गुणानुराग को
१. स त्वमेवाऽसि निर्दोषो युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् ।
अविरोधो यविष्ट ते प्रसिद्धेन न बध्यते ॥ स्वम्मतामतबाह्यानां सर्वथकान्तवादिनाम् । प्राप्ताभिमान दग्धानां स्वष्टं दृष्टेन बाध्यते ॥ -प्राप्तमीमांसा ६-७ २. 'एकालग्रह स्तेषु नाथ ! स्व-पर-वैरिषु, देवागम का०८ ३. इतीयामाप्तमीमांसा विहिताहितमिच्छता । सम्यग्मियोपदेशार्थ-विदोष-प्रतिपत्तये ।। –देवागम का० ११४