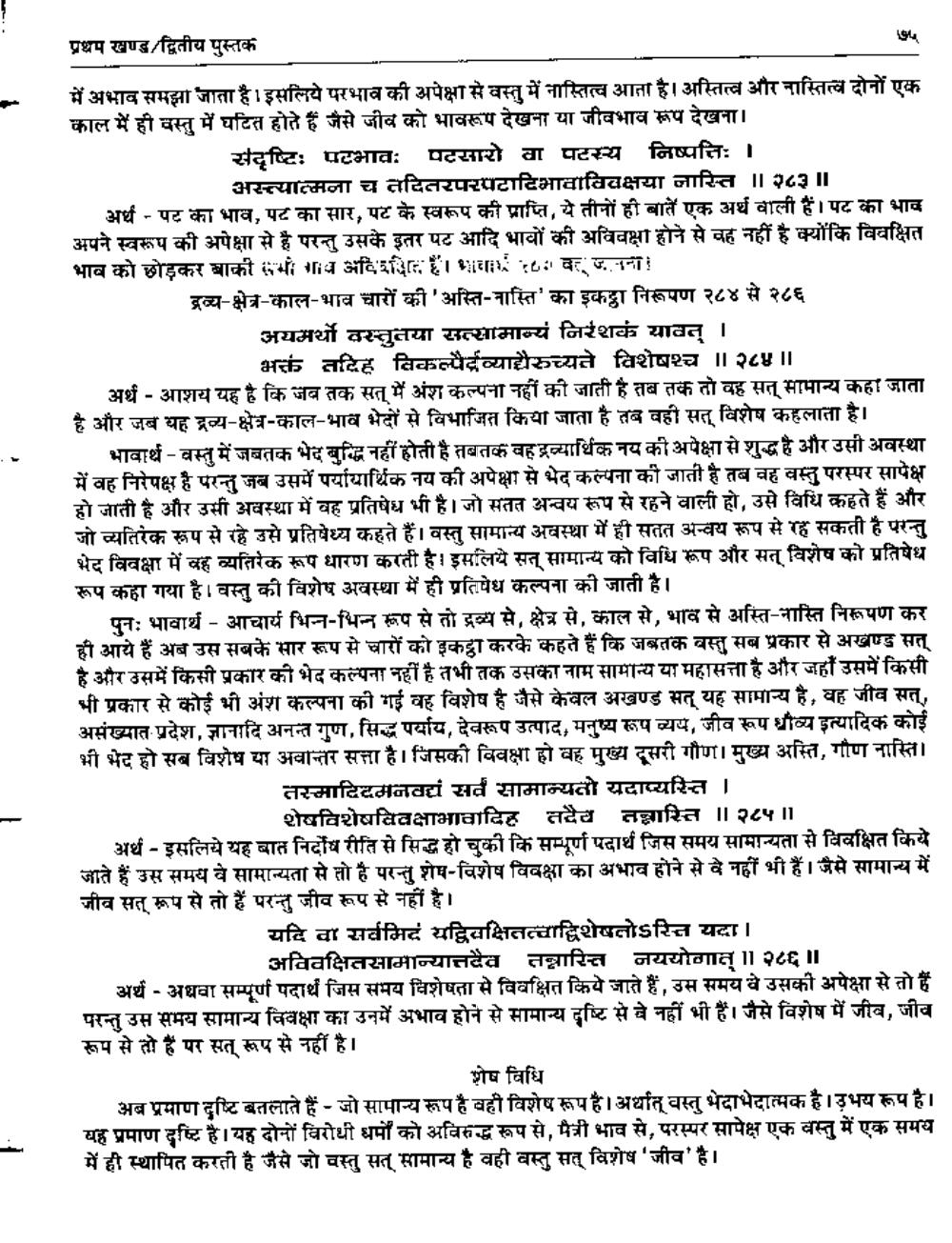________________
प्रथम खण्ड/द्वितीय पुस्तक
में अभाव समझा जाता है। इसलिये परभाव की अपेक्षा से वस्तु में नास्तित्व आता है। अस्तित्व और नास्तित्व दोनों एक काल में ही वस्तु में घटित होते हैं जैसे जीव को भावरूप देखना या जीवभाव रूप देखना।
संदृष्टिः पटभातः पटसारो वा पटस्य निष्पत्तिः ।
अस्त्यात्मना च तदितरपरपटाटिभावाविवक्षया नास्ति ॥२८३॥ अर्थ - पद का भाव, पट का सार, पट के स्वरूप की प्राप्ति, ये तीनों ही बातें एक अर्थ वाली हैं। पद का भाव अपने स्वरूप की अपेक्षा से है परन्तु उसके इतर पट आदि भावों की अविवक्षा होने से वह नहीं है क्योंकि विवक्षित भाव को छोड़कर बाकी रूमी गाव अविवक्षित है। भावावर ज. ना!
द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव चारों की 'अस्ति-नास्ति' का इकट्ठा निरूपण २८४ से २८६
अयमर्थो वस्तुतया सत्सामान्य निरंशकं यावत् ।
भक्त तदिह विकल्पैदव्याद्यैरुच्यते विशेषश्च ॥ २८४ ॥ अर्थ- आशय यह है कि जब तक सत् में अंश कल्पना नहीं की जाती है तब तक तो वह सत् सामान्य कहा जाता है और जब यह द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव भेदों से विभाजित किया जाता है तब वही सत् विशेष कहलाता है।
भावार्थ - वस्त में जबतक भेद बद्धि नहीं होती है तबतक वह द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षासेशन और उसी अवस्था में वह निरेपक्ष है परन्तु जब उसमें पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भेद कल्पना की जाती है तब वह वस्तु परस्पर सापेक्ष हो जाती है और उसी अवस्था में वह प्रतिषेध भी है। जो सतत अन्वय रूप से रहने वाली हो, उसे विधि कहते हैं और जो व्यतिरेक रूप से रहे उसे प्रतिषेध्य कहते हैं। वस्तु सामान्य अवस्था में ही सतत अन्वय रूप से रह सकती है परन्तु भेद विवक्षा में वह व्यतिरेक रूप धारण करती है। इसलिये सत् सामान्य को विधि रूप और सत् विशेष को प्रतिषेध रूप कहा गया है। वस्तु की विशेष अवस्था में ही प्रतिषेध कल्पना की जाती है।
पुनः भावार्थ - आचार्य भिन्न-भिन्न रूप से तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से अस्ति-नास्ति निरूपण कर ही आये हैं अब उस सबके सार रूप से चारों को इकट्ठा करके कहते हैं कि जबतक वस्तु सब प्रकार से अखण्ड सत् है और उसमें किसी प्रकार की भेद कल्पना नहीं है तभी तक उसका नाम सामान्य या महासत्ता है और जहाँ उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी अंश कल्पना की गई वह विशेष है जैसे केवल अखण्ड सत् यह सामान्य है, वह जीव सत्, असंख्यात-प्रदेश, ज्ञानादि अनन्त गुण,सिद्ध पर्याय, देवरूप उत्पाद, मनुष्य रूपव्यय, जीव रूप धौव्य इत्यादिक कोई भी भेद हो सब विशेष या अवान्तर सत्ता है। जिसकी विवक्षा हो वह मुख्य दूसरी गौण। मुख्य अस्ति, गौण नास्ति।
तस्मादिटमनवां सर्व सामान्यतो यदाप्यस्ति ।
शेषविशेषविवक्षाभावादिह तदैव तनास्ति ।। २८५॥ अर्थ- इसलिये यह बात निर्दोष रीति से सिद्ध हो चुकी कि सम्पूर्ण पदार्थ जिस समय सामान्यता से विवक्षित किये जाते हैं उस समय वे सामान्यता से तो है परन्तु शेष-विशेष विवक्षा का अभाव होने से वे नहीं भी हैं। जैसे सामान्य में जीव सत रूप से तो हैं परन्त जीव रूप से नहीं है।
यदि वा सर्वमिदं यद्विवक्षितत्वाद्विशेषतोऽरित यदा ।
अविवक्षितसामान्यात्तदैव तन्नास्ति नययोगात् ॥ २८६ ॥ अर्थ - अधवा सम्पूर्ण पदार्थ जिस समय विशेषता से विवक्षित किये जाते हैं, उस समय वे उसकी अपेक्षा से तो हैं परन्तु उस समय सामान्य विवक्षा का उनमें अभाव होने से सामान्य दृष्टि से वे नहीं भी हैं। जैसे विशेष में जीव, जीव रूप से तो है पर सत् रूप से नहीं है।
शेष विधि अब प्रमाण दृष्टि बतलाते हैं - जो सामान्य रूप है वही विशेष रूप है। अर्थात् वस्तु भेदाभेदात्मक है। उभय रूप है। यह प्रमाण दृष्टि है। यह दोनों विरोधी धर्मों को अविरुद्ध रूप से, मैत्री भाव से, परस्पर सापेक्ष एक वस्तु में एक समय में ही स्थापित करती है जैसे जो वस्तु सत् सामान्य है वही वस्तु सत् विशेष 'जीव' है।