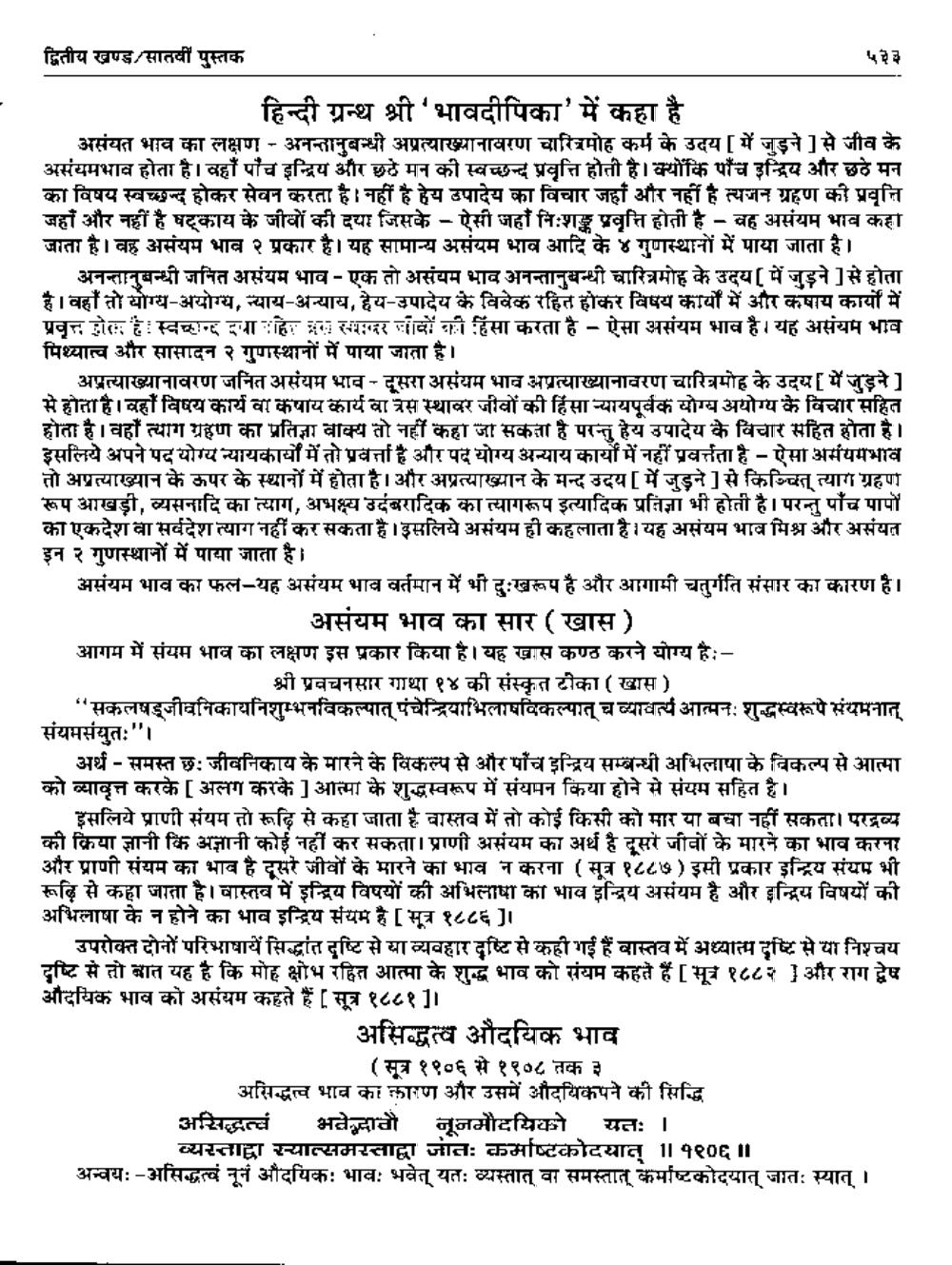________________
द्वितीय खण्ड/सातवीं पुस्तक
५३३
हिन्दी ग्रन्थ श्री 'भावदीपिका' में कहा है असंयत भाव का लक्षण - अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यानावरण चारित्रमोह कर्म के उदय [ में जडने 1से जीव के असंयमभाव होता है। वहाँ पाँच इन्द्रिय और छठे मन की स्वच्छन्द प्रवृत्ति होती है। क्योंकि पाँच इन्द्रिय और छठे मन का विषय स्वच्छन्द होकर सेवन करता है। नहीं है हेय उपादेय का विचार जहाँ और नहीं है त्यजन ग्रहण की प्रवृत्ति जहाँ और नहीं है घट्काय के जीवों की दया जिसके-ऐसी जहाँ निःशङ्क प्रवृत्ति होती है - वह असंयम भाव कहा जाता है। वह असंयम भाव २ प्रकार है। यह सामान्य असंयम भाव आदि के ४ गुणस्थानों में पाया जाता है।
अनन्तानुबन्धी जनित असंयम भाव - एक तो असंयम भाव अनन्तानुबन्धी चारित्रमोह के उदय[ में जुड़ने] से होता है। वहाँ तो योग्य-अयोग्य, न्याय-अन्याय, हेय-उपादेय के विवेक रहित होकर विषय कार्यों में और कषाय कार्यों में प्रवृत्त होता है। स्वच्छान्द दया माहेक सान्दर जादों की हिंसा करता है - ऐसा असंयम भाव है। यह असंयम भाव मिथ्यात्व और सासादन २ गुणस्थानों में पाया जाता है।
अप्रत्याख्यानावरण जनित असंयम भाव- दूसरा असंयम भाव अप्रत्याख्यानावरण चारित्रमोह के उदय [ में जुड़ने] से होता है। वहाँ विषय कार्य वा कषाय कार्य वा त्रस स्थावर जीवों की हिंसान्यायपूर्वक योग्य अयोग्य के विचार सहित होता है। वहाँ त्याग ग्रहण का प्रतिज्ञा वाक्य तो नहीं कहा जा सकता है परन्तु हेय उपादेय के विचार सहित होता है। इसलिये अपने पद योग्य न्यायकार्यों में तो प्रवर्ता है और पद योग्य अन्याय कार्यों में नहीं प्रवर्त्तता है - ऐसा अमंयमभाव तो अप्रत्याख्यान के ऊपर के स्थानों में होता है। और अप्रत्याख्यान के मन्द उदय [ में जुड़ने] से किञ्चित् त्याग ग्रहण रूप आखड़ी, व्यसनादिका त्याग, अभक्ष्य उदंबरादिक का त्यागरूप इत्यादिक प्रतिज्ञा भी होती है। परन्तु पाँच पापों का एकदेश वा सर्वदेश त्याग नहीं कर सकता है। इसलिये असंयम ही कहलाता है। यह असंयम भाव मिश्र और असंयत इन २ गुणस्थानों में पाया जाता है। असंयम भाव का फल-यह असंयम भाव वर्तमान में भी दुःखरूप है और आगामी चतुर्गति संसार का कारण है।
असंयम भाव का सार (खास) आगम में संयम भाव का लक्षण इस प्रकार किया है। यह खास कण्ठ करने योग्य है:
श्री प्रवचनसार गाथा १४ की संस्कत टीका(खास) "सकलषड्जीवनिकायनिशुम्भनविकल्पात् पंचेन्द्रियाभिलाषदिकल्पात् च व्यावत्यं आत्मनः शुद्धस्वरूपे संयमनात् संयमसंयुतः"। ___ अर्थ - समस्त छ: जीवनिकाय के मारने के विकल्प से और पाँच इन्द्रिय सम्बन्धी अभिलाषा के विकल्प से आत्मा को व्यावृत्त करके [ अलग करके ] आत्मा के शुद्धस्वरूप में संयमन किया होने मे संयम सहित है।
इसलिये प्राणी संयम तो रूढ़ि से कहा जाता है वास्तव में तो कोई किसी को मार या बचा नहीं सकता। परद्रव्य की क्रिया ज्ञानी कि अज्ञानी कोई नहीं कर सकता। प्राणी असंयम का अर्थ है दूसरे जीवों के मारने का भाव करना और प्राणी संयम का भाव है दूसरे जीवों के मारने का भाव न करना (सूत्र १८८७) इसी प्रकार इन्द्रिय संयम भी रूढ़ि से कहा जाता है। वास्तव में इन्द्रिय विषयों की अभिलाषा का भाव इन्द्रिय असंयम है और इन्द्रिय विषयों की अभिलाषा के न होने का भाव इन्द्रिय संयम है [सूत्र १८८६]।
उपरोक्त दोनों परिभाषायें सिद्धांत दृष्टि से या व्यवहार दृष्टि से कही गई हैं वास्तव में अध्यात्म दृष्टि से या निश्चय दृष्टि से तो बात यह है कि मोह क्षोभ रहित आत्मा के शुद्ध भाव को संयम कहते हैं [ सूत्र १८८२ ] और राग द्वेष औदयिक भाव को असंयम कहते हैं [ सूत्र १८८१]।
असिद्धत्व औदयिक भाव
(सूत्र १९०६ से १९०८ तक ३ असिद्धत्व भाव का कारण और उसमें औदयिकपने की सिद्धि असिद्धत्वं भवेदाती नूनमौदयिको यतः ।
व्यस्ताद्वा स्यात्समरताद्वा जातः कष्टिकोदयात् ॥ १९०६ ॥ अन्वयः -असिद्धत्वं नून औदयिक: भावः भवेत् यत: व्यस्तात् वा समस्तात् कर्माष्टकोदयात् जातः स्यात् ।