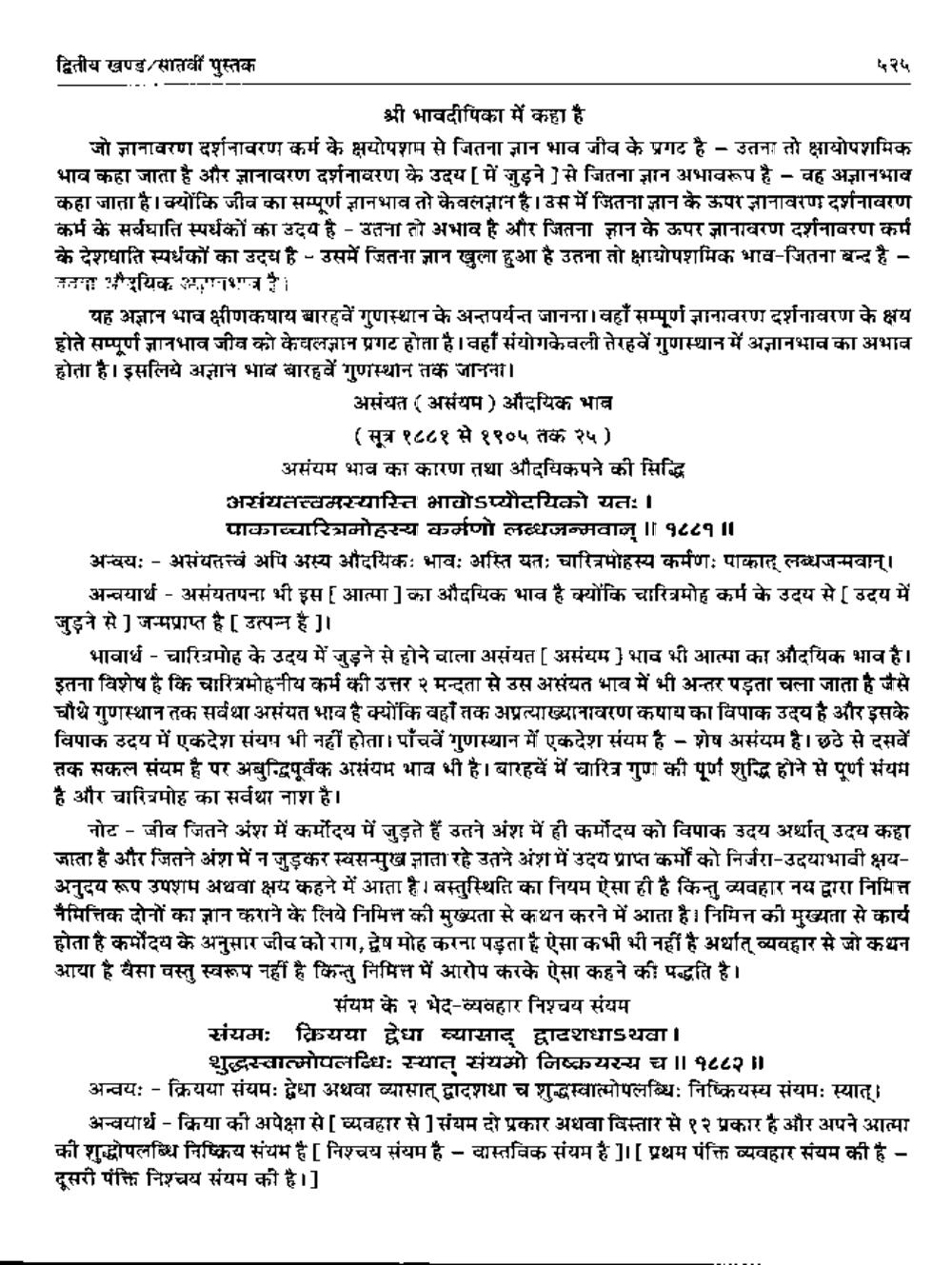________________
द्वितीय खण्ड/सातवीं पुस्तक
श्री भावदीपिका में कहा है जो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से जितना ज्ञान भाव जीव के प्रगट है - उतना तो क्षायोपशामिक भाव कहा जाता है और ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय [में जुड़ने] से जितना ज्ञान अभावरूप है - वह अज्ञानभाव कहा जाता है। क्योंकि जीव का सम्पूर्ण ज्ञानभाव तो केवलज्ञान है। उस में जितना ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के सर्वघाति स्पर्धकों का उदय है - उतना तो अभाव है और जितना ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के देशधाति स्पर्धकों का उदय है- उसमें जितना ज्ञान खुला हुआ है उतना तोक्षायोपशामिक भाव-जितना बन्द हैजनता दयिक अपनपत्र है।
यह अज्ञान भाव क्षीणकषाय बारहवें गुणस्थान के अन्तपर्यन्त जानना। वहाँ सम्पूर्ण ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षय होते सम्पूर्ण ज्ञानभाव जीव को केवलज्ञान प्रगट होता है। वहाँ संयोगकेचली तेरहवें गुणस्थान में अज्ञानभाव का अभाव होता है। इसलिये अज्ञान भाव बारहवें गणस्थान तक जानना।
असंयत (असंयम) औदयिक भाव
(सूत्र १८८१ से १९०५ तक २५) असंयम भाव का कारण तथा औदयिकपने की सिद्धि असंयतत्वमस्यास्ति भावोऽप्यौदायिको यतः ।
पाकाच्चारित्रमोहस्य कर्मणो लब्धजन्मवान ।। १८८१ ॥ अन्वयः - असंयतत्त्वं अपि अस्य औदयिकः भावः अस्ति यतः चारित्रमोहस्य कर्मणः पाका लब्धजन्मवान्।
अन्वयार्थ - असंयतपना भी इस [ आत्मा ] का औदयिक भाव है क्योंकि चारित्रमोह कर्म के उदय से [ उदय में जुड़ने से ] जन्मप्राप्त है [ उत्पन्न है ।
भावार्थ - चारित्रमोह के उदय में जुड़ने से होने वाला असंयत [ असंयम ] भाव भी आत्मा का औदयिक भाव है। इतना विशेष है कि चारित्रमोहनीय कर्म की उत्तर २ मन्दता से उस असंयत भाव में भी अन्तर पड़ता चला जाता है जैसे चौथे गुणस्थान तक सर्वथा असंयत भाव है क्योंकि वहाँ तक अप्रत्याख्यानावरण कषाय का विपाक उदय है और इसके विपाक उदय में एकदेश संया भी नहीं होता। पाँचवें गुणस्थान में एकदेश संयम है - शेष असंयम है। छठे से दसवें तक सकल संयम है पर अबुद्धिपूर्वक असंयम भाव भी है। बारहवें में चारित्र गुण की पूर्ण शुद्धि होने से पूर्ण संयम है और चारित्रमोह का सर्वथा नाश है।
नोट - जीव जितने अंश में कर्मोदय में जुड़ते हैं उतने अंश में ही कर्मोदय को विपाक उदय अर्थात् उदय कहा जाता है और जितने अंश में न जड़कर स्वसन्मुख जाता रहे उतने अंश में उदय प्राप्त कर्मों को निर्जरा-उदयाभावी क्षयअनुदय रूप उपशम अथवा क्षय कहने में आता है। वस्तुस्थिति का नियम ऐसा ही है किन्तु व्यवहार नय द्वारा निमित्त नैमित्तिक दोनों का ज्ञान कराने के लिये निमित्त की मुख्यता से कथन करने में आता है। निमिन की मुख्यता से कार्य होता है कर्मोदय के अनुसार जीव को राग, द्वेष मोह करना पड़ता है ऐसा कभी भी नहीं है अर्थात् व्यवहार से जो कथन आया है वैसा वस्तु स्वरूप नहीं है किन्तु निमित्त में आरोप करके ऐसा कहने की पद्धति है।
संयम के २ भेद-व्यवहार निश्चय संयम संयमः क्रियया द्वेधा व्यासाद् द्वाटशधाऽथवा।
शुद्धस्तात्मोपलब्धि: स्यात् संयमो निष्क्रयस्य च ।। १८८२॥ अन्वयः - क्रियया संयमः द्वेधा अथवा व्यासात् द्वादशधा च शुद्धस्वात्मोपलब्धिः निष्क्रियस्य संयम: स्यात्।
अन्वयार्थ - क्रिया की अपेक्षा से [ व्यवहार से ] संयम दो प्रकार अथवा विस्तार से १२ प्रकार है और अपने आत्मा की शद्धोपलब्धि निष्क्रिय संयम है। निश्चय संयम है- वास्तविक संयम है ][प्रथम पंक्ति व्यवहार संयम की हैदूसरी पंक्ति निश्चय संयम की है।]