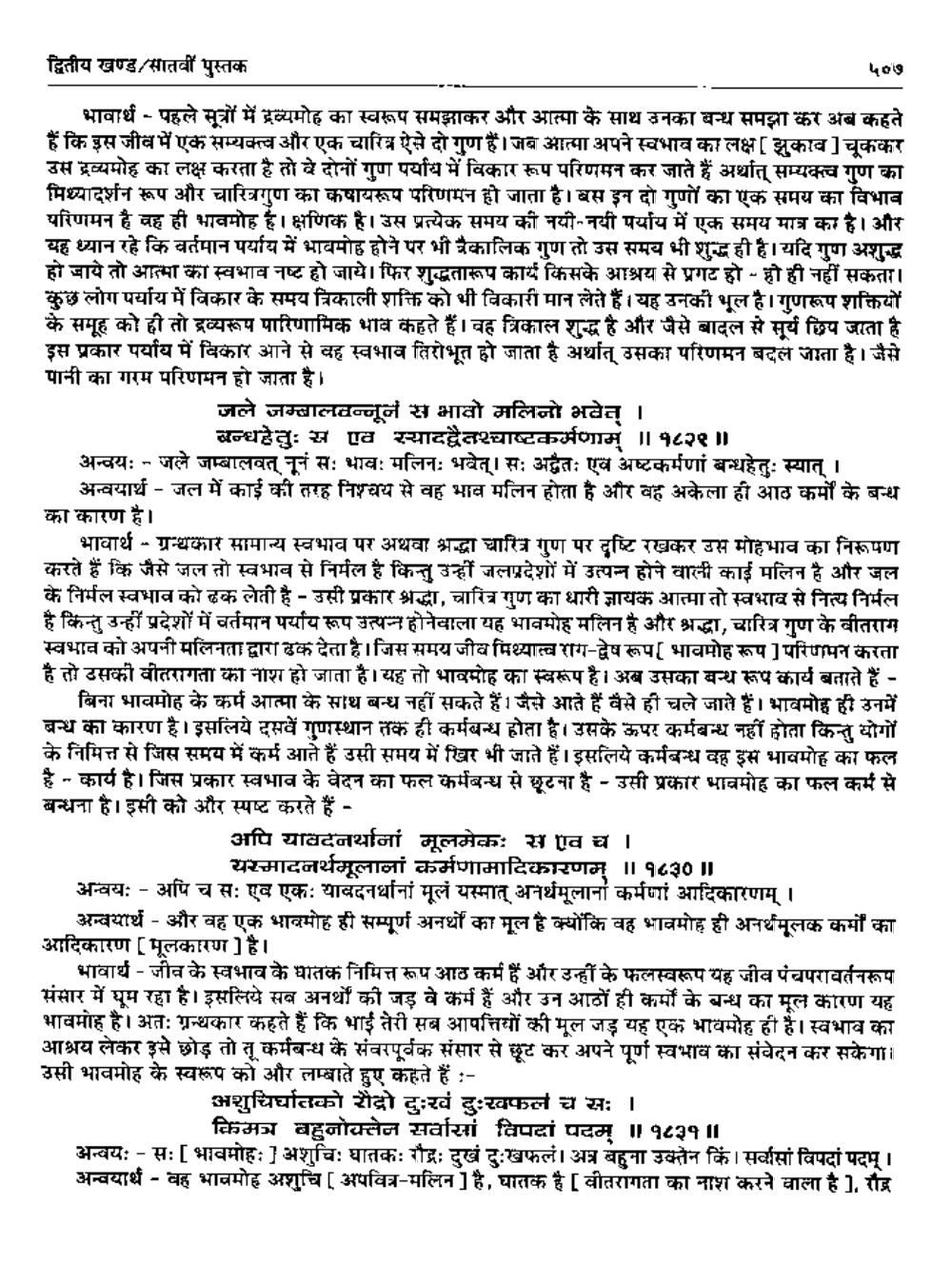________________
द्वितीय खण्ड / सातवीं पुस्तक
भावार्थ- पहले सूत्रों में द्रव्यमोह का स्वरूप समझाकर और आत्मा के साथ उनका बन्ध समझा कर अब कहते हैं कि इस जीव में एक सम्यक्त्व और एक चारित्र ऐसे दो गुण हैं। जब आत्मा अपने स्वभाव का लक्ष [ झुकाव ] चूककर उस द्रव्यमोह का लक्ष करता है तो वे दोनों गुण पर्याय में विकार रूप परिणमन कर जाते हैं अर्थात् सम्यक्त्व गुण का मिथ्यादर्शन रूप और चारित्रगुण का कषायरूप परिणमन हो जाता है। बस इन दो गुणों का एक समय का विभाव परिणमन है वह ही भावमोह है। क्षणिक है। उस प्रत्येक समय की नयी-नयी पर्याय में एक समय मात्र का है। और यह ध्यान रहे कि वर्तमान पर्याय में भावमोह होने पर भी त्रैकालिक गुण तो उस समय भी शुद्ध ही है। यदि गुण अशुद्ध हो जाये तो आत्मा का स्वभाव नष्ट हो जाये। फिर शुद्धतारूप कार्य किसके आश्रय से प्रगट हो हो ही नहीं सकता। कुछ लोग पर्याय में विकार के समय त्रिकाली शक्ति को भी विकारी मान लेते हैं। यह उनकी भूल है। गुणरूप शक्तियों के समूह को ही तो द्रव्यरूप पारिणामिक भाव कहते हैं। वह त्रिकाल शुद्ध है और जैसे बादल से सूर्य छिप जाता है इस प्रकार पर्याय में विकार आने से वह स्वभाव तिरोभूत हो जाता है अर्थात् उसका परिणमन बदल जाता है। जैसे पानी का गरम परिणमन हो जाता है।
M
५०७
जले जम्बालवन्नूनं स भावो मलिनो भवेत् ।
बन्धहेतुः स एव स्यादद्वैतश्चाष्टकर्मणाम् || १८२९ ॥ अन्वयः - जले जम्बालवत् नूनं सः भावः मलिनः भवेत् । सः अद्वैतः एव अष्टकर्मणां बन्धहेतुः स्यात् । अन्वयार्थ - जल में काई की तरह निश्चय से वह भाव मलिन होता है और वह अकेला ही आठ कर्मों के बन्ध का कारण है।
-
भावार्थ - ग्रन्थकार सामान्य स्वभाव पर अथवा श्रद्धा चारित्र गुण पर दृष्टि रखकर उस मोहभाव का निरूपण करते हैं कि जैसे जल तो स्वभाव से निर्मल है किन्तु उन्हीं जलप्रदेशों में उत्पन्न होने वाली काई मलिन है और जल के निर्मल स्वभाव को ढक लेती है उसी प्रकार श्रद्धा, चारित्र गुण का धारी ज्ञायक आत्मा तो स्वभाव से नित्य निर्मल है किन्तु उन्हीं प्रदेशों में वर्तमान पर्याय रूप उत्पन्न होनेवाला यह भावमोह मलिन है और श्रद्धा, चारित्र गुण के वीतराग स्वभाव को अपनी मलिनता द्वारा ढक देता है। जिस समय जीव मिथ्यात्व राग-द्वेष रूप [ भावमोह रूप ] परिणमन करता है तो उसकी वीतरागता का नाश हो जाता है। यह तो भावमोह का स्वरूप है। अब उसका बन्ध रूप कार्य बताते हैं - बिना भावमोह के कर्म आत्मा के साथ बन्ध नहीं सकते हैं। जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। भावमोह ही उनमें बन्ध का कारण है। इसलिये दसवें गुणस्थान तक ही कर्मबन्ध होता है। उसके ऊपर कर्मबन्ध नहीं होता किन्तु योगों के निमित्त से जिस समय में कर्म आते हैं उसी समय में खिर भी जाते हैं। इसलिये कर्मबन्ध वह इस भावमोह का फल है - कार्य है। जिस प्रकार स्वभाव के वेदन का फल कर्मबन्ध से छूटना है उसी प्रकार भावमोह का फल कर्म से बन्धना है। इसी को और स्पष्ट करते हैं
-
अपि यावदनर्थानां मूलमेकः स एव च ।
यस्मादनर्थमूलानां कर्मणामादिकारणम् ॥ १८३० ॥
अपि च सः एव एकः यावदनर्थानां मूलं यस्मात् अनर्थमूलानां कर्मणां आदिकारणम् ।
अन्वयः
अन्वयार्थ और वह एक भावमोह ही सम्पूर्ण अनर्थो का मूल है क्योंकि वह भावमोह ही अनर्थमूलक कर्मों का आदिकारण [ मूलकारण ] है ।
भावार्थ जीव के स्वभाव के घातक निमित्त रूप आठ कर्म हैं और उन्हीं के फलस्वरूप यह जीव पंचपरावर्तनरूप संसार में घूम रहा है। इसलिये सब अनर्थों की जड़ वे कर्म हैं और उन आठों ही कर्मों के बन्ध का मूल कारण यह भावमोह है। अतः ग्रन्थकार कहते हैं कि भाई तेरी सब आपत्तियों की मूल जड़ यह एक भावमोह ही है। स्वभाव का आश्रय लेकर इसे छोड़ तो तू कर्मबन्ध के संदरपूर्वक संसार से छूट कर अपने पूर्ण स्वभाव का संवेदन कर सकेगा। उसी भावमोह के स्वरूप को और लम्बाते हुए कहते हैं :
अशुचिर्घातको रौद्रो दुःखं दुःखफलं च सः ।
किमत्र बहुनोक्तेन सर्वासां विपदां पदम् ॥ १८३१ ॥
अन्वयः - स: [ भावमोहः ] अशुचिः घातकः रौद्रः दुखं दुःखफलं । अत्र बहुना उक्तेन किं । सर्वासां विपदां पदम् । अन्वयार्थं - वह भावमोह अशुचि [ अपवित्र मलिन ] है, घातक है [ वीतरागता का नाश करने वाला है ] रौद्र