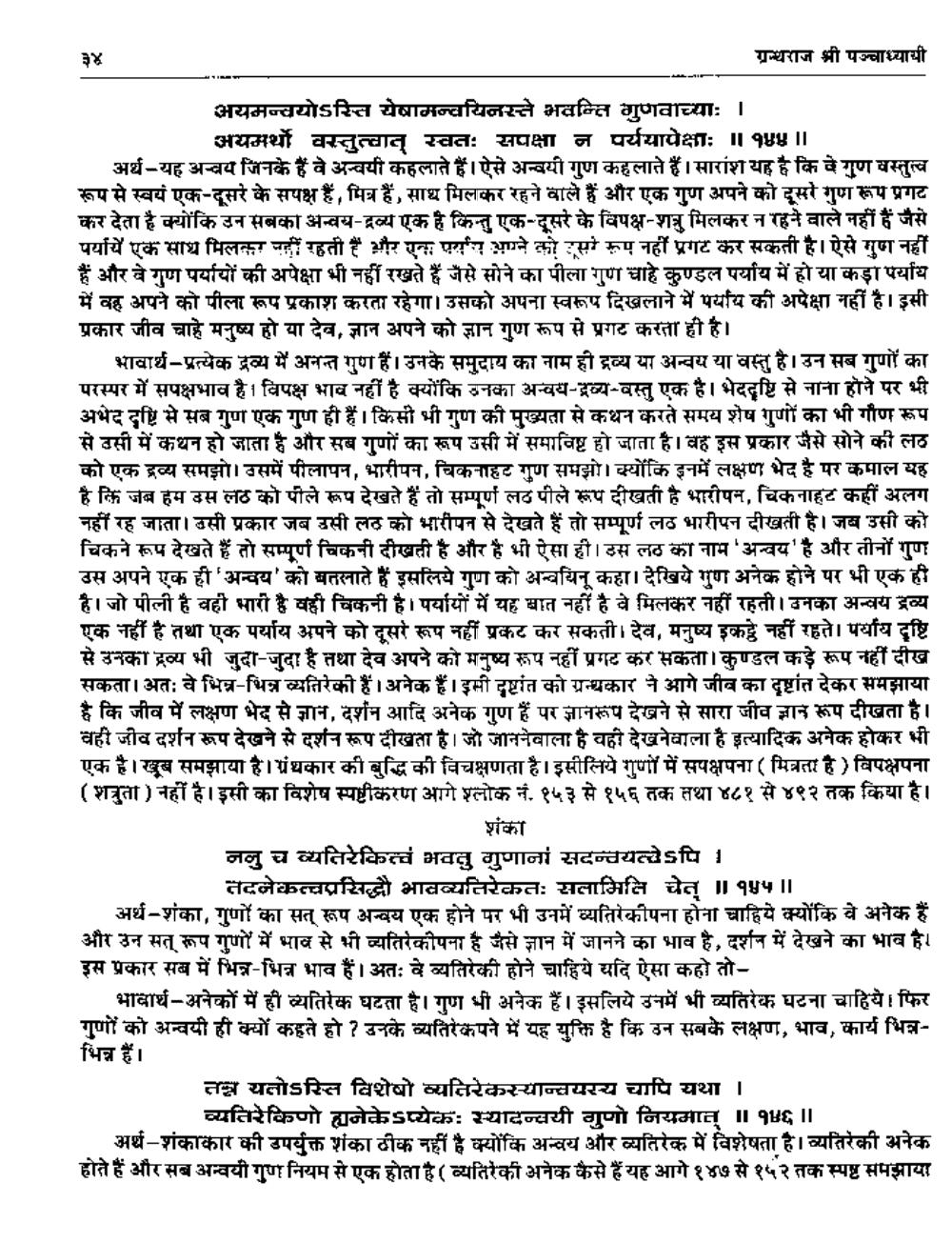________________
३४
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
अयमन्वयोऽस्ति येषामन्वयिनस्ते भवन्ति गुणवाच्याः ।
अयमों वस्तत्वात स्वतः सपक्षा न पर्ययापेक्षाः ॥ १४ ॥ अर्थ-यह अञ्चय जिनके हैं वे अन्वयी कहलाते हैं। ऐसे अन्वयी गुण कहलाते हैं। सारांश यह है कि वे गुण वस्तुत्व रूप से स्वयं एक-दूसरे के सपक्ष हैं, मित्र हैं, साथ मिलकर रहने वाले हैं और एक गुण अपने को दूसरे गुण रूप प्रगट कर देता है क्योंकि उन सबका अन्वय-द्रव्य एक है किन्तु एक-दूसरे के विपक्ष-शत्रु मिलकर न रहने वाले नहीं हैं जैसे पर्यायें एक साथ मिलकर नहीं रहती है और एक पर्याय आपने को रसोरुप नहीं प्रगट कर सकती है। ऐसे गुण नहीं हैं और वे गुण पर्यायों की अपेक्षा भी नहीं रखते हैं जैसे सोने का पीला गुण चाहे कुण्डल पर्याय में हो या कड़ा पर्याय में वह अपने को पीला रूप प्रकाश करता रहेगा। उसको अपना स्वरूप दिखलाने में पर्याय की अपेक्षा नहीं है। इसी प्रकार जीव चाहे मनुष्य हो या देव, ज्ञान अपने को ज्ञान गुण रूप से प्रगट करता ही है।
भावार्थ-प्रत्येक द्रव्य में अनन्त गुण हैं। उनके समुदाय का नाम ही द्रव्य या अन्बय या वस्तु है। उन सब गुणों का परस्पर में सपक्षभाव है। विपक्ष भाव नहीं है क्योंकि उनका अन्वय-द्रव्य-वस्तु एक है। भेददृष्टि से नाना होने पर भी अभेद दृष्टि से सब गुण एक गुण ही हैं। किसी भी गुण की मुख्यता से कथन करते समय शेष गुणों का भी गौण रूप से उसी में कथन हो जाता है और सब गुणों का रूप उसी में समाविष्ट हो जाता है। वह इस प्रकार जैसे सोने की लठ को एक द्रव्य समझो। उसमें पीलापन, भारीपन, चिकनाहट गुण समझो। क्योंकि इनमें लक्षण भेद है पर कमाल यह है कि जब हम उस लठ को पीले रूप देखते हैं तो सम्पूर्ण लठ पीले रूप दीखती है भारीपन, चिकनाहट कहीं अलग नहीं रह जाता। उसी प्रकार जब उसी लठ को भारीपन से देखते हैं तो सम्पूर्ण लठ भारीपन दीखती है। जब उसी को चिकने रूप देखते हैं तो सम्पूर्ण चिकनी दीखती है और है भी ऐसा ही। उस लठ का नाम 'अन्वय' है और तीनों गुण उस अपने एक ही 'अन्वय' को बतलाते हैं इसलिये गुण को अन्वयिनू कहा। देखिये गुण अनेक होने पर भी एक ही है। जो पीली है वहीं भारी है वहीं चिकनी है। पर्यायों में यह बात नहीं है वे मिलकर नहीं रहती। उनका अन्वय द्रव्य एक नहीं है तथा एक पर्याय अपने को दूसरे रूप नहीं प्रकट कर सकती। देव, मनुष्य इकट्ठे नहीं रहते। पर्याय दृष्टि से उनका द्रव्य भी जुदा-जुदा है तथा देव अपने को मनुष्य रूप नहीं प्रगट कर सकता। कुण्डल कड़े रूप नहीं दीख सकता। अत: वे भिन्न-भिन्न व्यतिरेकी हैं। अनेक हैं। इसी दृष्टांत को ग्रन्थकार ने आगे जीव का दृष्टांत देकर समझाया है कि जीव में लक्षण भेद से ज्ञान, दर्शन आदि अनेक गुण हैं पर ज्ञानरूप देखने से सारा जीव ज्ञान रूप दीखता है।
से दर्शन रूप दीखता है। जो जाननेवाला है वही देखनेवाला है इत्यादिक अनेक होकर भी एक है। खुब समझाया है। ग्रंथकार की बुद्धि की विचक्षणता है। इसीलिये गुणों में सपक्षपना ( मित्रता है) विपक्षपना (शत्रुता) नहीं है। इसी का विशेष स्पष्टीकरण आगे श्लोक नं. १५३ से तक तथा ४८१ से ४९२ तक किया है।
शंका ननु च व्यतिरेकित्वं भवतु गुणानां सदन्तयत्वेऽपि ।
तदनेकत्वप्रसिद्धौ भावव्यतिरेकत: सलामिलि चेत ॥१५॥ अर्थ-शंका, गुणों का सत् रूप अन्बय एक होने पर भी उनमें व्यतिरेकीपना होना चाहिये क्योंकि वे अनेक हैं और उन सत् रूप गुणों में भाव से भी व्यतिरेकीपना है जैसे ज्ञान में जानने का भाव है, दर्शन में देखने का भाव है। इस प्रकार सब में भिन्न-भिन्न भाव हैं। अतः वे व्यतिरेकी होने चाहिये यदि ऐसा कहो तो
भावार्थ-अनेकों में ही व्यतिरेक घटता है। गुण भी अनेक हैं। इसलिये उनमें भी व्यतिरेक घटना चाहिये। फिर गुणों को अन्बयी ही क्यों कहते हो ? उनके व्यतिरेकपने में यह युक्ति है कि उन सबके लक्षण, भाव, कार्य भिन्नभिन्न हैं।
तन्न यतोऽस्ति विशेषो व्यतिरेकस्यान्वयस्य चापि यथा ।
व्यतिरेकिणो हानेकेऽप्येकः स्यादन्वयी गुणो नियमात ॥ १६॥ अर्थ-शंकाकार की उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक में विशेषता है। व्यतिरेकी अनेक होते हैं और सब अन्वयी गण नियम से एक होता है (व्यतिरेकी अनेक कैसे हैं यह आगे १४७ से १५२ तक स्पष्ट समझाया