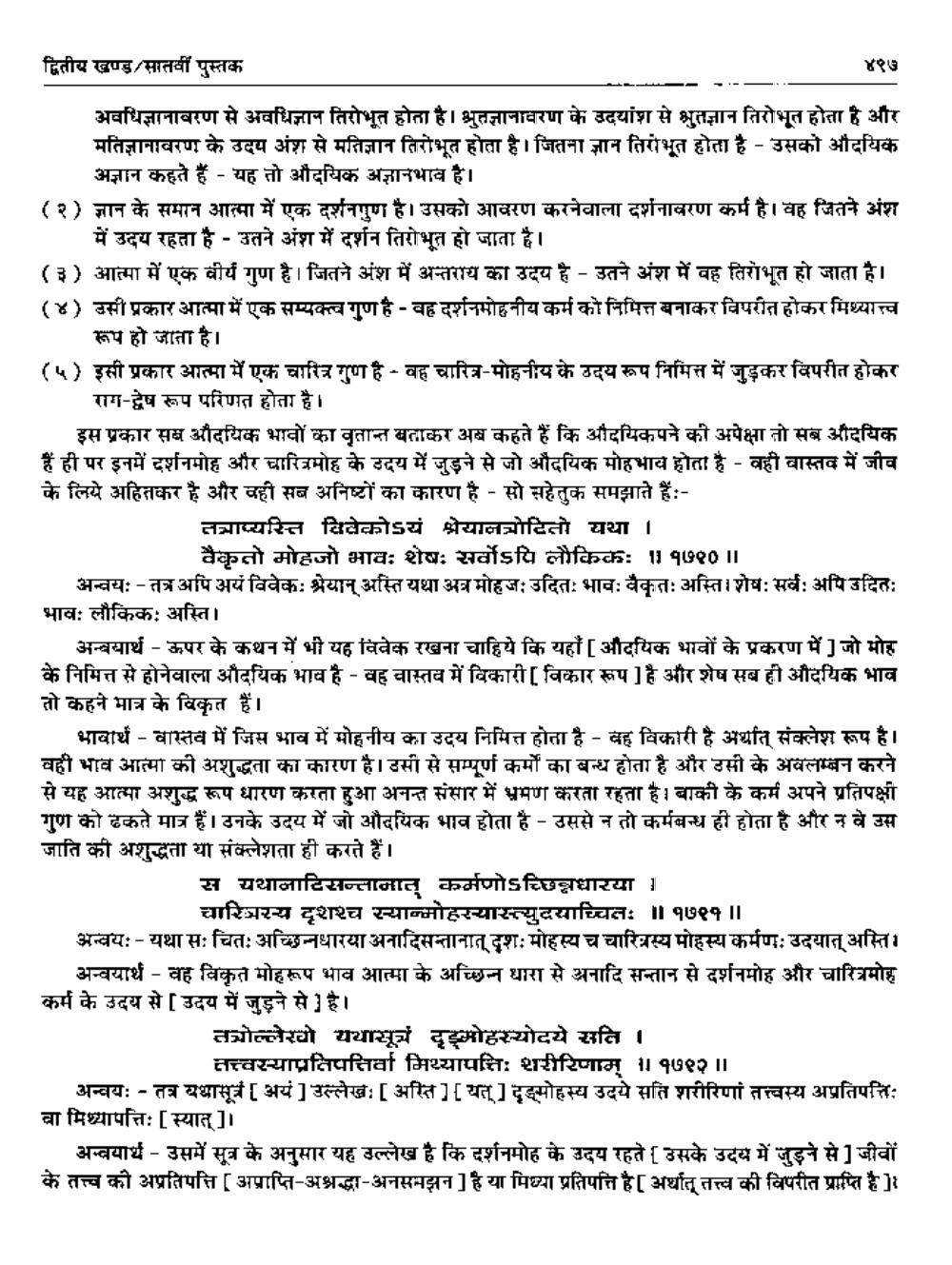________________
द्वितीय खण्ड/सातवीं पुस्तक
४९७
अवधिज्ञानावरण से अवधिज्ञान तिरोभूत होता है। श्रुतज्ञानावरण के उदयांश से भुतज़ान तिरोभूत होता है और मतिज्ञानावरण के उदय अंश से मतिज्ञान तिरोभूत होता है। जितना ज्ञान तिरोभूत होता है - उसको औदयिक
अज्ञान कहते हैं - यह तो औदयिक अज्ञानभाव है। (२) ज्ञान के समान आत्मा में एक दर्शनपुण है। उसको आवरण करनेवाला दर्शनावरण कर्म है। वह जितने अंश
में उदय रहता है - उतने अंश में दर्शन तिरोभूत हो जाता है। (३) आत्मा में एक वीर्य गुण है। जितने अंश में अन्तराय का उदय है - उतने अंश में वह तिरोभूत हो जाता है। (४) उसी प्रकार आत्मा में एक सम्यक्त्व गुण है - वह दर्शनमोहनीय कर्म को निमित्त बनाकर विपरीत होकर मिथ्यात्त्व
रूप हो जाता है। (५) इसी प्रकार आत्मा में एक चारित्र गुण है - वह चारित्र-मोहनीय के उदय रूप निमित्त में जुड़कर विपरीत होकर
राग-द्वेष रूप परिणत होता है। इस प्रकार सब औदयिक भावों का वृतान्त बताकर अब कहते हैं कि औदयिकपने की अपेक्षा तो सब औदयिक हैं ही पर इनमें दर्शनमोह और चारित्रमोह के उदय में जड़ने से जो औदयिक मोहभाव होता है - वही वास्तव में जीव के लिये अहितकर है और वही सब अनिष्टों का कारण है - सो सहेतुक समझाते हैं:
तत्राप्यस्ति विवेकोऽयं श्रेयालचोटितो यथा ।
वैकृतो मोहजो भावः शेषः सर्वोऽपि लौकिकः ॥ १७९० ॥ अन्वयः - तत्र अपि अयं विवेकः श्रेयान् अस्ति यथा अत्र मोहजः उदितः भावः वैकृतः अस्ति। शेष: सर्वः अपि उदितः भावः लौकिकः अस्ति।
अन्वयार्थ - ऊपर के कथन में भी यह विवेक रखना चाहिये कि यहाँ[आदयिक भावों के प्रकरण में] जो मोह के निमित्त से होनेवाला औदयिक भाव है - वह वास्तव में विकारी [विकार रूप] है और शेष सब ही औदयिक भाव तो कहने मात्र के विकृत हैं।
भावार्थ - वास्तव में जिस भाव में मोहनीय का उदय निमित्त होता है - वह विकारी है अर्थात् संक्लेश रूप है। वही भाव आत्मा की अशद्धता का कारण है। उसी से सम्पूर्ण कर्मों का बन्ध होता है और उसी के अवलम्बन करने से यह आत्मा अशुद्ध रूप धारण करता हुआ अनन्त संसार में भ्रमण करता रहता है। बाकी के कर्म अपने प्रतिपक्षी गुण को ढकते मात्र हैं। उनके उदय में जो औदयिक भाव होता है - उससे न तो कर्मबन्ध ही होता है और न वे उस जाति की अशुद्धता या संक्लेशता ही करते हैं।
स यथानाटिसन्तानात् कर्मणोऽच्छिन्नधारया ।
चारित्ररम्य दृशश्च स्यान्मोहरयारत्युदयाच्चिलः ॥ १७९१ ॥ अन्वयः- यथा सः चितः अच्छिन्नधारया अनादिसन्तानात् दशः मोहस्य च चारित्रस्य मोहस्य कर्मणः उदयात् अस्ति।
अन्वयार्थ - वह विकृत मोहरूप भाव आत्मा के अच्छिन धारा से अनादि सन्तान से दर्शनमोह और चारित्रमोह कर्म के उदय से [ उदय में जुड़ने से ] है।
तत्रोल्लेरो यथासूत्रं दृमोहस्योदये सति ।
तत्त्वस्याप्रतिपत्तिर्वा मिथ्यापत्तिः शरीरिणाम ॥ १७९२॥ अन्वयः - तत्र यथासूत्रं [ अयं ] उल्लेख: [ अस्ति] [ यत् ] दृङ्मोहस्य उदये सति शरीरिणां तत्त्वस्य अप्रतिपत्तिः वा मिथ्यापत्तिः [स्यात् ]। ___ अन्वयार्थ - उसमें सूत्र के अनुसार यह उल्लेख है कि दर्शनमोह के उदय रहते [ उसके उदय में जुड़ने से] जीवों के तत्त्व की अप्रतिपत्ति [अप्राप्ति-अश्रद्धा-अनसमझन] है या मिथ्या प्रतिपत्ति है। अर्थात तत्त्व की विपरीत प्राप्ति है।