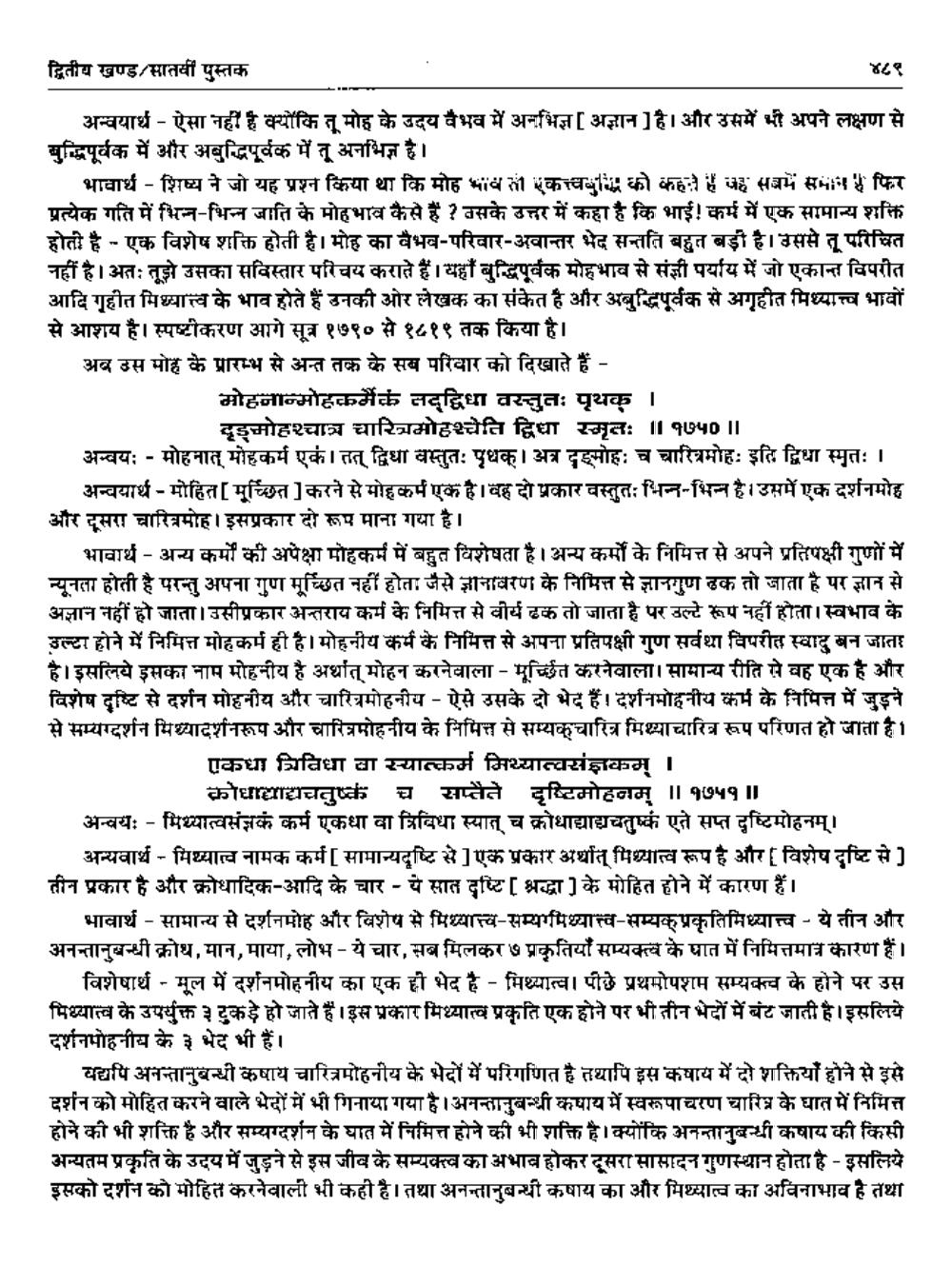________________
द्वितीय खण्ड / सातवीं पुस्तक
अन्वयार्थ - ऐसा नहीं है क्योंकि तू मोह के उदय वैभव में अनभिज्ञ [ अज्ञान ] है और उसमें भी अपने लक्षण से बुद्धिपूर्वक में और अबुद्धिपूर्वक में तू अनभिज्ञ है ।
भावार्थ शिष्य ने जो यह प्रश्न किया था कि मोह भाव ती एकत्वबुद्धि को कहते हैं यह सबमें समान है फिर प्रत्येक गति में भिन्न-भिन्न जाति के मोहभाव कैसे हैं ? उसके उत्तर में कहा है कि भाई ! कर्म में एक सामान्य शक्ति होती है - एक विशेष शक्ति होती है। मोह का वैभव-परिवार अवान्तर भेद सन्तति बहुत बड़ी है। उससे तू परिचित नहीं है । अतः तूझे उसका सविस्तार परिचय कराते हैं । यहाँ बुद्धिपूर्वक मोहभाव से संज्ञी पर्याय में जो एकान्त विपरीत आदि गृहीत मिध्यात्व के भाव होते हैं उनकी ओर लेखक का संकेत है और अबुद्धिपूर्वक से अगृहीत मिध्यात्त्व भावों से आशय है। स्पष्टीकरण आगे सूत्र १७९० से १८१९ तक किया है।
अब उस मोह के प्रारम्भ से अन्त तक के सब परिवार को दिखाते हैं -
मोहनान्मोहकर्मे कं तद्विधा वस्तुतः पृथक् । दृङ्मोहश्चात्र चारित्रमोहश्चेति द्विधा अन्वयः - मोहनात् मोहकर्म एकं । तत् द्विधा वस्तुतः पृथक् । अत्र
४८९
स्मृतः ॥ १७५० ॥
मोहः च चारित्रमोहः इति द्विधा स्मृतः । अन्वयार्थ - मोहित [ मूर्च्छित ] करने से मोहकर्म एक है। वह दो प्रकार वस्तुतः भिन्न-भिन्न है। उसमें एक दर्शनमोह 'दूसरा चारित्रमोह। इसप्रकार दो रूप माना गया है।
और
भावार्थ - अन्य कर्मों की अपेक्षा मोहकर्म में बहुत विशेषता है। अन्य कर्मों के निमित्त से अपने प्रतिपक्षी गुणों में न्यूनता होती है परन्तु अपना गुण मूच्छित नहीं होता जैसे ज्ञानावरण के निमित्त से ज्ञानगुण ढक तो जाता है पर ज्ञान से अज्ञान नहीं हो जाता। उसीप्रकार अन्तराय कर्म के निमित्त से वीर्य ढक तो जाता है पर उल्टे रूप नहीं होता। स्वभाव के उल्टा होने में निमित्त मोहकर्म ही है। मोहनीय कर्म के निमित्त से अपना प्रतिपक्षी गुण सर्वथा विपरीत स्वादु बन जाता है । इसलिये इसका नाम मोहनीय है अर्थात् मोहन करनेवाला मूर्च्छित करनेवाला । सामान्य रीति से वह एक है और विशेष दृष्टि से दर्शन मोहनीय और चारित्रमोहनीय ऐसे उसके दो भेद हैं। दर्शनमोहनीय कर्म के निमित्त में जुड़ने से सम्यग्दर्शन मिथ्यादर्शनरूप और चारित्रमोहनीय के निमित्त से सम्यक्चारित्र मिथ्याचारित्र रूप परिणत हो जाता है । एकधा त्रिविधा वा स्यात्कर्म मिथ्यात्वसंज्ञकम् । क्रोधाद्याद्यचतुष्कं च सप्तैते
दृष्टिमोहनम् ॥ १७५१ ॥
अन्वयः - मिथ्यात्वसंज्ञकं कर्म एकधा वा त्रिविधा स्यात् च क्रोधाद्याद्यचतुष्कं एते सप्त दृष्टिमोहनम् । अन्यवार्थ - मिथ्यात्व नामक कर्म [ सामान्यदृष्टि से ] एक प्रकार अर्थात् मिध्यात्व रूप है और [ विशेष दृष्टि से ] तीन प्रकार है और क्रोधादिक आदि के चार- ये सात दृष्टि [ श्रद्धा ] के मोहित होने में कारण हैं।
भावार्थ - सामान्य से दर्शनमोह और विशेष से मिथ्यात्त्व- सम्यगमिथ्यात्त्व- सम्यक्प्रकृतिमिध्यात्त्व ये तीन और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ- ये चार, सब मिलकर ७ प्रकृतियाँ सम्यक्त्व के पात में निमित्तमात्र कारण हैं।
विशेषार्थ मूल में दर्शनमोहनीय का एक ही भेद है- मिथ्यात्व । पीछे प्रथमोपशम सम्यक्त्व के होने पर उस मिथ्यात्व के उपर्युक्त ३ टुकड़े हो जाते हैं। इस प्रकार मिध्यात्व प्रकृति एक होने पर भी तीन भेदों में बंट जाती है । इसलिये दर्शनमोहनीय के ३ भेद भी हैं।
-
raft अनन्तानुबन्ध कषाय चारित्रमोहनीय के भेदों में परिगणित है तथापि इस कषाय में दो शक्तियाँ होने से इसे दर्शन को मोहित करने वाले भेदों में भी गिनाया गया है। अनन्तानुबन्धी कषाय में स्वरूपाचरण चारित्र के घात में निमित्त होने की भी शक्ति है और सम्यग्दर्शन के घात में निमित्त होने की भी शक्ति है। क्योंकि अनन्तानुबन्धी कषाय की किसी अन्यतम प्रकृति के उदय में जुड़ने से इस जीव के सम्यक्त्व का अभाव होकर दूसरा सासादन गुणस्थान होता है - इसलिये इसको दर्शन को मोहित करनेवाली भी कही है। तथा अनन्तानुबन्धी कषाय का और मिथ्यात्व का अविनाभाव है तथा