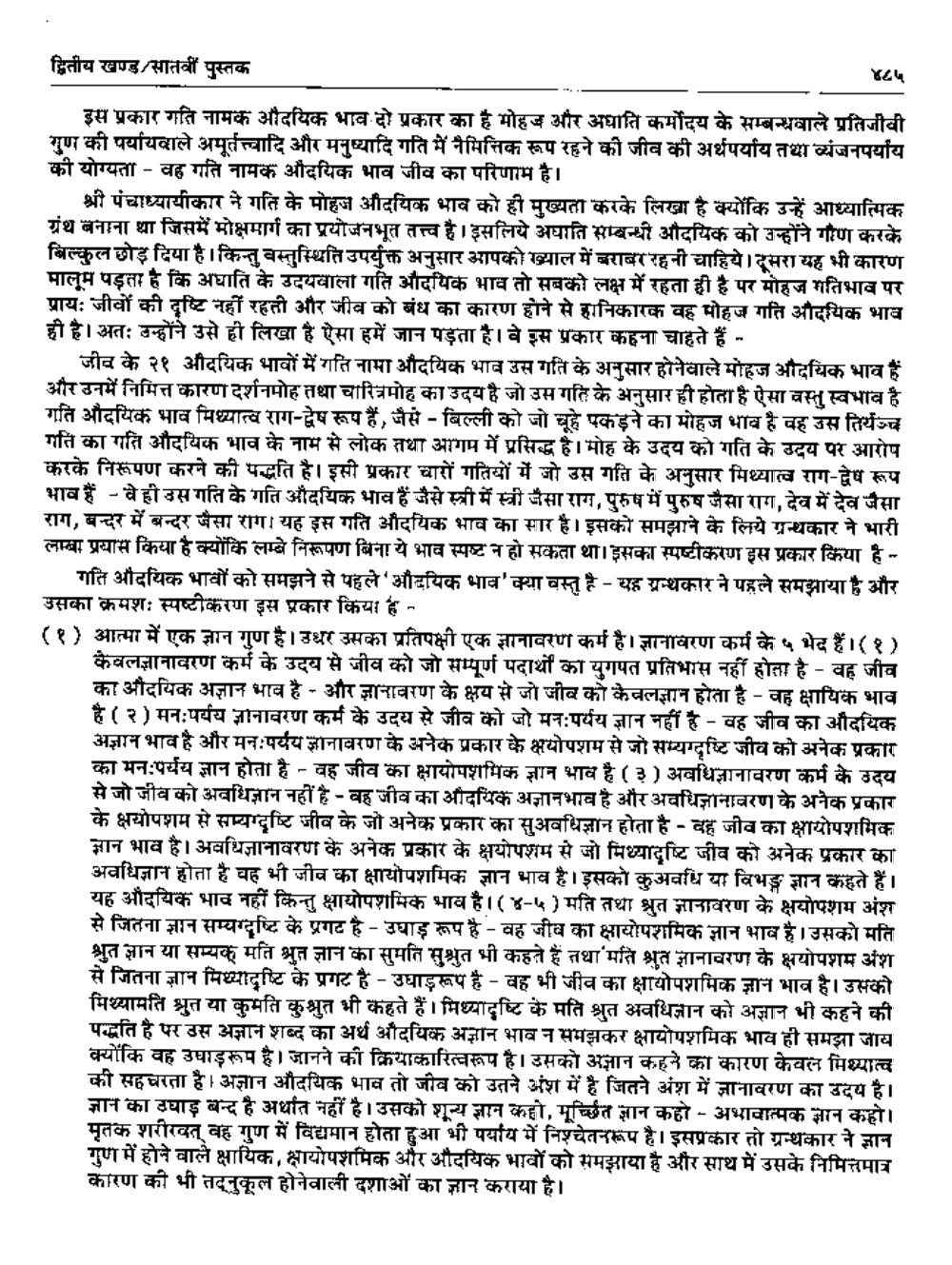________________
द्वितीय खण्ड/सातवीं पुस्तक
४८५
इस प्रकार गति नामक औदयिक भाव दो प्रकार का है मोहज और अघाति कर्मोदय के सम्बन्धवाले प्रतिजीवी गुण की पर्यायवाले अमूर्तत्त्वादि और मनुष्यादि गति में नैमित्तिक रूप रहने की जीव की अर्थपर्याय तथा व्यंजनपर्याय की योग्यता- वह गति नामक औदयिक भाव जीव का परिणाम है।
श्री पंचाध्यायीकार ने गति के मोहज औदयिक भाव को ही मुख्यता करके लिखा है क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक ग्रंथ बनाना था जिसमें मोक्षमार्ग का प्रयोजनभूत तत्त्व है। इसलिये अघाति सम्बन्धी औदायिक को उन्होंने गौण करके बिल्कुल छोड़ दिया है। किन्तु वस्तुस्थिति उपर्युक्त अनुसार आपको ख्याल में बराबर रहनी चाहिये। दूसरा यह भी कारण मालूम पड़ता है कि अघाति के उदयवाला गति औदयिक भाव तो सबको लक्ष में रहता ही है पर मोहज गतिभाव पर प्रायः जीवों की दृष्टि नहीं रहती और जीव को बंध का कारण होने से हानिकारक वह मोहज गति औदयिक भाव ही है। अतः उन्होंने उसे ही लिखा है ऐसा हमें जान पड़ता है। वे इस प्रकार कहना चाहते हैं -
जीव के २१ औदयिक भावों में गति नामा औदयिक भाव उस गति के अनुसार होनेवाले मोहज औदयिक भाव हैं और उनमें निमित्त कारण दर्शनमोह तथा चारित्रमोह का उदय है जो उस गति के अनुसार ही होता है ऐसा वस्तु स्वभाव है गति औदयिक भाव मिथ्यात्व राग-द्वेष रूप हैं, जैसे - बिल्ली को जो चूहे पकड़ने का मोहज भाव है वह उस तिर्यञ्च गति का गति औदयिक भाव के नाम से लोक तथा आगम में प्रसिद्ध है। मोह के उदय को गति के उदय पर आरोप करके निरूपण करने की पद्धति है। इसी प्रकार चारों गतियों में जो उस गति के अनुसार मिथ्यात्व राग-द्वेष रूप भाव हैं - वे ही उस गति के गति औदयिक भाव हैं जैसे स्त्री में स्त्री जैसा राग, पुरुष में पुरुष जैसा राग, देव में देव जैसा राग, बन्दर में बन्दर जैसा रागा यह इस गति औदयिक भाव का सार है। इसको समझाने के लिये ग्रन्थकार ने भारी लम्बा प्रयास किया है क्योंकि लम्बे निरूपण बिनाये भाव स्पष्ट न हो सकता था। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है
गति औदयिक भावों को समझने से पहले औदयिक भाव'क्या वस्त है - यह ग्रन्थकार ने पहले समझाया है और उसका क्रमशः स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है(१) आत्मा में एक ज्ञान गण है। उधर उसका प्रतिपक्षी एक ज्ञानावरण कर्म है। ज्ञानावरण कर्म के ५भेद हैं।(१)
केवलज्ञानावरण कर्म के उदय से जीव को जो सम्पर्ण पदार्थो का युगपत प्रतिभास नहीं होता है - वह जीव का औदयिक अज्ञान भाव है - और ज्ञानावरण के क्षय से जो जीव को केवलज्ञान होता है - वह क्षायिक भाव है(२)मनःपर्यय ज्ञानावरण कर्म के उदय से जीव को जो मन:पर्यय ज्ञान नहीं है - वह जीव का औदयिक अज्ञान भाव है और मनःपर्यय ज्ञानावरण के अनेक प्रकार के क्षयोपशम से जो सम्यग्दृष्टि जीव को अनेक प्रकार का मनःपर्यय ज्ञान होता है - वह जीव का क्षायोपशामिक ज्ञान भाव है (३) अवधिज्ञानावरण कर्म के उदय से जो जीव को अवधिज्ञान नहीं है - वह जीव का औदयिक अज्ञानभाव है और अवधिज्ञानावरण के अनेक प्रकार के क्षयोपशम से सम्यग्दृष्टि जीव के जो अनेक प्रकार का सुअवधिज्ञान होता है - वह जीव का क्षायोपशामिक ज्ञान भाव है। अवधिज्ञानावरण के अनेक प्रकार के क्षयोपशम से जो मिथ्यादृष्टि जीव को अनेक प्रकार का अवधिज्ञान होता है वह भी जीव का क्षायोपशमिक ज्ञान भाव है। इसको कुअवधि या विभङ्ग ज्ञान कहते हैं। यह औदयिक भाव नहीं किन्तु क्षायोपशामिक भाव है। (४-५) मति तथा श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम अंश से जितना ज्ञान सम्यग्दृष्टि के प्रगट है - उघाड़ रूप है - वह जीव का क्षायोपशमिक ज्ञान भाव है। उसको मति श्रुत ज्ञान या सम्यक् मति श्रुत ज्ञान का सुमति सुश्रुत भी कहते हैं तथा मति श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम अंश से जितना ज्ञान मिथ्यादृष्टि के प्रगट है- उघाड़रूप है - वह भी जीव का क्षायोपशमिक ज्ञान भाव है। उसको मिथ्यामति श्रुत या कुमति कुश्रुत भी कहते हैं। मिध्यादृष्टि के मति श्रुत अवधिज्ञान को अज्ञान भी कहने की पद्धति है पर उस अज्ञान शब्द का अर्थ औदयिक अज्ञान भाव न समझकर क्षायोपशमिक भाव ही समझा जाय क्योंकि वह उघाड़रूप है। जानने की क्रियाकारित्वरूप है। उसको अज्ञान कहने का कारण केवल मिथ्यात्व की सहचरता है। अज्ञान औदयिक भाव तो जीव को उतने अंश में है जितने अंश में ज्ञानावरण का उदय है। ज्ञान का उघाड़ बन्द है अर्थात नहीं है। उसको शून्य ज्ञान कहो, मूर्छित ज्ञान कहो - अभावात्मक ज्ञान कहो। मृतक शरीरवत् वह गुण में विद्यमान होता हुआ भी पर्याय में निश्चेतनरूप है। इसप्रकार तो ग्रन्धकार ने ज्ञान गुण में होने वाले क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक भावों को समझाया है और साथ में उसके निमित्तमात्र कारण की भी तद्नुकूल होनेवाली दशाओं का ज्ञान कराया है।