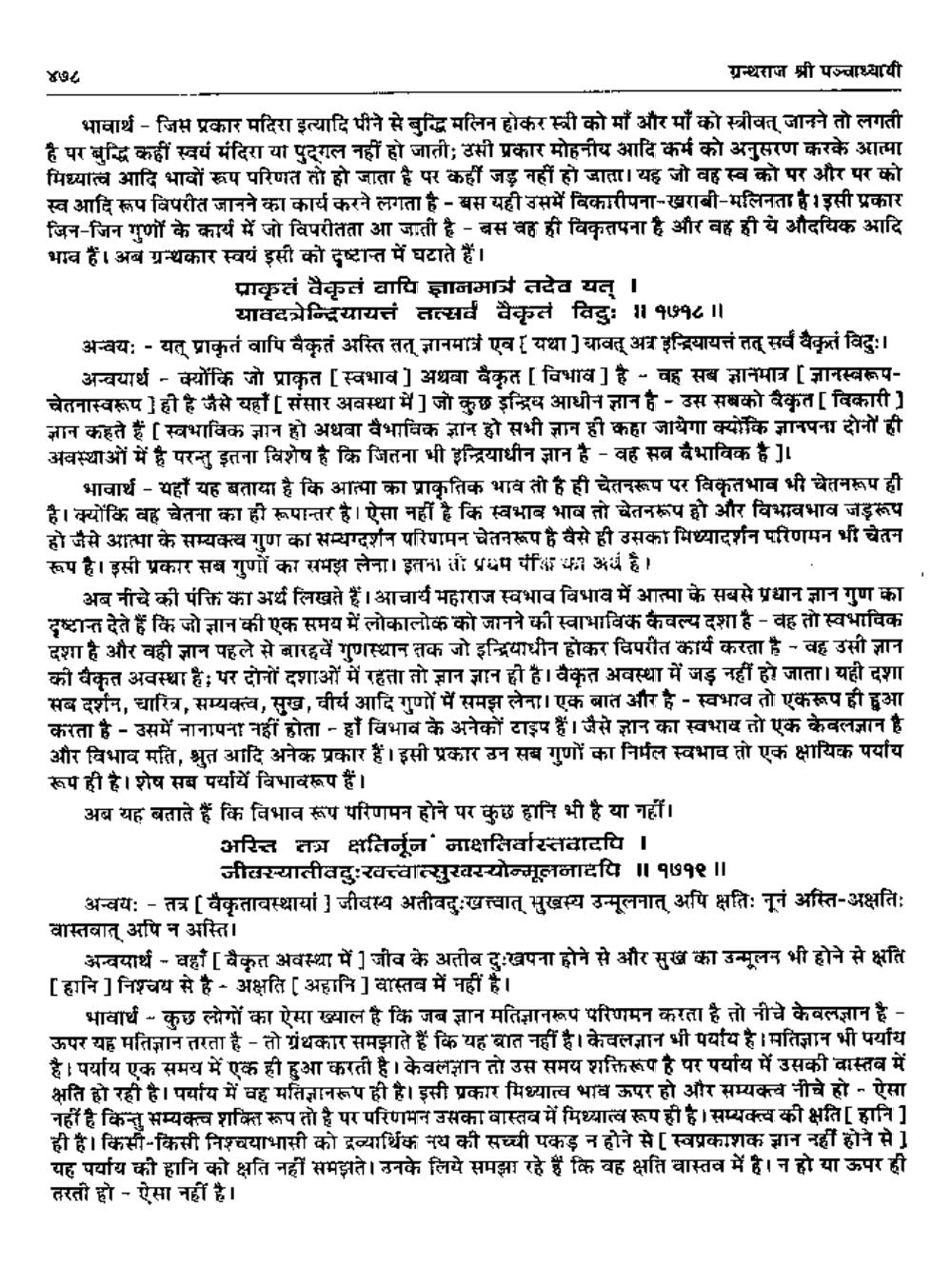________________
४७८
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
__ भावार्थ - जिस प्रकार मदिरा इत्यादि पीने से बुद्धि मलिन होकर स्त्री को माँ और माँ को स्त्रीवत् जानने तो लगती है पर बुद्धि कहीं स्वयं मंदिरा या पुद्गल नहीं हो जाती; उसी प्रकार मोहनीय आदि कर्म को अनुसरण करके आत्मा मिथ्यात्व आदि भावों रूप परिणत तो हो जाता है पर कहीं जड़ नहीं हो जाता। यह जो वह स्व को पर और पर को स्व आदि रूप विपरीत जानने का कार्य करने लगता है - बस यही उसमें विकारीपना-खराबी-मलिनता है। इसी प्रकार जिन-जिन गुणों के कार्य में जो विपरीतता आ जाती है - बस वह ही विकृतपना है और वह ही ये औदयिक आदि भाव हैं। अब ग्रन्थकार स्वयं इसी को दृष्टान्त में घटाते हैं।
प्राकृतं वैकृतं वापि ज्ञानमात्र तदेव यत् ।।
यावदनेन्द्रियायत्तं तत्सर्वं वैकृत विदुः ॥ १७१८ ॥ अन्वय: - यत् प्राकृतं वापि वैकृतं अस्ति तत् ज्ञानमात्र एव । यथा ] यावत् अब इन्द्रियायत्तं तत् सर्वं वैकृतं विदुः।
अन्वयार्थ - क्योंकि जो प्राकृत [स्वभाव ] अथवा वैकृत [ विभाव ] है - वह सब ज्ञानमात्र [ज्ञानस्वरूपचेतनास्वरूप] ही है जैसे यहाँ[संसार अवस्था में] जो कुछ इन्द्रिय आधीन ज्ञान है- उस सबको वैकता विकारी] ज्ञान कहते हैं [स्वभाविक ज्ञान हो अथवा वैभाविक ज्ञान हो सभी ज्ञान ही कहा जायेगा क्योकि ज्ञानपना दोनों ही अवस्थाओं में है परन्तु इतना विशेष है कि जितना भी इन्द्रियाधीन ज्ञान है - वह सब वैभाविक है]
भावार्थ- यहाँ यह बताया है कि आत्मा का प्राकृतिक भाव तो है ही चेतनरूप पर विकतभाव भी चेतमरूपही है। क्योंकि वह चेतना का ही रूपान्तर है। ऐसा नहीं है कि स्वभाब भाव तो चेतनरूप हो और विभावभाव जड़रूप हो जैसे आत्मा के सम्यक्व गुण का सम्यग्दर्शन परिणामन चेतनरूप ह वस ह रूप है। इसी प्रकार सब गुणों का समझ लेना। इतना ती प्रथम पाका अय है।
अब नीचे की पंक्ति का अर्थ लिखते हैं। आचार्य महाराज स्वभाव विभाव में आत्मा के सबसे प्रधान ज्ञान गुण का दृष्टान्त देते हैं कि जो ज्ञान की एक समय में लोकालोक को जानने की स्वाभाविक कैवल्य दशा है - वह तो स्वभाविक दशा है और वही ज्ञान पहले से बारहवें गुणस्थान तक जो इन्द्रियाधीन होकर विपरीत कार्य करता है - वह उसी ज्ञान की वैकृत अवस्था है; पर दोनों दशाओं में रहता तो ज्ञान ज्ञान ही है। वैकृत अवस्था में जड़ नहीं हो जाता। यही दशा सब दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व, सुख, वीर्य आदि गुणों में समझ लेना। एक बात और है - स्वभाव तो एकरूप ही हुआ करता है- उसमें नानापना नहीं होता - हाँ विभाव के अनेकों टाइप हैं। जैसे ज्ञान का स्वभाव तो एक केवलज्ञान है और विभाव मति, श्रुत आदि अनेक प्रकार हैं। इसी प्रकार उन सब गुणों का निर्मल स्वभाव तो एक क्षायिक पर्याय रूपही है। शेष सब पर्याय विभावरूप हैं। अब यह बताते हैं कि विभाव रूप परिणमन होने पर कुछ हानि भी है या नहीं।
अरित तत्र क्षतिजून नाक्षलिस्तिवादपि ।
जीवस्यालीवदु:खत्त्वात्सुरवस्योन्मूलनादपि ॥ १७१९॥ अन्वय: - तत्र [वैकृतावस्थायां ] जीवस्य अतीवदुःखत्त्वात् मुखस्य उन्मूलनात् अपि क्षति: नूनं अस्ति-अक्षतिः वास्तवात् अपि न अस्ति।
अन्वयार्थ - वहाँ [वैकृत अवस्था में ] जीव के अतीव दुःखपना होने से और सुख का उन्मूलन भी होने से क्षति [हानि ] निश्चय से है - अक्षति [अहानि] वास्तव में नहीं है।
भावार्थ- कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि जब ज्ञान मतिज्ञानरूप परिणमन करता है तो नीचे केवलज्ञान हैऊपर यह मतिज्ञान तरता है - तो ग्रंथकार समझाते हैं कि यह बात नहीं है। केवलज्ञान भी पर्याय है। मतिज्ञान भी पर्याय है। पर्याय एक समय में एक ही हुआ करती है। केवलज्ञान तो उस समय शक्तिरूप है पर पर्याय में उसकी वास्तव में क्षति हो रही है। पर्याय में वह मतिज्ञानरूप ही है। इसी प्रकार मिध्यात्व भाव ऊपर हो और सम्यक्त्व नीचे हो - ऐसा नहीं है किन्तु सम्यक्त्व शक्ति रूप तो है पर परिणमन उसका वास्तव में मिथ्यात्व रूप ही है। सम्यक्त्व की क्षति [हानि] ही है। किसी-किसी निश्चयाभासीको द्रव्यार्थिक नय की सच्ची पकड़न होने से[स्वप्रकाशक ज्ञान नहीं होने से ] यह पर्याय की हानि को क्षति नहीं समझते। उनके लिये समझा रहे हैं कि वह क्षति वास्तव में है। न हो या ऊपर ही तरती हो - ऐसा नहीं है।