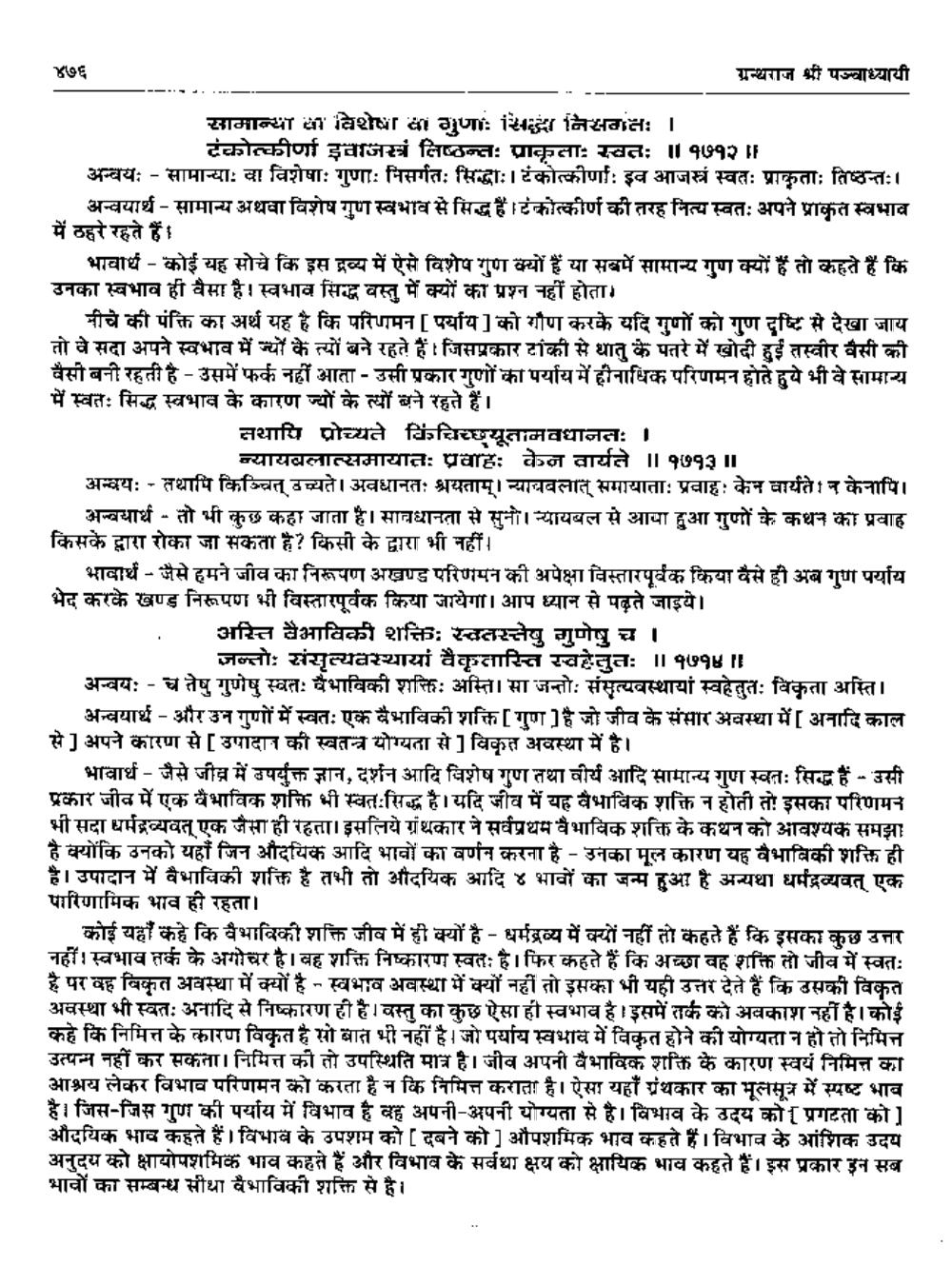________________
४७६
ग्रन्थराज श्री पञ्चाध्यायी
सामान्या का विशेषा या गुणाः सिद्धा निसगंतः । टंकोत्कीर्णा इवाजस्त्रं लिष्ठन्तः प्राकृताः स्वतः ॥ १७१२ ॥ अन्वयः - सामान्याः वा विशेषाः गुणाः निसर्गतः सिद्धाः । टंकोत्कीर्णाः इव आजस्त्रं स्वतः प्राकृताः तिष्ठन्तः । अन्वयार्थ सामान्य अथवा विशेष गुण स्वभाव से सिद्ध हैं। टंकोत्कीर्ण की तरह नित्य स्वतः अपने प्राकृत स्वभाव में ठहरे रहते हैं।
I
भावार्थ- कोई यह सोचे कि इस द्रव्य में ऐसे विशेष गुण क्यों हैं या सबमें सामान्य गुण क्यों हैं तो कहते हैं कि उनका स्वभाव ही वैसा है। स्वभाव सिद्ध वस्तु में क्यों का प्रश्न नहीं होता ।
नीचे की पंक्ति का अर्थ यह है कि परिधामन [ पर्याय ] को गौण करके यदि गुणों को गुण दृष्टि से देखा जाय तो वे सदा अपने स्वभाव में ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जिसप्रकार टांकी से धातु के पतरे में खोदी हुई तस्वीर वैसी की वैसी बनी रहती है उसमें फर्क नहीं आता उसी प्रकार गुणों का पर्याय में हीनाधिक परिणमन होते हुये भी वे सामान्य में स्वतः सिद्ध स्वभाव के कारण ज्यों के त्यों बने रहते हैं।
तथापि प्रोच्यते किंचिच्छ्यूतामवधानतः । न्यायबलात्समायातः प्रवाहः केन वार्यते ॥ १७१३ ॥
अन्वयः - तथापि किञ्चित् उच्यते । अवधानतः श्रयताम् । न्यायवलात् समायाताः प्रवाहः केन वार्यते । न केनापि । अन्वयार्थ तो भी कुछ कहा जाता है। सावधानता से सुनो। न्यायबल से आया हुआ गुणों के कथन का प्रवाह किसके द्वारा रोका जा सकता है? किसी के द्वारा भी नहीं ।
भावार्थं - जैसे हमने जीव का निरूपण अखण्ड परिणमन की अपेक्षा विस्तारपूर्वक किया वैसे ही अब गुण पर्याय
1
भेद करके खण्ड निरूपण भी विस्तारपूर्वक किया जायेगा। आप ध्यान से पढ़ते जाइये।
अस्ति वैभाविकी शक्तिः स्वतस्तेषु गुणेषु च ।
जन्तोः संसृत्यवस्थायां वैकृतास्ति स्वहेतुतः ॥ १७१४
अन्वयः - च तेषु गुणेषु स्वतः वैभाविकी शक्तिः अस्ति । सा जन्तोः संसृत्यवस्थायां स्वहेतुतः विकृता अस्ति ।
अन्वयार्थ और उन गुणों में स्वतः एक वैभाविकी शक्ति [ गुण] है जो जीव के संसार अवस्था में [ अनादि काल से ] अपने कारण से [ उपादान की स्वतन्त्र योग्यता से ] विकृत अवस्था में है।
-
-
भावार्थ जैसे जीन में उपर्युक्त ज्ञान, दर्शन आदि विशेष गुण तथा वीर्य आदि सामान्य गुण स्वतः सिद्ध हैं उसी प्रकार जीव में एक वैभाविक शक्ति भी स्वतः सिद्ध है। यदि जीव में यह वैभाविक शक्ति न होती तो इसका परिणमन भी सदा धर्मद्रव्यवत् एक जैसा ही रहता। इसलिये ग्रंथकार ने सर्वप्रथम वैभाविक शक्ति के कथन को आवश्यक समझा है क्योंकि उनको यहाँ जिन औदयिक आदि भावों का वर्णन करना है उनका मूल कारण यह वैभाविकी शक्ति ही है। उपादान में वैभाविकी शक्ति है तभी तो औदयिक आदि ४ भावों का जन्म हुआ है अन्यथा धर्मद्रव्यवत् एक पारिणामिक भाव ही रहता ।
-
कोई यहाँ कहे कि वैभाविकी शक्ति जीव में ही क्यों है- धर्मद्रव्य में क्यों नहीं तो कहते हैं कि इसका कुछ उत्तर नहीं । स्वभाव तर्क के अगोचर है। वह शक्ति निष्कारण स्वतः है। फिर कहते हैं कि अच्छा वह शक्ति तो जीव में स्वतः है पर वह विकृत अवस्था में क्यों है - स्वभाव अवस्था में क्यों नहीं तो इसका भी यही उत्तर देते हैं कि उसकी विकृत अवस्था भी स्वतः अनादि से निष्कारण ही है। वस्तु का कुछ ऐसा ही स्वभाव है। इसमें तर्क को अवकाश नहीं है। कोई कहे कि निमित्त के कारण विकृत है सो बात भी नहीं है। जो पर्याय स्वभाव में विकृत होने की योग्यता न हो तो निमित्त उत्पन्न नहीं कर सकता। निमित्त की तो उपस्थिति मात्र है। जीव अपनी वैभाविक शक्ति के कारण स्वयं निमित्त का आश्रय लेकर विभाव परिणमन को करता है न कि निमित्त कराता है। ऐसा यहाँ ग्रंथकार का मूलसूत्र में स्पष्ट भाव है। जिस-जिस गुण की पर्याय में विभाव है वह अपनी-अपनी योग्यता से है। विभाव के उदय को [ प्रगटता को ] औदयिक भाव कहते हैं। विभाव के उपशम को [ दबने को ] औपशमिक भाव कहते हैं। विभाव के आंशिक उदय अनुदय को क्षायोपशमिक भाव कहते हैं और विभाव के सर्वधा क्षय को क्षायिक भाव कहते हैं। इस प्रकार इन सब भावों का सम्बन्ध सीधा वैभाविकी शक्ति से है।