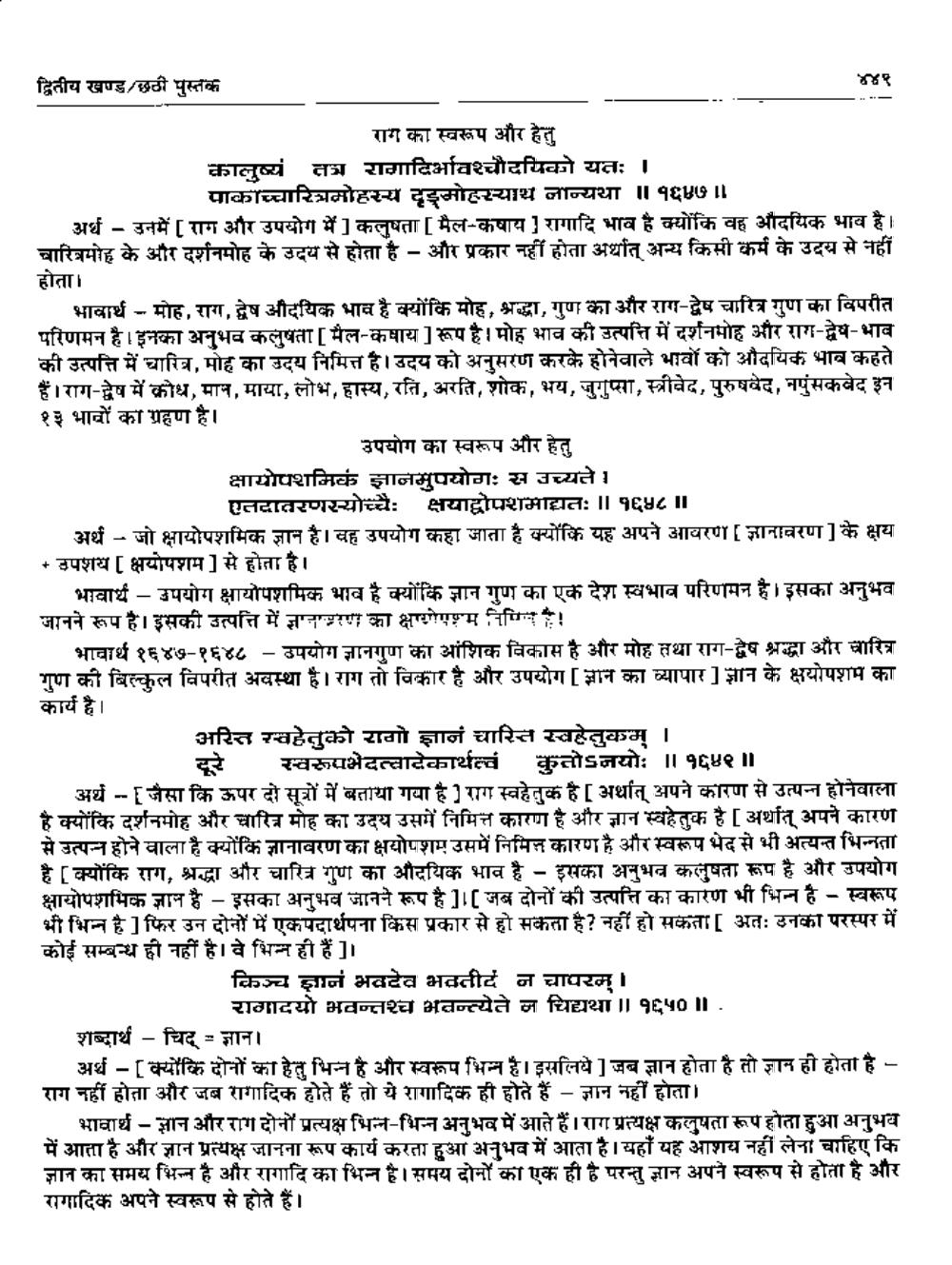________________
द्वितीय खण्ड/छठी पुस्तक
राग का स्वरूप और हेतु कानुष्यं तत्र रागादिर्भावश्चौदयिको यतः ।
पाकाच्चारित्रमोहस्य दृड्मोहस्याथ नान्यथा ।। १६४७ ।। अर्थ - उनमें [राग और उपयोग में] कलुषता [मैल-कषाय ] रागादि भाव है क्योंकि वह औदयिक भाव है। चारित्रमोह के और दर्शनमोह के उदय से होता है - और प्रकार नहीं होता अर्थात् अन्य किसी कर्म के उदय से नहीं होता।
भावार्थ - मोह, राग, द्वेष औदयिक भाव है क्योंकि मोह, श्रद्धा, गुण का और राग-द्वेष चारित्र गुण का विपरीत परिणमन है। इनका अनुभव कलुषता[मैल-कषाय ] रूप है। मोह भाव की उत्पत्ति में दर्शनमोह और राग-द्वेष-भाव की उत्पत्ति में चारित्र, मोह का उदय निमित्त है। उदय को अनुसरण करके होनेवाले भावों को औदयिक भाव कहते हैं। राग-द्वेष में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद इन १३ भावों का ग्रहण है।
उपयोग का स्वरूप और हेतु क्षायोपशमिकं ज्ञानमुपयोगः स उच्यते।
एतदातरणस्योच्चैः क्षयाद्वोपशमाातः ।। १६५८ ॥ अर्थ - जोक्षायोपशमिक ज्ञान है। वह उपयोग कहा जाता है क्योंकि यह अपने आवरण[ज्ञानावरण] के क्षय + उपशय [क्षयोपशम] से होता है।
भावार्थ - उपयोग क्षायोपशमिक भाव है क्योंकि ज्ञान गुण का एक देश स्वभाव परिणमन है। इसका अनुभव जानने रूप है। इसकी उत्पत्ति में ज्ञानामरण का क्षयोपशम निषित।
भावार्थ १६४७-१६४८ - उपयोग ज्ञानगुण का आंशिक विकास है और मोह तथा राग-द्वेष श्रद्धा और चारित्र गुण की बिल्कुल विपरीत अवस्था है। राग तो विकार है और उपयोग [ज्ञान का व्यापार ] ज्ञान के क्षयोपशम का कार्य है।
अरित रचहेतुको रागो ज्ञानं चारित स्वहेतुकम् ।
दूरे स्वरूपभेदत्तादेकार्थत्वं कुतोऽजयोः ॥ १६४९॥ अर्थ -- जैसा कि ऊपर दो सूत्रों में बताया गया है राग स्वहेतुक है [ अर्थात् अपने कारण से उत्पन्न होनेवाला है क्योंकि दर्शनमोह और चारित्र मोह का उदय उसमें निमित्त कारण है और ज्ञान स्वहेतुक है [अर्थात् अपने कारण से उत्पन्न होने वाला है क्योंकि ज्ञानावरणका क्षयोपशम उसमें निमित्त कारण है और स्वरूप भेद से भी अत्यन्त भिन्नता है क्योंकि राग, श्रद्धा और चारित्र गुण का औदयिक भाव है - इसका अनुभव कलुषता रूप है और उपयोग क्षायोपशभिक ज्ञान है - इसका अनुभव जानने रूप है ] [जब दोनों की उत्पत्ति का कारण भी भिन्न है - स्वरूप भी भिन्न है ] फिर उन दोनों में एकपदार्थपना किस प्रकार से हो सकता है? नहीं हो सकता[ अतः उनका परस्पर में कोई सम्बन्ध ही नहीं है। वे भिन्न ही हैं ।
किञ्च जानं भवदेव भक्तीदं न चापरम।
रागादयो भवन्तश्च भवन्त्येते न चिद्यथा ॥ १६५०॥ . शब्दार्थ - चिद् - ज्ञान।
अर्थ - [क्योंकि दोनों का हेतु भिन्न है और स्वरूप भिन्न है। इसलिये ] जब ज्ञान होता है तो ज्ञान ही होता है - राग नहीं होता और जब रागादिक होते हैं तो ये रागादिक ही होते हैं - जान नहीं होता।
भावार्थ-ज्ञान और राग दोनों प्रत्यक्ष भिन्न-भिन्न अनुभव में आते हैं। राग प्रत्यक्ष कलुषतारूपहोता हुआ अनुभव में आता है और ज्ञान प्रत्यक्ष जानना रूप कार्य करता हुआ अनुभव में आता है। यहाँ यह आशय नहीं लेना चाहिए कि ज्ञान का समय भिन्न है और रागादि का भिन्न है। समय दोनों का एक ही है परन्तु ज्ञान अपने स्वरूप से होता है और रागादिक अपने स्वरूप से होते हैं।
गादिक होते है ताय
आते हैं। राग प्रत्यक्ष
नहीं लेना चाहिए