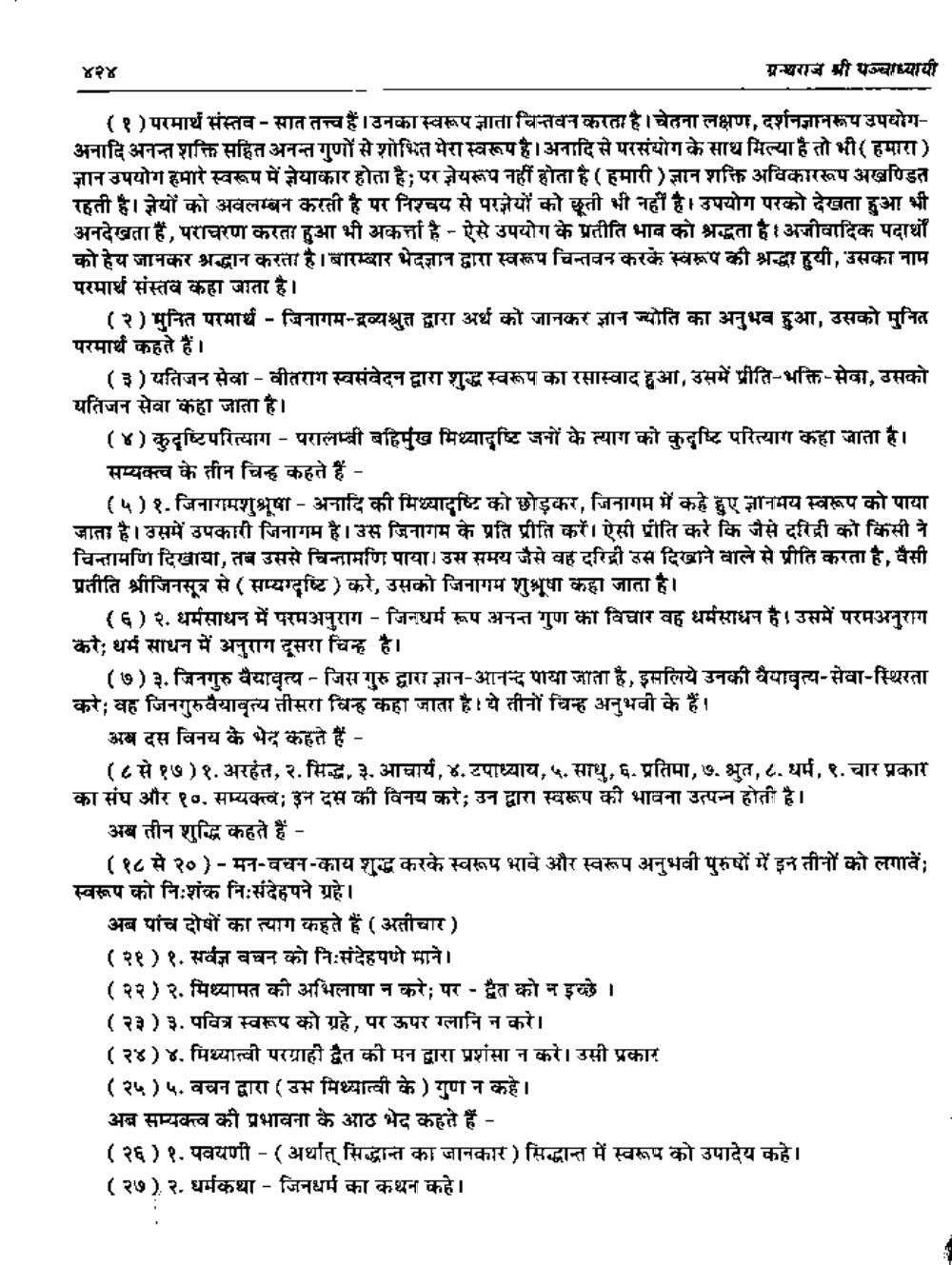________________
४२४
ग्रन्थराज श्रीपञ्चाध्यायी
(१) परमार्थ संस्तव - सात तत्त्व हैं। उनका स्वरूप ज्ञाता चिन्तवन करता है।चेतना लक्षण, दर्शनज्ञानरूप उपयोगअनादि अनन्त शक्ति सहित अनन्त गुणों से शोभित मेरा स्वरूप है। अनादि से परसंयोग के साथ मिल्या है तो भी( हमारा) ज्ञान उपयोग हमारे स्वरूप में ज्ञेयाकार होता है; पर ज्ञेयरूप नहीं होता है (हमारी)ज्ञान शक्ति अविकाररूप अखण्डित रहती है। ज्ञेयों को अवलम्बन करती है पर निश्चय से परज्ञेयों को छूती भी नहीं है। उपयोग परको देखता हुआ भी अनदेखता हैं, पराचरण करता हुआ भी अकर्ता है-ऐसे उपयोग के प्रतीति भाव को श्रद्धता है। अजीबादिक पदार्थों को हेय जानकर श्रद्धान करता है। बारम्बार भेदज्ञान द्वारा स्वरूप चिन्तवन करके स्वरूप की श्रद्धा हुयी, उसका नाम परमार्थ संस्तव कहा जाता है।
(२) मुनित परमार्थ - जिनागम-द्रव्यश्रुत द्वारा अर्थ को जानकर ज्ञान ज्योति का अनुभव हुआ, उसको मुनित परमार्थ कहते हैं।
(३) यतिजन सेवा - वीतराग स्वसंवेदन द्वारा शुद्ध स्वरूप का रसास्वाद हुआ, उसमें प्रीति-भक्ति-सेवा, उसको यतिजन सेवा कहा जाता है।
( ४ ) कुदृष्टिपरित्याग - परालम्बी बहिर्मुख मिथ्यादष्टि जनों के त्याग को कुदृष्टि परित्याग कहा जाता है। सम्यक्त्व के तीन चिन्ह कहते हैं -
(५) १.जिनागमशुश्रूषा - अनादि की मिथ्यादृष्टि को छोड़कर, जिनागम में कहे हुए ज्ञानमय स्वरूप को पाया जाता है। उसमें उपकारी जिनागम है। उस जिनागम के प्रति प्रीति करें। ऐसी प्रीति करे कि जैसे दरिद्री को किसी ने चिन्तामणि दिखाया, तब उससे चिन्तामणि पाया। उस समय जैसे वह दरिद्री उस दिखाने वाले से प्रीति करता है, वैसी प्रतीति श्रीजिनसूत्र से ( सम्यग्दृष्टि ) करे, उसको जिनागम शुश्रूषा कहा जाता है।
(६) २. धर्मसाधन में परमअनुराग - जिनधर्म रूप अनन्त गुण का विचार वह धर्मसाधन है। उसमें परमअनुराग करे; धर्म साधन में अनुराग दूसरा चिन्ह है।
(७) ३. जिनगुरु वैयावृत्य - जिस गुरु द्वारा ज्ञान-आनन्द पाया जाता है, इसलिये उनकी वैयावत्य-सेवा-स्थिरता करे; वह जिनगुरुवयावृत्य तीसरा विन्ह कहा जाता है। ये तीनों चिन्ह अनुभवी के हैं।
अब दस विनय के भेद कहते हैं - (८ से १७ ) १. अरहंत, २.सिद्ध, ३. आचार्य, ४. टपाध्याय, ५. साधु, ६. प्रतिमा, ७. श्रुत, ८. धर्म, १. चार प्रकार का संघ और १०. सम्यक्त्व; इन दस की विनय करे; उन द्वारा स्वरूप की भावना उत्पन्न होती है।
अब तीन शुद्धि कहते हैं -
( १८ से २०)- मन-वचन-काय शुद्ध करके स्वरूप भावे और स्वरूप अनुभवी पुरुषों में इन तीनों को लगावें; स्वरूप को निःशंक निःसंदेहपने ग्रहे।
अब पांच दोषों का त्याग कहते हैं ( अतीचार) (२१) १. सर्वज्ञ वचन को निःसंदेहपणे माने। (२२) २. मिथ्यामत की अभिलाषा न करे; पर - द्वैत को न इच्छे । (२३) ३. पवित्र स्वरूप को ग्रहे, पर ऊपर ग्लानि न करे। ( २४) ४. मिथ्यात्वी परग्राही द्वैत की मन द्वारा प्रशंसा न करे। उसी प्रकार (२५)५. वचन द्वारा ( उस मिथ्यात्वी के ) गुण न कहे। अब सम्यक्त्व की प्रभावना के आठ भेद कहते हैं - (२६) १. पवयणी - (अर्थात् सिद्धान्त का जानकार) सिद्धान्त में स्वरूप को उपादेय कहे। (२७), २.धर्मकथा- जिनधर्म का कथन कहे।