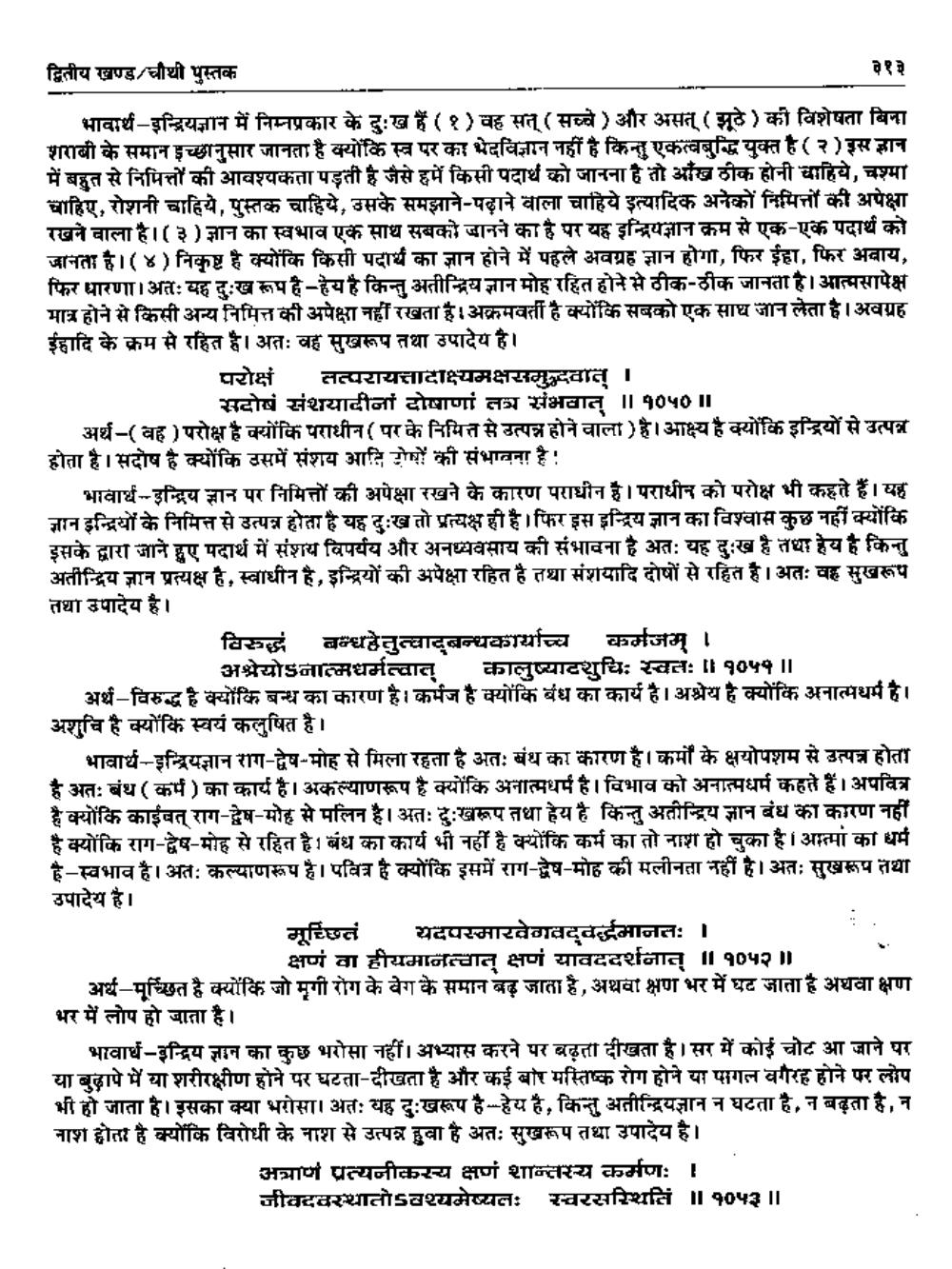________________
द्वितीय खण्ड/चौथी पुस्तक
३१३
भावार्थ-इन्द्रियज्ञान में निम्नप्रकार के दुःख हैं (१) वह सत् ( सच्चे ) और असत् ( झूठे) की विशेषता बिना शराबी के समान इच्छानुसार जानता है क्योंकि स्व पर का भेदविज्ञान नहीं है किन्तु एकत्वबुद्धि युक्त है (२) इस ज्ञान में बहुत से निमित्तों की आवश्यकता पड़ती है जैसे हमें किसी पदार्थ को जानना है तो आँख ठीक होनी चाहिये, चश्मा चाहिए, रोशनी चाहिये, पुस्तक चाहिये, उसके समझाने-पढ़ाने वाला चाहिये इत्यादिक अनेकों निमित्तों की अपेक्षा रखने वाला है।(३) ज्ञान का स्वभाव एक साथ सबको जानने का है पर यह इन्द्रियज्ञान क्रम से एक-एक पदार्थ को जानता है।(४) निकृष्ट है क्योंकि किसी पदार्थ का ज्ञान होने में पहले अवग्रह ज्ञान होगा, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा।अत: यह दुःख रूप है-हेय है किन्तु अतीन्द्रिय ज्ञान मोह रहित होने से ठीक-ठीक जानता है। आत्मसापेक्ष मात्र होने से किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं रखता है।अक्रमवर्ती है क्योंकि सबको एक साथ जान लेता है। अवग्रह ईहादि के क्रम से रहित है। अतः वह सुखरूप तथा उपादेय है।
परोक्षं तत्परायत्तादाक्ष्यमक्षसमुन्दवात् ।
सदोषं संशयादीनां दोषाणां तत्र संभवात् ।। १०५०॥ अर्थ-(वह ) परोक्ष है क्योंकि पराधीन (पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाला) है।आक्ष्य है क्योंकि इन्द्रियों से उत्पन्न होता है। सदोष है क्योंकि उसमें संशय आदि दोषों की संभावना है।
भावार्थ- इन्द्रिय ज्ञान पर निमित्तों की अपेक्षा रखने के कारण पराधीन है। पराधीन को परोक्ष भी कहते हैं। यह ज्ञान इन्द्रियों के निमित्त से उत्पन्न होता है यह दुःख तो प्रत्यक्ष ही है। फिर इस इन्द्रिय ज्ञान का विश्वास कुछ नहीं क्योंकि इसके द्वारा जाने हुए पदार्थ में संशय विपर्यय और अनध्यवसाय की संभावना है अत: यह दुःख है तथा हेय है किन्तु अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है, स्वाधीन है, इन्द्रियों की अपेक्षा रहित है तथा संशयादि दोषों से रहित है। अतः वह सुखरूप तथा उपादेय है।
विरुद्धं बन्धहेतुत्वाद्बन्धकार्याच्च कर्मजम् ।
अश्रेयोऽनात्मधर्मत्वात् कालुष्याटशुधिः स्वतः ।। १०५१॥ अर्थ-विरुद्ध है क्योंकि बन्ध का कारण है। कर्मज है क्योंकि बंध का कार्य है। अश्रेय है क्योंकि अनात्मधर्म है। अशुचि है क्योंकि स्वयं कलुषित है।
भावार्थ-इन्द्रियज्ञान राग-द्वेष-मोह से मिला रहता है अतः बंध का कारण है। कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है अत:बंध (कर्म) का कार्य है। अकल्याणरूप है क्योंकि अनात्मधर्म है। विभाव को अनात्मधर्म कहते हैं। अपवित्र है क्योंकि काईंवत् राग-द्वेष-मोह से मलिन है। अतः दुःखरूप तथा हेय है किन्तु अतीन्द्रिय ज्ञान बंध का कारण नहीं है क्योंकि राग-द्वेष-मोह से रहित है। बंध का कार्य भी नहीं है क्योंकि कर्म का तो नाश हो चुका है। आत्मा का धर्म है-स्वभाव है। अत: कल्याणरूप है। पवित्र है क्योंकि इसमें राग-द्वेष-मोह की मलीनता नहीं है। अतः सुखरूप तथा उपादेय है।
मूछितं यदपस्मारवेगवदद्वर्द्धमानतः ।
क्षणं वा हीयमानत्वात् क्षणं यावददर्शनात् ॥ १०५२॥ अर्थ-मूच्छित है क्योंकि जो मृगी रोग के वेग के समान बढ़ जाता है, अथवा क्षण भर में घट जाता है अथवा क्षण भर में लोप हो जाता है।
भावार्थ-इन्द्रिय ज्ञान का कुछ भरोसा नहीं। अभ्यास करने पर बढ़ता दीखता है। सर में कोई चोट आ जाने पर या बुढ़ापे में या शरीरक्षीण होने पर घटता-दीखता है और कई बार मस्तिष्क रोग होने या पागल वगैरह होने पर लोप भी हो जाता है। इसका क्या भरोसा। अत: यह दुःखरूप है-हेय है, किन्तु अतीन्द्रियज्ञान न घटता है, न बढ़ता है, न नाश होता है क्योंकि विरोधी के नाश से उत्पन्न हुवा है अतः सुखरूप तथा उपादेय है।
अत्राणं प्रत्यनीकरय क्षणं शान्तस्य कर्मणः । जीवदवस्थातोऽवश्यमेष्यल: स्वरसस्थिति ॥ १०५३||