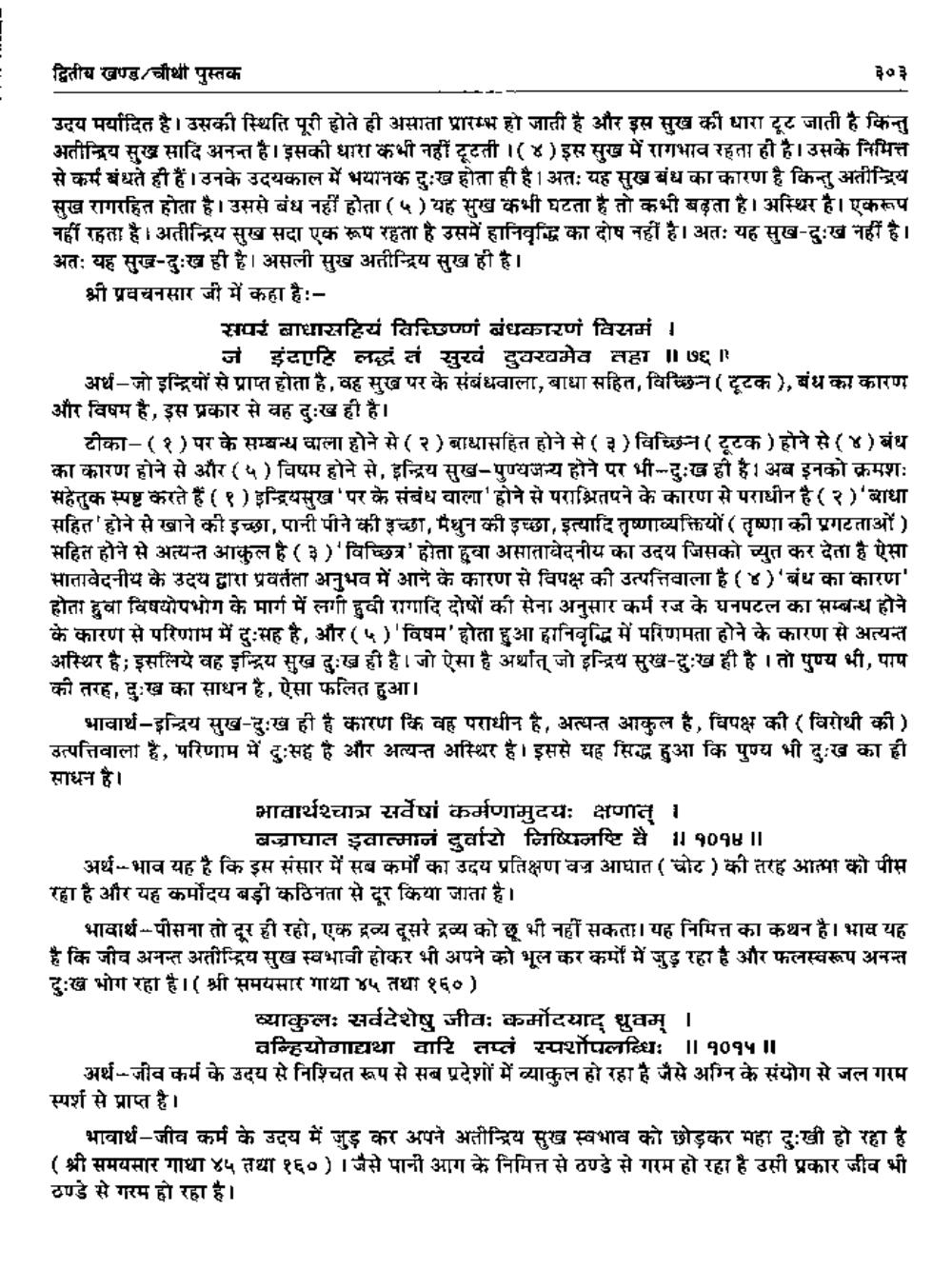________________
द्वितीय खण्ड/चौथी पुस्तक
३०३
उदय मर्यादित है। उसकी स्थिति पूरी होते ही असाता प्रारम्भ हो जाती है और इस सुख की धारा टूट जाती है किन्तु अतीन्द्रिय सुख सादि अनन्त है। इसकी धारा कभी नहीं टूटती । (४) इस सुख में रागभाव रहता ही है। उसके निमित्त से कर्म बंधते ही हैं। उनके उदयकाल में भयानक दुःख होता ही है । अतः यह सुख बंध का कारण है किन्तु अतीन्द्रिय सुख रागरहित होता है। उससे बंध नहीं होता (५)यह सुख कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। अस्थिर है। एकरूप नहीं रहता है। अतीन्द्रिय सुख सदा एक रूप रहता है उसमें हानिवृद्धि का दोष नहीं है। अत: यह सुख-दुःख नहीं है। अत: यह सुख-दुःख ही है। असली सुख अतीन्द्रिय सुख ही है। श्री प्रवचनसार जी में कहा है:
सपरं बाधासहियं विच्छिण्णं बंधकारणं विसमं ।
जं इंटएहि लद्धं तं सुरवं दुवरखमेव तहा ॥७६ ।। अर्थ-जो इन्द्रियों से प्राप्त होता है, वह सुख पर के संबंधवाला, बाधा सहित, विच्छिन्न ( टूटक), बंध का कारण और विषम है, इस प्रकार से वह दुःख ही है।
टीका-(१) पर के सम्बन्ध वाला होने से (२) बाधासहित होने से (३) विच्छिन्ना टूटक ) होने से ( ४ ) बंध का कारण होने से और (५) विषम होने से, इन्द्रिय सुख-पुण्यजन्य होने पर भी दुःख ही है। अब इनको क्रमशः सहेतुक स्पष्ट करते हैं (१) इन्द्रियसुख 'पर के संबंध वाला होने से पराश्रितपने के कारण से पराधीन है (२) बाधा सहित होने से खाने की इच्छा, पानी पीने की इच्छा, मैथुन की इच्छा, इत्यादि तृष्णाव्यक्तियों ( तृष्णा की प्रगटताओं) साहित होने से अत्यन्त आकुल है (३) विच्छित्र' होता हुवा असाताबेदनीय का उदय जिसको च्युत कर देता है ऐसा सातावेदनीय के उदय द्वारा प्रवर्तता अनुभव में आने के कारण से विपक्ष की उत्पत्तिवाला है (४) बंध का कारण' होता हुवा विषयोपभोग के मार्ग में लगी हुवी रागादि दोषों की सेना अनुसार कर्म रज के घनपटल का सम्बन्ध होने के कारण से परिणाम में दुःसह है, और (५) विषम' होता हुआ हानिवृद्धि में परिणमता होने के कारण से अत्यन्त अस्थिर है। इसलिये वह इन्द्रिय सुख दुःख ही है। जो ऐसा है अर्थात् जो इन्द्रिय सुख-दुःख ही है । तो पुण्य भी, पाप की तरह, दुःख का साधन है, ऐसा फलित हुआ।
भावार्थ-इन्द्रिय सुख-दुःख ही है कारण कि वह पराधीन है, अत्यन्त आकुल है, विपक्ष की (विरोथी की) उत्पत्तिवाला है, परिणाम में दुःसह है और अत्यन्त अस्थिर है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पुण्य भी दुःख का ही साधन है।
भावार्थश्चान्न सर्वेषां कर्मणामुदयः क्षणात ।
बज्राघात इवात्मानं दुर्वारो जिष्पिनष्टि वै ॥१०१४ ॥ अर्थ-भाव यह है कि इस संसार में सब कर्मों का उदय प्रतिक्षण वज्र आघात (चोट) की तरह आत्मा को पीस रहा है और यह कर्मोदय बड़ी कठिनता से दूर किया जाता है।
भावार्थ-पीसना तो दूर ही रहो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू भी नहीं सकता। यह निमित्त का कथन है। भाव यह है कि जीव अनन्त अतीन्द्रिय सुख स्वभावी होकर भी अपने को भूल कर कर्मों में जुड़ रहा है और फलस्वरूप अनन्त दुःख भोग रहा है।(श्री समयसार गाथा ४५ तथा १६०)
व्याकुलः सर्वदेशेषु जीवः कर्मोदयाद् ध्रुवम् ।
वन्हियोगाद्यथा वारि तप्तं स्पर्शोपलब्धिः ॥ १०१५।। अर्थ-जीव कर्म के उदय से निश्चित रूप से सब प्रदेशों में व्याकुल हो रहा है जैसे अग्नि के संयोग से जल गरम स्पर्श से प्राप्त है।
भावार्थ-जीव कर्म के उदय में जुड़ कर अपने अतीन्द्रिय सुख स्वभाव को छोड़कर महा दुःखी हो रहा है (श्री समयसार गाथा ४५ तथा १६०)।जैसे पानी आग के निमित्त से ठण्डे से गरम हो रहा है उसी प्रकार जीव भी ठण्डे से गरम हो रहा है।