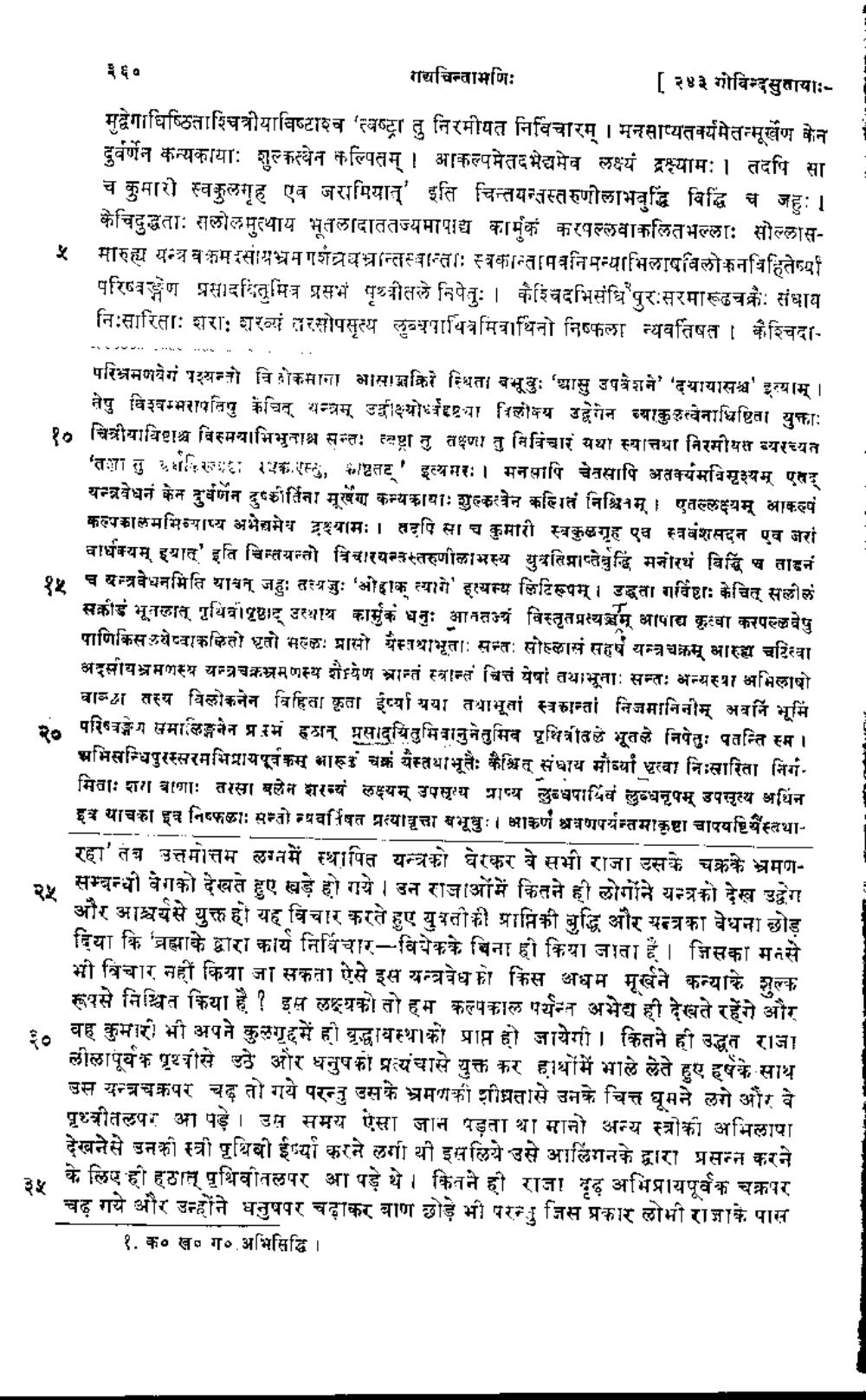________________
५
ܘ܀
रायचिन्तामणिः
[ २४३ गोविन्दसुताया:
मुगाधिष्ठिताश्चित्रीयाविष्टाश्च त्वष्ट्रा तु निरमीयत निर्विचारम् । मनसाप्यतमेतन्मूर्खेण केन दुर्वर्णेन कन्यकायाः शुल्कत्वेन कल्पितम् । आकल्पमेतदभेद्यमेव लक्ष्यं द्रक्ष्यामः । तदपि सा च कुमारी स्वकुलगृह एव जयमियात्' इति चिन्तयन्तस्तरुणीलाभबुद्धिं विद्धि च जहुः । केचिदुद्धताः सलोलमुत्थाय भूतलादाततज्यमापाद्य कार्मुकं करपल्लवाकलितभल्ला: सोल्लासमारुह्य यन्त्र वक्रम दसांयभ्रम भ्रान्तस्वान्ताः स्वकान्तामवनिमन्याभिलाषविलोकनविहितेय परिष्वङ्गेण प्रसादवितुमित्र प्रसभ पृथ्वीतले निपेतुः । कैश्चिदभिसंधि पुरःसरमारूढचक्रः संधाय निःसारिताः शराः शरव्यं तरसोपसृत्य पार्थित्रमित्रार्थिनो निष्फला न्यवर्तिषत । कैश्चिदा
३६०
परिभ्रमणपश्यन्तो विठोकमाना भासानकिरे स्थिता बभूवुः 'यासु उपवेशने' 'दयायासश्च' इत्याम् | तेषु विश्वम्भरापति केचित् यन्त्रम् उद्वीक्ष्योर्ध्वा विलोक्य उद्वेगेन व्याकुलत्वेनाधिष्टिता युक्ताः १० चित्रीयाविशश्व विस्मयाभिभुतान सन्तः स्वष्टा तु वक्ष्णातु निर्विचारं यथा स्यात्तथा निरमीयस व्यरच्यत 'तशा तु विरूपारक. एक कष्टतट्' इत्यमरः । मनसापि चेतसापि अतर्क्यमविसृश्यम् एतद् यन्त्रवेधनं केन दुर्वर्णेन दुष्कीर्तिना मूर्खेण कन्यकायाः शुल्कत्वेन कलितं निश्चिनम् । एतल्लक्ष्यम् आकल्पं कल्पकालमभिव्याप्य अभेद्यमेव द्रक्ष्यामः । तदपि सा च कुमारी स्वकुलगृह एव स्त्रवंशसदन एव जरां वार्धक्यम् इयात्' इति चिन्तयन्तो विचारयन्तस्तरुणीलाभस्य युवतिप्राप्तेर्बुद्धि मनोरथं विद्धि व ताडनं १५ च यन्त्रवेधनमिति यावत् जहुः तस्यजुः 'ओहाक् त्यागे' इत्यस्य लिटिरूपम् । उद्धता गर्दिशः केचित् सलीलं सक्रीडं भूतलात् पृथिवीपृष्ठाद् उत्थाय कार्मुकं धनुः आनतभ्यं विस्तृतप्रत्यञ्चम् आपाद्य कृत्वा करपल्लवेषु पाणिकिस वाकतो तो मकः प्रासो यैस्तथाभूताः सन्तः सोल्लासं सहर्षं यन्त्रचक्रम् आरा चरित्वा अदसीय भ्रमणस्य यन्त्रचक्रभ्रमणस्य शैणि भ्रान्तं स्वान्तं चित्तं येषां तथाभूताः सन्तः अन्यस्था अभिलाषो वादा तस्य विलोकनेन विहिता कृता ईर्ष्या यया तथाभूतां स्वकान्तां निजमानिनीम् अवनिं भूमिं २० परिष्वङ्गे समालिङ्गनेन प्रमं हठात् प्रसादयितुमिवानुनेतुमिव पृथिवीतले भूतले निपेतुः पतन्ति स्म । अभिसन्धिपुरस्सरमभिप्राय पूर्वकम भरूडं चक्रं यैस्तथाभूतैः कैश्चित् संघायमध्य चत्वा निःसारिता निर्ग मिठाः शरा बाणा: तरसा बलेन शरव्यं लक्ष्यम् उपसृत्य प्राप्य लुब्धपार्थिवं लुब्धनृपम् उपसृत्य अर्थिन * याचका इव निष्फळाः सन्तो न्यवर्तिषत प्रत्यावृत्ता बभूवुः । आकर्ण श्रवणपर्यन्तमाकृष्टा चारयष्टिस्तथारहा' तंत्र उत्तमोत्तम लग्न में स्थापित यन्त्रको घेरकर वे सभी राजा उसके चक्र के भ्रमणसम्बन्धी वेगको देखते हुए खड़े हो गये। उन राजाओं में कितने ही लोगोंने यन्त्रको देख उद्वेग और आश्चर्य से युक्त हो यह विचार करते हुए युवती की प्राप्तिकी बुद्धि और यन्त्रका बेधना छोड़ दिया कि 'ब्रह्माके द्वारा कार्य निर्विचार - विवेकके बिना ही किया जाता है। जिसका मनसे भी विचार नहीं किया जा सकता ऐसे इस यन्त्रवेध को किस अधम मूर्खने कन्याके शुल्क रूपसे निश्चित किया है ? इस लक्ष्यको तो हम कल्पकाल पर्यन्त अभेद्य ही देखते रहेंगे और वह कुमारी भी अपने कुलगृह में ही वृद्धावस्थाको प्राप्त हो जायेगी । कितने ही उद्धत राजा पूर्व पृथ्वीसे उठे और धनुषको प्रत्यंचासे युक्त कर हाथोंमें भाले लेते हुए हर्ष के साथ उस यन्त्रचक्रपर चढ़ तो गये परन्तु उसके भ्रमण की शीघ्रता से उनके चित्त घूमने लगे और वे पृथ्वीतलपर आ पड़े। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अन्य स्त्रीकी अभिलाषा देखने से उनकी स्त्री पृथिवी ईर्ष्या करने लगी थी इसलिये उसे आलिंगनके द्वारा प्रसन्न करने के लिए ही हठात् पृथिवीतलपर आ पड़े थे। कितने ही राजा दृढ़ अभिप्रायपूर्वक चक्रपर चढ़ गये और उन्होंने धनुषपर चढ़ाकर बाण छोड़े भी परन्तु जिस प्रकार लोभी राजा के पास
२५
३५
१. क० ख० ग०. अभिसिद्धि ।