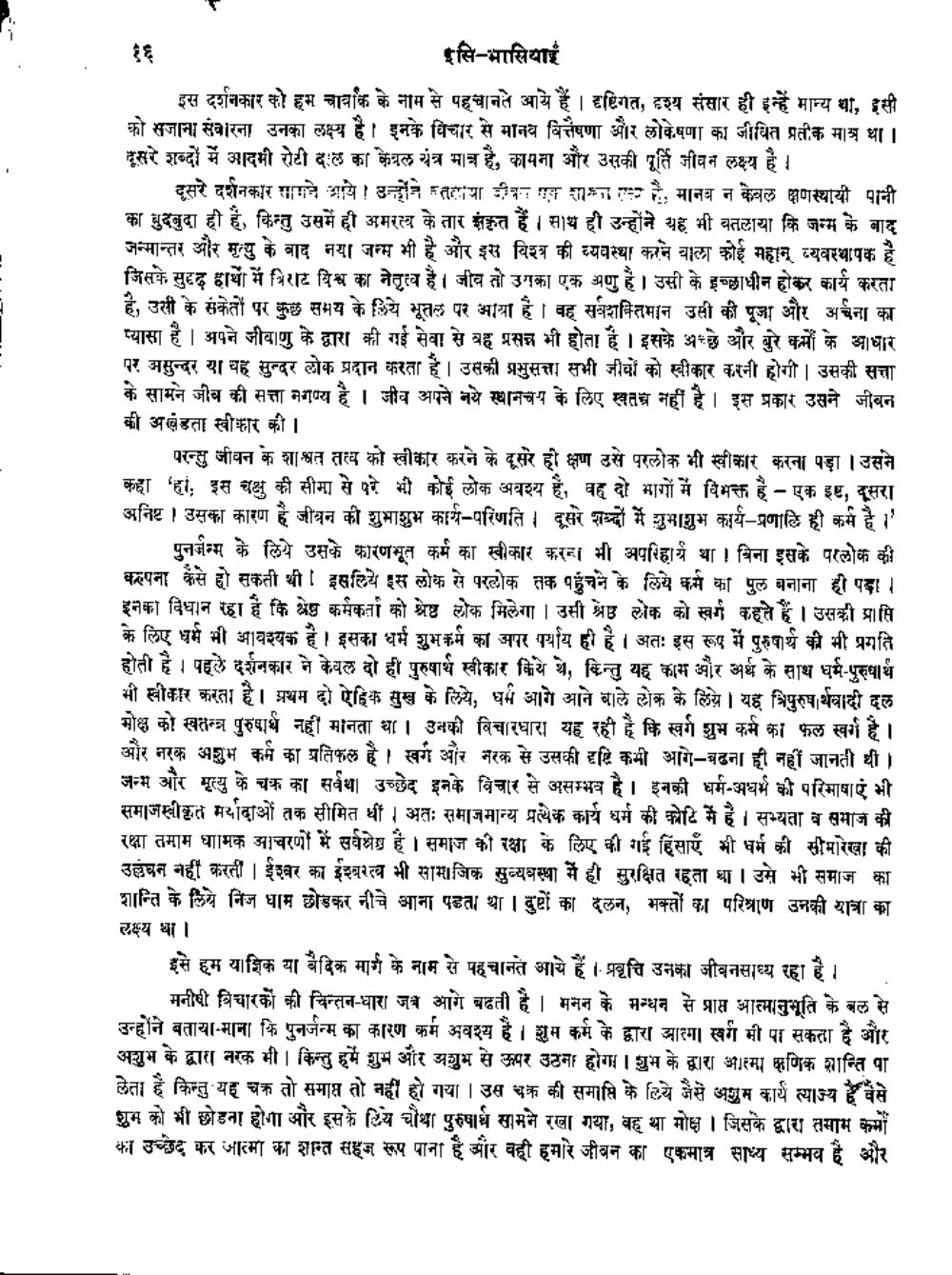________________
इसि-भासियाई इस दर्शनकार को हम चावांक के नाम से पहचानते आये हैं | दृष्टिगत, दृश्य संसार ही इन्हें मान्य था, इसी को सजाना संवारना उनका लक्ष्य है। इनके विचार से मानव वित्तषणा और लोकेषणा का जीवित प्रतीक मात्र था। दूसरे शब्दों में आदमी रोटी दाल का केवल यंत्र मात्र है, कामना और उसकी पूर्ति जीवन लक्ष्य है।
दूसरे दर्शनकार सामने आये। उन्होंने बताया दीवागल शाम है, मानब न केवल क्षणस्थायी पानी का बुदबुदा ही है, किन्तु उसमें ही अमरत्व के तार झंकृत हैं । साथ ही उन्होंने यह भी बतलाया कि जन्म के बाद जन्मान्तर और मृत्यु के बाद नया जन्म भी है और इस विश्त्र की व्यवस्था करने वाला कोई महान् व्यवस्थापक है जिसके सुदृढ़ हाथों में विराट विश्व का नेतृत्व है। जीव तो उगका एक अणु है। उसी के इच्छाधीन होकर कार्य करता है, उसी के संकेतों पर कुछ समय के लिये भूतल पर आया है। वह सर्वशक्तिमान उसी की पूजा और अर्चना का प्यासा है । अपने जीवाणु के द्वारा की गई सेवा से यह प्रसन्न भी होता है । इसके अछे और बुरे कर्मों के आधार पर असुन्दर या वह सुन्दर लोक प्रदान करता है। उसकी प्रभुसत्ता सभी जीवों को स्वीकार करनी होगी। उसकी सत्ता के सामने जीव की सत्ता नगण्य है । जीव अपने नये स्थानचय के लिए स्वतन्त्र नहीं है। इस प्रकार उसने जीवन की अखंडता स्वीकार की।
परन्तु जीवन के शाश्वत तत्व को स्वीकार करने के दूसरे ही क्षण उसे परलोक भी स्वीकार करना पड़ा । उसने कहा 'हां, इस चक्षु की सीमा से परे भी कोई लोक अवश्य हैं, वह दो भागों में विभक्त है - एक इष्ट, दूसरा अनिष्ट । उसका कारण है जीवन की शुभाशुभ कार्य-परिणति । दूसरे शब्दों में शुभाशुभ कार्य-प्रणालि ही कर्म है ।'
पुनर्जन्म के लिये उसके कारणभूत कर्म का स्वीकार करना भी अपरिहार्य था। बिना इसके परलोक की कल्पना कैसे हो सकती थी। इसलिये इस लोक से परलोक तक पहुंचने के लिये कर्म का पुल बनाना ही पड़ा । इनका विधान रहा है कि श्रेष्ठ कर्मकर्ता को श्रेष्ठ लोक मिलेगा । उसी श्रेष्ठ लोक को स्वर्ग कहते हैं । उसकी प्राप्ति के लिए धर्म भी आवश्यक है। इसका धर्म शुभकर्म का अपर पर्याय ही है । अतः इस रूप में पुरुषार्थ की भी प्रगति होती है । पहले दर्शनकार ने केवल दो ही पुरुषार्थ स्वीकार किये थे, किन्तु यह काम और अर्थ के साथ धर्म-पुरुषार्थ भी स्वीकार करता है। प्रथम दो ऐहिक सुख के लिये, धर्म आगे आने वाले लोक के लिये । यह त्रिपुरुषार्थवादी दल मोक्ष को खतन्त्र पुरुषार्थ नहीं मानता था। उनकी विचारधारा यह रही है कि स्वर्ग शुभ कर्म का फल स्वर्ग है। और नरक अशुभ कर्म का प्रतिफल है। स्वर्ग और नरक से उसकी दृष्टि कमी आगे-बढना ही नहीं जानती थी। जन्म और मृत्यु के चक्र का सर्वथा उच्छेद इनके विचार से असम्भव है। इनकी धर्म-अधर्म की परिभाषाएं भी समाजस्वीकृत मर्यादाओं तक सीमित थीं। अतः समाजमान्य प्रत्येक कार्य धर्म की कोटि में है। सभ्यता व समाज की रक्षा तमाम धाामक आचरणों में सर्वश्रेष्ठ है। समाज की रक्षा के लिए की गई हिंसाएँ भी धर्म की सीमारेखा की उलंघन नहीं करती । ईश्वर का ईश्वरत्व भी सामाजिक सुव्यवस्था में ही सुरक्षित रहता था । उमे भी समाज का शान्ति के लिये निज धाम छोडकर नीचे आना पडता था । दुष्टों का दलन, भक्तों का परित्राण उनकी यात्रा का लक्ष्य था।
इसे हम याशिक या बैदिक मार्ग के नाम से पहचानते आये हैं । प्रवृचि उनका जीवनसाध्य रहा है ।
मनीषी विचारकों की चिन्तन-धार। जब आगे बढ़ती है। मनन के मन्धन से प्राप्त आत्मानुभूति के बल से उन्होंने बताया-माना कि पुनर्जन्म का कारण कम अवश्य है । शुम कर्म के द्वारा आत्मा स्वर्ग मी पा सकता है और अशुभ के द्वारा नरक भी | किन्तु हमें शुभ और अशुभ से ऊपर उठना होगा । शुभ के द्वारा आत्मा झाणिक शान्ति पा लेता है किन्तु यह चक्र तो समाप्त तो नहीं हो गया । उस चक्र की समाप्ति के लिये जैसे अशुम कार्य त्याज्य है वैसे शुभ को भी छोडना होगा और इसके लिय चौथा पुरुषार्थ सामने रखा गया, वह था मोक्ष । जिसके द्वारा तमाम कों का उच्छेद कर आत्मा का शान्त सहज रूप पाना है और वही हमारे जीवन का एकमात्र साध्य सम्भव है और