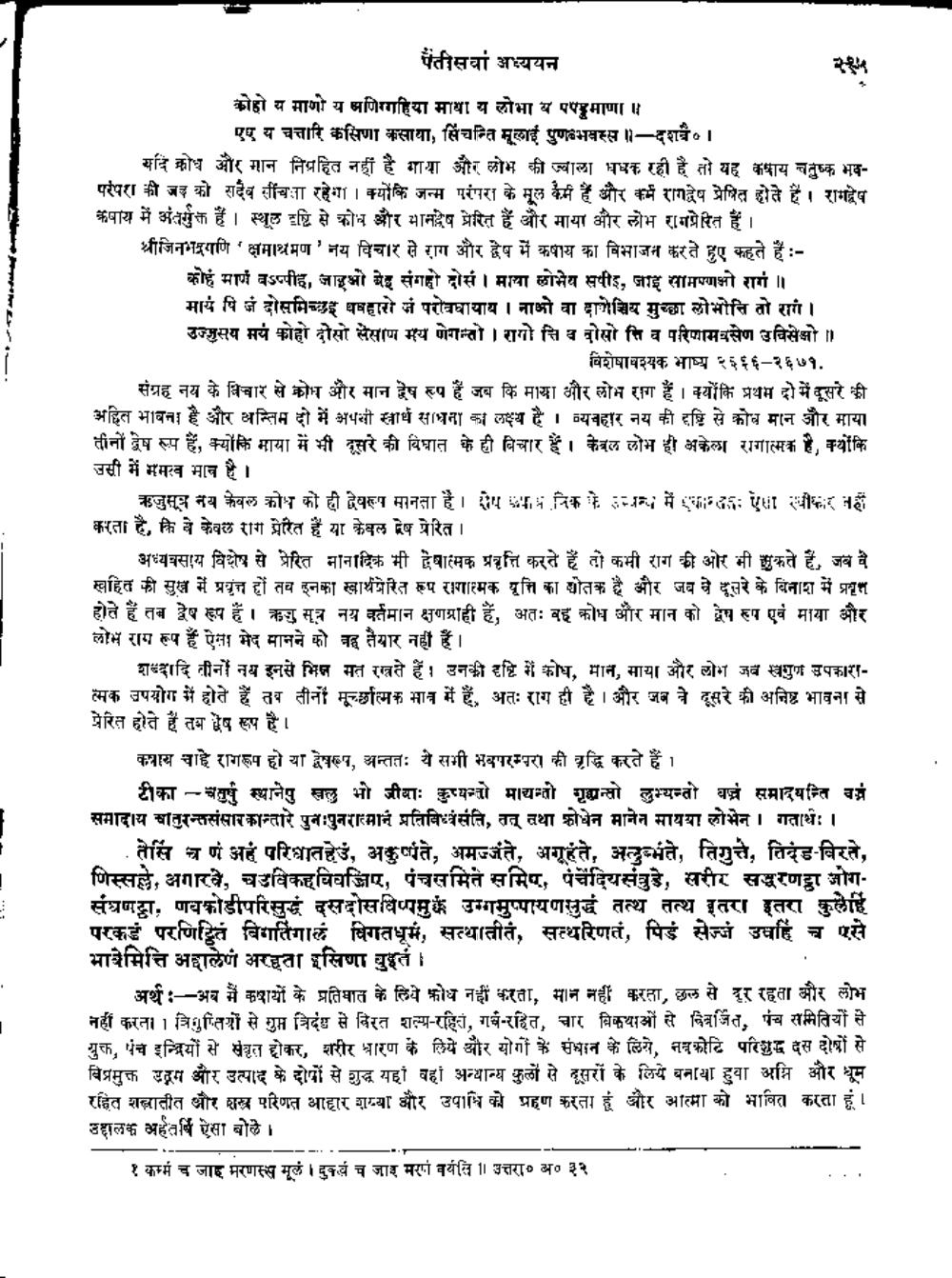________________
पैतीसवां अध्ययन कोहो य माणो य मणिग्गहिया माया य लोभा व पपमाणा ।।
एए य चत्तारि कसिणा कसाया, सिंचन्ति मूलाई पुणभवस्स-दशबैक। यदि क्रोध और मान निग्रहित नहीं है गाया और लोभ की ज्वाला धधक रही है तो यह कयाय चतुष्क भवपरंपरा की जड़ को सदैव सींचना रहेगा। क्योंकि जन्म परंपरा के मूल कैम हैं और कर्म रागद्वेष प्रेषित होते है। रामद्वेष ऋषाय में अंतमुक्त हैं। स्थूल दृष्टि से कोच और मानदेष प्रेरित हैं और माया और लोभ रामप्रेरित हैं। श्रीजिनभमुगणि 'क्षमाश्रमण'नय विचार से राग और द्वेष में कषाय का विभाजन करते हुए कहते है :
कोहं मार्ण वऽप्पीह, जाइओ बेह संगहो दोसं । माया लोभेय सपीइ, जाइ सामपणो राग । माय पिजं दोसमिच्छ धबहारो परोवघायाय । नाओ वा दाणेचिय मुख्छा लोमोति तो राग । उज्मुसय मयं कोहो दोसो सेसाण मय गन्तो। रागो तिव वोसो ति व परिणामबसेण उविसेको।
विशेषावश्यक भाष्य २६६६-२६७१. संग्रह नय के विचार से क्रोध और मान द्वेष रूप है जब कि माया और लोभ राग हैं। क्योंकि प्रथम दो में दूसरे की अहित भावना है और अन्तिम दो में अपनी स्वार्थ साधना का लक्ष्य है । व्यवहार नय की दृष्टि से कोष मान और माया तीनों द्वेष रूप हैं, क्योंकि माया में भी दूसरे की विघात के ही विचार है। केवल लोभ ही अकेला रागात्मक है, क्योंकि उसी में ममत्व भाव है।
ऋजुसूत्र नय केवल क्रोध को ही द्वेयरूप मानता है। पानिकके जन्म में कान्ताः एमा स्वीकार नहीं करता है, कि वे केवल राग प्रेरित है या केवल देष प्रेरित ।
अध्यवसाय विशेष से प्रेरित मानादिक भी द्वेषात्मक प्रवृत्ति करते हैं तो कमी राग की ओर भी सकते है, जब वे स्वहित की सुख में प्रयुक्त हों तब इनका स्वार्थप्रेरित रूप रागात्मक यूति का योतक है और जब वे दूसरे के विनाश में प्रवृत होते हैं तब द्वेष रूप है। ऋजु सूत्र नय वर्तमान क्षणग्राही हैं, अतः वह क्रोध और मान को द्वेष रूप एवं माया और लोभ राग रूप हैं ऐला भेद मानने को वह तैयार नहीं हैं।
शब्दादि वीनों नय इनसे भिन्न मत रखते हैं। उनकी दृष्टि में कोध, मान, माया और लोभ जव स्वगुण उपकारसत्मक उपयोग में होते हैं तब तीनो मूत्मिक मात्र में हैं, अतः राग ही है । और जब वे दूसरे की अनिष्ट भावना से प्रेरित होते हैं तम धेष रूप है।
कराय चाहे रागरूप हो या द्वेषरूप, अन्ततः ये सभी भवपरम्परा की वृद्धि करते हैं।
टीका - सुषु स्थानेषु स्खलु भो जीयाः कुष्यन्तो माद्यन्तो गृह्यन्तो लुभ्यन्तो बज्र समादयन्ति वन समादाय चातुरन्तसंसारकान्तारे पुन:पुनरात्मानं प्रतिविध्वंसंति, तत् तथा क्रोधेन मानेन मायया लोभेन । गताः । .. तेसि च णं अहं परिधातहेर्ड, अकुर्णते, अमज्जते, अगृहंते, अलुम्भंते, तिगुत्ते, तिदंड-विरते, णिस्सल्ले, अगारवे, चउविकविजिए, पंचसमिते समिप, पंचेंदियसंवुडे, सरीर सद्धरणट्ठा जोगसंघणट्ठा, णयकोडीपरिसुद्धं दसदोसधिष्पमुक उम्गमुप्पायणलुद्धं तत्थ तत्थ इतरा इतरा कुलेहि परकर्ड परणिहितं विगतिंगालं विगतधूम, सत्थातीतं, सत्थरिणतं, पिई सेज्ज उचाहिं च एसे भावमित्ति अहालेणं अरहता इसिणा बुइतं ।।।
अर्थ:-अब मैं कषायों के प्रतियात के लिये क्रोध नहीं करता, मान नहीं करता, छल से दूर रहता और लोभ नहीं करता । त्रिपितरों से गुप्त त्रिदंष्ट से विरत शल्प-रहित, गर्ब-रहित, चार विकथाओं से विवर्जित, पंच समितियों से युक्त, पंच इन्द्रियों से सेवृत होकर, शरीर धारण के लिये और योगों के संधान के लिये, नवकोटि परिशुद्ध दस दोषों से विप्रमुक्त उद्रम और उत्पाद के दोषों से शुद्ध यहां वहां अन्यान्य कुलों से दूसरों के लिये बनाया हुवा अग्नि और धूम रहित शलातीत और शस्त्र परिणत आहार शय्या और उपाधि को प्रहण करता हूं और आत्मा को भावित करता हूं। उहालक अहंतर्षि ऐसा बोले ।
१ कर्म च जाह मरणस्स मूलं । दुखं च जाइ मरण वयति ।। उत्तरा० अ०३२