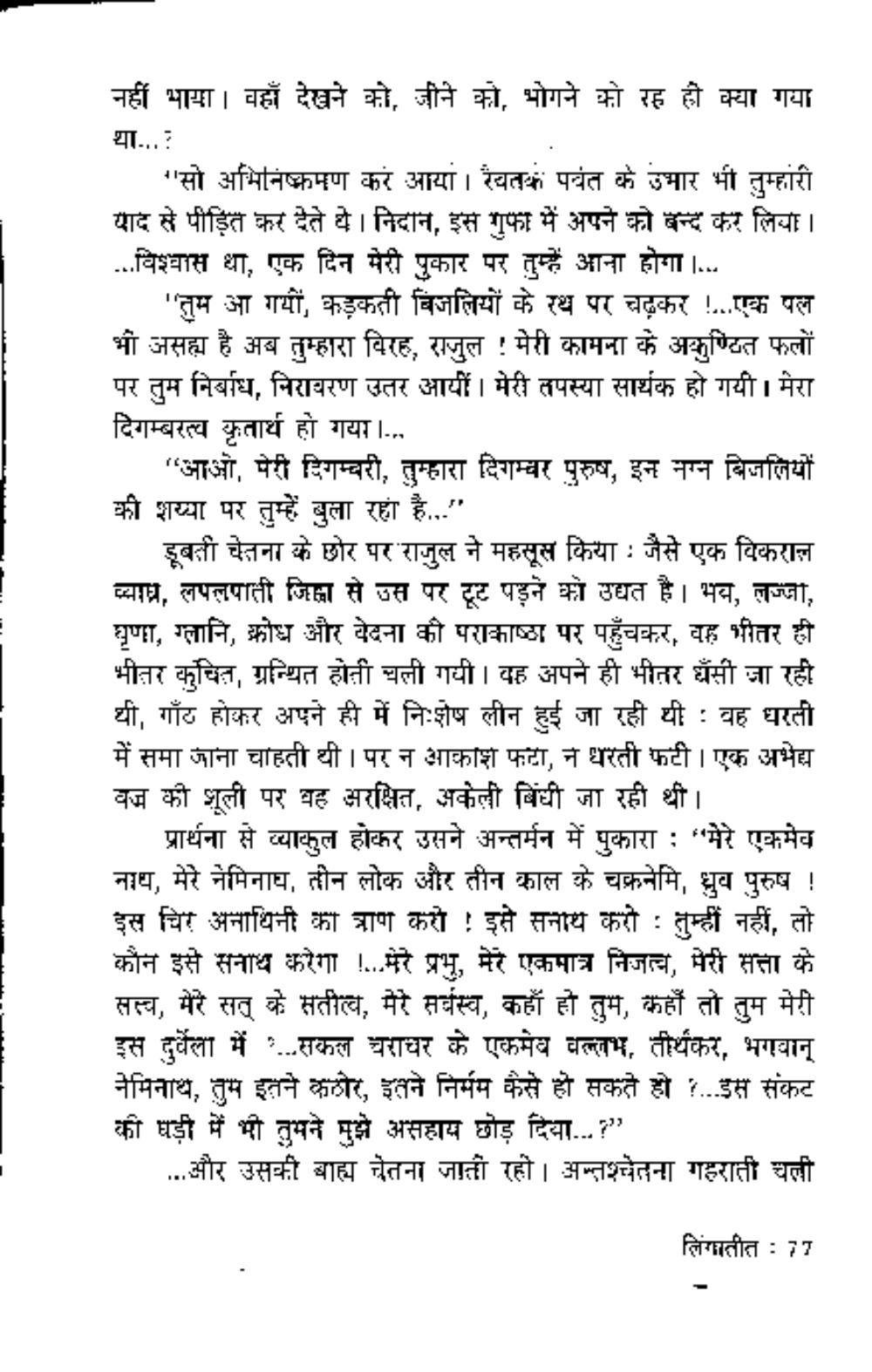________________
नहीं भाया। वहाँ देखने को, जीने को भोगने को रह हो क्या गया था...
"सो अभिनिष्क्रमण कर आया। रैवतकं पर्वत के उभार भी तुम्हारी याद से पीड़ित कर देते थे। निदान, इस गुफा में अपने को बन्द कर लिया । ... विश्वास था, एक दिन मेरी पुकार पर तुम्हें आना होगा ।....
"तुम आ गयीं, कड़कती बिजलियों के रथ पर चढ़कर !...एक पल भी असह्य है अब तुम्हारा विरह, राजुल ! मेरी कामना के अकुण्ठित फलों पर तुम निर्बाध, निरावरण उतर आयीं। मेरी तपस्या सार्थक हो गयी। मेरा दिगम्बरत्व कृतार्थ हो गया । ....
"आओ, मेरी दिगम्बरी, तुम्हारा दिगम्बर पुरुष, इन नग्न बिजलियों की शय्या पर तुम्हें बुला रहा है..."
:
डूबती चेतना के छोर पर राजुल ने महसूस किया जैसे एक विकराल व्याघ्र, लपलपाती जिह्वा से उस पर टूट पड़ने को उद्यत है । भव, लज्जा, घृणा, ग्लानि, क्रोध और वेदना की पराकाष्ठा पर पहुँचकर वह भीतर ही भीतर कुचित, ग्रन्थित होती चली गयी। वह अपने ही भीतर धँसी जा रही थी, गाँठ होकर अपने ही में निःशेष लीन हुई जा रही थी : वह धरती में समा जाना चाहती थी। पर न आकाश फटा, न धरती फटी एक अभेद्य वज्र की शूली पर वह अरक्षित, अकेली बिंधी जा रही थी ।
I
प्रार्थना से व्याकुल होकर उसने अन्तर्मन में पुकारा: "मेरे एकमेव नाथ, मेरे नेमिनाथ, तीन लोक और तीन काल के चक्रनेमि, ध्रुव पुरुष ! इस चिर अनाधिनी का त्राण करो इसे सनाथ करो तुम्हीं नहीं, तो कौन इसे सनाथ करेगा !...मेरे प्रभु, मेरे एकमात्र निजत्व, मेरी सत्ता के सत्त्व, मेरे सत् के सतीत्व, मेरे सर्वस्व कहाँ हो तुम, कहाँ तो तुम मेरी इस दुर्वेला में ... सकल चराचर के एकमेव वल्लभ, तीर्थकर, भगवान् नेमिनाथ, तुम इतने कठोर, इतने निर्मम कैसे हो सकते हो ?इस संकट की घड़ी में भी तुमने मुझे असहाय छोड़ दिया... ?”
·
... और उसकी बाह्य चेतना जाती रही। अन्तश्चेतना गहराती चली
लिंगातीत 77