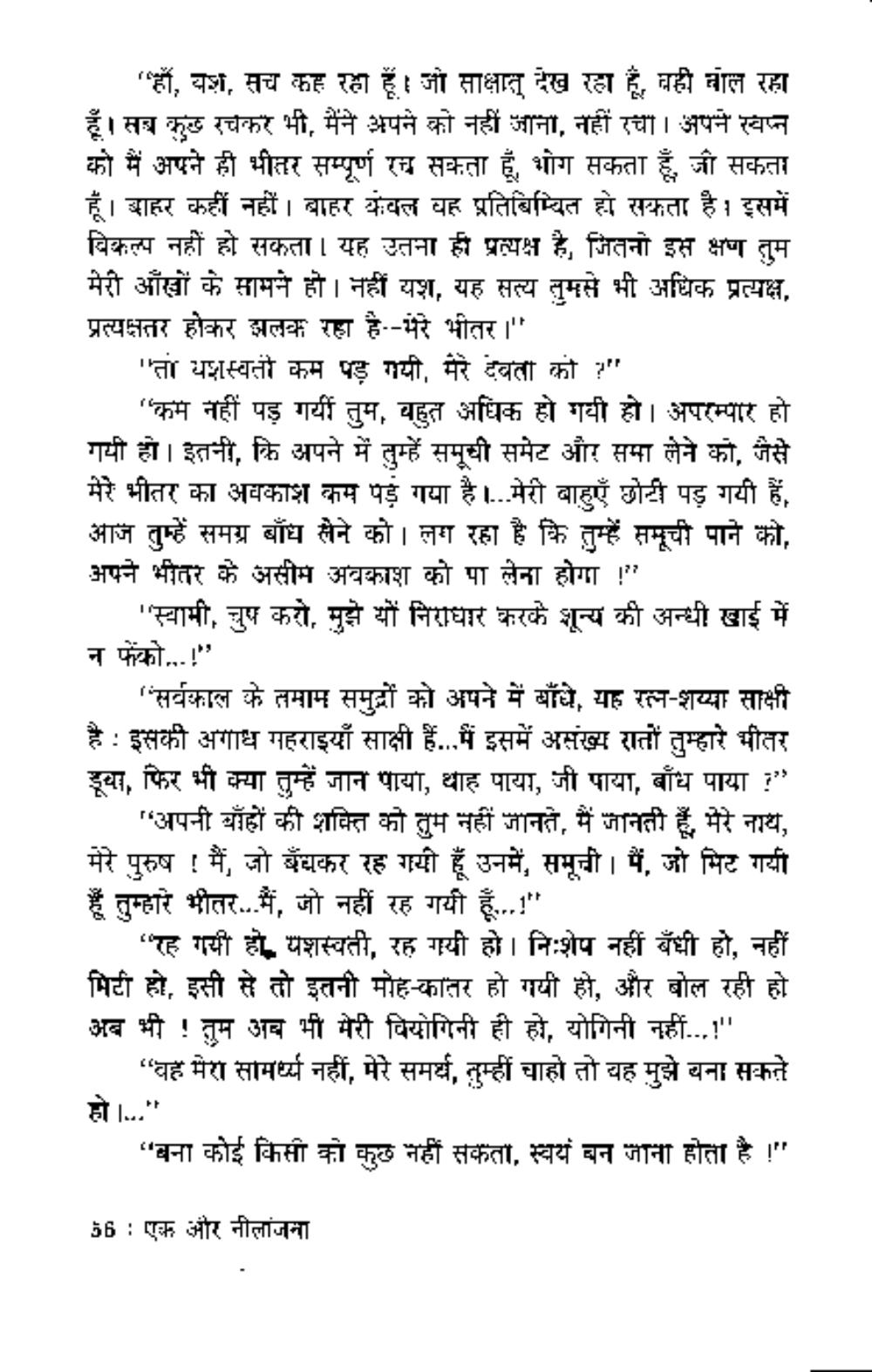________________
"हाँ, यश, सच कह रहा हूँ। जो साक्षात् देख रहा हूँ, वही बोल रहा
r
हूँ। सब कुछ रचकर भी मैंने अपने को नहीं जाना नहीं रचा। अपने स्वप्न को मैं अपने ही भीतर सम्पूर्ण रच सकता हूँ, भोग सकता हूँ, जी सकता हूँ। बाहर कहीं नहीं। बाहर केवल वह प्रतिबिम्बित हो सकता है। इसमें विकल्प नहीं हो सकता। यह उतना ही प्रत्यक्ष है, जितनी इस क्षण तुम मेरी आँखों के सामने हो । नहीं यश, यह सत्य तुमसे भी अधिक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षतर होकर झलक रहा है मेरे भीतर ।"
"तो यशस्वती कम पड़ गयी, मेरे देवता को "
P
"कम नहीं पड़ गयीं तुम बहुत अधिक हो गयी हो। अपरम्पार हो गयी हो। इतनी कि अपने में तुम्हें समूची समेट और समा लेने को, जैसे मेरे भीतर का अवकाश कम पड़ गया है।... मेरी बाहुएँ छोटी पड़ गयी हैं, आज तुम्हें समग्र बाँध लेने को लग रहा है कि तुम्हें समूची पाने को, अपने भीतर के असीम अवकाश को पा लेना होगा !"
"स्वामी, चुप करो, मुझे यों निराधार करके शून्य की अन्धी खाई में न फेंको...!"
"सर्वकाल के तमाम समुद्रों को अपने में बाँधे, यह रत्न - शय्या साक्षी है: इसकी अगाध गहराइयाँ साक्षी हैं... मैं इसमें असंख्य रातों तुम्हारे भीतर डूबा, फिर भी क्या तुम्हें जान पाया, थाह पाया, जी पाया, बाँध पाया ?" "अपनी बाँहों की शक्ति को तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ, मेरे नाथ, मेरे पुरुष ! मैं, जो बँचकर रह गयी हूँ उनमें समूची में जो मिट गयी हूँ तुम्हारे भीतर... मैं, जो नहीं रह गयी हूँ...!"
I
"रह गयी हो यशस्वती, रह गयी हो। निःशेष नहीं बँधी हो, नहीं मिटी हो, इसी से तो इतनी मोह-कातर हो गयी हो, और बोल रही हो अब भी ! तुम अब भी मेरी वियोगिनी ही हो, योगिनी नहीं...!" "वह मेरा सामर्थ्य नहीं, मेरे समर्थ, तुम्हीं चाहो तो यह मुझे बना सकते हो ।... "
"बना कोई किसी को कुछ नहीं सकता, स्वयं बन जाना होता है !"
56 एक और नीलांजना