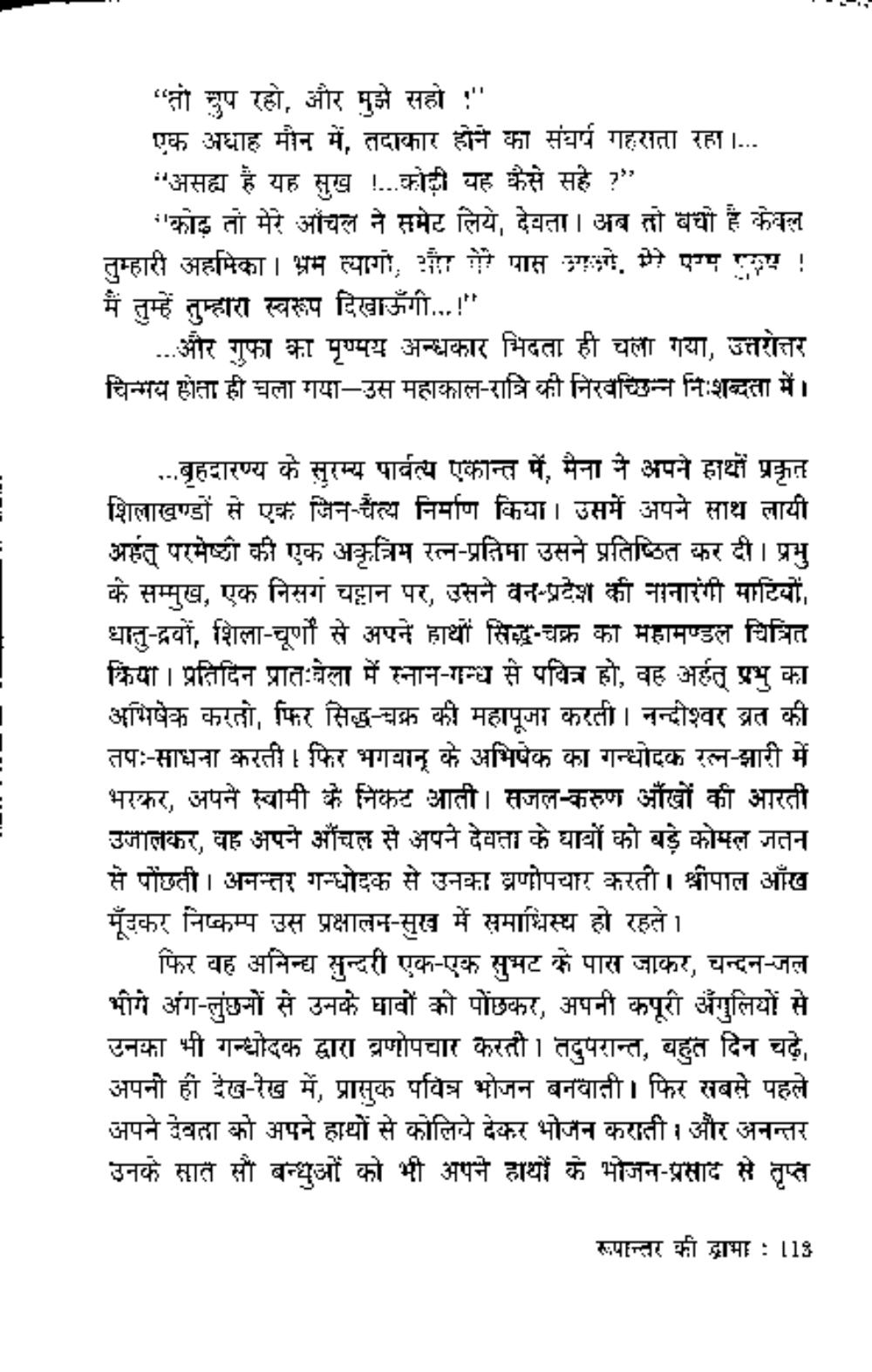________________
"तो चुप रहो, और मुझे सहो !" एक अधाह मौन में, तदाकार होने का संघर्ष गहराता रहा।... "असह्य है यह सुख !...कोड़ी यह कैसे सहे ?"
'कोड़ तो मेरे आंचल ने समेट लिये, देवता । अब तो बचो हैं केवल तुम्हारी अहमिका । भ्रम त्यागी, और मेरे पास आगे भी एग्म पाप ! मैं तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिखाऊँगी...!" ।
...और गुफा का पृण्मय अन्धकार भिदता ही चला गया, उत्तरोत्तर चिन्मय होता ही चला गया-उस महाकाल-रात्रि की निरवच्छिन्न निःशब्दता में।
...बृहदारण्य के सुरम्य पार्वत्य एकान्त में, मैना ने अपने हाथों प्रकृत शिलाखण्डों से एक जिन-चैत्य निर्माण किया। उसमें अपने साथ लायी अहंत परमेष्ठी की एक अकृत्रिम रत्न-प्रतिमा उसने प्रतिष्ठित कर दी। प्रभु के सम्मुख, एक निसगं चट्टान पर, उसने वन-प्रदेश की नानारंगी माटियों, धातु-द्रवों, शिला-चूर्गों से अपने हाथों सिद्ध-चक्र का महामण्डल चित्रित किया। प्रतिदिन प्रातःबेला में स्नान-गन्ध से पवित्र हो, वह अर्हत् प्रभु का
अभिषेक करतो, फिर सिद्ध-चक्र की महापूजा करती। नन्दीश्वर ब्रत की तपः-साधना करती। फिर भगवान के अभिषेक का गन्धोदक रन-झारी में भरकर, अपने स्वामी के निकट आती। सजल-करुण आँखों की आरती उजालकर, वह अपने आँचल से अपने देवता के घावों को बड़े कोपल जतन से पोंछती। अनन्तर गन्धोदक से उनका प्रणोपचार करती। श्रीपाल आँख मूंडकर निष्कम्प उस प्रक्षालन-सुख में समाधिस्थ हो रहते। ___ फिर वह अनिन्द्य सुन्दरी एक-एक सुमट के पास जाकर, चन्दन-जल भीगे अंग-लुंछनों से उनके घावों को पोंछकर, अपनी कपूरी अँगुलियों से उनका भी गन्धोदक द्वारा व्रणोपचार करती । तदुपरान्त, बहुत दिन चढ़े, अपनी ही देख-रेख में, प्रासक पवित्र भोजन बनवाती। फिर सबसे पहले अपने देवता को अपने हाथों से कोलिये देकर भोजन कराती । और अनन्तर उनके सात सौ बन्धुओं को भी अपने हाथों के भोजन-प्रसाद से तृप्त
रूपान्तर की द्रामा : [13