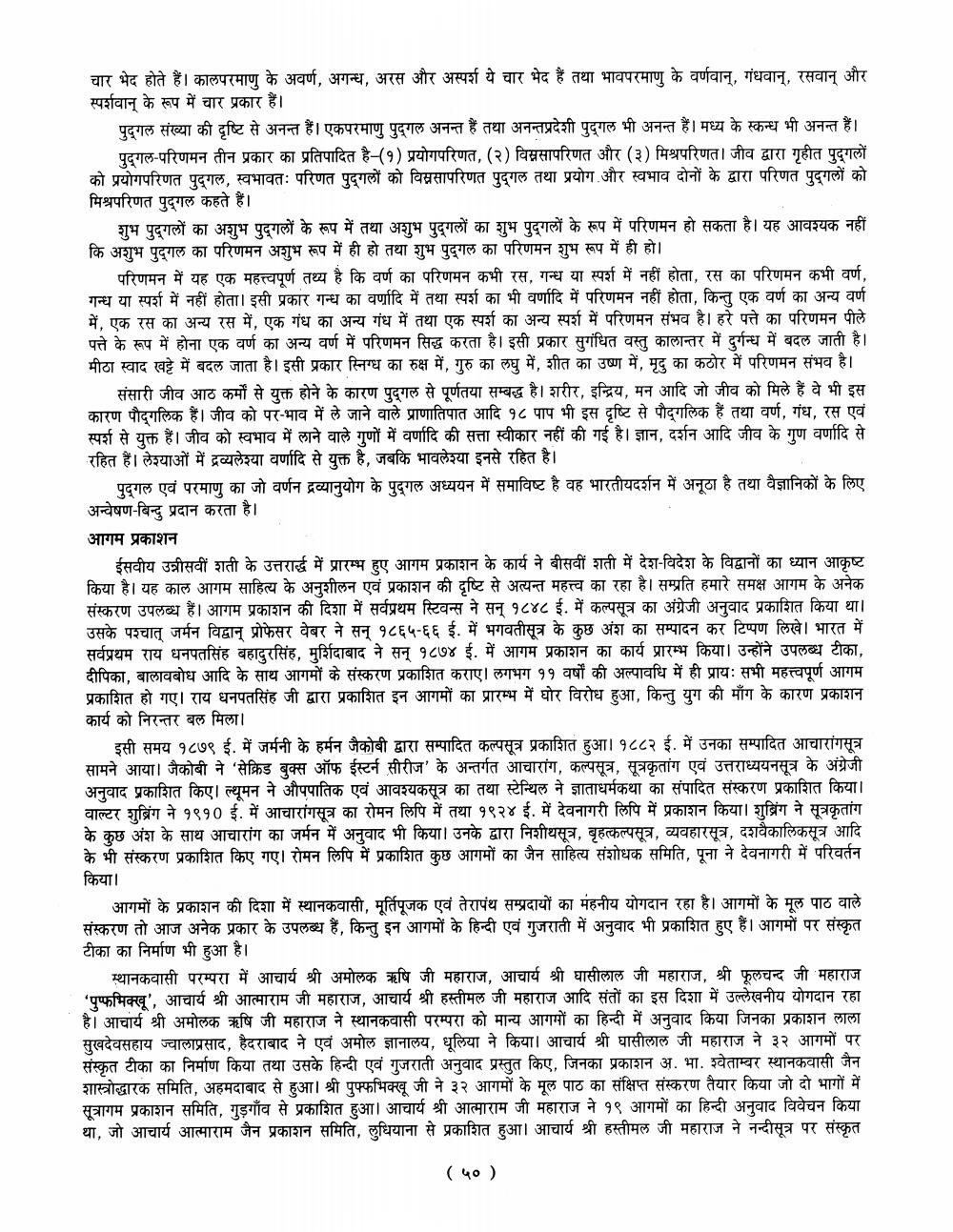________________
चार भेद होते हैं। कालपरमाणु के अवर्ण, अगन्ध, अरस और अस्पर्श ये चार भेद हैं तथा भावपरमाणु के वर्णवान्, गंधवान्, रसवान् और स्पर्शवान् के रूप में चार प्रकार हैं।
पुद्गल संख्या की दृष्टि से अनन्त हैं। एकपरमाणु पुद्गल अनन्त हैं तथा अनन्तप्रदेशी पुद्गल भी अनन्त हैं। मध्य के स्कन्ध भी अनन्त हैं।
पुद्गल-परिणमन तीन प्रकार का प्रतिपादित है-(१) प्रयोगपरिणत, (२) विनसापरिणत और (३) मिश्रपरिणत। जीव द्वारा गृहीत पुद्गलों को प्रयोगपरिणत पुद्गल, स्वभावतः परिणत पुद्गलों को विनसापरिणत पुद्गल तथा प्रयोग और स्वभाव दोनों के द्वारा परिणत पुद्गलों को मिश्रपरिणत पुद्गल कहते हैं।
शुभ पुद्गलों का अशुभ पुद्गलों के रूप में तथा अशुभ पुद्गलों का शुभ पुद्गलों के रूप में परिणमन हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि अशुभ पुद्गल का परिणमन अशुभ रूप में ही हो तथा शुभ पुद्गल का परिणमन शुभ रूप में ही हो।
परिणमन में यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि वर्ण का परिणमन कभी रस, गन्ध या स्पर्श में नहीं होता, रस का परिणमन कभी वर्ण, गन्ध या स्पर्श में नहीं होता। इसी प्रकार गन्ध का वर्णादि में तथा स्पर्श का भी वर्णादि में परिणमन नहीं होता, किन्तु एक वर्ण का अन्य वर्ण में, एक रस का अन्य रस में, एक गंध का अन्य गंध में तथा एक स्पर्श का अन्य स्पर्श में परिणमन संभव है। हरे पत्ते का परिणमन पीले पत्ते के रूप में होना एक वर्ण का अन्य वर्ण में परिणमन सिद्ध करता है। इसी प्रकार सुगंधित वस्तु कालान्तर में दुर्गन्ध में बदल जाती है। मीठा स्वाद खट्टे में बदल जाता है। इसी प्रकार स्निग्ध का रुक्ष में, गुरु का लघु में, शीत का उष्ण में, मृदु का कठोर में परिणमन संभव है। ___ संसारी जीव आठ कर्मों से युक्त होने के कारण पुद्गल से पूर्णतया सम्बद्ध है। शरीर, इन्द्रिय, मन आदि जो जीव को मिले हैं वे भी इस कारण पौद्गलिक हैं। जीव को पर-भाव में ले जाने वाले प्राणातिपात आदि १८ पाप भी इस दृष्टि से पौद्गलिक हैं तथा वर्ण, गंध, रस एवं स्पर्श से युक्त हैं। जीव को स्वभाव में लाने वाले गुणों में वर्णादि की सत्ता स्वीकार नहीं की गई है। ज्ञान, दर्शन आदि जीव के गुण वर्णादि से रहित हैं। लेश्याओं में द्रव्यलेश्या वर्णादि से युक्त है, जबकि भावलेश्या इनसे रहित है।
पुद्गल एवं परमाणु का जो वर्णन द्रव्यानुयोग के पुद्गल अध्ययन में समाविष्ट है वह भारतीयदर्शन में अनूठा है तथा वैज्ञानिकों के लिए अन्वेषण-बिन्दु प्रदान करता है। आगम प्रकाशन
ईसवीय उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में प्रारम्भ हुए आगम प्रकाशन के कार्य ने बीसवीं शती में देश-विदेश के विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है। यह काल आगम साहित्य के अनुशीलन एवं प्रकाशन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व का रहा है। सम्प्रति हमारे समक्ष आगम के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। आगम प्रकाशन की दिशा में सर्वप्रथम स्टिवन्स ने सन् १८४८ ई. में कल्पसूत्र का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था। उसके पश्चात् जर्मन विद्वान् प्रोफेसर वेबर ने सन् १८६५-६६ ई. में भगवतीसूत्र के कुछ अंश का सम्पादन कर टिप्पण लिखे। भारत में सर्वप्रथम राय धनपतसिंह बहादुरसिंह, मुर्शिदाबाद ने सन् १८७४ ई. में आगम प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने उपलब्ध टीका, दीपिका, बालावबोध आदि के साथ आगमों के संस्करण प्रकाशित कराए। लगभग ११ वर्षों की अल्पावधि में ही प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण आगम प्रकाशित हो गए। राय धनपतसिंह जी द्वारा प्रकाशित इन आगमों का प्रारम्भ में घोर विरोध हुआ, किन्तु युग की माँग के कारण प्रकाशन कार्य को निरन्तर बल मिला।
इसी समय १८७९ ई. में जर्मनी के हर्मन जैकोबी द्वारा सम्पादित कल्पसूत्र प्रकाशित हुआ। १८८२ ई. में उनका सम्पादित आचारांगसूत्र सामने आया। जैकोबी ने 'सेक्रिड बुक्स ऑफ ईस्टर्न सीरीज' के अन्तर्गत आचारांग, कल्पसूत्र, सूत्रकृतांग एवं उत्तराध्ययनसूत्र के अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किए। ल्यूमन ने औपपातिक एवं आवश्यकसूत्र का तथा स्टेन्थिल ने ज्ञाताधर्मकथा का संपादित संस्करण प्रकाशित किया। वाल्टर शुब्रिग ने १९१० ई. में आचारांगसूत्र का रोमन लिपि में तथा १९२४ ई. में देवनागरी लिपि में प्रकाशन किया। शुब्रिग ने सूत्रकृतांग के कुछ अंश के साथ आचारांग का जर्मन में अनुवाद भी किया। उनके द्वारा निशीथसूत्र, बृहत्कल्पसूत्र, व्यवहारसूत्र, दशवैकालिकसूत्र आदि के भी संस्करण प्रकाशित किए गए। रोमन लिपि में प्रकाशित कुछ आगमों का जैन साहित्य संशोधक समिति, पूना ने देवनागरी में परिवर्तन किया।
आगमों के प्रकाशन की दिशा में स्थानकवासी, मूर्तिपूजक एवं तेरापंथ सम्प्रदायों का महनीय योगदान रहा है। आगमों के मूल पाठ वाले संस्करण तो आज अनेक प्रकार के उपलब्ध हैं, किन्तु इन आगमों के हिन्दी एवं गुजराती में अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। आगमों पर संस्कृत
संस्करण तानमाण भी हुआ है।
श्री अमोलक ऋषि का हस्तीमल जी महाराज का हिन्दी में अनुवात
स्थानकवासी परम्परा में आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज, आचार्य श्री घासीलाल जी महाराज, श्री फूलचन्द जी महाराज 'पुष्फभिक्खू', आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज आदि संतों का इस दिशा में उल्लेखनीय योगदान रहा है। आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज ने स्थानकवासी परम्परा को मान्य आगमों का हिन्दी में अनुवाद किया जिनका प्रकाशन लाला सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद, हैदराबाद ने एवं अमोल ज्ञानालय, धूलिया ने किया। आचार्य श्री घासीलाल जी महाराज ने ३२ आगमों पर संस्कृत टीका का निर्माण किया तथा उसके हिन्दी एवं गुजराती अनुवाद प्रस्तुत किए, जिनका प्रकाशन अ. भा. श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन शास्त्रोद्धारक समिति, अहमदाबाद से हुआ। श्री पुफ्फभिक्खू जी ने ३२ आगमों के मूल पाठ का संक्षिप्त संस्करण तैयार किया जो दो भागों में सूत्रागम प्रकाशन समिति, गुड़गाँव से प्रकाशित हुआ। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने १९ आगमों का हिन्दी अनुवाद विवेचन किया था, जो आचार्य आत्माराम जैन प्रकाशन समिति, लुधियाना से प्रकाशित हुआ। आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज ने नन्दीसूत्र पर संस्कृत
(५०)