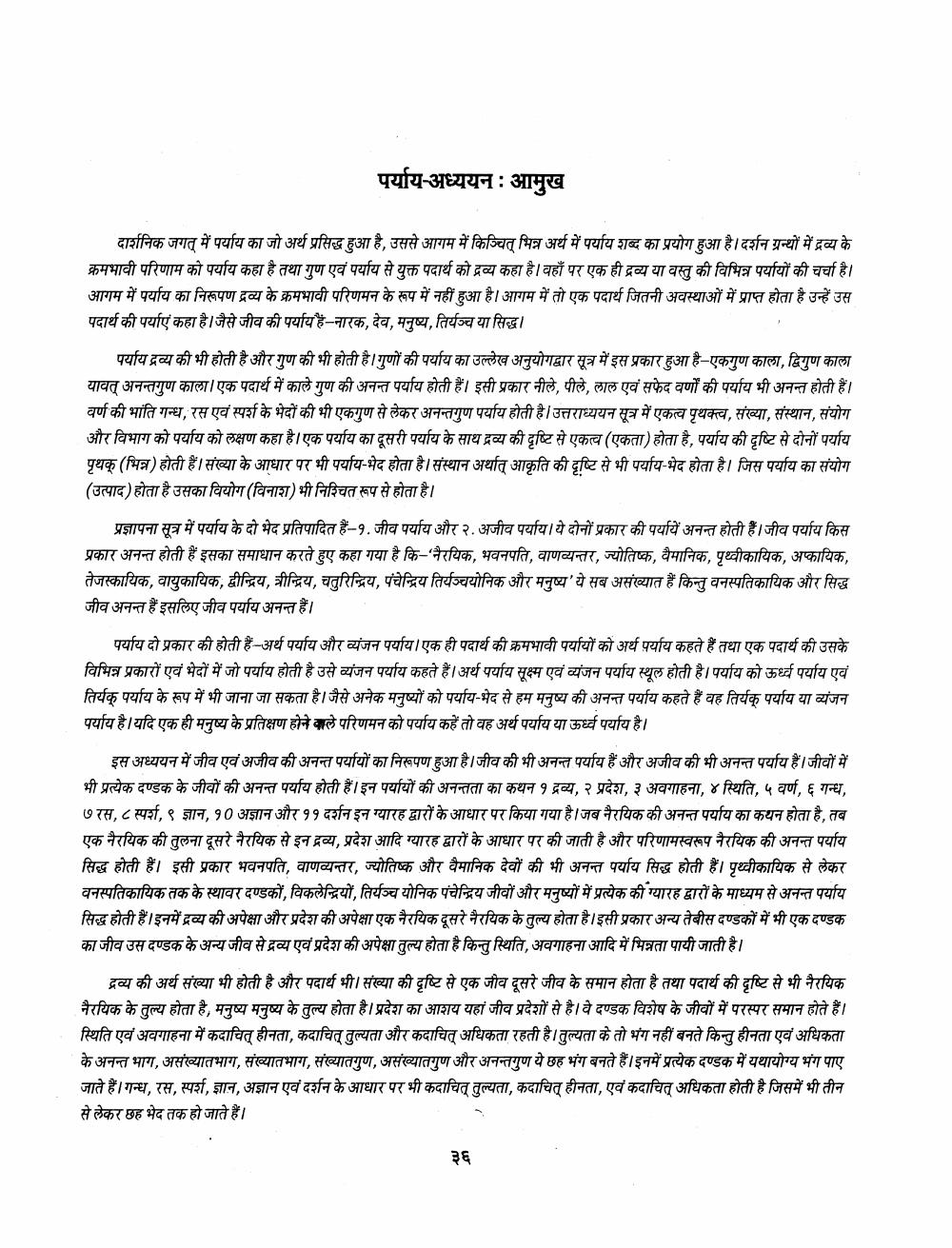________________
पर्याय-अध्ययन : आमुख
दार्शनिक जगत् में पर्याय का जो अर्थ प्रसिद्ध हुआ है, उससे आगम में किञ्चित् भिन्न अर्थ में पर्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। दर्शन ग्रन्थों में द्रव्य के क्रमभावी परिणाम को पर्याय कहा है तथा गुण एवं पर्याय से युक्त पदार्थ को द्रव्य कहा है। वहाँ पर एक ही द्रव्य या वस्तु की विभिन्न पर्यायों की चर्चा है। आगम में पर्याय का निरूपण द्रव्य के क्रमभावी परिणमन के रूप में नहीं हुआ है। आगम में तो एक पदार्थ जितनी अवस्थाओं में प्राप्त होता है उन्हें उस पदार्थ की पर्याए कहा है। जैसे जीव की पर्याय हैं-नारक, देव, मनुष्य, तिर्यञ्च या सिद्ध ।
पर्याय द्रव्य की भी होती है और गुण की भी होती है। गुणों की पर्याय का उल्लेख अनुयोगद्वार सूत्र में इस प्रकार हुआ है-एकगुण काला, द्विगुण काला यावत् अनन्तगुण काला। एक पदार्थ में काले गुण की अनन्त पर्याय होती हैं। इसी प्रकार नीले, पीले, लाल एवं सफेद वर्गों की पर्याय भी अनन्त होती हैं। वर्ण की भांति गन्ध, रस एवं स्पर्श के भेदों की भी एकगुण से लेकर अनन्तगुण पर्याय होती है। उत्तराध्ययन सूत्र में एकत्व पृथक्त्व, संख्या, संस्थान, संयोग
और विभाग को पर्याय को लक्षण कहा है। एक पर्याय का दूसरी पर्याय के साथ द्रव्य की दृष्टि से एकत्व (एकता) होता है, पर्याय की दृष्टि से दोनों पर्याय पृथक् (भिन्न) होती हैं। संख्या के आधार पर भी पर्याय-भेद होता है। संस्थान अर्थात् आकृति की दृष्टि से भी पर्याय-भेद होता है। जिस पर्याय का संयोग (उत्पाद) होता है उसका वियोग (विनाश) भी निश्चित रूप से होता है।
प्रज्ञापना सूत्र में पर्याय के दो भेद प्रतिपादित हैं-१. जीव पर्याय और २. अजीव पर्याय। ये दोनों प्रकार की पर्याय अनन्त होती हैं। जीव पर्याय किस प्रकार अनन्त होती हैं इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि-'नैरयिक, भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क, वैमानिक, पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिक और मनुष्य' ये सब असंख्यात हैं किन्तु वनस्पतिकायिक और सिद्ध जीव अनन्त हैं इसलिए जीव पर्याय अनन्त हैं।
पर्याय दो प्रकार की होती हैं-अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। एक ही पदार्थ की क्रमभावी पर्यायों को अर्थ पर्याय कहते हैं तथा एक पदार्थ की उसके विभिन्न प्रकारों एवं भेदों में जो पर्याय होती है उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। अर्थ पर्याय सूक्ष्म एवं व्यंजन पर्याय स्थूल होती है। पर्याय को ऊर्ध्व पर्याय एवं तिर्यक् पर्याय के रूप में भी जाना जा सकता है। जैसे अनेक मनुष्यों को पर्याय-भेद से हम मनुष्य की अनन्त पर्याय कहते हैं वह तिर्यक् पर्याय या व्यंजन पर्याय है। यदि एक ही मनुष्य के प्रतिक्षण होने काले परिणमन को पर्याय कहें तो वह अर्थ पर्याय या ऊर्ध्व पर्याय है।
इस अध्ययन में जीव एवं अजीव की अनन्त पर्यायों का निरूपण हुआ है। जीव की भी अनन्त पर्याय हैं और अजीव की भी अनन्त पर्याय हैं। जीवों में भी प्रत्येक दण्डक के जीवों की अनन्त पर्याय होती हैं। इन पर्यायों की अनन्तता का कथन १ द्रव्य, २ प्रदेश, ३ अवगाहना, ४ स्थिति, ५ वर्ण, ६ गन्ध, ७ रस, ८ स्पर्श, ९ ज्ञान, १० अज्ञान और ११ दर्शन इन ग्यारह द्वारों के आधार पर किया गया है। जब नैरयिक की अनन्त पर्याय का कथन होता है, तब एक नैरयिक की तुलना दूसरे नैरयिक से इन द्रव्य, प्रदेश आदि ग्यारह द्वारों के आधार पर की जाती है और परिणामस्वरूप नैरयिक की अनन्त पर्याय सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों की भी अनन्त पर्याय सिद्ध होती हैं। पृथ्वीकायिक से लेकर वनस्पतिकायिक तक के स्थावर दण्डकों, विकलेन्द्रियों, तिर्यञ्च योनिक पंचेन्द्रिय जीवों और मनुष्यों में प्रत्येक की ग्यारह द्वारों के माध्यम से अनन्त पर्याय सिद्ध होती हैं। इनमें द्रव्य की अपेक्षा और प्रदेश की अपेक्षा एक नैरयिक दूसरे नैरयिक के तुल्य होता है। इसी प्रकार अन्य तेबीस दण्डकों में भी एक दण्डक का जीव उस दण्डक के अन्य जीव से द्रव्य एवं प्रदेश की अपेक्षा तुल्य होता है किन्तु स्थिति, अवगाहना आदि में भिन्नता पायी जाती है।
द्रव्य की अर्थ संख्या भी होती है और पदार्थ भी। संख्या की दृष्टि से एक जीव दूसरे जीव के समान होता है तथा पदार्थ की दृष्टि से भी नैरयिक नैरयिक के तुल्य होता है, मनुष्य मनुष्य के तुल्य होता है। प्रदेश का आशय यहां जीव प्रदेशों से है। वे दण्डक विशेष के जीवों में परस्पर समान होते हैं। स्थिति एवं अवगाहना में कदाचित् हीनता, कदाचित् तुल्यता और कदाचित् अधिकता रहती है। तुल्यता के तो भंग नहीं बनते किन्तु हीनता एवं अधिकता के अनन्त भाग, असंख्यातभाग, संख्यातभाग, संख्यातगुण, असंख्यातगुण और अनन्तगुण ये छह भंग बनते हैं। इनमें प्रत्येक दण्डक में यथायोग्य भंग पाए जाते हैं। गन्ध, रस, स्पर्श, ज्ञान, अज्ञान एवं दर्शन के आधार पर भी कदाचित् तुल्यता, कदाचित् हीनता, एवं कदाचित् अधिकता होती है जिसमें भी तीन से लेकर छह भेद तक हो जाते हैं।
३६