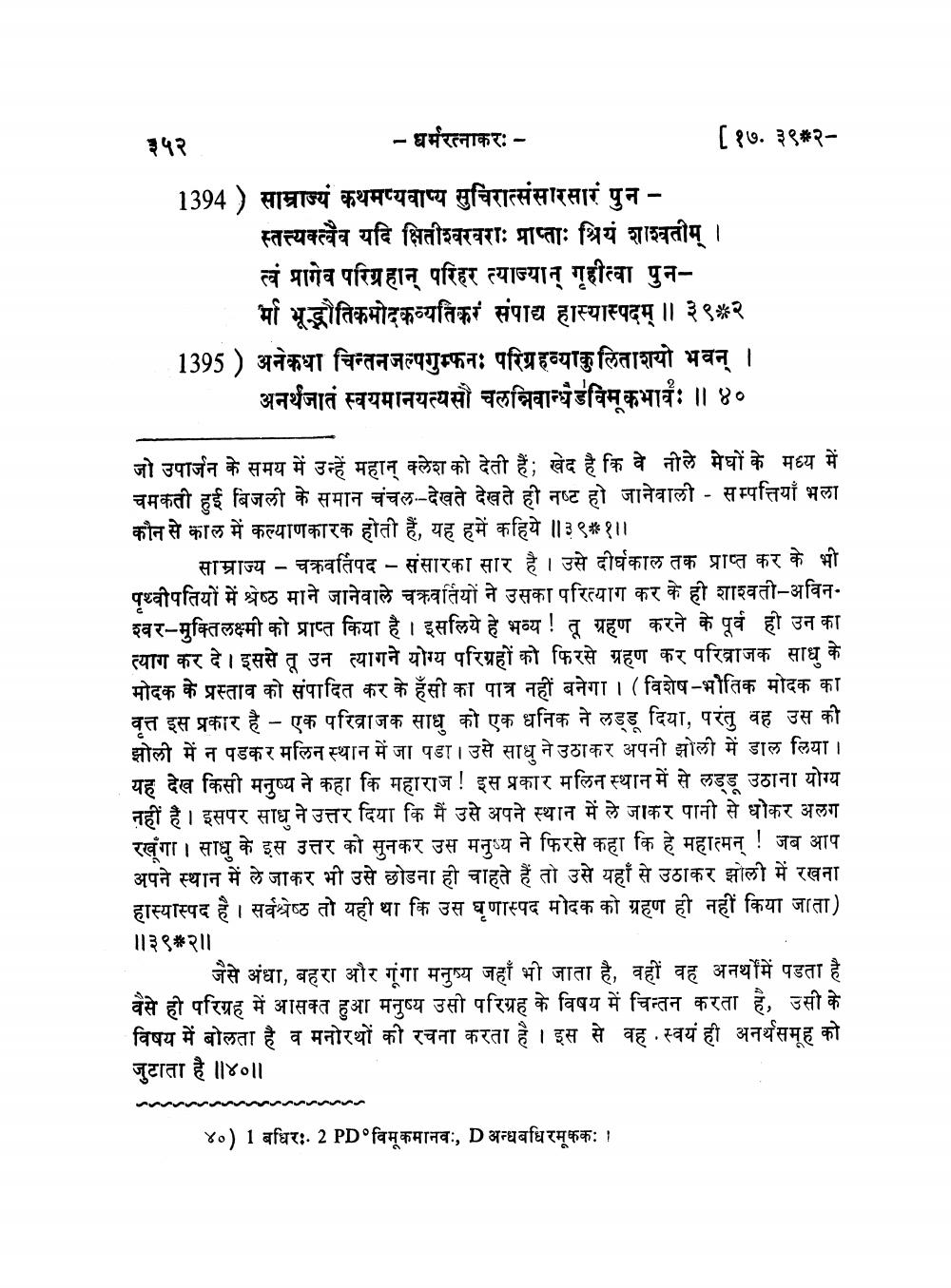________________
- धर्मरत्नाकरः -
1394 ) साम्राज्यं कथमप्यवाप्य सुचिरात्संसारसारं पुन - त्यक्त्यैव यदि क्षितीश्वरवराः प्राप्ताः श्रियं शाश्वतीम् । त्वं प्रागेव परिग्रहान् परिहर त्याज्यान् गृहीत्वा पुन - भूद्भौतिक मोदकव्यतिकरं संपाद्य हास्यास्पदम् || ३९*२ 1395 ) अनेकधा चिन्तन जल्प गुम्फनः परिग्रहव्याकुलिताशयो भवन् । अनर्थंजातं स्वयमानयत्यसौ चलन्निवान्धे डेविमूकभावः ॥ ४०
[ १७. ३९*२
३५२
जो उपार्जन के समय में उन्हें महान् क्लेश को देती हैं; खेद है कि वे नीले मेघों के मध्य में चमकती हुई बिजली के समान चंचल-देखते देखते ही नष्ट हो जानेवाली - सम्पत्तियाँ भला कौन से काल 'कल्याणकारक होती हैं, यह हमें कहिये ॥ ३९* १।।
साम्राज्य - चक्रवर्तिपद - संसारका सार है । उसे दीर्घकाल तक प्राप्त कर के भी पृथ्वीपतियों में श्रेष्ठ माने जानेवाले चक्रवर्तियों ने उसका परित्याग कर के ही शाश्वती - अविन श्वर - मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त किया है । इसलिये हे भव्य ! तू ग्रहण करने के पूर्व ही उनका त्याग कर दे। इससे तू उन त्यागने योग्य परिग्रहों को फिरसे ग्रहण कर परिव्राजक साधु मोदक के प्रस्ताव को संपादित कर के हँसी का पात्र नहीं बनेगा । ( विशेष - भौतिक मोदक का वृत्त इस प्रकार है - एक परिव्राजक साधु को एक धनिक ने लड्डू दिया, परंतु वह उस की झोली में न पडकर मलिन स्थान में जा पडा । उसे साधु ने उठाकर अपनी झोली डाल लिया । यह देख किसी मनुष्य ने कहा कि महाराज ! इस प्रकार मलिन स्थान में से लड्डू उठाना योग्य नहीं है । इसपर साधु ने उत्तर दिया कि मैं उसे अपने स्थान में ले जाकर पानी से धोकर अलग रखूंगा। साधु के इस उत्तर को सुनकर उस मनुष्य ने फिरसे कहा कि हे महात्मन् ! जब आप अपने स्थान में ले जाकर भी उसे छोडना ही चाहते हैं तो उसे यहाँ से उठाकर झोली में रखना हास्यास्पद है । सर्वश्रेष्ठ तो यही था कि उस घृणास्पद मोदक को ग्रहण ही नहीं किया जाता ) ॥३९*२॥
I
जैसे अंधा, बहरा और गूंगा मनुष्य जहाँ भी जाता है, वहीं वह अनर्थों में पडता है वैसे ही परिग्रह में आसक्त हुआ मनुष्य उसी परिग्रह के विषय में चिन्तन करता है, उसी के विषय में बोलता है व मनोरथों की रचना करता है । इस से वह स्वयं ही अनर्थसमूह जुटाता है ॥४०॥
.
४०) 1 बधिरः. 2 PD° विमूकमानवः, D अन्धबधिरमूककः ।