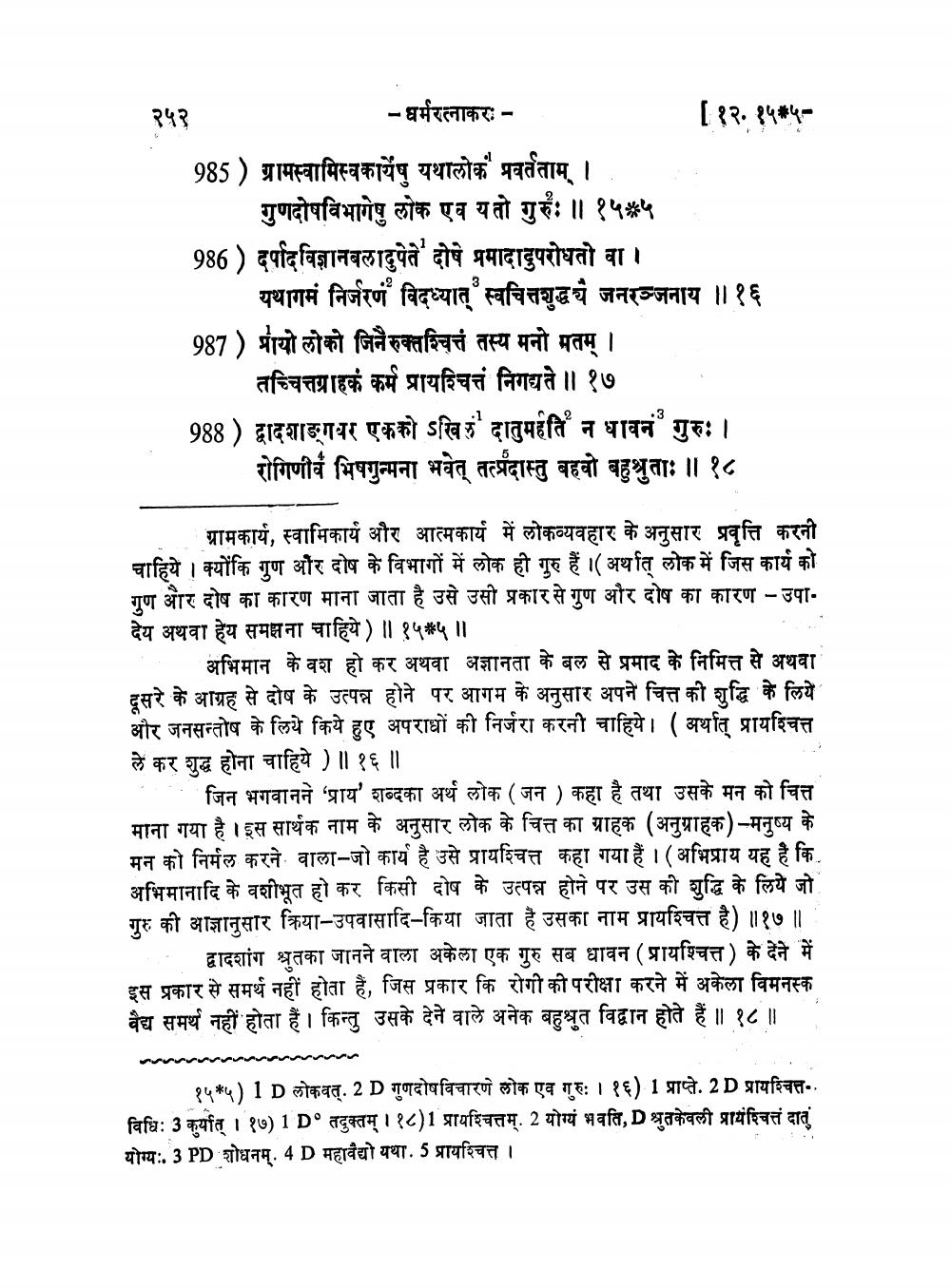________________
२५२ - धर्मरत्नाकरः -
[ १२. १५२५985) ग्रामस्वामिस्वकार्येषु यथालोक प्रवर्तताम् ।
गुणदोषविभागेषु लोक एव यतो गुरुः ॥ १५*५ 986) दर्पादविज्ञानबलादुपेते दोषे प्रमादादुपरोधतो वा।
यथागमं निर्जरणं विदध्यात् स्वचित्तशुद्धय जनरञ्जनाय ॥ १६ 987) प्रायो लोको जिनै रुक्तश्चित्तं तस्य मनो मतम् ।
तच्चित्तग्राहकं कर्म प्रायश्चित्तं निगद्यते ॥ १७ 988 ) द्वादशाङ्गवर एकको ऽखिलं दातुमर्हति न धावनं गुरुः ।
रोगिणीवं भिषगुन्मना भवेत् तत्प्रदास्तु बहवो बहुश्रुताः ॥ १८
ग्रामकार्य, स्वामिकार्य और आत्मकार्य में लोकव्यवहार के अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिये । क्योंकि गुण और दोष के विभागों में लोक ही गुरु हैं ।( अर्थात् लोक में जिस कार्य को गुण और दोष का कारण माना जाता है उसे उसी प्रकार से गुण और दोष का कारण - उपा. देय अथवा हेय समझना चाहिये ) ॥ १५*५ ॥ ' अभिमान के वश हो कर अथवा अज्ञानता के बल से प्रमाद के निमित्त से अथवा दूसरे के आग्रह से दोष के उत्पन्न होने पर आगम के अनुसार अपने चित्त की शुद्धि के लिये
और जनसन्तोष के लिये किये हुए अपराधों की निर्जरा करनी चाहिये। ( अर्थात् प्रायश्चित्त ले कर शुद्ध होना चाहिये ) ॥ १६ ॥
जिन भगवानने 'प्राय' शब्दका अर्थ लोक ( जन ) कहा है तथा उसके मन को चित्त माना गया है । इस सार्थक नाम के अनुसार लोक के चित्त का ग्राहक (अनुग्राहक)-मनुष्य के मन को निर्मल करने वाला-जो कार्य है उसे प्रायश्चित्त कहा गया हैं । ( अभिप्राय यह है कि. अभिमानादि के वशीभूत हो कर किसी दोष के उत्पन्न होने पर उस की शुद्धि के लिये जो गुरु की आज्ञानुसार क्रिया-उपवासादि-किया जाता है उसका नाम प्रायश्चित्त है) ॥१७ ॥
- द्वादशांग श्रुतका जानने वाला अकेला एक गुरु सब धावन (प्रायश्चित्त) के देने में इस प्रकार से समर्थ नहीं होता हैं, जिस प्रकार कि रोगी की परीक्षा करने में अकेला विमनस्क वैद्य समर्थ नहीं होता हैं। किन्तु उसके देने वाले अनेक बहुश्रुत विद्वान होते हैं ॥ १८ ॥
१५*५) 1 D लोकवत्. 2 D गुणदोषविचारणे लोक एव गुरुः । १६) 1 प्राप्ते. 2 D प्रायश्चित्त.. विधि: 3 कुर्यात् । १७) 1 D° तदुक्तम् । १८)1 प्रायश्चित्तम्. 2 योग्यं भवति, D श्रुतकेवली प्रायश्चित्तं दातुं योग्यः. 3 PD शोधनम्. 4 D महावैद्यो यथा. 5 प्रायश्चित्त ।