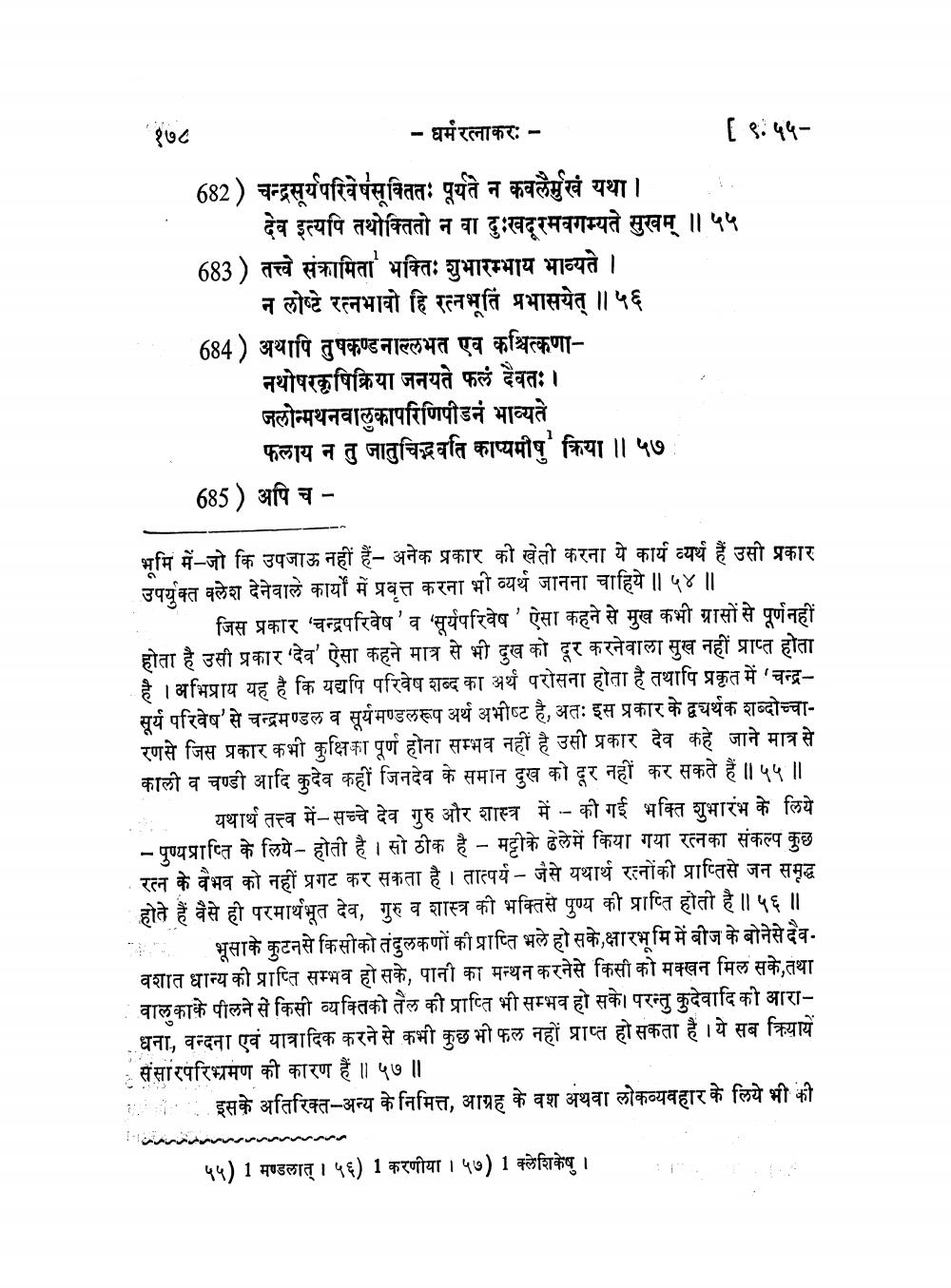________________
१७८ - धर्मरत्नाकरः -
[ ९.५५682) चन्द्रसूर्यपरिवेषसूक्तितः पूर्यते न कवलैर्मुखं यथा ।
देव इत्यपि तथोक्तितो न वा दुःखदूरमवगम्यते सुखम् ॥ ५५ 683) तत्त्वे संक्रामिता भक्तिः शुभारम्भाय भाव्यते ।
न लोष्टे रत्नभावो हि रत्नभूति प्रभासयेत् ॥५६ 684) अथापि तुषकण्डनाल्लभत एव कश्चित्कणा
नथोषरकृषिक्रिया जनयते फलं दैवतः। जलोन्मथनवालुकापरिणिपीडनं भाव्यते
फलाय न तु जातुचिद्भवति काप्यमीषु क्रिया ।। ५७ 685) अपि च -
भमि में जो कि उपजाऊ नहीं हैं- अनेक प्रकार की खेती करना ये कार्य व्यर्थ हैं उसी प्रकार उपर्युक्त क्लेश देनेवाले कार्यों में प्रवृत्त करना भी व्यर्थ जानना चाहिये ।। ५४ ॥
जिस प्रकार 'चन्द्रपरिवेष' व 'सूर्यपरिवेष' ऐसा कहने से मुख कभी ग्रासों से पूर्ण नहीं होता है उसी प्रकार 'देव' ऐसा कहने मात्र से भी दुख को दूर करनेवाला सुख नहीं प्राप्त होता है । अभिप्राय यह है कि यद्यपि परिवेष शब्द का अर्थ परोसना होता है तथापि प्रकृत में ‘चन्द्रसूर्य परिवेष' से चन्द्रमण्डल व सूर्यमण्डलरूप अर्थ अभीष्ट है, अतः इस प्रकार के द्वयर्थक शब्दोच्चारणसे जिस प्रकार कभी कुक्षिका पूर्ण होना सम्भव नहीं है उसी प्रकार देव कहे जाने मात्र से काली व चण्डी आदि कुदेव कहीं जिनदेव के समान दुख को दूर नहीं कर सकते हैं ।। ५५ ॥
___ यथार्थ तत्त्व में- सच्चे देव गुरु और शास्त्र में -- की गई भक्ति शुभारंभ के लिये - पुण्यप्राप्ति के लिये- होती है । सो ठीक है - मट्टीके ढेलेमें किया गया रत्नका संकल्प कुछ रत्न के वैभव को नहीं प्रगट कर सकता है । तात्पर्य - जैसे यथार्थ रत्नोंकी प्राप्तिसे जन समृद्ध होते हैं वैसे ही परमार्थभूत देव, गुरु व शास्त्र की भक्तिसे पुण्य की प्राप्ति होती है ॥ ५६ ॥
भूसाके कुटनसे किसीको तंदुलकणों की प्राप्ति भले हो सके,क्षारभूमि में बीज के बोनेसे दैव. वशात धान्य की प्राप्ति सम्भव हो सके, पानी का मन्थन करनेसे किसी को मक्खन मिल सके,तथा वालुकाके पीलने से किसी व्यक्तिको तैल की प्राप्ति भी सम्भव हो सके। परन्तु कुदेवादि को आराधना, वन्दना एवं यात्रादिक करने से कभी कुछ भी फल नहीं प्राप्त हो सकता है । ये सब क्रियायें - संसारपरिभ्रमण की कारण हैं ॥ ५७ ।।
की इसके अतिरिक्त अन्य के निमित्त, आग्रह के वश अथवा लोकव्यवहार के लिये भी की
५५) 1 मण्डलात् । ५६) 1 करणीया । ५७) 1 क्लेशिकेषु ।