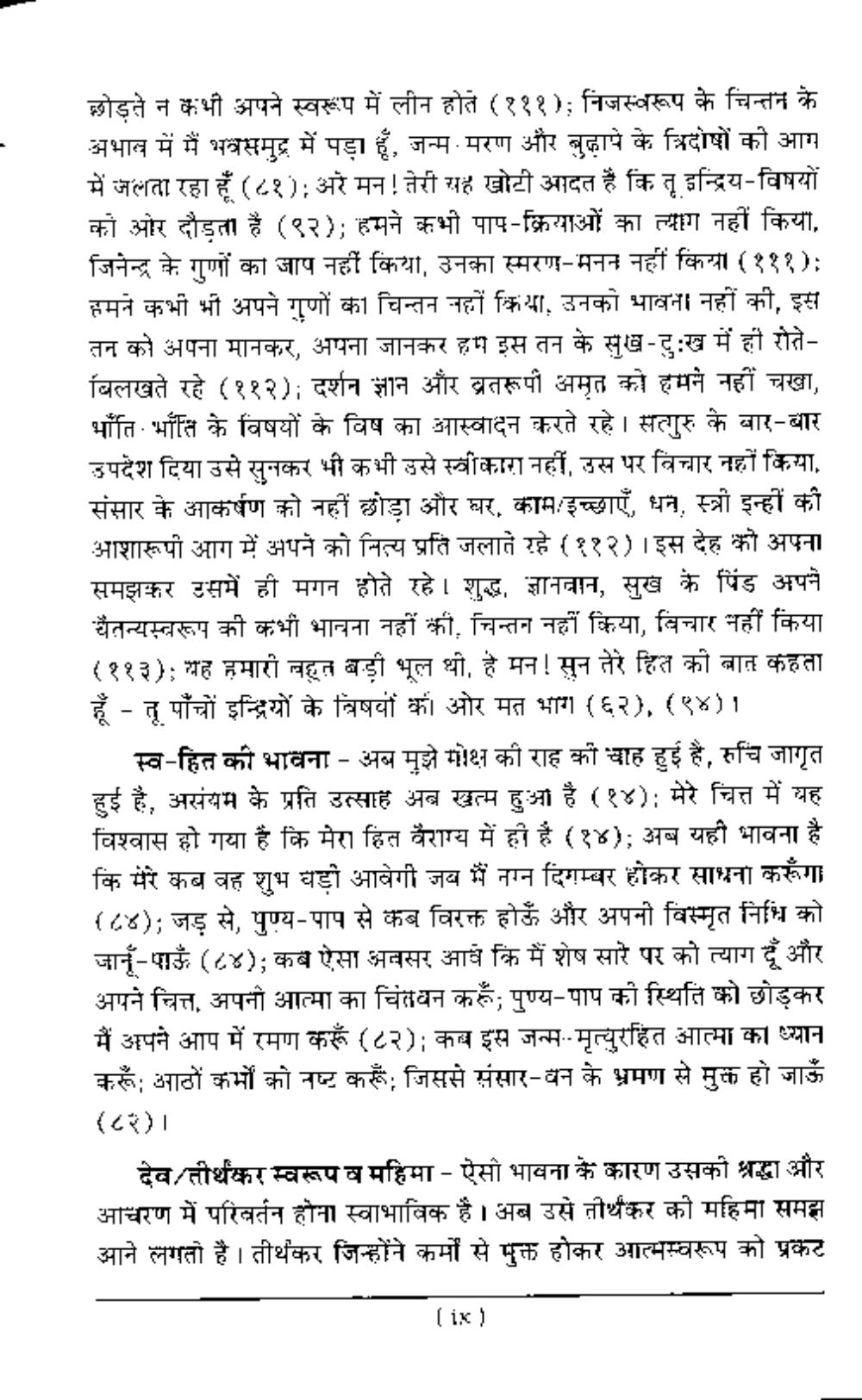________________
छोड़ते न कभी अपने स्वरूप में लीन होते (१११); निजस्वरूप के चिन्तन के अभाव में मैं भवसमुद्र में पड़ा हूँ, जन्म मरण और बुढ़ापे के त्रिदोषों की आग में जलाता रहा हूँ (८१); अरे मन ! तेरी राह खोटी आदत है कि तृ इन्द्रिय-विषयों को ओर दौड़ता है (९२); हमने कभी पाप-क्रियाओं का त्याग नहीं किया, जिनेन्द्र के गुणों का जाप नहीं किया, उनका स्मरणा-मनन नहीं किया (१११); हमने कभी भी अपने गुणों का चिन्तन नहीं किया, उनको भावना नहीं की, इस तन को अपना मानकर, अपना जानकर हम इस तन के सुख-दु:ख में ही रोतेबिलखते रहे (११२); दर्शन ज्ञान और व्रतरूपी अमृत को हमने नहीं चखा, भाँति भाँति के विषयों के विष का आस्वादन करते रहे । सत्गुरु के बार-बार उपदेश दिया उसे सुनकर भी कभी उसे स्वीकारा नहीं, उस पर विचार नहीं किया, संसार के आकर्षण को नहीं छोड़ा और घर, काम इच्छाएँ, धन, स्त्री इन्हीं की आशारूपी आग में अपने को नित्य प्रति जलाते रहे (११२) । इस देह को अपना समझकर उसमें ही मगन होते रहे। शुद्ध, ज्ञानवान, सुख के पिंड अपने चैतन्यस्वरूप की कभी भावना नहीं की. चिन्तन नहीं किया, विचार नहीं किया (११३); यह हमारी बहुत बड़ी भूल थी, हे मन ! सुन तेरे हित की बात कहता हूँ - तू पाँचों इन्द्रियों के विषयों की ओर मत भाग (६२), (९४)।
स्व-हित की भावना - अब मुझे मोक्ष की राह की चाह हुई है, रुचि जागृत हुई है, असंयम के प्रति उत्साह अब खत्म हुआ है (१४); मेरे चित्त में यह विश्वास हो गया है कि मेरा हित वैराग्य में ही है (१४); अब यही भावना है कि मेरे कब वह शुभ घड़ी आवेगी जब मैं नग्न दिगम्बर होकर साधना करूँगा (८४); जड़ से, पुण्य- पाप से कब विरक्त होऊँ और अपनी विस्मृत निधि को जान-पाऊँ (८४); कब ऐसा अवसर आवे कि मैं शेष सारे पर को त्याग दूं और अपने चित्त, अपनी आत्मा का चिंतवन करूँ; पुण्य-पाप की स्थिति को छोड़कर मैं अपने आप में रमण करूँ (८२); कब इस जन्म मृत्युरहित आत्मा का ध्यान करूँ; आठों कर्मों को नष्ट करूँ; जिससे संसार-वन के भ्रमण से मुक्त हो जाऊँ (८२)।
देव/तीर्थंकर स्वरूप व महिमा - ऐसी भावना के कारण उसकी श्रद्धा और आचरण में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अब उसे तीर्थकर की महिमा समझ आने लगतो है। तीर्थकर जिन्होंने कर्मों से मुक्त होकर आत्मस्वरूप को प्रकट
[ ix)