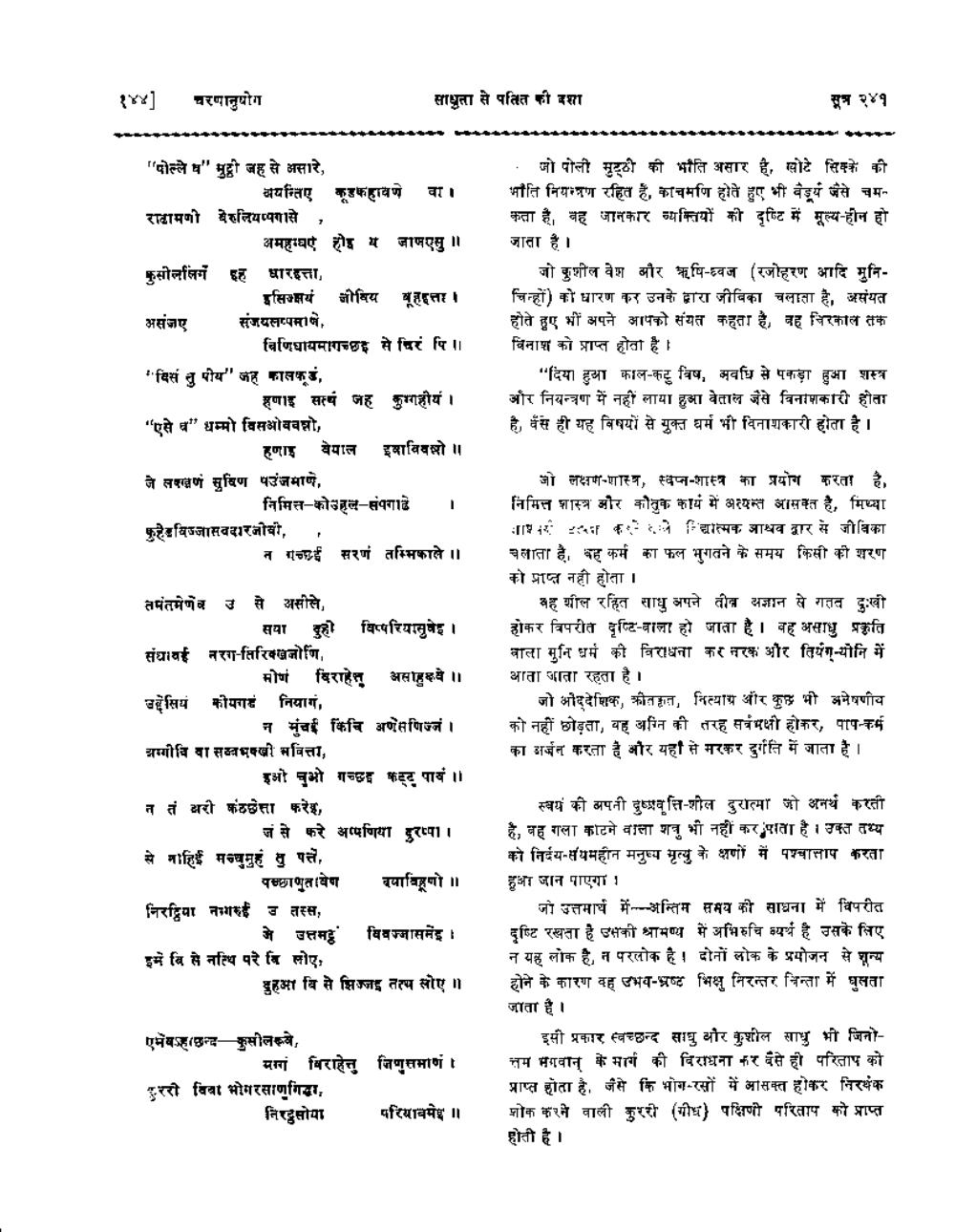________________
१४४] चरणानुयोग
"पोल्ले घ" मुट्ठी जह से असारे, जयन्तिए कूड कहावणे राहामको निय
कुसीलिंग इह धारइत्ता,
असं ए
अमहग्घए होइ य जाणएसु ॥
इसिका जोषिय बृहद्दत्ता । संवा
"दिसं तु पीय" जह कालकूड,
विणिघायमागच्छ से चिरंपि॥
"एसे " धम्मो विस
हाइ सत्यं जह कुग्गहीयं ।
जेवण पजमाये
हाइ वेयाल safar ||
निमित को संपा
कुवासवदारजीबी,
साधुता से पतित की दशा
"
वा ।
तमतमेणेव उसे असीले, संघाई मरण-तिरिक्नोणि
उद्देसिय कोयगढं नियागं,
न गच्छई सरणं तम्भिकाले ।।
सया तुही विपपरियासुद्द ।
भोणं विराहेतु ।।
अग्गीवि वा सव्वमक्खी भवित्ता,
न मुंबई किचि अणेस णिज्नं ।
इस भोक पाये ।।
पछतायेग
नखरी डाकरे
जं से करे अप्पणिया दुरध्वा । मापसे,
निरट्रिया नगद तरस,
इमे वि से नथि परे दि सोए
विवरणसमे
॥
विसेति सोए ।
एमें वह (छन्द–कुसीलरूये,
मागं विराहेतु जिणुत्समाणं । दूर दिवा भोमरसागडा,
निरसोया
परिवारमे ॥
सूत्र २४१
जो पोनी मुट्ठी की भाँति असार है, खोटे सिक्के की भाँति रहित है, काचमणि होते हुए भी पूर्व जैसे चम कता है, वह जानकार व्यक्तियों की दृष्टि में मूल्य-हीन हो जाता है ।
जो कुशील वेश और ऋषि ध्वज (रजोहरण आदि मुनिचिन्हों ) को धारण कर उनके द्वारा जीविका चलाता है, जसंयंत होते हुए भी अपने आपको संयत कहता है, वह चिरकाल तक विनाश को प्राप्त होता है।
" दिया हुआ काल-कटु विष, अवधि से पकड़ा हुआ शस्त्र और नियन्त्रण में नहीं लाया हुआ वेताल जैसे विनाशकारी होता है, वैसे ही यह विषयों से मुक्त धर्म भी विनाशकारी होता है।
जो लक्षण शास्त्र, स्वप्न शास्त्र का प्रयोग करता है, निमित्त शास्त्र और कौतुक कार्य में अत्यन्त आसक्त है, मिथ्या वाश्वदीपकद्यात्मक आश्रव द्वार से जीविका चलाता है, वह कर्म का फल भुगतने के समय किसी की शरण को प्राप्त नहीं होता ।
वह शील रहित साधु अपने तीव्र अज्ञान से गतव दुःखी होकर विपरीत दृष्टि-वाला हो जाता है। वह असाधु प्रकृति वाला मुनि धर्म की विराधना कर नरक और तिर्यग्योनि में आता जाता रहता है ।
जोति विश्वाय और कुछ भी बनेगी को नहीं छोड़ता, वह अग्नि की तरह सर्वभक्षी होकर पाप कर्म का अर्जन करता है और यहाँ से मरकर दुर्गति में जाता है।
स्वयं की अपनी
शीतला को अनर्थ करती है, वह गला काटने वाला शत्रु भी नहीं कर पाता है। उक्त तथ्य को निर्दय संयमहीन मनुष्य मृत्यु के क्षणों में पश्चाताप करता
हुआ जान पाएगा |
जो उत्तमार्थ में --अन्तिम दृष्टि रखता है उसकी श्रामण्य न यह लोक है, न परलोक है। होने के कारण वह उभव भ्रष्ट जाता है ।
समय की साधना में विपरीत में अभिरुचि व्यर्थ है उसके लिए दोनों लोक के प्रयोजन से शून्य भिक्षु निरन्तर चिन्ता में घुलता
इसी प्रकार स्वच्छन्द साधु और कुशील साधु भी जिनोतम भगवान् के मार्ग की विराधना कर वैसे ही परिताप को प्राप्त होता है, जैसे कि भोग-रसों में आसक्त होकर निरर्थक शोक करने वाली (पीच) पक्षिणी परिताप को प्राप्त
होती है।