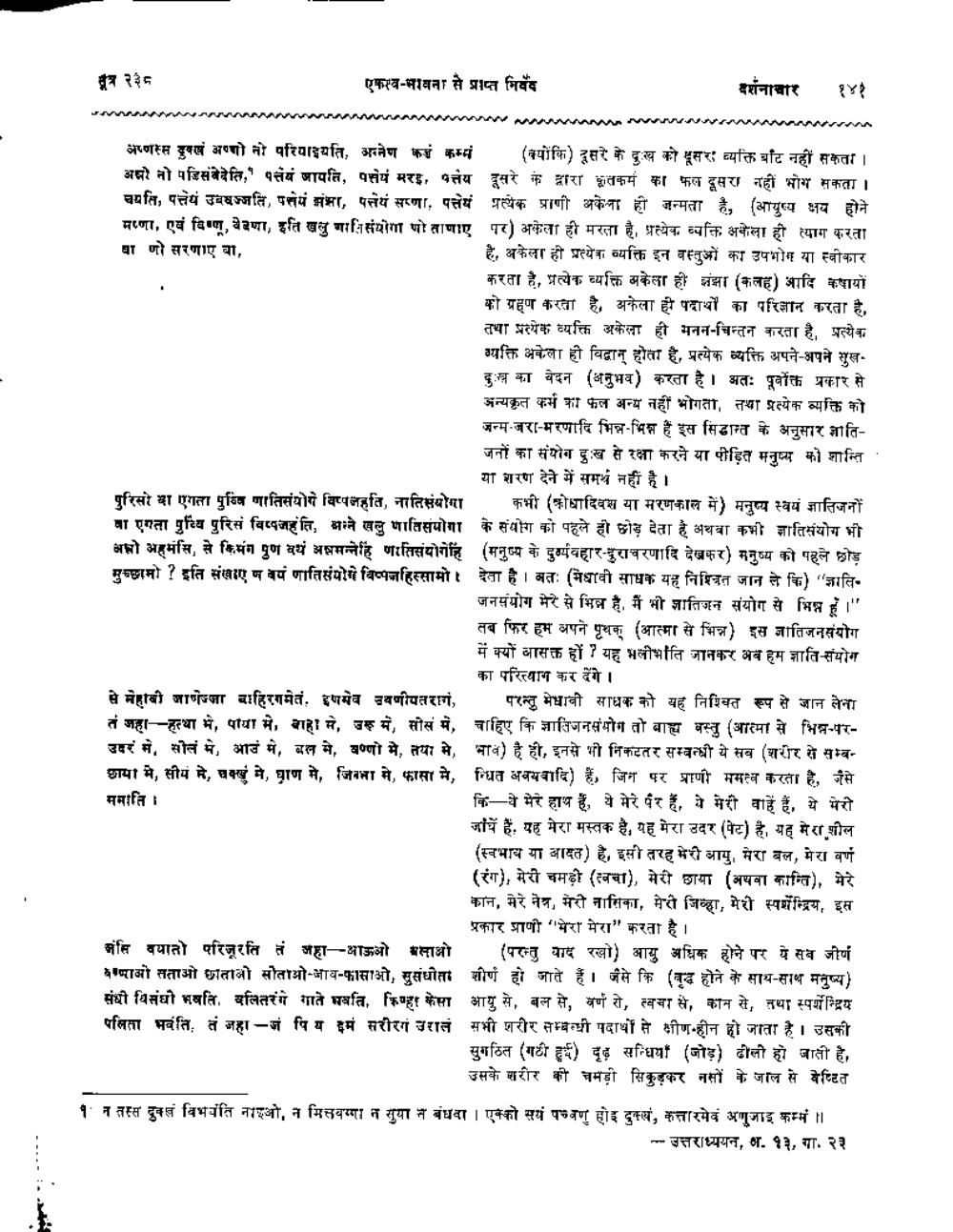________________
सूत्र २३८
एफश्व-भावना से प्राप्त मिर्वेद
दर्शनाचार
१४१
अण्णस्स दुक्खं अग्गो नो परिवाइयति, अनेण फवं कम्मं (क्योंकि) दूसरे के दुःख को दूसरा व्यक्ति बाँट नहीं सकता । अनरेनो पतिसंवेदेति,' पत्तयं जापति, पसेयं मरह, पत्त्य दूसरे के द्वारा पूतिकर्म का फल दूसरा नहीं भोग सकता। चयति, पत्तेयं उबधज्जति, पत्तेयं झंझा, पत्तेयं सप्णा, पत्तेयं प्रत्येक प्राणी अकेला ही जन्मता है, (आयुष्य क्षय होने मष्णा, एवं विष्ण, वेण्णा, इति खलु गानिसंयोगा पो ताणाए पर) अकेला ही मरता है, प्रत्येक व्यक्ति अबेला ही त्याग करता था णो सरणाए बा,
है, अकेला ही प्रत्येक व्यक्ति इन वस्तुओं का उपभोग या स्वीकार करता है, प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही झंझा (कलह) आदि कषायों को ग्रहण करता है, अकेला ही पदार्थों का परिज्ञान करता है, तथा प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही मनन-चिन्तन करता है, प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही विद्वान् होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने सुखदुःख का वेदन (अनुभव) करता है। अतः पूर्वोक्त प्रकार से अन्यकृत कर्म का फल अन्य नहीं भोगता, तथा प्रत्येक व्यक्ति को जन्म-जरा-मरणादि भिन्न-भिन्न हैं इस सिद्धान्त के अनुसार जातिजनों का संयोग दुःख से रक्षा करने या पीड़ित मनुष्य को शान्ति
या शरण देने में समर्थ नहीं है। पुरिसो या एगला पुरिव णातिसंयोगे विप्पजहति, नातिसंयोगा कभी (क्रोधादिवश या मरणकाल में) मनुष्य स्वयं जातिजनों वा एगता पुखि पुरिसं विष्पजहं ति, मन्ने खलु जातिसंयोगा के संयोग को पहले ही छोड़ देता है अथवा कभी ज्ञातिसंयोग भी असो अहमंसि, से किमंग पुण वयं अन्नमन्नेहि जातिसंयोहिं (मनुष्य के दुव्र्यवहार-दुराचरणादि देखकर) मनुष्य को पहले छोड़ मुच्छामो ? इति संखाए ण वयं णातिसंयोग विप्पजहिस्सामो। देता है। अतः (मधावी साधक यह निश्चित जान ले कि) "ज्ञाति
जनसंयोग मेरे से भिन्न है, मैं भी ज्ञातिजन संयोग से भिन्न हूँ।" तब फिर हम अपने पृथक् (आत्मा से भिन्न) इस जातिजनसंयोग में क्यों आसक्त हों ? यह भलीभांति जानकर अब हम ज्ञाति-संयोग
का परित्याग कर देंगे। से महावी जाणेज्जा वाहिरगमेतं. इणमेव उवणीयतराग, परन्तु मेधावी साधक को यह निश्चित रूप से जान लेना तं जहा-हत्था में, पाया मे, वाहा मे, जरू मे, सोस में, चाहिए कि ज्ञातिजनसंयोग तो बाद्य वस्तु (आत्मा से भिन्न-परउधर में, सोल में, आ मे, बल मे, वणो मे, तया मे, भाव) है ही, इनसे भी निकटतर सम्बन्धी ये सब (शरीर से सम्बछाया में, सीय है, चक्षु मे, घाण मे, जिवना मे, फासा मे, धित अवयवादि) हैं, जिन पर प्राणी ममत्व करता है, जैसे ममाति।
कि वे मेरे हाथ हैं, ये मेरे पर हैं, ये मेरी वाहें हैं, ये मेरी जांघे हैं. यह मेरा मस्तक है, यह मेरा उदर (पेट) है, यह मेरा शील (स्वभाव या आदत) है, इसी तरह मेरी आयु, मेरा बल, मेरा वर्ण (रंग), मेरी चमढ़ी (त्वचा), मेरी छाया (अथवा कान्ति), मेरे कान, मेरे नेत्र, मेरी नासिका, मेरी जिव्हा, मेरी स्पन्द्रिय, इस
प्रकार प्राणी "मेरा मेरा" करता है। मंसि वयातो परिजूरति तं जहा-आऊओ अलाओ (परन्तु याद रखो) आयु अधिक होने पर ये सब जीर्ण अम्माओ सताओ छातानो सोतामो-नाव-कासाओ, सुसंधौता शीणं हो जाते हैं। जैसे कि (वृद्ध होने के साथ-साथ मनुष्य) संधी विसंधो भवति, दलितरंगे गाते भवति, किव्हा केसा आयु से, बल से, वर्ण रो, त्वचा से, कान से, तथा स्पर्थेन्द्रिय पलिता भवंति, तं जहा-जं पि य इमं सरीरंग उरालं सभी शरीर सम्बन्धी पदार्थों से क्षीण हीन हो जाता है। उसकी
सुगठित (गटी हुई) दृढ़ सन्धियाँ (जोड़) ढीली हो जाती है, उसके शरीर की चमड़ी सिकुड़कर नसों के जाल से वेष्टित
1 न तस्स दुक्खं विभवंति नाइओ, न मित्तबग्गा न सुया न बंधदा । एक्को सयं पञ्चण होइ दुक्वं, कत्तारमेवं अणुजाइ फम्म ।
- उत्तराध्ययन, अ. १३, गा. २३