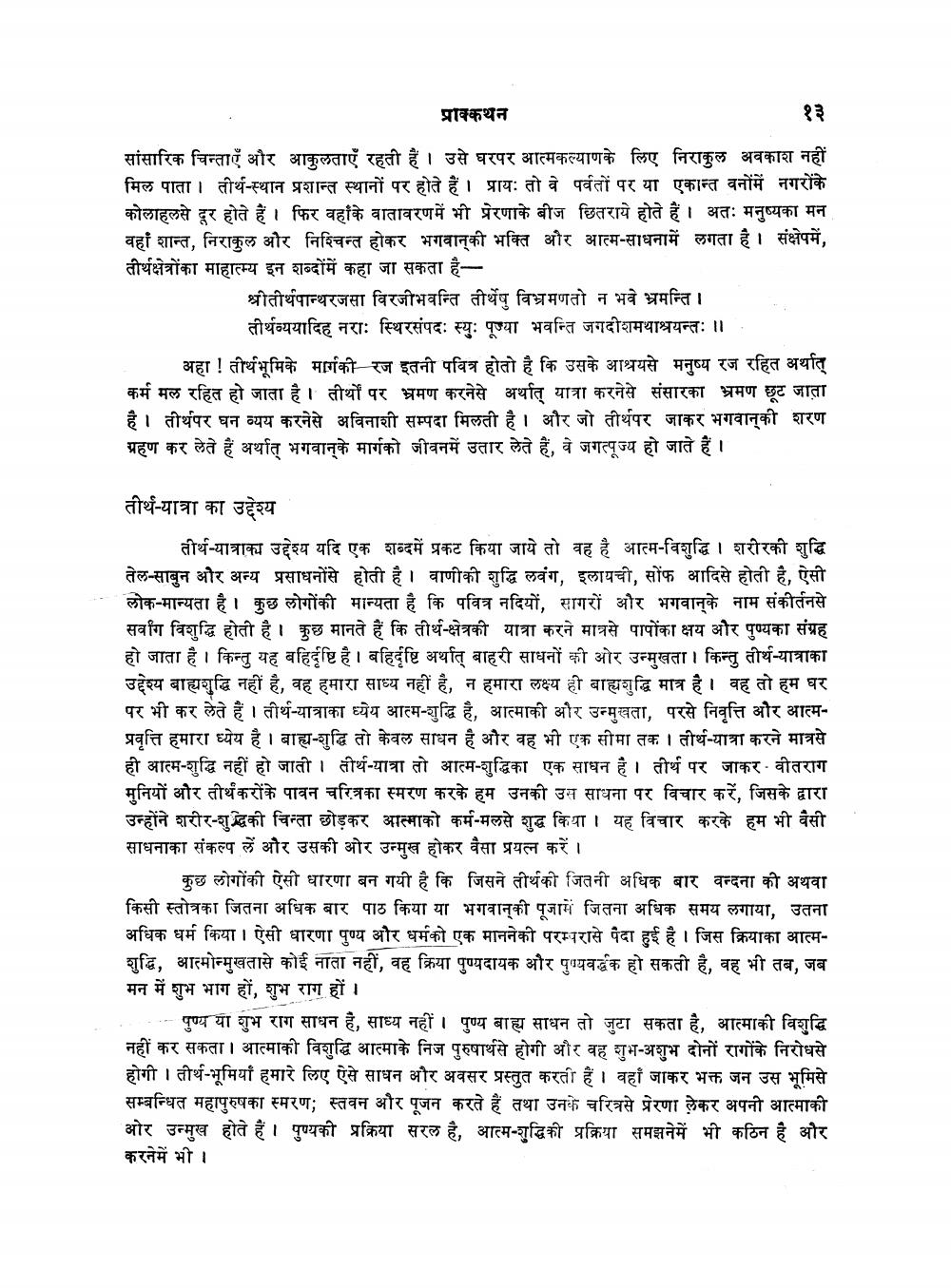________________
प्राक्कथन
१३
सांसारिक चिन्ताएँ और आकुलताएँ रहती है। उसे घरपर आत्मकल्याणके लिए निराकुल अवकाश नहीं मिल पाता। तीर्थ-स्थान प्रशान्त स्थानों पर होते हैं। प्रायः तो वे पर्वतों पर या एकान्त वनोंमें नगरोंके कोलाहलसे दूर होते हैं। फिर वहाँके वातावरण में भी प्रेरणाके बीज छितराये होते हैं। अतः मनुष्यका मन वहाँ शान्त, निराकुल और निश्चिन्त होकर भगवान्की भक्ति और आत्म-साधनामें लगता है। संक्षेपमें, तीर्थक्षेत्रोंका माहात्म्य इन शब्दोंमें कहा जा सकता है
श्रीतीर्थपान्थरजसा विरजीभवन्ति तीर्थेषु विभ्रमणतो न भवे भ्रमन्ति।
तीर्थव्ययादिह नराः स्थिरसंपदः स्युः पूज्या भवन्ति जगदीशमथाश्रयन्तः ।। अहा ! तीर्थभूमिके मार्गकी रज इतनी पवित्र होतो है कि उसके आश्रयसे मनुष्य रज रहित अर्थात् कर्म मल रहित हो जाता है। तीर्थों पर भ्रमण करनेसे अर्थात् यात्रा करनेसे संसारका भ्रमण छूट जाता है। तीर्थपर घन व्यय करनेसे अविनाशी सम्पदा मिलती है। और जो तीर्थपर जाकर भगवान्की शरण ग्रहण कर लेते हैं अर्थात् भगवान्के मार्गको जीवनमें उतार लेते हैं, वे जगत्पूज्य हो जाते हैं।
तीर्थ यात्रा का उद्देश्य
तीर्थ-यात्राका उद्देश्य यदि एक शब्दमें प्रकट किया जाये तो वह है आत्म-विशुद्धि । शरीरकी शुद्धि तेल-साबुन और अन्य प्रसाधनोंसे होती है। वाणीकी शुद्धि लवंग, इलायची, सोंफ आदिसे होती है, ऐसी लोक-मान्यता है। कुछ लोगोंकी मान्यता है कि पवित्र नदियों, सागरों और भगवान्के नाम संकीर्तनसे सर्वांग विशुद्धि होती है। कुछ मानते हैं कि तीर्थ-क्षेत्रकी यात्रा करने मात्रसे पापोंका क्षय और पुण्यका संग्रह हो जाता है। किन्तु यह बहिर्दृष्टि है । बहिर्दृष्टि अर्थात् बाहरी साधनों की ओर उन्मुखता। किन्तु तीर्थ-यात्राका उद्देश्य बाह्यशुद्धि नहीं है, वह हमारा साध्य नहीं है, न हमारा लक्ष्य ही बाह्यशुद्धि मात्र है। वह तो हम घर पर भी कर लेते हैं । तीर्थ-यात्राका ध्येय आत्म-शुद्धि है, आत्माकी और उन्मुखता, परसे निवृत्ति और आत्मप्रवृत्ति हमारा ध्येय है । बाह्य-शुद्धि तो केवल साधन है और वह भी एक सीमा तक । तीर्थ यात्रा करने मात्रसे ही आत्म-शुद्धि नहीं हो जाती। तीर्थ-यात्रा तो आत्म-शुद्धिका एक साधन है। तीर्थ पर जाकर - वीतराग मुनियों और तीर्थंकरोंके पावन चरित्रका स्मरण करके हम उनकी उस साधना पर विचार करें, जिसके द्वारा उन्होंने शरीर-शुद्धिकी चिन्ता छोड़कर आत्माको कर्म-मलसे शुद्ध किया। यह विचार करके हम भी वैसी साधनाका संकल्प लें और उसकी ओर उन्मुख होकर वैसा प्रयत्न करें।
कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा बन गयी है कि जिसने तीर्थकी जितनी अधिक बार वन्दना की अथवा किसी स्तोत्रका जितना अधिक बार पाठ किया या भगवान्की पूजामें जितना अधिक समय लगाया, उतना अधिक धर्म किया। ऐसी धारणा पुण्य और धर्मको एक माननेकी परम्परासे पैदा हुई है । जिस क्रियाका आत्मशुद्धि, आत्मोन्मुखतासे कोई नाता नहीं, वह क्रिया पुण्यदायक और पुण्यवर्द्धक हो सकती है, वह भी तब, जब मन में शुभ भाग हों, शुभ राग हो । ..-पुण्य या शुभ राग साधन है, साध्य नहीं। पुण्य बाह्य साधन तो जुटा सकता है, आत्माकी विशुद्धि नहीं कर सकता। आत्माकी विशुद्धि आत्माके निज पुरुषार्थसे होगी और वह शुभ-अशुभ दोनों रागोंके निरोधसे होगी । तीर्थ-भूमियाँ हमारे लिए ऐसे साधन और अवसर प्रस्तुत करती हैं। वहाँ जाकर भक्त जन उस भूमिसे सम्बन्धित महापुरुषका स्मरण; स्तवन और पूजन करते हैं तथा उनके चरित्रसे प्रेरणा लेकर अपनी आत्माकी ओर उन्मुख होते हैं। पुण्यकी प्रक्रिया सरल है, आत्म-शुद्धिकी प्रक्रिया समझनेमें भी कठिन है और करने में भी।