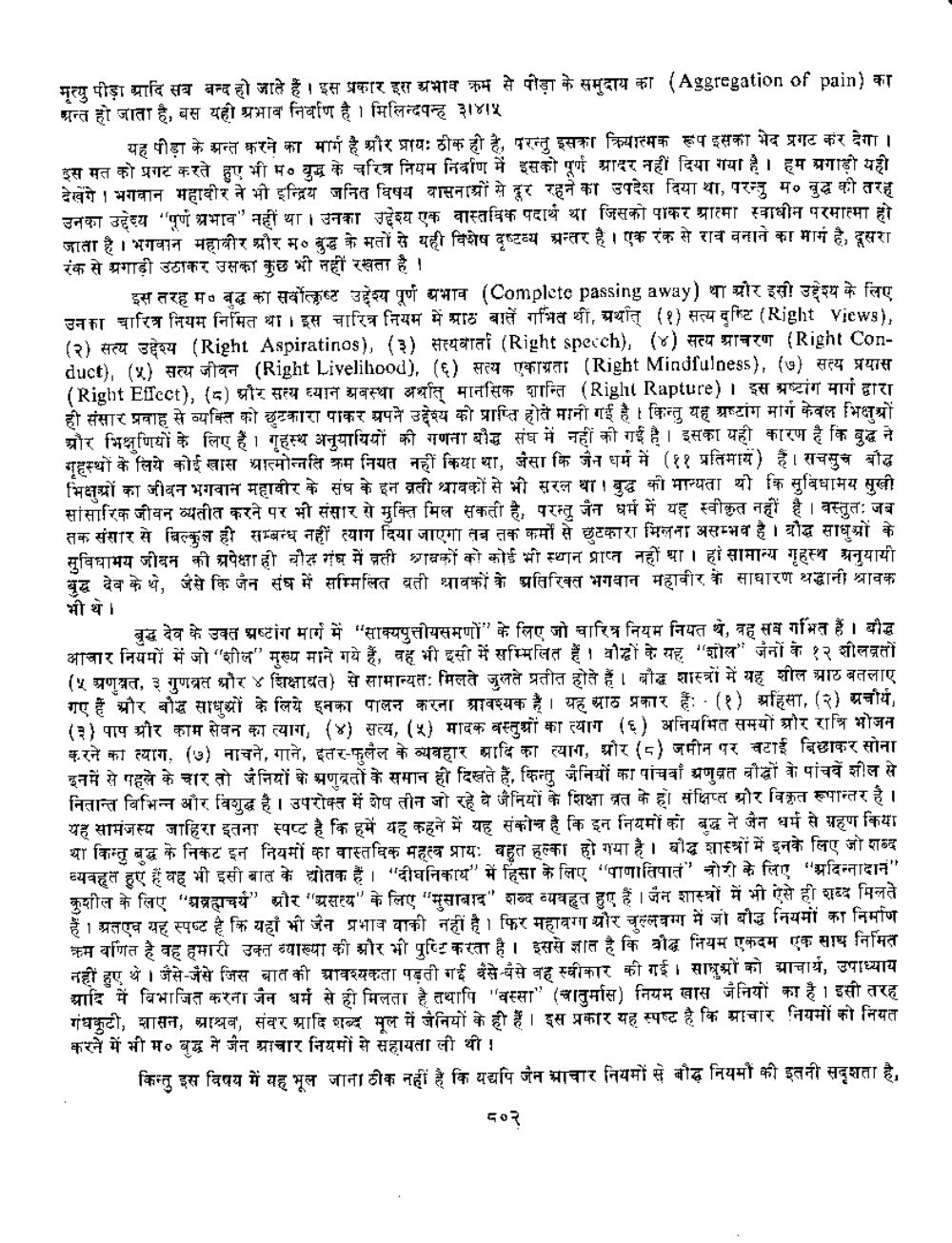________________
मृत्यु पीड़ा प्रादि सब बन्द हो जाते हैं । इस प्रकार इस अभाव क्रम से पीड़ा के समुदाय का (Aggregation of pain) का अन्त हो जाता है, बस यही प्रभाव निर्वाण है । मिलिन्दपन्ह ३।४५
यह पीड़ा के अन्त करने का मार्ग है और प्रायः ठीक ही है, परन्तु इसका क्रियात्मक रूप इसका भेद प्रगट कर देगा। इस मत को प्रगट करते हुए भी म० बुद्ध के चरित्र नियम निर्वाण में इसको पूर्ण आदर नहीं दिया गया है। हम अगाडी यही देखेंगे। भगवान महावीर ने भी इन्द्रिय जनित विषय वासनाओं से दूर रहने का उपदेश दिया था, परन्तु म. बुद्ध की तरह उनका उद्देश्य "पूर्ण प्रभाव" नहीं था। उनका उद्देश्य एक वास्तविक पदार्थ था जिसको पाकर प्रात्मा स्वाधीन परमात्मा हो जाता है। भगवान महावीर और म० बुद्ध के मतों से यही विशेष दृष्टव्य अन्तर है। एक रंक से राव बनाने का मार्ग है, दूसरा रंक से प्रगाड़ी उठाकर उसका कुछ भी नहीं रखता है।
इस तरह म बद्ध का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य पुर्ण अभाव (Complete passing away) था और इसी उद्देश्य के लिए उनका चारित्र नियम निर्मित था। इस चारित्र नियम में पाठ बातें गभित थीं, अर्थात् (१) सत्य दृष्टि (Right Views), (२) सत्य उद्देश्य (Right Aspiratinos), (३) सत्यवार्ता (Right speech), (४) सत्य पाचरण (Right Conduct), (५) सत्य जीवन (Right Livelihood), (६) सत्य एकाग्रता (Right Mindfulness), (७) सत्य प्रयास (Right Effect), (८) और सत्य ध्यान अवस्था अर्थात् मानसिक शान्ति (Right Rapture)। इस अष्टांग मार्ग द्वारा ही संसार प्रवाह से व्यक्ति को छुटकारा पाकर अपने उद्देश्य को प्राप्ति होते मानी गई है। किन्तु यह अष्टांग मार्ग केवल भिक्षत्रों और भिक्षुणियों के लिए हैं। गृहस्थ अनुयायियों की गणना बौद्ध संघ में नहीं की गई है। इसका यही कारण है कि बुद्ध ने गृहस्थों के लिये कोई खास प्रात्मोन्नति श्रम नियत नहीं किया था, जैसा कि जैन धर्म में (११ प्रतिमाय) हैं। सचमुच बौद्ध भिक्षयों का जीवन भगवान महावीर के संघ के इन व्रती थावकों से भी सरल था। बुद्ध की मान्यता थी कि सुविधामय सूखी सांसारिक जीवन व्यतीत करने पर भी संसार से मुक्ति मिल सकती है, परन्तु जैन धर्म में यह स्वीकृत नहीं है । वस्तुत: जब तक संसार से बिल्कुल ही सम्बन्ध नहीं त्याग दिया जाएगा तब तक कर्मों से छुटकारा मिलना असम्भव है। बौद्ध साधुओं के सुविधामय जीवन की अपेक्षा ही बौद्ध संघ में व्रती श्रावकों को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं था। हां सामान्य गृहस्थ अनुयायी बुद्ध देव के थे, जैसे कि जैन संघ में सम्मिलित व्रती थावकों के अतिरिक्त भगवान महावीर के साधारण श्रद्धानी श्रावक भी थे।
बुद्ध देव के उक्त अष्टांग मार्ग में "साक्यपुत्तीयसमणों" के लिए जो चारित्र नियम नियत थे, वह सब गभित हैं। बौद्ध आचार नियमों में जो "शील" मुख्य माने गये हैं, वह भी इसी में सम्मिलित हैं। वौद्धों के यह "शोल" जनों के १२ शीलव्रतों (५ अणुवत, ३ गुणव्रत और ४ शिक्षायत) से सामान्यत: मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। बौद्ध शास्त्रों में यह शील पाठ बतलाए गए हैं और बौद्ध साधुओं के लिये इनका पालन करना आवश्यक है। यह आठ प्रकार हैं: - (१) अहिंसा, (२) प्रचौर्य, (३) पाप और काम सेवन का त्याग, (४) सत्य, (५) मादक वस्तुनों का त्याग (६) अनियमित समयों और रात्रि भोजन करने का त्याग, (७) नाचने, गाने, इतर-फुलैल के व्यवहार आदि का त्याग, प्रौर (८) जमीन पर चटाई बिछाकर सोना इनमें से पहले के चार तो जैनियों के अणुबतों के समान ही दिखते हैं, किन्तु जैनियों का पांचवां अणुव्रत बौद्धों के पांचवें शील से नितान्त विभिन्न और विशुद्ध है। उपरोक्त में शेष तीन जो रहे वे जैनियों के शिक्षा व्रत के हो संक्षिप्त और विकृत रूपान्तर है। यह सामंजस्य जाहिरा इतना स्पष्ट है कि हमें यह कहने में यह संकोच है कि इन नियमों को बुद्ध ने जैन धर्म से ग्रहण किया था किन्तु बुद्ध के निकट इन नियमों का वास्तविक महत्व प्रायः बहुत हल्का हो गया है। बौद्ध शास्त्रों में इनके लिए जो शब्द व्यवहृत हुए हैं वह भी इसी बात के द्योतक है। "दीघनिकाय" में हिंसा के लिए "पाणातिपात' चोरी के लिए "अदिन्नादान" कुशील के लिए "प्रब्रह्मचर्य" और "असत्य" के लिए "मुसाबाद" शब्द व्यवहृत हुए हैं । जैन शास्त्रों में भी ऐसे ही शब्द मिलते हैं । अतएव यह स्पष्ट है कि यहाँ भी जैन प्रभाव वाकी नहीं है। फिर महावा और चल्लवग्ग में जो बौद्ध नियमों का निर्माण क्रम वणित है वह हमारी उक्त व्याख्या की और भी पुष्टि करता है। इससे ज्ञात है कि बौद्ध नियम एकदम एक साथ निर्मित नहीं हुए थे। जैसे-जैसे जिस बात की आवश्यकता पड़ती गई वैसे-वैसे वह स्वीकार की गई। साधुओं को आचार्य, उपाध्याय
आदि में विभाजित करना जैन धर्म से ही मिलता है तथापि "वस्सा" (चातुर्मास) नियम खास जैनियों का है। इसी तरह गंधकुटी, शासन, प्राथव', संवर आदि शब्द मूल में जैनियों के ही हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचार नियमों को नियत करने में भी म० बुद्ध मे जैन प्राचार नियमों से सहायता ली थी।
किन्तु इस विषय में यह भूल जाना ठीक नहीं है कि यद्यपि जैन आचार नियमों से बौद्ध नियमों की इतनी सदृशता है,
८०२