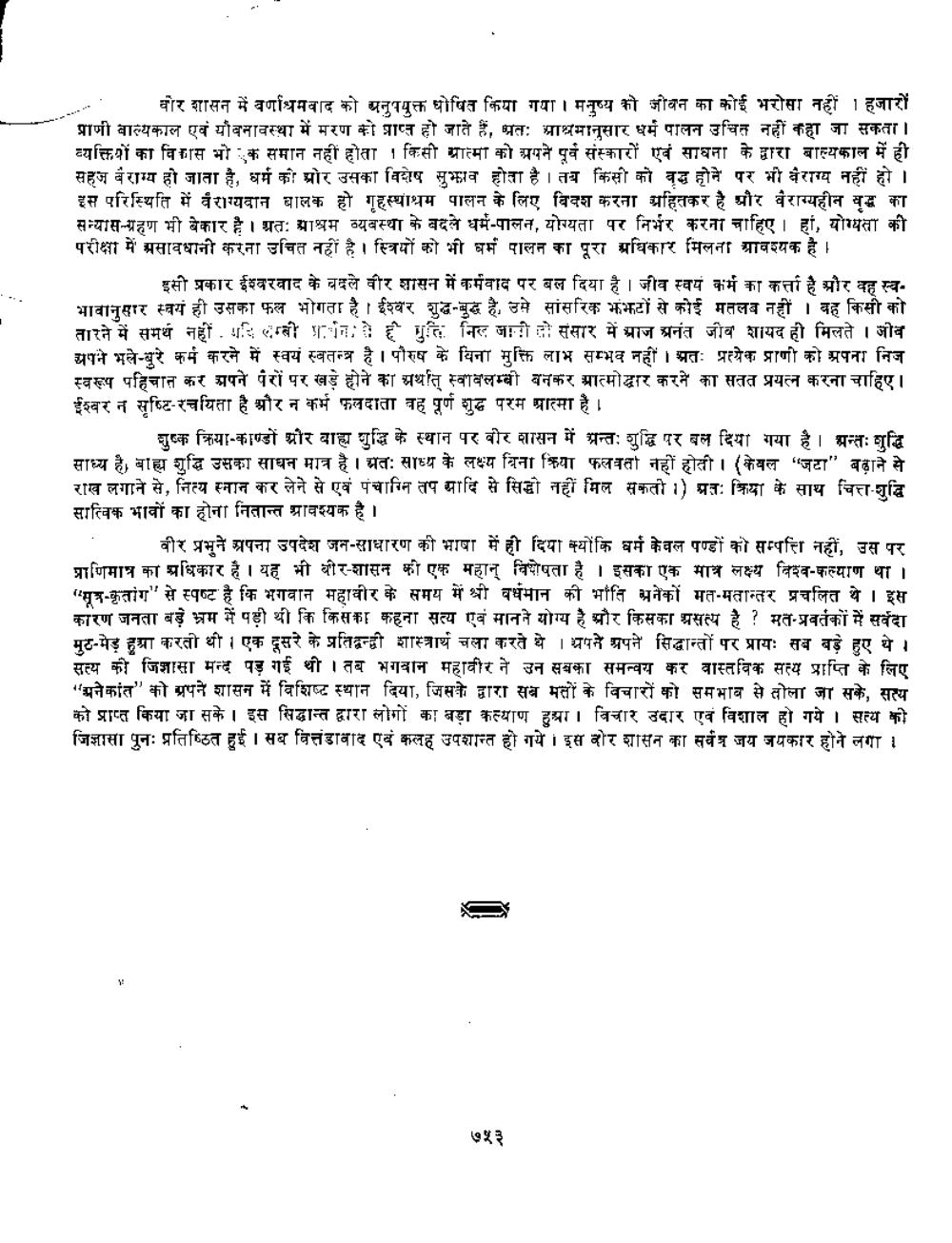________________
वीर शासन में वर्णाधमवाद को अनुपयुक्त घोषित किया गया। मनुष्य को जीवन का कोई भरोसा नहीं । हजारों प्राणी बाल्यकाल एवं यौवनावस्था में मरण को प्राप्त हो जाते हैं, अत: आश्रमानुसार धर्म पालन उचित नहीं कहा जा सकता। व्यक्तियों का विकास भोके समान नहीं होता । किसी प्रात्मा को अपने पूर्व संस्कारों एवं साधना के द्वारा बाल्यकाल में ही सहज वैराग्य हो जाता है, धर्म को प्रोर उसका विशेष सुझाव होता है । तब किसी को वृद्ध होने पर भी वैराग्य नहीं हो । इस परिस्थिति में वैराग्यवान बालक हो गृहस्थाश्रम पालन के लिए विवश करना अहितकर है और वैराग्यहीन वृद्ध का सन्यास-ग्रहण भी बेकार है। अत: आश्रम व्यवस्था के बदले धर्म-पालन, योग्यता पर निर्भर करना चाहिए। हां, योग्यता की परीक्षा में असावधानी करना उचित नहीं है। स्त्रियों को भी धर्म पालन का पूरा अधिकार मिलना यावश्यक है।
इसी प्रकार ईश्वरवाद के बदले वीर शासन में कर्मवाद पर बल दिया है । जीव स्वयं कर्म का कर्ता है और वह स्व. भावानुसार स्वयं ही उसका फल भोगता है। ईश्वर शुद्ध-बुद्ध है. उसे सांसरिक झंझटों से कोई मतलब नहीं । वह किसी को तारने में समर्थ नहीं . लम्बी पनि ह मुक्ति मिल जाती तो संसार में आज अनंत जीव' शायद ही मिलते । जीव अपने भले-बुरे कर्म करने में स्वयं स्वतन्त्र है । पौरुष के विना मुक्ति लाभ सम्भव नहीं। अतः प्रत्येक प्राणी को अपना निज स्वरूप पहिचान कर अपने घरों पर खड़े होने का अर्थात् स्वावलम्बी बनकर आत्मोद्धार करने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर ने सृष्टि-रचयिता है और न कर्म फलदाता वह पूर्ण शुद्ध परम प्रात्मा है।
शुष्क क्रिया-काण्डों और बाह्य शुद्धि के स्थान पर वीर शासन में अन्तः शुद्धि पर बल दिया गया है। अन्तः शुद्धि साध्य है, बाह्य शुद्धि उसका साधन मात्र है । अत: साध्य के लक्ष्य बिना क्रिया फलवता नहीं होती। (केवल "जटा" बढ़ाने से राख लगाने से, नित्य स्नान कर लेने से एवं पंचाग्मि तप मादि से सिद्धो नहीं मिल सकती।) प्रतः क्रिया के साथ चित्त-शद्धि सात्विक भावों का होना नितान्त आवश्यक है।
वीर प्रभुने अपना उपदेश जन-साधारण की भाषा में ही दिया क्योंकि धर्म केवल पण्डों को सम्पत्ति नहीं, उस पर प्राणिमात्र का अधिकार है। यह भी बीर-शासन की एक महान् विशेषता है । इसका एक मात्र लक्ष्य विश्व-कल्याण था। सत्र-कृतांग" से स्पष्ट है कि भगवान महावीर के समय में श्री वर्धमान की भांति अनेकों मत-मतान्तर प्रचलित थे । इस कारण जनता बड़े भ्रम में पड़ी थी कि किसका कहना सत्य एवं मानने योग्य है और किसका असत्य है ? मत-प्रवर्तकों में सर्वदा मुठ-मेड़ हुआ करती थी। एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी शास्त्रार्थ चला करते थे । अपने अपने सिद्धान्तों पर प्रायः सब बड़े हए थे। सत्य की जिज्ञासा मन्द पड़ गई थी। तब भगवान महावीर ने उन सबका समन्वय कर वास्तविक सत्य प्राप्ति के लिए "अनेकांत" को अपने शासन में विशिष्ट स्थान दिया, जिसके द्वारा सब मतों के विचारों को समभाव से तोला जा सके, सत्य को प्राप्त किया जा सके। इस सिद्धान्त द्वारा लोगों का बड़ा कल्याण हया। विचार उदार एवं विशाल हो गये। सत्य को जिज्ञासा पुनः प्रतिष्ठित हुई । सब वित्तंडावाद एवं कलह उपशान्त हो गये। इस शेर शासन का सर्वत्र जय जयकार होने लगा।