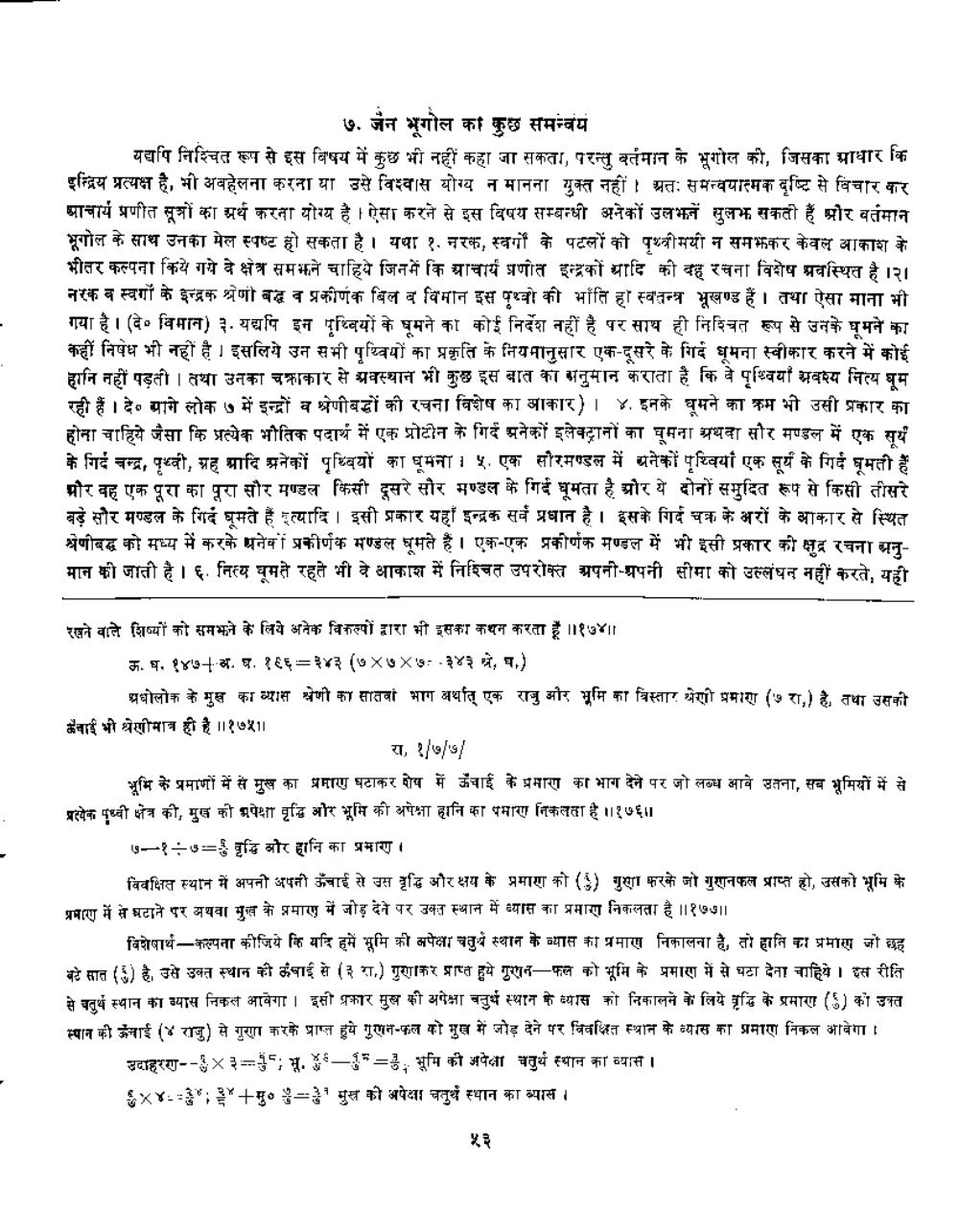________________
७. जैन भूगोल का कुछ समन्वय
यद्यपि निश्चित रूप से इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, परन्तु वर्तमान के भूगोल की, जिसका आधार कि इन्द्रिय प्रत्यक्ष है, भी अवहेलना करना था उसे विश्वास योग्य न मानना युक्त नहीं। अतः समन्वयात्मक दृष्टि से विचार कर आचार्य प्रणीत सूत्रों का अर्थ करना योग्य है। ऐसा करने से इस विषय सम्वन्धी अनेकों उलझनें सुलझ सकती हैं और वर्तमान भूगोल के साथ उनका मेल स्पष्ट हो सकता है यथा १. नरक, स्वयों के पटलों को पृथ्वीमयी न समझकर केवल आकाश के भीतर कल्पना किये गये वे क्षेत्र समझने चाहिये जिनमें कि प्राचार्य प्रणीत इन्द्रकों आदि की वह रचना विशेष अवस्थित है |२| नरक व स्वगों के इन्द्रक श्रेणी बद्ध व प्रकीर्णक बिल व विमान इस पृथ्वी की भाँति हा स्वतन्त्र भूखण्ड हैं । तथा ऐसा माना भी गया है । (दे० विमान ) ३. यद्यपि इन पृथ्वियों के घूमने का कोई निर्देश नहीं है पर साथ ही निश्चित रूप से उनके घूमने का कहीं निषेध भी नहीं है । इसलिये उन सभी पृथ्वियों का प्रकृति के नियमानुसार एक-दूसरे के गिर्द घूमना स्वीकार करने में कोई हानि नहीं पड़ती । तथा उनका चक्राकार से अवस्थान भी कुछ इस बात का अनुमान कराता है कि वे पृथ्वियाँ अवश्य नित्य घूम रही हैं । दे० मागे लोक ७ में इन्द्रों व श्रेणीबद्धों की रचना विशेष का आकार ) ४. इनके घूमने का क्रम भी उसी प्रकार का होना चाहिये जैसा कि प्रत्येक भौतिक पदार्थ में एक प्रोटीन के गिर्द अनेकों इलेक्ट्रानों का घूमना अथवा सौर मण्डल में एक सूर्य के गिर्द चन्द्र पृथ्वी ग्रह आदि अनेकों पृथ्वियों का घूमना ५. एक सौरमण्डल में अनेकों पृथ्वियां एक सूर्य के गिर्द घूमती है और वह एक पूरा का पूरा सौर मण्डल किसी दूसरे सौर मण्डल के गिर्द घूमता है और ये दोनों समुदित रूप से किसी तीसरे बड़े सौर मण्डल के गिर्द घूमते हैं इत्यादि। इसी प्रकार यहाँ इन्द्रक सर्वे प्रधान है। इसके गिर्द पत्र के अरों के आकार से स्थित श्रेणीबद्ध को मध्य में करके धनेव प्रकीर्णक मण्डल घूमते हैं एक-एक प्रकीर्णक मण्डल में भी इसी प्रकार की क्षुद्र रचना अनु मान की जाती है । ६. नित्य घूमते रहते भी रे आकाश में निश्चित उपरोक्त अपनी-अपनी सीमा को उल्लंघन नहीं करते, वही
रखने वाले शिष्यों को समझने के लिये अनेक विकल्पों द्वारा भी इसका कथन करता हूँ || १७४ ॥
क. घ. १४७ - अ. घ. १६६ = ३४३ (७७७ ३४३, घ)
अधोलोक के मुख का व्यास श्रेणी का सातवां भाग अर्थात् एक राजु और भूमि का विस्तार श्रेणी प्रमाण (७ रा ) है, तथा उसकी नाई भी खीमा ही है ।। १७५ ।।
भूमि के प्रमाणों में से मुख का प्रत्येक पृथ्वी क्षेत्र की मुख की अपेक्षा वृद्धि
रा, १/७/७/
प्रमाण घटाकर शेष में ऊँचाई के प्रमाण का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना सब भूमियों में से और भूमि की अपेक्षा हानि का प्रमाण किता है ॥१७६॥
७- १ ÷ ७ = वृद्धि और हानि का प्रमाण ।
विवक्षित स्थान में अपनी अपनी ऊँचाई से उस वृद्धि और क्षय के
प्रमाण में से घटाने पर अथवा मुख के प्रमाण में जोड़ देने पर उक्त स्थान में व्यास का प्रमाण निकलता है || १७७ ||
प्रमाण को (3) गुणा करके जो गुणनफल प्राप्त हो, उसको भूमि के
विशेषार्थ – कल्पना कीजिये कि यदि हमें भूमि की अपेक्षा चतुर्थ स्थान के व्यास का प्रमाण निकालना है, तो हाति का प्रभाग जो छह बटे खात (5) है, उसे उक्त स्थान की ऊँचाई से (३) प्राप्त हुये गुणनफल को भूमि के प्रमाण में से घटा देना चाहिये। इस रीति से चतुर्थ स्थान का व्यास निकल आयेगा। इसी प्रकार मुख की अपेक्षा चतुर्थ स्थान के व्यास को निकालने के लिये वृद्धि के प्रमाण (5) को उक्त स्थान की ऊँचाई (४ राजु) से गुणा करके प्राप्त हुये गुणनफल को मुख में जोड़ देने पर विवक्षित स्थान के व्यास का प्रमाण निकल आवेगा । भूमि की अपेक्षा चतुर्थ स्थान का व्यास ।
उदाहरण-- ३३=
भू.
5 × ४ : 33+ मु० डे मुख की अपेक्षा चतुर्थ स्थान का व्यास ।
५.३