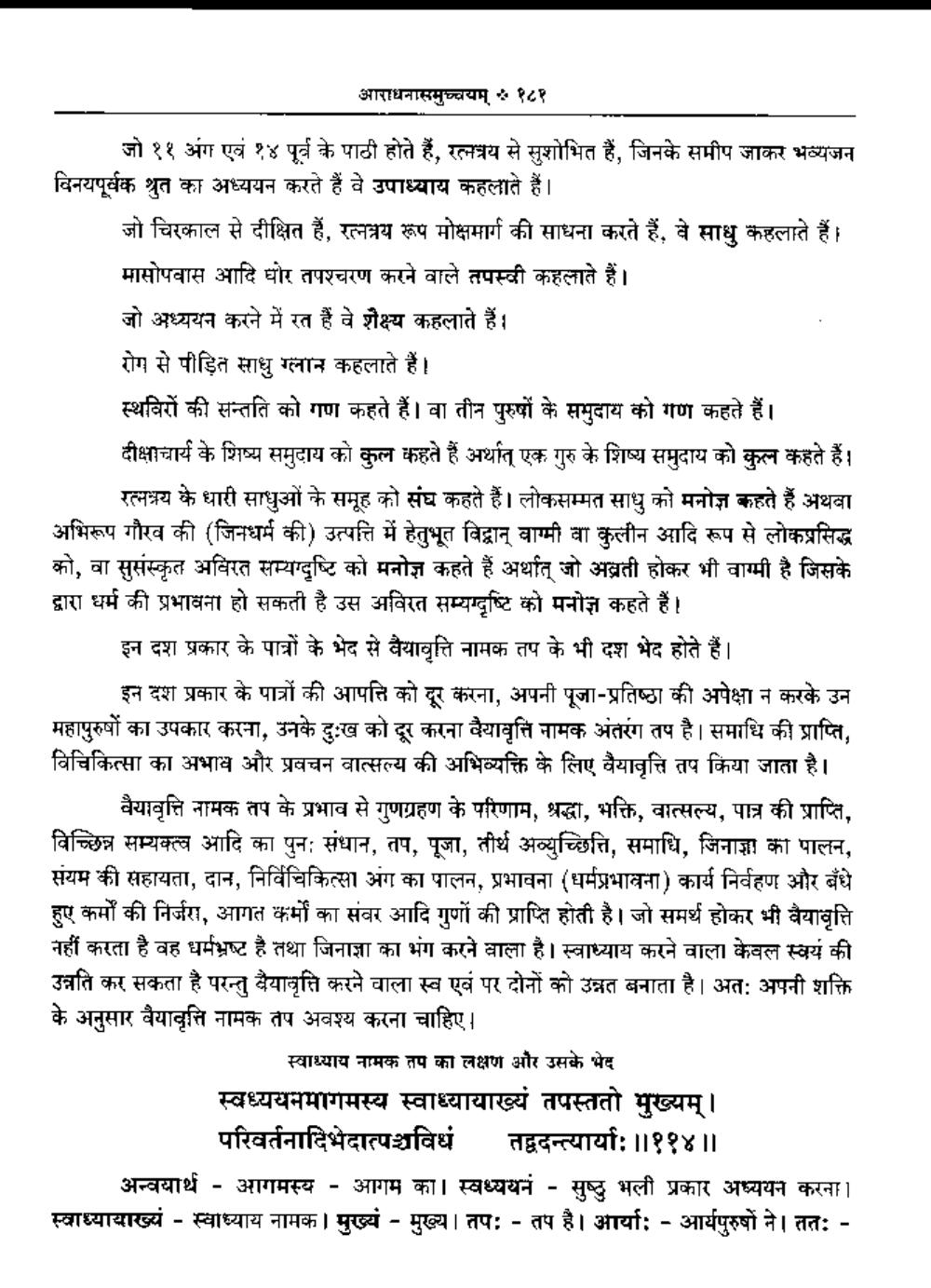________________
आराधनासमुच्चयम् १८१
जो ११ अंग एवं १४ पूर्व के पाठी होते हैं, रत्नत्रय से सुशोभित हैं, जिनके समीप जाकर भव्यजन विनयपूर्वक श्रुत का अध्ययन करते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं।
जो चिरकाल से दीक्षित हैं, रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग की साधना करते हैं, वे साधु कहलाते हैं। मासोपवास आदि घोर तपश्चरण करने वाले तपस्वी कहलाते हैं। जो अध्ययन करने में रत हैं वे शैक्ष्य कहलाते हैं। रोग से पीड़ित साधु ग्लान कहलाते हैं। स्थविरों की सन्तति को गण कहते हैं। वा तीन पुरुषों के समुदाय को गण कहते हैं। दीक्षाचार्य के शिष्य समुदाय को कुल कहते हैं अर्थात् एक गुरु के शिष्य समुदाय को कुल्ल कहते हैं।
रत्नत्रय के धारी साधुओं के समूह को संघ कहते हैं। लोकसम्मत साधु को मनोज्ञ कहते हैं अथवा अभिरूप गौरव की (जिनधर्म की) उत्पत्ति में हेतुभूत विद्वान् वाग्मी वा कुलीन आदि रूप से लोकप्रसिद्ध को, वा सुसंस्कृत अविरत सम्यग्दृष्टि को मनोज्ञ कहते हैं अर्थात् जो अव्रती होकर भी वाग्मी है जिसके द्वारा धर्म की प्रभावना हो सकती है उस अविरत सम्यग्दृष्टि को मनोज्ञ कहते हैं। ___ इन दश प्रकार के पात्रों के भेद से वैयावृत्ति नामक तप के भी दश भेद होते हैं।
इन दश प्रकार के पात्रों की आपत्ति को दूर करना, अपनी पूजा-प्रतिष्ठा की अपेक्षा न करके उन महापुरुषों का उपकार करना, उनके दुःख को दूर करना वैयावृत्ति नामक अंतरंग तप है। समाधि की प्राप्ति, विचिकित्सा का अभाव और प्रवचन वात्सल्य की अभिव्यक्ति के लिए वैयावृत्ति तप किया जाता है।
वैयावृत्ति नामक तप के प्रभाव से गुणग्रहण के परिणाम, श्रद्धा, भक्ति, वात्सल्य, पात्र की प्राप्ति, विच्छिन्न सम्यक्त्व आदि का पुन: संधान, तप, पूजा, तीर्थ अव्युच्छित्ति, समाधि, जिनाज्ञा का पालन, संयम की सहायता, दान, निर्विचिकित्सा अंग का पालन, प्रभावना (धर्मप्रभावना) कार्य निर्वहण और बँधे हुए कर्मों की निर्जरा, आगत कर्मों का संवर आदि गुणों की प्राप्ति होती है। जो समर्थ होकर भी वैयावृत्ति नहीं करता है वह धर्मभ्रष्ट है तथा जिनाज्ञा का भंग करने वाला है। स्वाध्याय करने वाला केवल स्वयं की उन्नति कर सकता है परन्तु वैयावृत्ति करने वाला स्व एवं पर दोनों को उन्नत बनाता है। अत: अपनी शक्ति के अनुसार वैयावृत्ति नामक तप अवश्य करना चाहिए।
स्वाध्याय नामक तप का लक्षण और उसके भेद स्वध्ययनमागमस्य स्वाध्यायाख्यं तपस्ततो मुख्यम्।
परिवर्तनादिभेदात्पशविधं तद्वदन्त्यार्याः ॥११४ ॥ अन्वयार्थ - आगमस्य - आगम का। स्वध्ययनं - सुष्टु भली प्रकार अध्ययन करना । स्वाध्यायाख्यं - स्वाध्याय नामक । मुख्यं - मुख्य । तपः - तप है। आर्याः - आर्यपुरुषों ने । ततः -