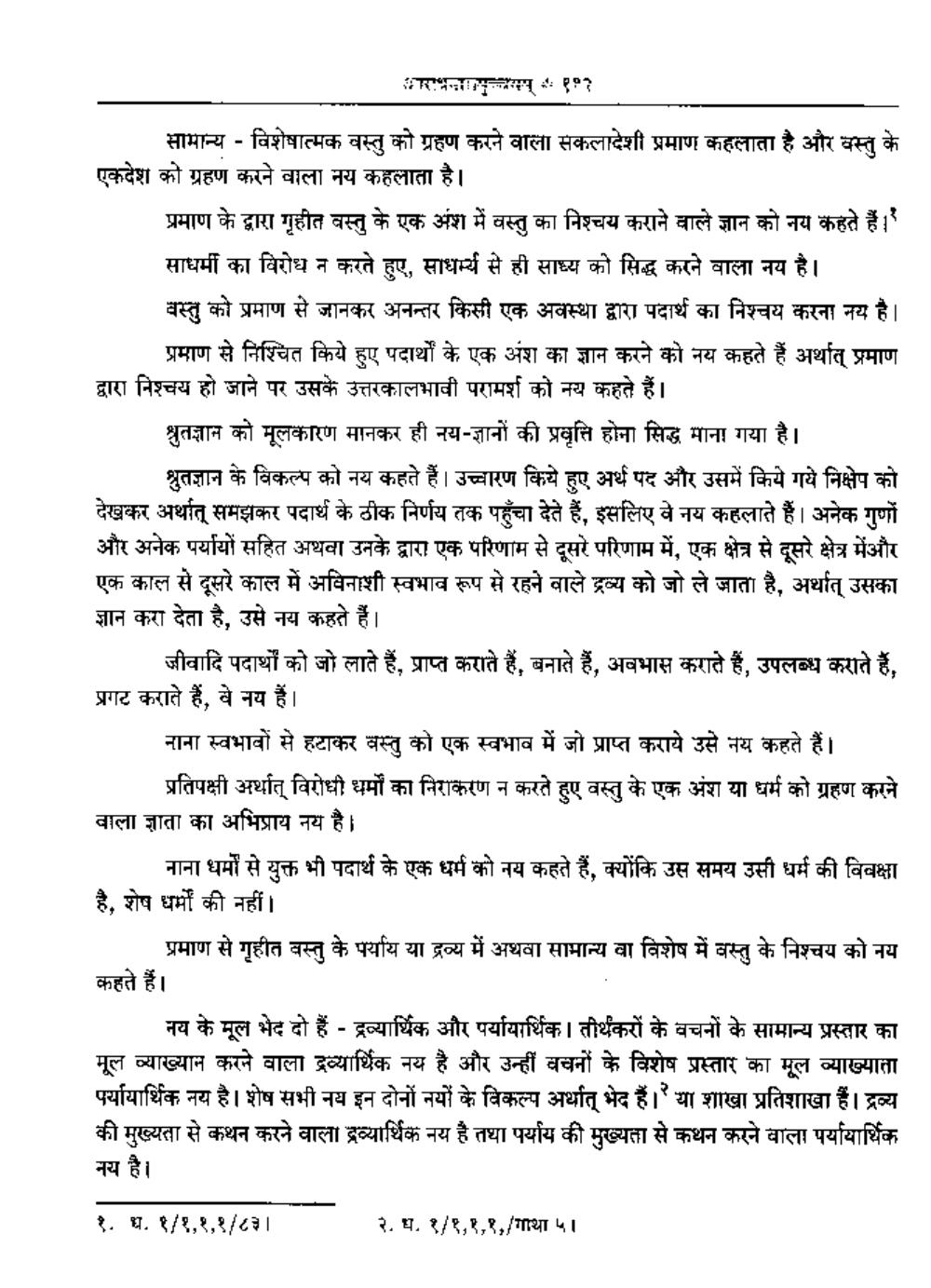________________
भन्तपुर ९११
के
सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ग्रहण करने वाला सकलादेशी प्रमाण कहलाता है और वस्तु एकदेश को ग्रहण करने वाला नय कहलाता है।
प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु के एक अंश में वस्तु का निश्चय कराने वाले ज्ञान को नय कहते हैं । ' साधर्मी का विरोध न करते हुए, साधर्म्य से ही साध्य को सिद्ध करने वाला नय है। वस्तुको प्रमाण से जानकर अनन्तर किसी एक अवस्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना नय है। प्रमाण से निश्चित किये हुए पदार्थों के एक अंश का ज्ञान करने को नय कहते हैं अर्थात् प्रमाण द्वारा निश्चय हो जाने पर उसके उत्तरकालभावी परामर्श को नय कहते हैं।
श्रुतज्ञान को मूलकारण मानकर ही नय ज्ञानों की प्रवृत्ति होना सिद्ध माना गया है।
श्रुतज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं। उच्चारण किये हुए अर्थ पद और उसमें किये गये निक्षेप को देखकर अर्थात् समझकर पदार्थ के ठीक निर्णय तक पहुँचा देते हैं, इसलिए वे नय कहलाते हैं। अनेक गुणों और अनेक पर्यायों सहित अथवा उनके द्वारा एक परिणाम से दूसरे परिणाम में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र मेंऔर एक काल से दूसरे काल में अविनाशी स्वभाव रूप से रहने वाले द्रव्य को जो ले जाता है, अर्थात् उसका ज्ञान करा देता है, उसे नय कहते हैं ।
जीवादि पदार्थों को जो लाते हैं, प्राप्त कराते हैं, बनाते हैं, अवभास कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, प्रगट कराते हैं, वे नय हैं।
नाना स्वभावों से हटाकर वस्तु को एक स्वभाव में जो प्राप्त कराये उसे नय कहते हैं।
प्रतिपक्षी अर्थात् विरोधी धर्मो का निराकरण न करते हुए वस्तु के एक अंश या धर्म को ग्रहण करने वाला ज्ञाता का अभिप्राय नय है।
नाना धर्मों से युक्त भी पदार्थ के एक धर्म को नय कहते हैं, क्योंकि उस समय उसी धर्म की विवक्षा है, शेष धर्मों की नहीं ।
प्रमाण से गृहीत वस्तु के पर्याय या द्रव्य में अथवा सामान्य वा विशेष में वस्तु के निश्चय को नय कहते हैं।
नय के मूल भेद दो हैं- द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। तीर्थंकरों के वचनों के सामान्य प्रस्तार का मूल व्याख्यान करने वाला द्रव्यार्थिक नय है और उन्हीं वचनों के विशेष प्रस्तार का मूल व्याख्याता पर्यायार्थिक नय है । शेष सभी नय इन दोनों नयों के विकल्प अर्थात् भेद हैं। या शाखा प्रतिशाखा हैं। द्रव्य की मुख्यता से कथन करने वाला द्रव्यार्थिक नय है तथा पर्याय की मुख्यता से कथन करने वाला पर्यायार्थिक नय है।
१. ध. १/१,९,१/८३ ।
२. ध. १/१, १, १, / गाथा ५।