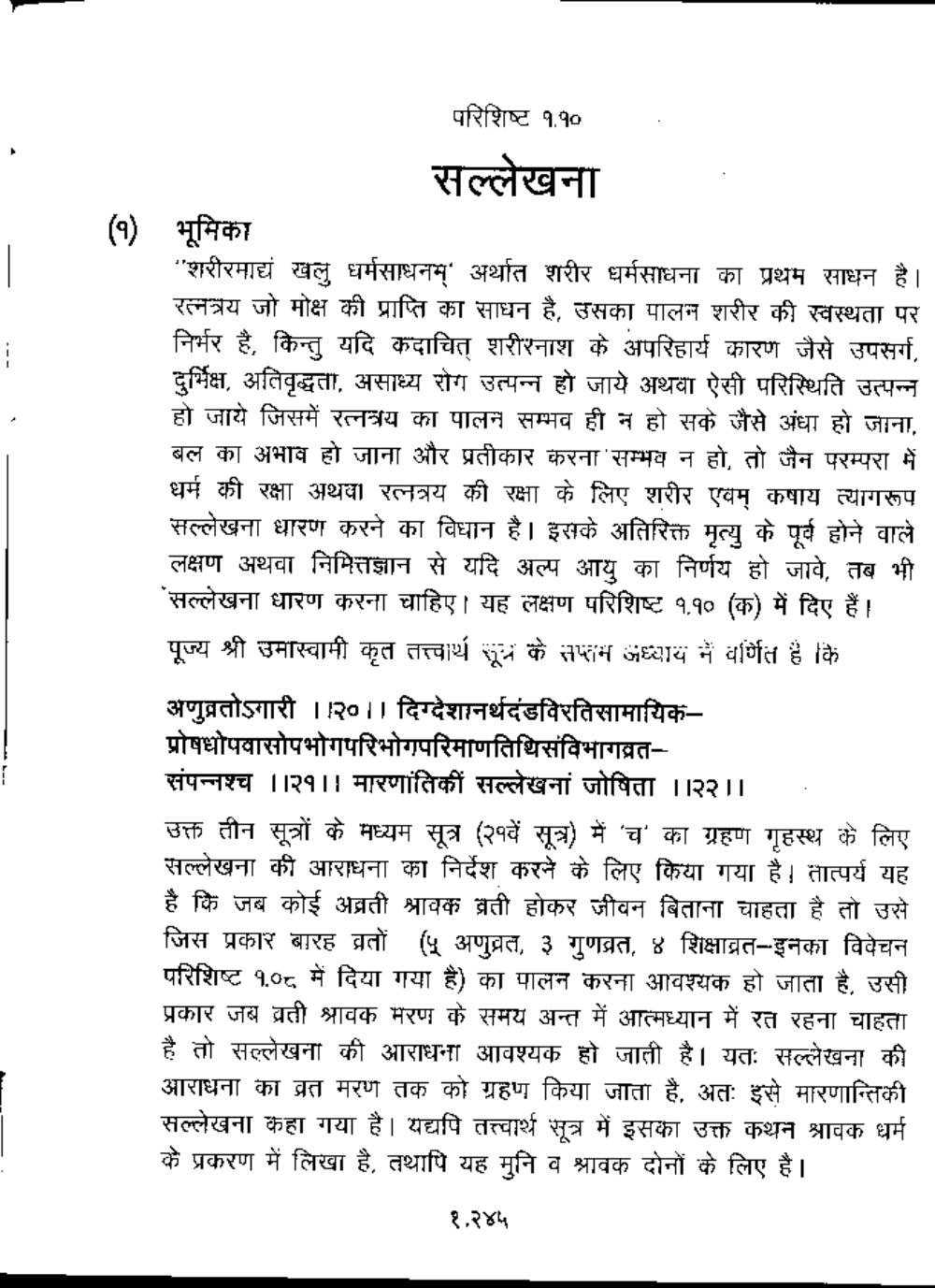________________
|
परिशिष्ट १.१०
सल्लेखना
(१) भूमिका
"शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् अर्थात शरीर धर्मसाधना का प्रथम साधन है I रत्नत्रय जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, उसका पालन शरीर की स्वस्थता पर निर्भर है, किन्तु यदि कदाचित् शरीरनाश के अपरिहार्य कारण जैसे उपसर्ग, दुर्भिक्ष, अतिवृद्धता, असाध्य रोग उत्पन्न हो जाये अथवा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाये जिसमें रत्नत्रय का पालन सम्भव ही न हो सके जैसे अंधा हो जाना, बल का अभाव हो जाना और प्रतीकार करना सम्भव न हो, तो जैन परम्परा में धर्म की रक्षा अथवा रत्नत्रय की रक्षा के लिए शरीर एवम् कषाय त्यागरूप सल्लेखना धारण करने का विधान है। इसके अतिरिक्त मृत्यु के पूर्व होने वाले लक्षण अथवा निमित्तज्ञान से यदि अल्प आयु का निर्णय हो जावे, तब भी " सल्लेखना धारण करना चाहिए। यह लक्षण परिशिष्ट १.१० (क) में दिए हैं। पूज्य श्री उमास्वामी कृत तत्त्वार्थ सूत्र के सप्तम अध्याय में वर्णित है कि
अणुव्रतोऽगारी ।। २० ।। दिग्देशानर्थदंडविरतिसामायिक
प्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणतिथिसंविभागव्रत
संपन्नश्च ||२१|| मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता ।। २२ ।।
उक्त तीन सूत्रों के मध्यम सूत्र ( २१ वें सूत्र) में 'च' का ग्रहण गृहस्थ के लिए सल्लेखना की आराधना का निर्देश करने के लिए किया गया है। तात्पर्य यह हैं कि जब कोई अव्रती श्रावक व्रती होकर जीवन बिताना चाहता है तो उसे जिस प्रकार बारह व्रतों (५ अणुव्रत ३ गुणव्रत ४ शिक्षाव्रत - इनका विवेचन परिशिष्ट १.०८ में दिया गया है) का पालन करना आवश्यक हो जाता है, उसी प्रकार जब व्रती श्रावक मरण के समय अन्त में आत्मध्यान में रत रहना चाहता है तो सल्लेखना की आराधना आवश्यक हो जाती है । यतः सल्लेखना की आराधना का व्रत मरण तक को ग्रहण किया जाता है, अतः इसे मारणान्तिकी सल्लेखना कहा गया है । यद्यपि तत्त्वार्थ सूत्र में इसका उक्त कथन श्रावक धर्म के प्रकरण में लिखा है, तथापि यह मुनि व श्रावक दोनों के लिए है ।
१.२४५