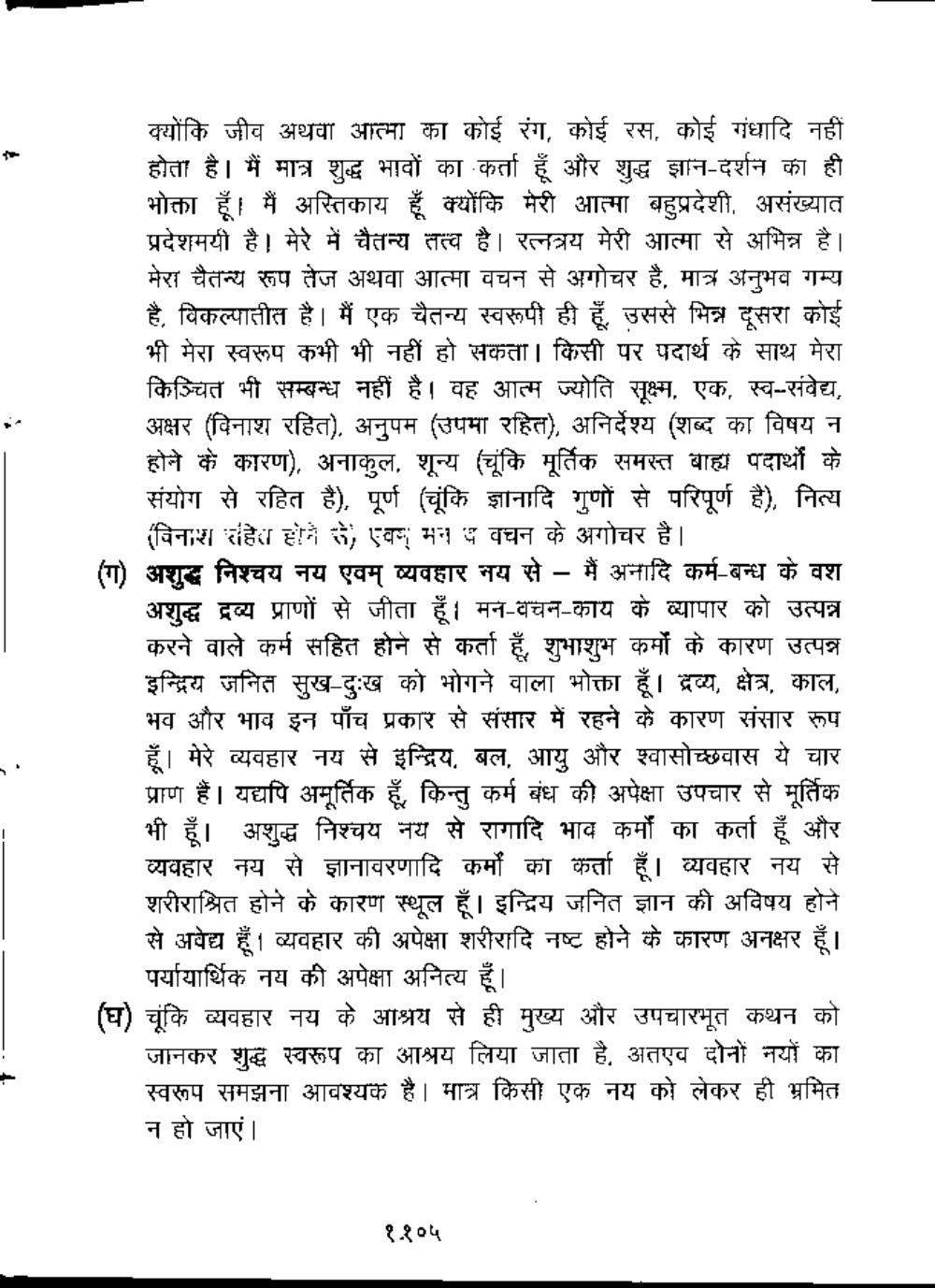________________
क्योंकि जीव अथवा आत्मा का कोई रंग, कोई रस, कोई गंधादि नहीं होता है। मैं मात्र शुद्ध भावों का कर्ता हूँ और शुद्ध ज्ञान-दर्शन का ही भोक्ता हूँ। मैं अस्तिकाय हूँ क्योंकि मेरी आत्मा बहुप्रदेशी, असंख्यात प्रदेशमयी है। मेरे में चैतन्य तत्व है। रत्नत्रय मेरी आत्मा से अभिन्न है। मेरा चैतन्य रूप तेज अथवा आत्मा वचन से अगोचर है, मात्र अनुभव गम्य है, विकल्पातीत है। मैं एक चैतन्य स्वरूपी ही हूँ, उससे भिन्न दूसरा कोई भी मेरा स्वरूप कभी भी नहीं हो सकता। किसी पर पदार्थ के साथ मेरा किञ्चित भी सम्बन्ध नहीं है। वह आत्म ज्योति सूक्ष्म, एक, स्व-संवेद्य, अक्षर (विनाश रहित), अनुपम (उपमा रहित), अनिर्देश्य (शब्द का विषय न होने के कारण), अनाकुल, शून्य (चूंकि मूर्तिक समस्त बाह्य पदार्थों के संयोग से रहित है), पूर्ण (चूंकि ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण है), नित्य
(विनाश रहा होने ते, एवम् मन वचन के अगोचर है। (ग) अशुद्ध निश्चय नय एवम् व्यवहार नय से - मैं अनादि कर्म-बन्ध के वश
अशुद्ध द्रव्य प्राणों से जीता हूँ। मन-वचन-काय के व्यापार को उत्पन्न करने वाले कर्म सहित होने से कर्ता हूँ, शुभाशुभ कर्मों के कारण उत्पन्न इन्द्रिय जनित सुख-दुःख को भोगने वाला भोक्ता हूँ। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव इन पाँच प्रकार से संसार में रहने के कारण संसार रूप हूँ। मेरे व्यवहार नय से इन्द्रिय. बल, आयु और श्वासोच्छवास ये चार प्राण हैं। यद्यपि अमूर्तिक हूँ, किन्तु कर्म बंध की अपेक्षा उपचार से मूर्तिक भी हूँ। अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव कर्मों का कर्ता हूँ और व्यवहार नय से ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता हूँ। व्यवहार नय से शरीराश्रित होने के कारण स्थूल हूँ। इन्द्रिय जनित ज्ञान की अविषय होने से अवेद्य हूँ। व्यवहार की अपेक्षा शरीरादि नष्ट होने के कारण अनक्षर हूँ|
पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अनित्य हूँ। (घ) चूंकि व्यवहार नय के आश्रय से ही मुख्य और उपचारभूत कथन को
जानकर शुद्ध स्वरूप का आश्रय लिया जाता है. अतएव दोनों नयों का स्वरूप समझना आवश्यक है। मात्र किसी एक नय को लेकर ही भ्रमित न हो जाएं।
१.१०५