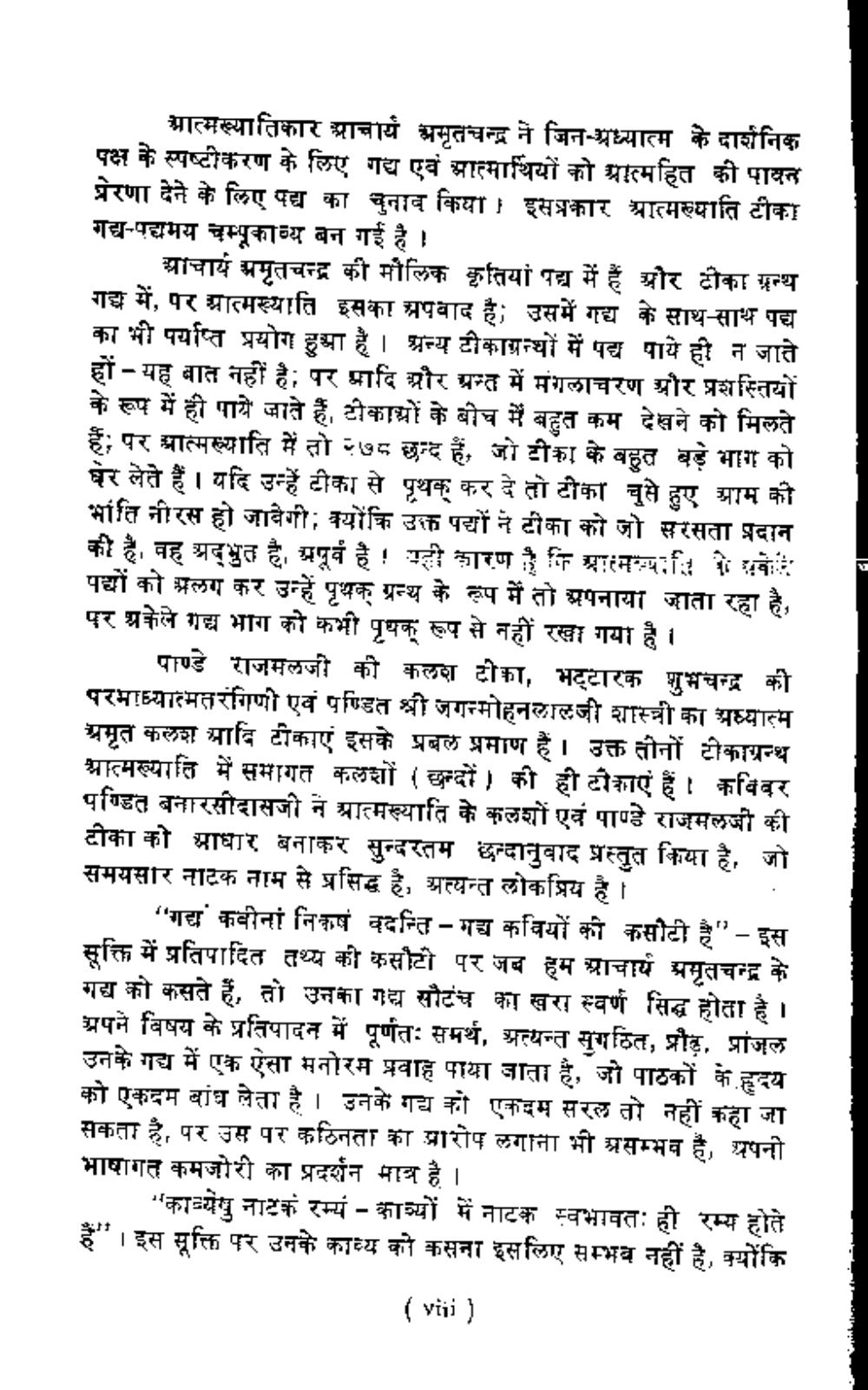________________
आत्मख्यातिकार आचार्य अमृतचन्द्र ने जिन-अध्यात्म के दार्शनिक पक्ष के स्पष्टीकरण के लिए गद्य एवं आत्मार्थियों को प्रात्महित की पावन प्रेरणा देने के लिए पद्य का चुनाव किया। इसप्रकार प्रात्मख्याति टीका गद्य-पद्यमय चम्पूकाव्य बन गई है।
___ आचार्य अमृतचन्द्र की मौलिक कृतियां पद्य में हैं और टीका ग्रन्थ गद्य में, पर यात्मख्याति इसका अपवाद है; उसमें गद्य के साथ-साथ पद्य का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है। अन्य टीकाग्रन्थों में पद्य पाये ही न जाते हों- यह बात नहीं है; पर प्रादि और अन्त में मंगलाचरण और प्रशस्तियों के रूप में ही पाये जाते हैं, टीकायों के बीच में बहुत कम देखने को मिलते हैं, पर प्रात्मख्याति में तो २७८ छन्द हैं, जो टीका के बहुत बड़े भाग को घेर लेते हैं। यदि उन्हें टीका से पृथक कर दे तो टीका चुसे हए आम की भांति नीरस हो जावेगी; क्योंकि उक्त पद्यों ने टीका को जो सरसता प्रदान की है, वह अद्भुत है, अपूर्व है ! यही कारण है कि प्रात्मयादि के एक पद्यों को अलग कर उन्हें पृथक ग्रन्थ के रूप में तो अपनाया जाता रहा है, पर अकेले गद्य भाग को कभी पृथक रूप से नहीं रखा गया है।
पाण्डे राजमलजी की कलश टीका, भट्टारक शुभचन्द्र की परमाध्यात्मतरंगिणी एवं पण्डित श्री जगन्मोहनलालजी शास्त्री का अध्यात्म अमृत कलश आदि टीकाएं इसके प्रबल प्रमाण हैं। उक्त तीनों टीकाग्रन्थ आत्मख्याति में समागत कलशों ( छन्दों) की ही टोकाएं हैं। कविवर पण्डित बनारसीदासजी ने प्रात्मख्याति के कलशों एवं पाण्डे राजमलजी की टीका को आधार बनाकर सुन्दरतम छन्दानुवाद प्रस्तुत किया है, जो समयसार नाटक नाम से प्रसिद्ध है, अत्यन्त लोकप्रिय है ।
__ "गद्य कवीनां निकष वदन्ति - मद्य कवियों की कसौटी है" - इस सक्ति में प्रतिपादित तथ्य की कसौटी पर जब हम प्राचार्य अमृतचन्द्र के गद्य को कसते हैं, तो उनका गद्य सौटंच का खरा स्वर्ण सिद्ध होता है। अपने विषय के प्रतिपादन में पूर्णतः समर्थ, अत्यन्त सुगठित, प्रौढ़, प्रांजल उनके गद्य में एक ऐसा मनोरम प्रवाह पाया जाता है, जो पाठकों के हृदय को एकदम बांध लेता है। उनके गद्य को एकदम सरल तो नहीं कहा जा सकता है, पर उस पर कठिनता का आरोप लगाना भी असम्भव है, अपनी भाषागत कमजोरी का प्रदर्शन मात्र है ।
"कान्येषु नाटकं रम्यं - काश्यों में नाटक स्वभावतः ही रम्य होते हैं। इस सूक्ति पर उनके काव्य को कसना इस लिए सम्भव नहीं है, क्योंकि
(viii)