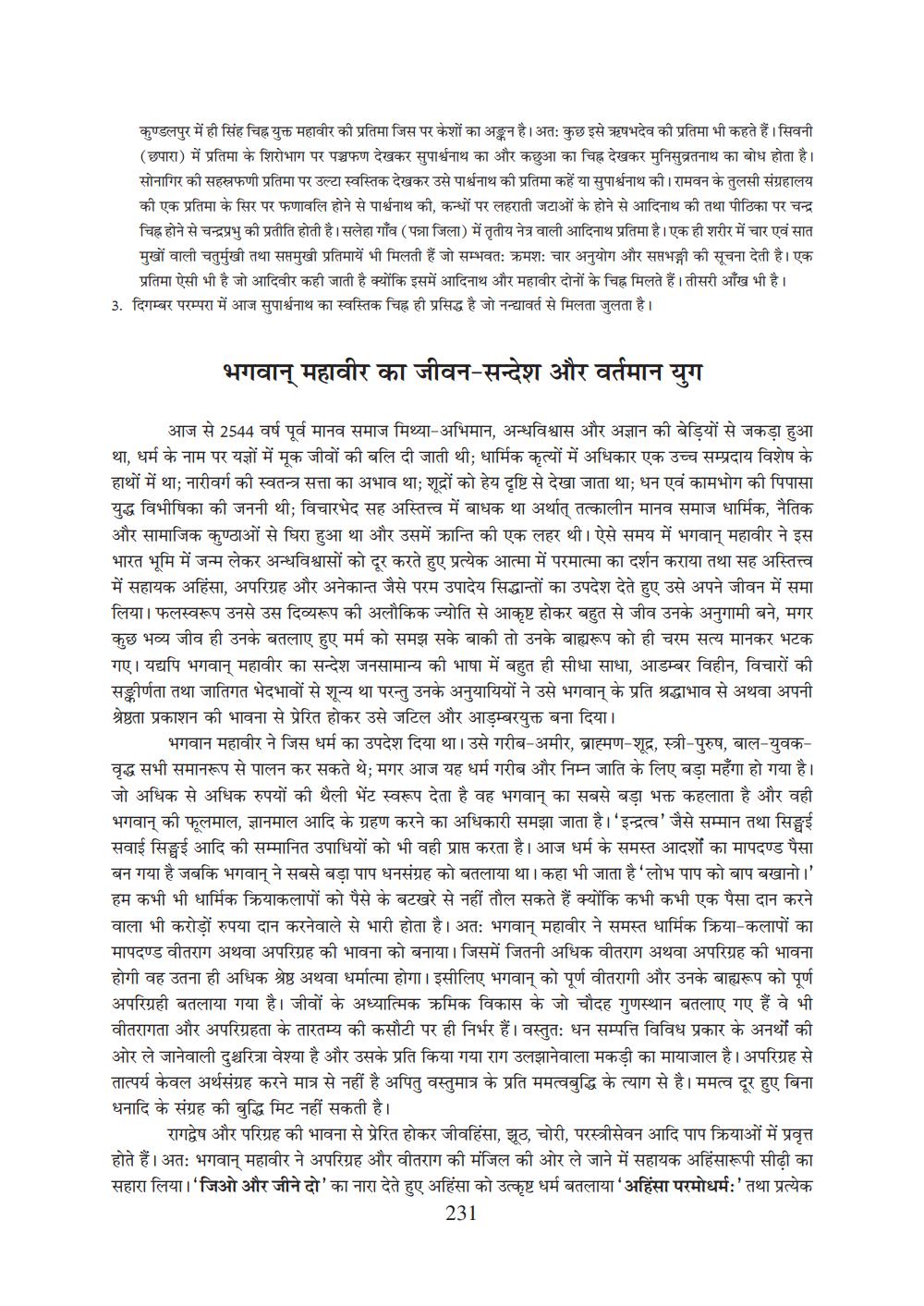________________ कुण्डलपुर में ही सिंह चिह्न युक्त महावीर की प्रतिमा जिस पर केशों का अङ्कन है। अत: कुछ इसे ऋषभदेव की प्रतिमा भी कहते हैं। सिवनी (छपारा) में प्रतिमा के शिरोभाग पर पञ्चफण देखकर सुपार्श्वनाथ का और कछुआ का चिह्न देखकर मुनिसुव्रतनाथ का बोध होता है। सोनागिर की सहस्रफणी प्रतिमा पर उल्टा स्वस्तिक देखकर उसे पार्श्वनाथ की प्रतिमा कहें या सुपार्श्वनाथ की। रामवन के तुलसी संग्रहालय की एक प्रतिमा के सिर पर फणावलि होने से पार्श्वनाथ की, कन्धों पर लहराती जटाओं के होने से आदिनाथ की तथा पीठिका पर चन्द्र चिह्न होने से चन्द्रप्रभु की प्रतीति होती है। सलेहा गाँव (पन्ना जिला) में तृतीय नेत्र वाली आदिनाथ प्रतिमा है। एक ही शरीर में चार एवं सात मुखों वाली चतुर्मुखी तथा सप्तमुखी प्रतिमायें भी मिलती हैं जो सम्भवतः क्रमश: चार अनुयोग और सप्तभङ्गी की सूचना देती है। एक प्रतिमा ऐसी भी है जो आदिवीर कही जाती है क्योंकि इसमें आदिनाथ और महावीर दोनों के चिह्न मिलते हैं। तीसरी आँख भी है। 3. दिगम्बर परम्परा में आज सुपार्श्वनाथ का स्वस्तिक चिह्न ही प्रसिद्ध है जो नन्द्यावर्त से मिलता जुलता है। भगवान् महावीर का जीवन-सन्देश और वर्तमान युग आज से 2544 वर्ष पूर्व मानव समाज मिथ्या-अभिमान, अन्धविश्वास और अज्ञान की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, धर्म के नाम पर यज्ञों में मूक जीवों की बलि दी जाती थी; धार्मिक कृत्यों में अधिकार एक उच्च सम्प्रदाय विशेष के हाथों में था; नारीवर्ग की स्वतन्त्र सत्ता का अभाव था; शूद्रों को हेय दृष्टि से देखा जाता था; धन एवं कामभोग की पिपासा युद्ध विभीषिका की जननी थी; विचारभेद सह अस्तित्त्व में बाधक था अर्थात् तत्कालीन मानव समाज धार्मिक, नैतिक और सामाजिक कुण्ठाओं से घिरा हुआ था और उसमें क्रान्ति की एक लहर थी। ऐसे समय में भगवान् महावीर ने इस भारत भूमि में जन्म लेकर अन्धविश्वासों को दूर करते हुए प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का दर्शन कराया तथा सह अस्तित्त्व में सहायक अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त जैसे परम उपादेय सिद्धान्तों का उपदेश देते हुए उसे अपने जीवन में समा लिया। फलस्वरूप उनसे उस दिव्यरूप की अलौकिक ज्योति से आकृष्ट होकर बहुत से जीव उनके अनुगामी बने, मगर कुछ भव्य जीव ही उनके बतलाए हुए मर्म को समझ सके बाकी तो उनके बाह्यरूप को ही चरम सत्य मानकर भटक गए। यद्यपि भगवान् महावीर का सन्देश जनसामान्य की भाषा में बहुत ही सीधा साधा, आडम्बर विहीन, विचारों की सङ्कीर्णता तथा जातिगत भेदभावों से शून्य था परन्तु उनके अनुयायियों ने उसे भगवान् के प्रति श्रद्धाभाव से अथवा अपनी श्रेष्ठता प्रकाशन की भावना से प्रेरित होकर उसे जटिल और आडम्बरयुक्त बना दिया। भगवान महावीर ने जिस धर्म का उपदेश दिया था। उसे गरीब-अमीर, ब्राह्मण-शूद्र, स्त्री-पुरुष, बाल-युवकवृद्ध सभी समानरूप से पालन कर सकते थे; मगर आज यह धर्म गरीब और निम्न जाति के लिए बड़ा महँगा हो गया है। जो अधिक से अधिक रुपयों की थैली भेंट स्वरूप देता है वह भगवान् का सबसे बड़ा भक्त कहलाता है और वही भगवान् की फूलमाल, ज्ञानमाल आदि के ग्रहण करने का अधिकारी समझा जाता है। 'इन्द्रत्व' जैसे सम्मान तथा सिङ्घई सवाई सिङ्कई आदि की सम्मानित उपाधियों को भी वही प्राप्त करता है। आज धर्म के समस्त आदर्शों का मापदण्ड पैसा बन गया है जबकि भगवान् ने सबसे बड़ा पाप धनसंग्रह को बतलाया था। कहा भी जाता है लोभ पाप को बाप बखानो।' हम कभी भी धार्मिक क्रियाकलापों को पैसे के बटखरे से नहीं तौल सकते हैं क्योंकि कभी कभी एक पैसा दान करने वाला भी करोड़ों रुपया दान करनेवाले से भारी होता है। अत: भगवान् महावीर ने समस्त धार्मिक क्रिया-कलापों का मापदण्ड वीतराग अथवा अपरिग्रह की भावना को बनाया। जिसमें जितनी अधिक वीतराग अथवा अपरिग्रह की भावना होगी वह उतना ही अधिक श्रेष्ठ अथवा धर्मात्मा होगा। इसीलिए भगवान् को पूर्ण वीतरागी और उनके बाह्यरूप को पूर्ण अपरिग्रही बतलाया गया है। जीवों के अध्यात्मिक क्रमिक विकास के जो चौदह गुणस्थान बतलाए गए हैं वे भी वीतरागता और अपरिग्रहता के तारतम्य की कसौटी पर ही निर्भर हैं। वस्तुतः धन सम्पत्ति विविध प्रकार के अनर्थों की ओर ले जानेवाली दुश्चरित्रा वेश्या है और उसके प्रति किया गया राग उलझानेवाला मकड़ी का मायाजाल है। अपरिग्रह से तात्पर्य केवल अर्थसंग्रह करने मात्र से नहीं है अपितु वस्तुमात्र के प्रति ममत्वबुद्धि के त्याग से है। ममत्व दूर हुए बिना धनादि के संग्रह की बुद्धि मिट नहीं सकती है। रागद्वेष और परिग्रह की भावना से प्रेरित होकर जीवहिंसा, झूठ, चोरी, परस्त्रीसेवन आदि पाप क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं। अतः भगवान् महावीर ने अपरिग्रह और वीतराग की मंजिल की ओर ले जाने में सहायक अहिंसारूपी सीढ़ी का सहारा लिया। 'जिओ और जीने दो' का नारा देते हुए अहिंसा को उत्कृष्ट धर्म बतलाया अहिंसा परमोधर्मः' तथा प्रत्येक 231